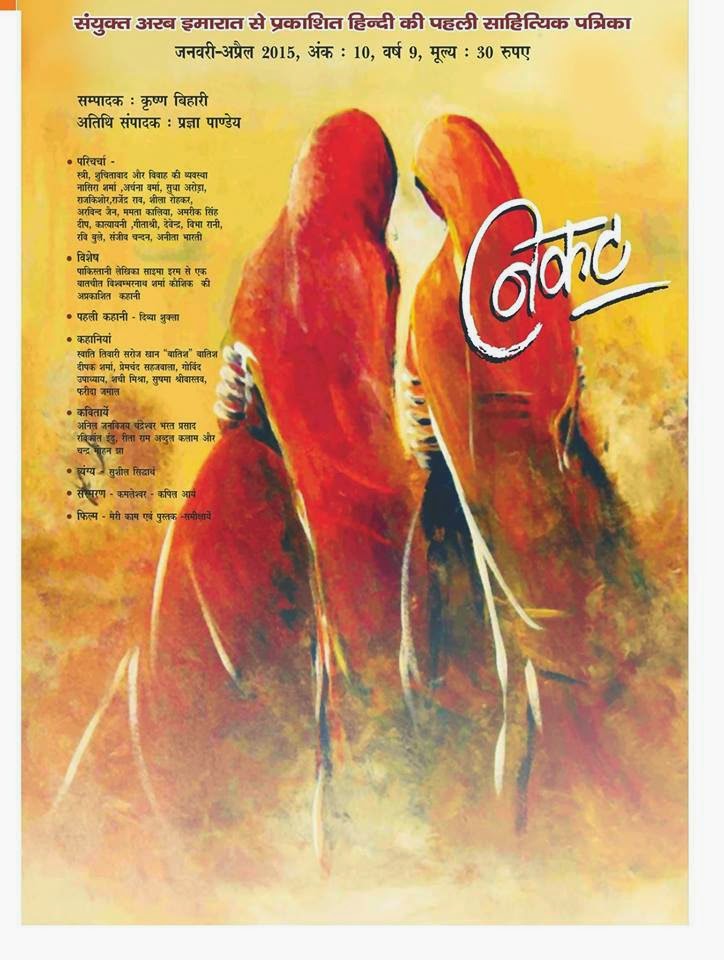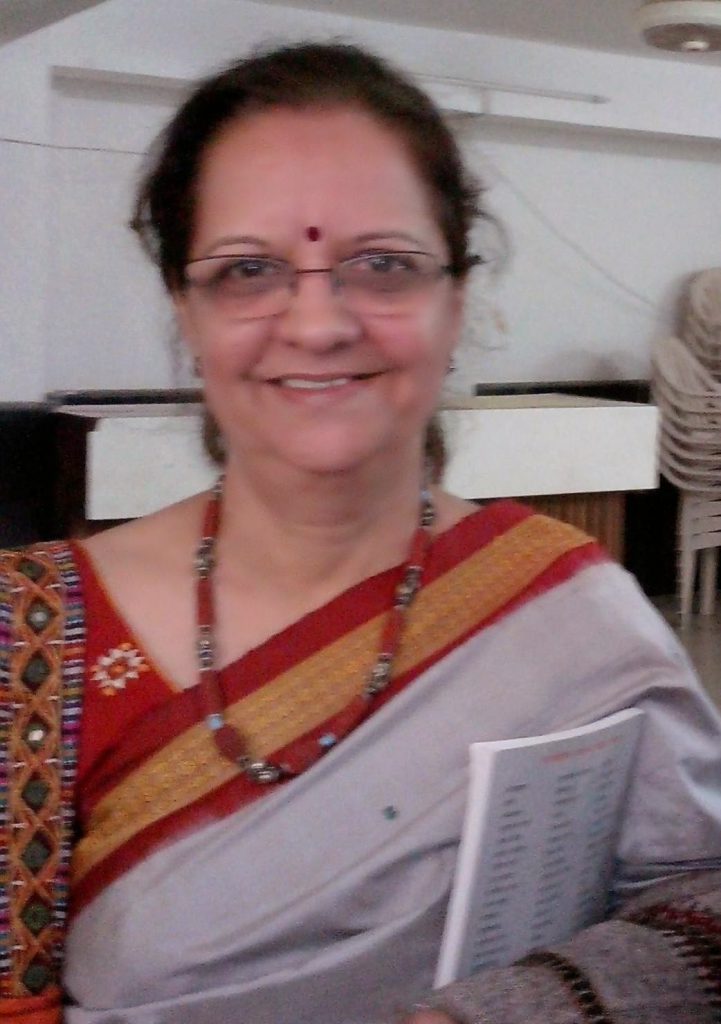 सुधा अरोड़ा सुप्रसिद्ध कथाकार और विचारक हैं. सम्पर्क : 1702 , सॉलिटेअर , डेल्फी के सामने , हीरानंदानी गार्डेन्स , पवई , मुंबई – 400 076
सुधा अरोड़ा सुप्रसिद्ध कथाकार और विचारक हैं. सम्पर्क : 1702 , सॉलिटेअर , डेल्फी के सामने , हीरानंदानी गार्डेन्स , पवई , मुंबई – 400 076
फोन – 022 4005 7872 / 097574 94505 / 090043 87272.
( प्रज्ञा पांडेय के अतिथि सम्पादन में हिन्दी की पत्रिका ‘ निकट ‘ ने स्त्री -शुचितावाद और विवाह की व्यवस्था पर एक परिचर्चा आयोजित की है . निकट से साभार हम उस परिचर्चा को क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं , आज सुधा अरोड़ा के जवाब . अरविंद जैन का जवाब और प्रज्ञा पांडे का सम्पादकीय पढ़ने के लिए क्लिक करें )
जो वैध व कानूनी है वह पुरुष का है : अरविंद जैन
वह हमेशा रहस्यमयी आख्यायित की गयी : प्रज्ञा पांडे
बकौल सिमोन द बोउआर स्त्री पैदा नहीं होती बनायी जाती है – आपकी दृष्टि में स्त्री का आदिम स्वरुप क्या है ?
आदिम स्वरूप हो या आधुनिक – स्त्री का बायोलाॅजिकल पक्ष शुरु से एक जैसा ही रहा है। समाजविज्ञान के अनुरूप लैंगिक स्वरूप और धारणाएं बदली है और लगातार बदल रही है। पुरातन समय में स्त्री को पूरी तरह उसकी प्रजनन क्षमता से जोड़कर देखा जाता था । पुरुष अपने भीतर से एक नये मानव का सृजन कर नहीं सकता था इसलिये पचास के दशक तक स्त्री का सारा महत्व उसकी प्रजनन क्षमता के इर्द – गिर्द समेट दिया गया। सन् 1950 के बाद ही प्रजनन से होने वाले हानिकारक प्रभाव जब स्त्री देह पर देखे गये, तभी प्रजनन को नियंत्रित करने और रोकने के उपाय तलाश जाने लगे और उनका इस्तेमाल स्त्री के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये सफलतापूर्वक किया गया । मसाला कूटने और चक्की पीसने की मशीनों, कोयले और लकड़ी के चूल्हों की जगह गैस के चूल्हे आविष्कृत हुए और स्त्री को घरेलू श्रम से राहत मिली । महिला अधिकारों का फिनाॅमिना भी औद्योगिक विकास, लोकतांत्रिक समाज और विज्ञान और तकनीकी प्रगति से बावस्ता है।
सिमोन द बोउआर का समय वही है जब समाज एक बदलाव की करवट ले रहा था। सिमोन के व्यक्तित्व में एक खास किस्म की सादगी थी जो स्त्रियों के लिये बनाये नियमों और पुरुश वर्चस्व वाले समाज में मानवीय बराबरी के भाव से ही पैदा होती है। सिमोन का पूरा जीवन स्त्री की शारीरिक मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता का पर्याय बन गया। सिमोन जीवन भर स्त्री के दैहिक आकर्षण , चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल से पुरुषों को आकर्षित करने की कोशीशों के बेहद खिलाफ थीं और उन्होंने निजी तौर पर न केवल इसका विरोध किया बल्कि तत्कालीन फ्रांस में विवाह और परिवार की अवधारणा से बहुत आगे बढ़कर सहजीवन का चुनाव किया। सात्र्र के साथ उनके संबंधों का एक आयाम यह भी है कि दोनों ने अपने जीवन, अपने संबंधों और अपनी भावनाओं को कभी छिपाया नहीं। सिमोन ने सार्त्र से अलग प्रेम संबंध को भी स्वीकृति दी। ऐसी सिमोन जब ‘ स्त्री बनाई जाती है’ , जैसा वक्तव्य देती है ,तो इसके पीछे उसकी जैविकी के आधार पर तय किये जाने वाला दर्जा, शारीरिक बदलावों और जरूरतों के हिसाब से स्थापित मूल्यों और पुरुष वर्चस्व के अनुरूप गढ़े गये स्त्री विरोधी मिथकों का खंडन एक आधारभूत कारण रहता है।
मेरी अपनी दृष्टि – पीढि़यों से चली आ रही परंपरा, उनमें आये बदलाव और उसके बाद अपनाए गए आधुनिकता के विचारों से बनती है । मैंने अपनी मां दादी नानी सास ननदों के रिश्ते में आने वाली स्त्रियों को हमेशा पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में जकड़े पाया। वस्तुतः यह मूल्य उनकी बेडि़यां ही थीं जैसे सामाजिक सम्मान और सुरक्षा, पिता और पति की आर्थिक हैसियत के अनुरूप संपन्नता जिसका सीधा अर्थ था – खाने पहनने और रहने के लिये मूलभूत सुविधाएं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें उतना ही आगे बढ़ने की छूट थी, जिससे हम पारिवारिक दायरे और मूल्यों के लिये चुनौती न बन सकें। आत्माभिव्यक्ति के स्तर पर एक संकट यह आया कि स्त्री और पुरुष के बीच सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से एक गहरी फांक थी। निर्णय पुरुषों के और मानना स्त्रियों को पड़ता था। यह प्रक्रिया एक अन्तरपीढ़ी- स्त्रीजगत की ओर जब ले जाती है, तो यह सवाल बार बार उठता है कि केवल भारत ही नहीं, दुनिया की सारी सभ्यताओं में स्त्री को जैविक कारणों से ही क्यों गुलाम बनाने की शुरुआत की गई होगी और उसके लिये नियमों और मिथकों का इतना भयानक जेलखाना बनाया गया होगा ।
 |
| सिमोन |
मुझे लगता है कि प्राचीन काल से जब स्त्री पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी होगी और दो कदम और आगे बढ़कर तत्कालीन जरूरतों के हिसाब से बच्चे पैदा करने में लगी होगी तब उसे जबरन जंगलों की खोज, युद्धों और विजयों से काटकर कबीले, तंबू और बस्तियों के जीवन में समेटा गया होगा और वह इससे कभी आजाद न हो सके इसके लिये उसके आसपास नियम और मिथक गढ़े गये होंगे। आदिम समाज की यह परिपाटी सभ्यताओं के विकास के साथ साथ विकसित होती रही और आज हम उसको एक पतनशील व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं इसका एक उदाहरण महानगरों में कामकाजी औरतों का ट्रेन और बसों में ठुंसकर कार्यस्थल पर जाना, घर और बाहर खटना लेकिन दाम्पत्य की सुरक्षा के लिये करवाचैथ या ऐसे अनेक व्रत उपवास रखना आदि में देखा जा सकता है।
क्या दैहिक शुचिता की अवधारणा स्त्री के खिलाफ कोई साजिश है ?
पहली बात तो यह कि अपनी शुरुआत में दैहिक पवित्रता न तो अवधारणा जैसी कोई चीज़ थी और न ही इसे साजिश के रूप में देखा जाना चाहिये। यह एक तरह से प्रजनन की आधारभूत प्रक्रिया को न समझकर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी । एक बच्चे की मां को पहचान पाना जितना आसान था, पिता या पुरुष की शिनाख़्त उतनी ही मुश्किल थी । इसलिये स्त्री पर अपना अंकुश और नियंत्रण बनाने के लिये दैहिक शुचिता को एक मूल्य के रूप में धीरे धीरे स्थापित कर दिया गया और बाद में यह पितृसत्ता की मशीनरी के तहत स्त्री को अनुशासित करने का एक ठोस औजार बन गया ।
आखिर किसे दैहिक शुचिता की ज़रूरत है और क्यों ? यह अवधारणा स्त्री के मनोबल को तोड़ने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां पहले ही वार में उसकी स्वतंत्रता का सवाल स्वाहा हो जाता है और वह पुरुष की ऐसी कृपा पर या हिकारत पर आजीवन जीने के लिये अभिशप्त हो जाती है, जिसका पुरुष को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी सत्ता बनाये रखने और मनमानेपन और अत्याचार को जायज ठहराने के लिये वह अलिखित रूप से इसका इस्तेमाल आजीवन करता रहता है ।
शुचिता का विचार इतना घातक होता है कि न सिर्फ स्त्री के हंसने बोलने और चहकने को कठघरे में खड़ा कर देता है बल्कि उसकी बौद्धिकता, संवेदनशीलता और समूचे विवेक को भी कुंद कर देता है और वह सिर्फ हां में हां मिलाने के लायक रह जाती है। उसके युवा होते ही उसपर प्रेम न करने की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। प्रेम करने पर उस पर पूरा हक और दखल परिवारवालों का होता है। वह किसके साथ जीवन बिताने का निर्णय ले, यह अधिकार उसे नहीं दिया जाता – यह कहकर कि वह नासमझ है, उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं ।
इन स्थितियों के खिलाफ़ बहुत कम लड़कियां सिर उठा पाती हैं, बल्कि ज्यादातर लड़कियां जीवन भर इस अनकिये अपराध की सजा भुगतती रहती हैं। सामान्य रूप से यदि एक मोटा आंकड़ा भी लिया जाए तो लाखों रचनात्मक प्रतिभाएं इस प्रक्रिया में मिट्टी में मिल जाती हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिये । दैहिक शुचिता का सवाल पुरुषों के लिये उठाया जाना चाहिये, क्योंकि उन्हें आज़ादी मिली हुई है और सब जानते हैं कि उसने इस आज़ादी का दुरुपयोग स्त्री के खिलाफ़ ही किया है।
भारत की खाप पंचायत इसका एक ठोस उदाहरण है । इसके अलावा मिडल ईस्ट, अफ्रीका , लैटिन अमरीकी देश और पूर्वी एशिया के कुछ देषों में स्त्रियों को तथाकथित रूप से शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिये सुन्नत, लोहे के जांघिये जैसी अमानवीय और क्रूर प्रथाओं का शिकार बनाया जाता रहा है। चीन में लड़कियों के पैर बांधने की क्रूर प्रथा उन्हें खूबसूरत और कमसिन बनाने के बजाय अशक्त और गुलाम बनाने की ही कवायद थी ।
समाज के सन्दर्भ में शुचितावाद और वर्जनाओं को किस तरह परिभाषित किया जाए ?
हम शुचितावाद की प्रक्रिया को देखें तो यह समझ पायेंगे कि अब शुचिता के निर्वाह की अपेक्षा रखना स्त्री की वैयक्तिक आज़ादी से उसे बेदखल करना है । सारी हिदायतें, वर्जनाएं और प्रतिबंध एकबारगी अतार्किक होकर खारिज हो जाते हैं , अगर हम किसी भी मनुष्य की वैयक्तिक आज़ादी को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं ।
आज के दौर में शुचितावाद और यौन वर्जनाएं मूलतः स्त्री यौनिकता और भावना पर सीधा हमला है। पुरुष के मुकाबले स्त्री की यौनेच्छा और कामभावना को हमेशा दोयम दर्जे पर डाल दिया जाता रहा है, इसलिये उसकी संतुष्टि – असंतुष्टि का तो सवाल ही बेमानी हो जाता है। शास्त्रों में जिस भारतीय नारी की कल्पना की गई है, और आज भी जिसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है वह वस्तुतः एक दमित स्त्री है, जो अपनी इच्छाओं के मुकाबले पति और परिवार की कल्याण भावना से ही संचालित होती है। स्त्रियों की सारी भावनाओं का दायरा उनके पति की इच्छा -अनिच्छा तक सीमित कर दिया जाता है। इस तरह व्यभिचारियों और नपुंसकों की बहुत बड़ी फ़ौज समाज में नाक ऊपर उठाये हुंकार भरती हुई मिल जायेगी और दुर्भाग्य से ऐसे ही लोग स्त्रियों के नियंता बन जाते हैं।
इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है – स्त्री का सामान्य जीवन से उदासीन होते हुए संपत्ति का केअरटेकर भर रह जाना और अपने आनंद और सुख को हर तरह भूल जाना। कभी -कभी स्त्रियां इन सब के खिलाफ़ एक विद्रोही तेवर लेकर शब्दों में उतर जाती हैं और मूल्यवान रचनाएं हमारे बीच आती हैं। लेकिन आज का अधिकांश स्त्री लेखन देह की आज़ादी से प्रेरित फूहड़ लेखन है, जो वस्तुतः स्त्री की आज़ादी और गुलामी के असली निकष पहचान ही नहीं पाता और पुरुष सत्ता में शामिल होने के लिये उसका मोहरा बनकर रह जाता है। यौन केंद्रित दृष्यों की बहुलता और संबंधों के द्वंद्वविहीन विन्यास असल में इसका बहुत बड़ा रूपक है कि स्त्री अपनी बेडि़यों को पहचान ही नहीं पा रही है और न ही उससे पैदा हुई तकलीफों का उसे कोई आभास है और इसीलिये वह पुरुषों की आज़ादी के अनुकूल एक और बेड़ी अपने ऊपर स्वेच्छा से डाल लेती है, जिसकी उसे पहचान तक नहीं होती जबकि उसके भीतर अतीत से गहरा संघर्ष और भविष्य की चुनौतियां स्वीकारने का माद्दा होना अधिक जरूरी है।
 |
| स्त्रियाँ, जिनका हस्तक्षेप है |
यदि स्वयं के लिए वर्जनाओं का निर्धारण स्वयं स्त्री करे तो क्या हो ?
वैयक्तिक स्तर पर स्त्रियों को संबंधों का चुनाव करते समय अपनी भीतरी खुशी और तनावमुक्त स्थिति पर अपने को फोकस करना चाहिये । साथ ही साथ वह इस बात का भी ख्याल रखे कि उसके निजी चुनाव किसी दूसरे की आज़ादी और सुरक्षा में खलल तो नहीं डाल रहे। अपनी आज़ादी को बचाये रखने के साथ उसे दूसरे की आज़ादी पर हमला करने का भी कोई हक नहीं है। यह स्त्री पुरुष का नहीं, मानवीयता का तकाज़ा है। उसे लिंग विभाजन और लिंग प्राथमिकता के तहत अपनी दिशा तय नहीं करनी है। सामाजिक स्तर पर भी यही रवैया कारगर होगा। वर्ग, वर्ण और जाति के तहत उसे विभेद रेखायें नहीं खींचनी हैं। हमेशा यह संभव नहीं होता पर अपनी सीमाओं और मानवीयता की पहचान एक ज़रूरी धरातल है।
आज़ादी को लड़की के लिए कुफ्र माना जाता है। बहुत सी बातें उनके ऊपर थोप दी जाती हैं। इसके बरक्स समाजों और राष्ट्रों को सभ्य बनाने की अधिक जरूरत है। जब स्त्री अपने लिए वर्जनाएं तय करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वह बराबरी और मनुष्यता से बाहर कोई मांग करेगी। उसका तो मूलभूत हक भी अब तक उसे मिला नहीं है। अगर वह अपने हकों के लिए संघर्ष कर रही है और आप उसे अराजक और आवारा समझ रहे हैं तो ठीक वही अपराध कर रहे हैं जो पीढि़यों से लोग करते आ रहे हैं। आजादी और अपराध की सीमारेखा को एक में नहीं मिलाया जा सकता।
विवाह की व्यवस्था में स्त्री की मनोवैज्ञानिक ,सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां कितनी स्त्री के पक्ष में हैं ?
विवाह की शुरूआती अवधारणा ही पूरी तरह से ग़ैरबराबरी पर टिकी है। स्त्री और पुरुष मिलकर एक पारिवारिक इकाई का निर्माण करते हैं लेकिन इस इकाई में कार्यविभाजन, भूमिकाओं के निर्धारण और निर्णय के अधिकार में दोनों को समान नहीं रहने दिया जाता और इसका बुनियादी कारण संपत्ति और अर्थोपार्जन है। एक समय तो रनिवासों और हरमों में स्त्री की हैसियत एक गुलाम से भी बदतर हो गई। गौरतलब है कि इनमें बंदियों की ही संख्या नहीं थी बल्कि ब्याहताओं की भी संख्या थी। चूँकि यह परिदृश्य शासक वर्ग के भीतर था इसलिए सामान्य जीवन भी इस असर से अछूता न रहा और इसका सबसे बड़ा असर स्त्री की अस्मिता पर पड़ा और वह सामाजिक जीवन की सबसे उपेक्षित स्थिति तक जा पहुंची।
विवाह का निर्धारण पुरुष के अनुकूल होता रहा है और स्त्री की सहमति-असहमति का उसमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। अक्सर देखा गया है कि बीमार और फटेहाल पति भी अपनी कामकाजी पत्नी को केवल इसलिए दबाता रहा है कि वह पुरुष है। आर्थिक स्थिति में स्त्री के प्राधिकार का अभाव इसका मुख्य कारण था। पारम्परिक विवाह की व्यवस्था में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां स्त्री के पक्ष में अमूमन कम ही रही हैं। हाँ, प्रेम विवाहों और नई अर्थव्यवस्था में चीजें तेजी से बदलने का आभास ज़रूर हुआ पर दोनों पक्षों में गहरे तक परंपरागत संस्कार धंस चुके थे इसलिये मानसिकता को बदल पाना बहुत मुश्किल हो गया।
समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन हुए। आज विवाह में इस गैरबराबरी की प्रचलित अवधारणा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लड़कियों को पहले की तरह इसे भाग्य और नियति मानकर एक गलत संबंध में आजीवन टिके रहकर अपने को होम करने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक सुरक्षा और सुविधा के संबंध को विस्तार देते हुए प्रेम के संबंध में बदलने की भरपूर कोषिष की जानी चाहिये । यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक स्त्री अपनी अस्मिता को बरकरार रखते हुए एक कोमल रिश्ता बनाये रखने में कितनी आश्वस्त और सर्जनात्मक है। स्त्रियों में प्रेम देने की अंतहीन संभावनाएं हैं। पुरुषों में भी हैं पर उनका अहं भरपूर आड़े आता रहता है। दो साथियों के बीच अगर मूल्यों , आस्थाओं और अस्तित्व का भीषण टकराव है , तो उसी स्थिति में विवाह से बाहर निकलकर दोनों का अपने को सम्मान के साथ बचाये रखना निहायत ज़रूरी है ।
मातृसत्तात्मक व्यवस्था में विवाह-संस्था क्या अधिक सुदृढ़ और समर्थ होती ? तब समाज भ्रूण हत्या दहेज हत्या एवं बलात्कार जैसे अपराधों से कितना मुक्त होता ?
मातृसत्तात्मक व्यवस्था की अवधारणा एक यूटोपिया से ज्यादा कुछ नहीं। सत्ता – वह किसी भी तरह की हो – पितृसत्ता या मातृसत्ता – हमेशा से ही त्याज्य है। उसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती। नारीवाद लोकतंत्र और उदारवाद का इच्छुक है। समानता और बराबरी इसका मूलमंत्र है और इसी के तहत हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान दिलाया जा सकता है । फेमिनिज़्म में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितृसत्ता की आलोचना या भर्त्सना करते हुए वह मातृसत्ता की स्थापना का हिमायती नहीं है।
यह निहायत गलत अवधारणा है कि भ्रूण हत्या, दहेज हत्या और बलात्कार जैसे अपराध पुरुषसत्तात्मक समाज की विशेषतायें हैं और ज्यादातर मातृसत्तात्मक व्यवस्थाओं में ये कुरीतियां नहीं होतीं। नारीवादी महिलाएं अगर समाज में बदलाव चाहती हैं तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिये कि वे पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जगह एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था चाहती हैं। नारीवादी अवधारणा बराबरी का हक, निर्णय लेने की आज़ादी और मानसिक गुलामी से मुक्ति की अवधारणा है, जिसमें पुरुष को साथ लेकर ही समाज को बदला जा सकता है, अलग से एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था कायम करके नहीं। यह एक शोषक व्यवस्था से निदान नहीं, सिर्फ़ खुद दूसरी भूमिका में उतर आना है।
सह जीवन की अवधारणा क्या स्त्री के पक्ष में दिखाई देती है ?
सहजीवन की अवधारणा विवाह संस्था की हिलती हुई नींव का ही नतीजा है। ज़ाहिर है इसमें स्त्री और पुरुष (या समान लिंग के दो साथी भी) दोनों के लिये अपेक्षाकृत ज्यादा आज़ादी है। सहजीवन सबसे पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा और बंधन से मुक्ति का रास्ता दिखा देता है, जिसमें हमेशा परंपरागत विवाह के छत्र तले आमतौर पर स्त्रियों को ही समझौते करने पड़ते थे। विवाह दो व्यक्तियों के बीच होता है पर एक लड़की को सिर्फ़ अपने पति से नहीं, उसके पूरे परिवार से समझौता करते हुए, तालमेल बिठाते हुए और आखिरकार इस प्रक्रिया में अपने को होम करते हुए इस संबंध को निभाना पड़ता है। अच्छे और सकारात्मक अर्थों में जिसे गठबंधन कहा गया वह अंततः पूरी तरह गर्दन पर जकड़ा हुआ बंधन साबित हुआ । दो वयस्क एक दूसरे के लिये जि़म्मेदार होते हैं और उन्हें इस जि़म्मेदारी को एक खुले मन और दिमाग़ से निभाना चाहिये।
सहजीवन खासतौर पर स्त्रियों के लिये आज़ादी की ओर बढ़ता अगला कदम है पर परिवार और विवाह की पारंपरिक अवधारणा ऐसे सहजीवन को स्वीकृति न देकर इन आज़ाद ख्याल व्यक्तियों को समाज से अलग-थलग रखने का उपक्रम रचती है। अगर कोई औरत ऐसे सहजीवन में रहते हुए मां बनना चाहती है, तो उसे एक लंबे अनुबंध की राह तकनी होती है। मध्यवर्ग की लड़की को सामाजिक रूप से अकेले पड़ जाना प्रभावित करता है। इसलिये सहजीवन का निर्णय एक मध्यवर्ग की लड़की ( और लड़के के लिये भी – क्योंकि परिवार उसे भी छोड़ देता है ) के लिये संकरी रस्सी पर चलने जैसा है। मध्यवर्ग से आये संस्कारी युवाओं के लिये यह एक कठिन निर्णय है। पर आज का युवा वर्ग, विवाह के साइड अफेक्ट्स देखते हुए इस प्रयोग को अंजाम देने से नहीं हिचकता और अक्सर उसे इसका लाभ भी मिलता है।
साथ होकर भी पुरुष एवं स्त्री की स्वतंत्र परिधि क्या है ?
किसी भी संबंध में – चाहे वह शादी हो या सहजीवन – अपनी निजी स्पेस को बनाये रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों साथी एक दूसरे की स्वायत्तता बनाये रखने में मददगार हों तो वे एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने को समृद्ध करेंगे और अपना विकास एक स्वस्थ तरीके से कर पायेंगे। इससे सहजीवन का भी स्वस्थ विकास होगा। यह पारस्परिक समृद्धि योजना है । स्वायत्तता को बरकरार रखना इसमें हमेशा इजाफ़ा करता है ।
एक दूसरे का ख्याल रखना और सम्मान करना तो पुरुष और स्त्री की स्वतंत्र परिधि का एक आधार होता ही है लेकिन इसके पीछे काम करनेवाले बुनियादी घटकों को और अधिक ध्यान से समझने की जरूरत है। जब तक स्त्री के श्रम , उसकी बौद्धिकता और क्षमता को पूरा महत्व नहीं मिलेगा, तब तक स्त्री स्वतंत्रता पुरुष की दयानतदारी पर निर्भर रहेगी। इसके साथ ही जबतक स्त्री का अपना घर, संपत्ति पर अपना हक, अपना खाता और नियमित आय नहीं होगी और उसको खर्च करने का निर्णय उसका अपना नहीं होगा तब तक यह परिधि कमजोर होगी और स्त्री सुरक्षा के लिए हमेशा पुरुष की चहारदीवारी में जाती रहेगी !