 चर्चित कहानीकार ,
चर्चित कहानीकार ,
‘ मेरी नाप के कपड़े,’ ‘उलटबांसी’, ‘नदी जो अब भी बहती है ‘ (कहानी संग्रह)
‘मेरा पता कोई और है’, ‘ये दिये रात की जरूरत थे ‘ (उपन्यास)
सम्पर्क: kavitasonsi@gmail.com
सीढी-दर-सीढी उतरती मैं हांफती हूं. दिन में भी ऐसा घुप्प अन्धेरा कि उंगलियों को उंगलियां न दिखाई दे…कबतक, आखिर कबतक चलती रहूंगी इस तरह… किस सफर में हूं मैं कि दहशत है – रगो रेशे में. अब आखिर कहां जाना है… कितना भीतर… कि अन्त क्यों नहीं आता आखिर. कैसी तलाश है यह.. किसकी तलाश है आखिर…?
कौन सा सपना है यह जो हर रात मेरी नींद में बदस्तूर जागता है, खंगाल कर ले आता है मेरे भीतर का वह कुछ जो कि मुझे पता ही नहीं, कि है भी मेरे भीतर. पानी… पानी चाहिये मुझे. पर पानी न जाने कहां विलुप्त… कई दृश्य भय बन कर कांप उठते हैं.. मेरे रोम-रोम से जैसे मेरा भय बह निकला हो. आत्मा सूखी.. डिहाईड्रेटेड… मैं खुद जैसे निचुड़ी जा रही हूं.
अनी.. अन्वी.. मेरी आवाज़ किसी भूत बंगले की तरह गूंजती है उस सन्नाटे में… लौट आती है फिर मेरे ही पास. मैं दौड़ रही हूं. हलक सूख रही है.. जीभ लटपटाई हुई, कि तभी अनी कहती है मुझे झकझोर कर – मम्मा पानी चाहिये..? इसी टेबल पर तो है पानी. आप ही ने तो सोते वक्त रखा था. मैं उसे गले से लगा लेती हूं. मेरी प्यास बुझ गई हो जैसे.
अनी की आंखें भी ठीक उसी की तरह है.. वाचाल, बातूनी. उसकी एक-एक चमक में हजारों किस्से.. किस्सों में भी कितने किस्सेतर अफसाने… वह ठीक मेरे उलट है, यह अम्मा कहती है… यह सब कहते हैं. अन्वी कहीं ठहरती नहीं, टिकती नहीं… कभी भी, किसी हाल में, किसी के भी कहने से.. मुझे भी पसन्द है यह. मैं उसको इसी तरह निडर बनाये रखना चाहती हूं और उसे इसी तरह बनाये रखने के इसी उपक्रम में न जाने कितने डर, कितना संशय, कितनी अनाम पीड़ायें… यह शायद मां हो कर ही समझा जा सकता है.
वे कहते हैं अक्सर, हद करती हो तुम भी. .. बेटी आंखों से ओझल नहीं हुई कि… उसे जीने दो उसका बचपन. इस तरह तो… सोचती हूं मैं भी, इस तरह तो… जानती हूं मैं भी इस तरह तो…
पर चारा कोई और नहीं हैं मेरे पास. मेरा भय दु:स्वप्न बनकर पीछा करता रहता है हमेशा. धुर जाड़े की रातों में पसीने से नहाई हुई उठती हूं मैं और जानलेवा गर्मी में भी भय से थरथराती हुई. सांसे धीरे-धीरे थिर होती हैं. बगल में सोई अनी को नींद में मुस्कुराते देखकर, कभी अपने गले में उसे गलबहियां डाले सोई जान कर, मैं अपनी बांहे उसके इर्द-गिर्द कसकर लपेट लेती हूं, इतना कसकर कि नींद में भी कई बार कसमसा उठती है वह. … मुझे लगता है कि अब सुरक्षित है वह… कि अब कोई डर नहीं. फिर भी नींद है कि आते-आते आती है और स्वप्न है कि जाते-जाते भी नहीं जाता.
 |
| साभार गूगल |
मेरा पांव अन्धेरे में किसी ठोस चीज़ से टकराया है. चीख निकलती है बहुत तेज, पर जैसे गले में ही रूंध जाती है. सबकुछ बिल्कुल उसी सपने जैसा. मेरी सांस-सांस रो रही है. मेरा रोम-रोम जैसे किसी अज्ञात पीड़ा से लिथड़ा हुआ. तलगृह में जैसे और अंधेरा हो आया हो, घना घनघोर, घुप्प अंधेरा. अब अपना ही भान कहां रह गया है. अन्वी, अनी, मेरी प्यारी अनी… मैं अंधेरे में टटोलती- टोहती जब किसी भी ज्ञात-अज्ञात वस्तु से टकराती हूं भीतर तक सिहर उठती हूं. सिहरना सुकून बनता है पर थोड़ा ठहरकर. कुछ नहीं, कुछ भी नही, कुछ भी तो नहीं. सुकून आता है और फिर बिला जाता है. कहां हैं.. कहां है मेरी बिटिया अनी…मैं हमेशा की तरह उस सपने के गिरफ्त में हूं. और हमेशा की तरह ही सोचना चाहती हूं, समझाना चाहती हूं खुद को, बेकार ही डरती हूं मैं. ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता उसके साथ…
…बच्ची जरूर है अनी पर समझदार भी है. उसे बनाया है मैंने समझदार. मैं कहती रहती हूं उससे, बेटा कोई भी अगर प्यार करते-करते टच करना चाहे तो मत करने देना. किसी को किस्सू भी मत करने देना चेहरे पर, लिप्स पर तो कभी नहीं… डांट देना उसे… समझीं आप? मैं जोड़ती हूं.. मम्मा, पापा और अपने परिवार के लोगों को छोड़कर. फिर कहते-कहते ठिठकती हूं इस ‘परिवार’ शब्द पर. नहीं, सिर्फ मम्मा-पापा. वह चुप सुनती रहती है सब हमेशा के बिल्कुल विपरीत… बेटा, मैं आपको कुछ बता रही हूं न.. सुन रही हैं न आप?.. हां, मां… वह अपनी चंचल नजरों से थाहती रहती है आस पास… कुछ अनोखा, कुछ अलग-सा, नटखट-सा करने, हो सकने की संभावना की तलाश में… मुझे लगता है मेरी बातें तो बस यूं हीं… बेटा पहले मेरी बात पर ध्यान दीजिये. सुनिये प्लीज… सुन तो रही हूं मम्मा … वह खीज भरे स्वरों में कहती है… इतने-इतने खिलौनों के बीच मां की ये बेकार की बातें, नसीहतें.
पहली बार मन तभी हिला था क्षण भर को, जब तीन-साढ़े तीन की ही थी वह.. टाऊनशिप की अपनी सुविधायें… क्लब, जिम, किड्स रूम, लायब्रेरी… मैं शाम को थोड़ा वक्त निकाल लेती हूं… अन्वी खेलती रहती है किड्स रूम में. मैं थोड़ा पढ़ लेती हूं… पर पढ़ते-पढ़ते सांस अंटकी होती है, बस अनी में. उठ-उठ कर झांक आती हूं. वह खेलने में मग्न होती है, दूसरे बच्चों के साथ. अन्वी को किड्स रूम का आकर्षण खींचता है. उसकी आंखों की चमक में दिखलाई देते हैं मुझे – ‘सी-सॉ’, ‘स्लाइड्स’, ‘रोप्स’ और झूले. उसके हाथों की लहक में होती है नन्हें चेस, टेबल टेनिस, कैरम, पज़ल्स और लूडो से खेलने की ललक. चीज़ों को हासिल करने की नन्हीं कोशिशें भी. वह दूसरे बच्चों से कभी-कभी लड़ती भी है. कभी-कभी रोती-रोती आती है मेरे पास… मां गुल्लू ने मुझ से पिंग-पॉंग छीन लिया… एंजल मुझे स्लाइड्स पर फिसलने नहीं देती. मैं झगड़े को सुलझाने की कोशिश में कभी कामयाब होती हूं, कभी नाकामयाब. मैंने एक तरकीब निकाली है. किड्स रूम खुलते-खुलते ही मैं अनी को लेकर पहुंच जाती हूं कि दूसरा कोई इतनी जल्दी कहां आ पायेगा. अनी खुश रहे, इन्ज्वाय करे, बस. और अनी भी शाम होते ही पूछती है, मम्मा लायब्रेरी नहीं जाना..? मैं मुस्कुरा कर कहती हूं, जाना है मेरी बच्ची.
…जल्दी-जल्दी पहुंचने की यही ललक उस दिन थिराती है, डर बन कर बैठ जाती है मेरे भीतर और तभी शुरु होती है अन्तहीन दु:स्वप्नों की यह श्रृंखला. मैं पढ़ रही हूं आदतन, डूब कर, भूल कर सबकुछ… अन्वी नहीं आती देर तक. मैं सोचती हूं खेल रही होगी वह. इस बियाबान में यही तो एक जगह है जहां कुछ ताजी पत्रिकाओं का चेहरा देख पाती हूं. फिर थोड़ी देर को ही सही, अन्वी से अलग होकर अपना कुछ लिख-पढ़ पाना. अन्वी नहीं आई है मेरे पास देर से, पर मुझे सुकून ही है. तभी, लिखते-लिखते थमती हूं मैं. मेरे भीतर जैसे कुछ कौंधा हो. चौंकती हूं मैं, मैं तेज कदमों से निकलती हूं. बस चार कदमों की दूरी पर है किड्स रूम. पर मुझे लगता है न जाने कितनी दूर है वह… यह दरवाज़ा क्यों भिड़ा रखा है अनी ने… अनी बेटा, दरवाज़ा क्यो बंद किया, खोलो… अनी कुछ बोलती नहीं. मैं सहमी सी अनी को जल्दी से अपनी गोद में समेट लेती हूं… “संजय तुम? तुम यहां क्या कर रहे थे.. दरवाज़ा क्यों बंद था…”
“अंदर ठंडी हवा आ रही थी…”
“तो…?” मेरी आवाज़ तल्ख है.
“और बगल के कमरे में पार्टी चल रही है. बच्चे आकर सारा सामान तितर-बितर कर देते हैं…” मेरी आवाज़ अब भी सम पर नहीं है… “तो..? ठीक करो. बच्चे तो खेलेंगे ही न.. तुम्हारा काम है ठीक करना.”
उसका सहमापन मेरी आवाज़ के तीखेपन को कुछ और कड़वाता है. क्षण भर को सोचती हूं मैं, शायद ठीक कह रहा है यह.. तभी तो इतना… पर भीतर से आती दूसरी आवाज़ जैसे मेरे भय में और पलीता लगा देती है. सहमता वह है जिसके भीतर कुछ गलत हो. वह पीठ फेर लेता है.. सामान ठीक करने के उपक्रम में लग जाता है. मैं निकलते-निकलते भी कहती हूं… “देखो आगे से कभी कोई बच्चा खेलता हो तो दरवाज़ा बन्द नहीं होना चाहिये…” मैं अनी को लिये-लिये लायब्रेरी से अपना बैग उठाती हूं और… मैं घर नहीं जाती, नीचे लॉन में लगे झूले पर आ बैठती हूं. अन्वी बहुत सहमी सी है. क्यों… मेरा भय या कि मां का यह रौद्र रूप देखकर… मै टटोलना चाहती हूं उसे… पर कैसे? मै ंपूछती हूं – “बेटा वो अंकल वहां क्या कर रहे थ्रे..?” अनि कुछ भी नहीं कहती…
मैं फिर उससे पूछती हूं… “बैठे हुये थे..? खेल रहे थे आपके साथ…? ट्वायज से या फिर…”
अनि छोटा सा उत्तर देती है – ” नहीं.”
“फिर…?” वह चुप है…
“बोलिये बेटा मम्मा तो आपकी फ्रेंड है न… मम्मा से तो आप सबकुछ बताते हैं…”
“वो…” अनी कह कर रुकती है थोड़ी देर को….
“वो क्या बेटा…? बोलिये…”
“अंकल मुझे प्यार कर रहे थे…” ‘प्यार’ शब्द मेरे भीतर गर्म लावे की तरह बहता है… यह ताप जैसे सहने लायक ही न हो…
“प्यार, कैसा प्यार…?” शायद मैं बच्ची पर चीखी हूं… “बोलिये बेटा, बोलिये कुछ… मम्मा से नहीं बतायेंगी? आप उनके इतने पास क्यों बैठी हुई थी..?”
“वो बातें कर रहे थे मुझसे…
“कौन सी बातें…?”
” कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही…”
मैं फिर नहीं कहती उससे कुछ. एक चॉकलेट ले कर आती हूं उसके लिये. सोचती हूं शायद वह अपने आप ही बताये कुछ.
… मैं सोचती हूं, शायद अन्वी ठीक कह रही हो… शायद वह बस बातें कर रहा हो उससे… शायद मैं बेबात डर रही हूं. कुछ होता तो अन्वी कहती नही..?
शेखर को मैं फोन करती हूं – ” जल्दी आओ…”
“कोई खास बात…? मैं साढ़े आठ तक घर आ जाउंगा…”
“नहीं, अभी आओ. और घर नहीं, क्लब. मैं यहीं हूं.”
शेखर का इंतजार करती मैं अन्वी को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिये भेजती हूं. शेखर आते हैं. मेरी बातें सुनते हैं ध्यान से. चुपचाप सुनते रहते हैं, कहते कुछ भी नहीं. मैं फिर चिढ़ उठती हूं – ” बोल क्यों नहीं रहे कुछ?”
“क्या बोलूं, यह सब तुम्हारा वहम है. इन टेम्पररी स्टाफ़ कि इतनी हिम्मत नहीं है कि…. और फिर मैं तो क्लब का सेक्रेटरी हूं. वह ऐसा नहीं कर सकता, बस थोड़ा खयाल रखता है मेरे कारण. तुम बस ऐसे ही…”
मैं खीज और चिढ़ के आवेग से जैसे गुस्से से बाहर हो रही हूं…”ऐसा नहीं कर सकता… यह विश्वास कितना घातक हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकते. इन छोटी-छोटी चीज़ों की अनदेखी करना दर असल हमारे डरपोक स्वभाव का ही परिचायक है. हम बुरी या फिर अप्रिय बातों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते…. इसे स्वीकार करना हमारे लिये मुश्किल होता है. अघटित घटित हो ले वह ठीक, पर उसे…. ऐसा नहीं कर सकता क्यों..? ऐसे ही टेम्पररी टाईप के लोग जो अपनी पत्नी और परिवार से दूर रह कर दो पैसे कमा रहे हैं, उनके इन दुष्कर्मों में लिप्त होने की संभावना ज्यादा होती है. ज्यादा पैसे नहीं, सुविधा नहीं, मनोरंजन का कोई साधन नहीं, शिक्षा नहीं और ढेर सारा खाली वक्त… शैतान का घर तो यह हमारा दिमाग ही होता है. रोज अखबार और टी वी में खबरें देखते हो पर…”
“मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता. मेरी बेटी ठीक है, नॉर्मल है और मैं क्यों मानूं तुम्हारी कोई उथली सी बात?” शेखर उठकर बेटी को बुलाने चल देते हैं…
 |
| साभार गूगल |
मैं भन्नाई सी उठ खड़ी होती हूं. बेटी को लेती हूं उनसे और चल देती हूं इस पशोपेश के साथ कि शेखर नहीं मानेंगे ऐसा कुछ. वह मेरे साथ नहीं खड़े होंगे बेटी की सुरक्षा के इस मोर्चे पर. वे स्त्री नहीं हैं और औरतों के इस भय को नहीं समझ सकते वे. मुझे ही अन्वी की परछाई बन कर रहना होगा, चलना होगा उसके साथ. परछाई की प्रवृत्ति से भी इतर रहना होगा उसके साथ. धूप और साये, दिन और रात, सुबह और शाम सब में. उससे बनाना होगा वह रिश्ता कि कुछ भी… मेरी आंखों से अदेखा न छूट जाये. कोई गुंजाइश ही कहीं छूटी न रह जाये.
मैं उस रात पहली बार अनी को एक पल को भी अपनी बाहों से अलग नहीं होने देती….
...उसी रात वह सपना जन्मा था मेरे भीतर, फिर पला-बढ़ा था. मेरी रातों के सुकून को किसी बाघ की तरह झपट्टा मार कर ले भागता. नींद के नाम से मैं डरने लगी थी उसी दिन से. जागना अच्छा लगने लगा था, सुकूनदेह. मैं ढूंढ़-ढूंढ़ कर काम निकालती, फिर निपटाती उसे देर रात तक. फिर कोई नया काम. सोना जब मजबूरी हो जाता तो सो लेती पर वैसे ही बेहिस, बेमन. आंखें दिन भर जले तो जले, थकान पूरे वज़ूद पर हावी हो तो हो. चेहरा चाहे जितना बुझा-बुझा लगे लेकिन कोई बात नहीं…
...मै सोचती हूं, खूब सोचती हूं इस सपने के बावत और नकारना चाहती हूं इसका अस्तित्व. तर्क ढूंढ़ती हूं, समझाती हूं खुद को चाहे वे तर्क कितने ही खोखले हों, कितने ही कमजोर. मै कई वर्ष पीछे देखती हूं… सपने में दिखनेवाली नीचे की ओर निरंतर जाती हुई वे सीढ़ियां… मुझे बावड़ियों की याद आती है…
दिल्ली में मेरे घूमने की मनपसन्द जगहें, बाबड़ियां… मतलब वो सीढ़ीदार कुंए जिनका इस्तेमाल प्राचीन काल में जल संरक्षण और उपयोग के लिये होता था. मुगल काल और उससे भी पहले दिल्ली में लोगों की पानी संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिये बादशाहों और राजाओं ने बावड़ियों का निर्माण करवाया, जहां मुसाफिर न सिर्फ अपनी प्यास बुझाते बल्कि आराम भी कर सकते थे.
हैली रोड की अग्रसेन की बावड़ी, कहते हैं, महाभारत काल में बनवाई गई वह बहुमंजिली बावड़ी है जो मुझे कभी भी किसी राजमहल से कम नहीं दिखी. इसकी कारीगरी मुझे मंत्रमुग्ध करती है. पंचमंजिले बावड़ी में छत की जगह छायादार नीम का बड़ा-सा पेड़, हर स्तर का आधा बुर्जीदार हिस्सा, लाल-पत्थर की इसकी सीढ़ियां सब मुझे बेतरह खींचती थी. शेखर कहते भी थे तब, क्या मिलता है तुम्हें इस खंडहर में… पानी… कहां है पानी… वह नीचे गंदला सा कुछ? मै मां से सुना हुआ मुहावरा दुहरा देती… ‘गुजरा हुआ फिर भी मसूदाबाद है…’ और सोचती हूं मसूदाबाद से मतलब मुर्सिदाबाद, मुरादाबाद या कि कुछ और सोचती रहती.
पानी के लिये मेरी ललक से शेखर तब भी वाकिफ थे. नहाना, तैरना कभी मुझे अच्छा नहीं लगा. पर पैर डाल कर बैठना, पानी में खड़े होना मुझे बेहद पसन्द है. पानी मुझे खींचता है बेतरह. सड़क मार्ग से जाते हुये अब भी कहीं छोटा सा जलाशय या कि पोखर मुझसे मिलने की जिद ठान लेता है और मैं बीच राह उतरने की. सारी थकान, सारी बेचैनी जैसे पानी खींच ले जाता है, मुझे मुक्त करता हुआ, नई ज़िंदगी देता हुआ. मुझे पानी से मतलब है, सिर्फ पानी से…
…वह दिल्ली थी. गरम, तपती, जलती, झुलसती दिल्ली और वहीं उन बावड़ियों का होना मेरे लिये राहत था. फ्रीलांसिंग के उस दौर में कहीं से कहीं जाती, गर्मी की दुपहरियों में रुक जाती ठिठक कर, खास कर कनॉट प्लेस या जनपथ में हुई तो अग्रसेन की बावड़ी पर. उनसे मिलना वैसा ही था जैसे अजनबी शहर में बहुत अपने से मिलना. सुख-दुख बतिया कर हल्का हो लेना. अतीत की कहानियां समेटे बावड़ियां मुझे नानी-दादी की तरह प्यारी लगतीं, अपनत्व और ममत्व से भरी हुई. अपने प्यार की छांह में सबको समेट लेने को आतुर. राजों की बावड़ी (मेहरौली), खाड़ी बावड़ी (चांदनी चौक), फिरोजशाह कोटला की बावड़ियां… मैं तालाशती रहती अपने लिये एक नया ठौर. एक नया पनाहगाह. मुझे लगता और हमेशा लगता दिल्ली को किलों और मकबरों का शहर कहने की बजाय बावड़ियों का शहर भी कह सकते हैं और खूब-खूब कह सकते हैं…
…तो मुझे लगता और खूब-खूब लगता यह सपना कहीं उन बावड़ियों से हो कर चला आया है मुझ तक. वही बुर्जिया, वही मेहराब, वही सीढ़ियां और वही मेरी बेचैनी और छटपटाहट. जब कभी किसी अपने से दूर हो जायें तो पुकारते ही हैं वे. छटपटाती ही है आत्मा उनकी खातिर. चारु कहती थी तब, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे एकांत में अकेले चल देने से, इन सुनसान जगहों पर. सेफ कहां होती है ऐसी जगहें, ऐसे मत जाया करो. मैं हंस देती, बस… अंदर का सन्नाटा बाहर के सन्नाटे से ज्यादा भयावह होता है.
पालिका बाज़ार के सेंट्रल पार्क में शाम दोपहर गुटर गूं करते जोड़े, जंतर-मंतर के कोने-कंदरे में बैठी आपस में मशगूल जोड़ियां… पर पता नहीं क्यों, मैं उनमें से एक नहीं थी, न होना चाहती थी. शेखर के साथ होने के बावजूद मैं जिद कर के अग्रसेन की बावड़ी ही जाती, और जाती तो जाती. शेखर भी तब साथ-साथ चल देते, पर आज की तरह कुढ़ते-खीजते हुये नहीं बल्कि दिल से.
मैं सोचती हूं और खूब-खूब सोचती हूं इस सपने का मतलब..? कि तभी कुछ याद आता है… ठीक शादी से पहले की बात… शेखर के बहुत दोस्त थे, मेरे कम. शेखर बोलते थे, बातें करते थे और मैं घुन्नी… ऐसे में ही प्रशांत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था. मैंने दोस्ती की थी, पर लक्ष्मण रेखा तय करते हुये. उसे शेखर के बारे में बताया भी था धीरे-धीरे… अपनी वर्षों पुरानी दोस्ती…. हमारे सपने… हमारा परिवार… हमारी मुश्किलें… हमारी ख्वाहिशें… और एक दोस्त की तरह वह सबकुछ सुनता, दिल से सुनता. और मुझे लगता कि मैं बोल भी सकती हूं किसी से इस तरह खुलकर. उस दिन जब मैं हिन्दुस्तान के दफ्तर से लौट रही थी, वह अपनी ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले कर आ गया था. उसी ने कहा था – इंडिया गेट चलते हैं, धूप में बैठ कर अच्छा लगेगा. मैं अपना हक दिखाते हुये कह गई थी नहीं, अग्रसेन की बावड़ी… इतिहास का वह विद्यार्थी चौंक पड़ा था क्षण भर को, यह कहां है..? मैं उसी हक से उसकी हथेलियां खींचती हुई कहती हूं, मैं ले चलती हूं न. वहां पहुंचने के बाद मेरे अंदाज़े के विपरीत वह खुश हुआ था. मुझे भी अच्छा लगा था. जाड़े का दिन सो इक्का-दुक्का लोग. सीढ़ियां उतरते वक्त वह इतना करीब था कि उसकी सांसें मेरी पसलियों को छू रही थीं. मैं थोड़ा अलग हो कर चलने लगी थी. वह ठिठका था थोड़ी देर को, फिर करीब आकर पूछा था उसने – ‘”यार ये जगहें कहां से तलाश लेती हो तुम?…”
“क्यों, पसन्द नहीं आई?”
“नहीं, बहुत पसन्द आई इसीलिये तो…” उसकी फुसफुसाहट मेरी कान के लबों को गर्मा गई थी. मुझे लगा लौट जाना चाहिये. मेरी जिद ने कहा था – क्यों?.
“और कहां तक चलना है?”
“मैंने कहा था न, इसकी गहराई डेढ़ सौ फुट है. सोचो अभी और कितना नीचे जाना होगा.”
“नीचे जाना मुझे बेहद पसन्द है.” उसके स्वरों के रहस्य भाव में ऐसा कुछ था जिससे मैं चौकी थी पहली बार. पर मैंने अपने चौंकने को एक चौकन्नेपन से ढंका था…”१९७५ तक इसमें खूब पानी था. पर अब जलस्तर थोड़ा नीचे चला गया है. बस एक मंजिल और, बीच वाले मंजिल से पानी दिखने लगता है…” मैं उसे जताना चाहती थी, मैं वैसी ही हूं अब भी – निडर, निरपराध और निर्बोध…
 |
| साभार गूगल |
मैं सबकुछ भूल कर खुशी से चिल्लाती हुई उसकी तरफ पलटती हूं – “प्रशांत, देखो पानी… वो देखो!”
पर प्रशांत की नजरों की तलाश की मंजिल कुछ और थी…. झुक कर उसने एक झटके से चूम लिये हैं मेरे दोनों होंठ…”पानी ही तो तलाश रहा था मैं भी…”
मेरे होठ बेवसी से ज्यादा सिले हैं या कि विस्मयविमूढ़ता से, कहना मुश्किल है. एक ही क्षण में बहते जल-सा साफ और पारदर्शी रिश्ता मैला और गंदला हो गया था और मैं मूक – हंसे-रोये बगैर…
मैं कब तक खड़ी थी चुपचाप मुझे नहीं पता. तंद्रा टूटी थी तो उसी की आवाज़ से…”कम ऑन, तुम तो ऐसे शो कर रही हू जैसे कि तुम्हें किसी ने पहली बार छुआ हो. शेखर तो साथ ही रहता है न तुम्हारे, फिर….”
मैं बटोरती हूं खुद को और कहती हूं…” शेखर और मैं साथ जरूर रहते हैं पर अकेले नहीं और शेखर ने मुझे कभी इस तरह नहीं…”
उसके होंठों का विद्रूप बढ़ जाता है. व्यंग्य और तिलमिलाहट से चेहरा टेढ़ा और लाल…”फिर किसी डॉक्टर से जाकर दिखलाओ उसे, मर्द ही है न…?” फिर थोड़ा रुक,कर थोड़े संयत स्वरों में कहता है वह… “तुम्हारी बेतकल्लुफी और संकेतों से ही तो… और तुम ऐसे दिखा रही हो…”
मेरा दुख, मेरी ग्लानि, मेरी पीड़ा सब थहरा देते हैं मुझे. मैं थकी-हारी सी बैठ जाती हूं वहीं. खूब रोती हूं. किसके लिये यह मुझे भी पता नहीं.
मेरे रोने से शायद ग्लानि जागी है उसके भीतर… कहता है वह – ” सॉरी, माफ कर दो मुझे.” उसके इस बार के कंधे छूने में कोई लस्ट नहीं है पर कोइ लगाव भी नहीं महसूसती मैं.
जो कुछ मरना था मर चुका है… खाली हो चुकी है वह कोई जगह… और मैं रोना चाहती हूं बस… मैं कहती हूं – “तुम जाओ प्रशांत…”
” और तुम?…”
” मैं यहीं रहना चाहती हूं.”
“यहां?”
” हां.” मेरा स्वर दृढ़ है. वह एक बार देखता है मुझे, फिर चला जाता है बिना मुड़े, रुके. मैं रोती हूं – खूब रोती हूं, वहीं बैठ कर… मेरा रोना तर्पण है एक रिश्ते का. तर्पित तो जल में ही करते हैं न सब.. ग्रहण करता है जल हमारी सारी इच्छायें, दुविधायें और वह सबकुछ जो हम समेट कर नहीं रख सकते या कि नहीं रखना चाहते. सचमुच गंदला हो आया है पानी का वह हिस्सा.
…मैं सोचती हूं, यह सपना यहीं से उपजा होगा. अपने भीतर के उस टूटन से. फिर सोचती हूं इस सपने से अन्वी का क्या वास्ता, उस सपने में अनी क्यों होती है आखिर? मैं एक कमजोर-सा ही सही पर नया तर्क तलाशती हूं… मैं टूटने नहीं देना चाहती अनी के भीतर कहीं भी, कुछ भी. इसीलिये उस सपने में अपनी जगह अनी दिखती है मुझे, ठीक उसी जगह – हताश, टूटी हुइ, निचुड़ी हुई-सी, कभी-कभी रोती-बिलखती, कभी बिसूरती, निस्सहाय, अकेली अनी. उसकी निर्भाव आंखें… और सीढ़ियां दर सीढ़ियां उतरती, उसे खोजती हुई मैं.
शेखर मुझे इस तरह परेशान देखकर कहते हैं कभी-कभी, अभी तो बच्ची है वह. आज के दौर की बच्ची… कल को बड़ी होगी, उसे तुम्हारा इस तरह परछाई बनना, पहरे देना भायेगा? कौन बच्चा पसन्द करता है यह सब? तुम्हें पसन्द था? कल बड़े होने पर वांछित-अवांछित कई तरह के संबंध होंगे उसकी ज़िंदगी में… देह भी कभी न कभी, कहीं न कहीं… कब तक उसे प्रोटेक्ट करती रहोगी?
…मुझे हैरत होती है, यह सब सुनकर. शेखर मुझे इतना ही समझते हैं.
मैं कहती हूं और पूरी दृढ़ता से कहती हूं, आगे क्या होगा, वह क्या करेगी, कैसे जीयेगी वह उसका निर्णय होगा. अभी तो मसला है और एक ही है कि वह खुद निर्णय और फैसले लेने तक तो निर्बाध बड़ी हो ले, एक पुरसुकून बचपन जीते हुये. एक ऐसा बचपन, जिसकी स्मृतियां उसे कल उदास या दुखी नहीं बनाये. उससे ज़िंदगी को खुशी-खुशी जीने का जज्बा न छीन ले. मेरी कोशिश तो बस इतनी सी है, शेखर!
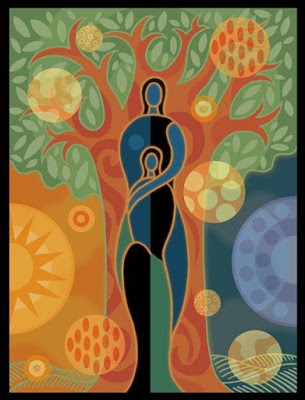 |
| साभार गूगल |
मैं जब अपनी सहेलियों को भीड़-भाड़ में आस-पड़ोस में, कहीं भी बच्चों को निर्द्वंद्व छोड़ती हुई देखती हूं तो अच्छा तो लगता है पर हैरत भी होती है. इन्हें कभी भय नहीं होता या कि मैं ही कुछ ज्यादा… शायद शेखर ठीक ही कहते हैं, अनी के बचपने को बनाये रखने की कोशिश में मैं जो लगतार उससे छीनती रही हूं वह उसका बचपन ही है… किसी आगत अनहोनी की आशंका में उससे उसका आज छीन रही हूं मैं.
निधि मेरे थोड़ी करीब है. अपनी बच्ची को ले कर कुछ पजेसिव भी. मैं उससे बांटती हूं अपनी भावनायें, कहती हूं कि जब भैया मायके में गर्मी के दिनों में अनी को अपने एसी वाले कमरे में सोने के लिये ले जाते हैं तो बारहा मना करती हूं मैं और अगर तब भी वो ले ही गये तो मैं तबतक नहीं सोती जबतक अनी को वहां से किसी बहाने ले न आऊं या कि वह खुद उठकर आ न जाये मेरे पास…बराबर के भाईयों के साथ उसे अकेले न खेलने देना… मैं जानती हूं इस तरह सोचना गलत है, रिश्तों पर इतना अविश्वास…पर मैं क्या करूं…. पूछती हूं मैं उससे कि क्या यह डर उसे भी सताता है, या कि मैं ही… वह पुष्ट करती है मेरे भय को. मुझे थोड़ा सुकून मिलता है.
अनी मेरे बगैर नहीं रह सकती. पांच साल की बच्ची की उम्र ही कितनी और औकात ही क्या? जहां कहीं जाती हूं, चाहते न चाहते चलना ही होता है उसे मेरे पीछे. इच्छा-अनिच्छा का यहां कोई महत्व नहीं रह जाता. चाहे मजबूरी ही सही पर लम्बी-लम्बी जर्नी, बाई रोड भी. यह समझते हुये भी कि उसे उल्टियां आयेंगी, चक्कर आयेगा, बीमार भी हो सकती है वह. फिर भी… मां लोगों से मिले, बाहर निकले, घूमने या सेमिनार में बोलने जाये अन्वी को बेहद पसन्द है. कहीं से कोई बुलावा आया नहीं कि अनी का कूदना शुरु. मुझे मां को बोलने के लिये ले कर जाना है… मैं अपनी मम्मा की सबसे अच्छी फ्रेंड हूं न! मैं मम्मा को फलां जगह ले कर जा रही हूं. अनी अपनी सहेलियों से ऐसी ही बातें करती है…
विजयनगरम जाने की बात से वह ऐसे ही फुदक रही थी और उसकी फुदकन मेरे भीतर भय जगा रही थी. दस घंटे की कार की सवारी, फिर ट्रेन, फिर तीन दिनों का सेमिनार. कैसे जाऊंगी मैं? कैसे संभाल पाऊंगी उसे? पर सब उसकी आंखों की उसी चमक की खातिर…
होटल में उसका बेड अलग है. मैं समझाती हूं उसे, मां को हर जगह ले के जाने वाली बच्ची तो नहीं हो सकती न! अब तुम्हें बड़ों की तरह अकेले सोना भी सीखना होगा. वह घबड़ाती है, परेशान होती है पर मान जाती है धीरे-धीरे…
दिन भर फुदकती रहती है वह, ऊपर-नीचे, दूसरे कमरे तक, दूसरे लोगों के पास. उन्हें कवितायें सुनाती है. मैं अपनी सांकल थोड़ी ढीली कर देती हूं. वह खुश रहे, मुस्कुराये बस…
…पर मुश्किलें हैं, और दूसरी हैं. अनी की हर पल कुछ न कुछ बोलते रहने वाली जुबान बेचैन है. बोले तो किससे और क्या.. भाषा की दीवार चीन की दीवार हुई जाती है. फिर भी बगैर बोले-बतियाये वह बांध ही लेती है लोगों को अपने नटखटपन से. साथ आये हिंदीभाषी लोगों को वह घोंट-घोंट कर कवितायें पिलाती है.
अन्वी खुश है. अनी दौड़ती-भागती रहती है, बातें करती रहती है. मेरा डर भी घूमता रहता है मुझसे आंख-मिचौली का खेल खेलता हुआ. अनी स्वतन्त्र है. पर यही तो है डर का सबब भी. मुझे पूरे दो सत्रों में मंच पर रहना है. बेचारी अनी… पहला दिन बीत जाता है, नि:शंक.. दूसरा… … मैं मंच से रह-रह कर देख रही हूं, ऊबी हुई है वह शायद लम्बे-लम्बे वक्तव्यों से. अपनी मम्मा की बारी की प्रतीक्षा में है वह. इशारे-इशारे में कहती है वह – ‘मम्मा आप कब बोलोगी?’ मैं नजरें झुका लेती हूं कोई देख न ले. समझ न ले इस मौन वार्तालाप को. मंच पर बैठने का अनुभव अभी बहुत नया-सा है. सो उसकी गरिमा का ध्यान थोड़ा ज्यादा. अपने से ज्यादा अपनी बेटी की खुशी में खुश हूं मैं. उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं.
चमकविहीन आंखें कैसी होती है.. कैसी होती है उनकी उदासी मैं जानती हूं…मैं समझती हूं… अनी के चेहरे पर उन आंखों की कल्पना भी असहनीय है मेरे लिये.
अनी कुछ देर तक दिखने के बाद गायब है. मैं सोचती हूं, वह होगी इधर-उधर कहीं. मेरी बारी आती है चली जाती है. पर अनी नहीं आती. यह अनहोनी ही है. ऐसा कैसे हो सकता है आखिर. मैं घबड़ाती हूं, बेचैन होती हूं पर प्रयत्नशील भी कि ये बेचैनी चेहरे पर न आ जाये. मैं उठ कर देखना चाहती हूं पर लगता है यह मंच की अवज्ञा होगी. मैं कुछ देर बाद धीरे से मंच से खिसक लेती हूं… मैं ढूंढ़ती हूं उसे हर तरफ, अपने कमरे में, परिचितों के कमरों में. कान्फ्रेन्स रूम के पीछे-आगे. रिसेप्शन पर पूछती हूं, बच्ची है कुछ खरीदने न निकल गई हो… ‘पीला फ्रॉक पहने कोई बच्ची बाहर गई है क्या?…’ ‘कौन?…’ ‘आपकी बच्ची?…’ ‘नहीं…’ घबराती हूं मैं, अब कहां.. कितने सारे डर, कितने सारे सपने सब इकट्ठे हो कर मेरे आंसुओं में निकलने लगते हैं.
मुझे खयाल आता है तलगृह का… कल बुक एक्जीवीशन तो उसी में था. तलगृह का खयाल मन में जैसे सारी आशंकाओं को जगा जाता है. मेरे हाथ-पांव सब ठंडे मेरे लिये. कदम उठाऊं तो कैसे, और जाऊं तो कहां?
सीढ़ियां उतरते हुये मुझे खयाल आता है सपनों का, ऐसे ही तो बस सीढ़ियां-सीढ़ियां. मैं जिसे अबतक बाबड़ी की सीढ़ियां समझती रही… मैं बेसमेंट के अन्धेरे में टटोलती-टोहती हूं, हर टकराहट मन में बेचैनी पैदा करती है. फिर शान्त होती हूं यह सोच कर कि अनी यहां नहीं है… बेचैनी फिर बढ़ती है, अनी यहां भी नहीं है. फिर कहां है आखिर?
 |
| साभार गूगल |
मैं दौड़ती हूं ऊपर की तरफ. कान्फ्रेन्स रूम के पास तक पहुचती हूं… अनी सामने से आती दिखती है. हाथों में जलेबियां लिये और किन्हीं एक महिला की उंगलियां थामे हुये. मैं चीख पड़ती हूं, गले लगा लेती हूं उसे… “कहां चली गई थी मुझे बताये बगैर.”
वह शांत भाव से कहती है – “मम्मा, आप तो ऊपर बैठी थीं न फिर आप से कैसे कहती! और आपने ही तो कहा था कि वहां बातें नहीं करते.”
“फिर भी आप इशारे से कह कर जातीं.” मैं एक बेचारा-सा ही सही तर्क ढूंढ़ने की कोशिश करती हूं.
“मम्मा आप तो मुझे देख भी नहीं रही थीं. देखती तब न!”
वह महिला हंसती है. मुझे पहले-पहल लगता है मुझ पर हंस रही है वो. मैं अपने आप से कहती हूं, नहीं वह ऐसे ही हंस रही है… वो कहती है – ” बच्ची का मुंह मीठा करवाने ले गई थी. बहुत ही अच्छी कवितायें सुनाती है. मैं इसे इसकी प्रतिभा के लिये प्रोत्साहित करना चाहती थी.” अहिंदीभाषी लोगों की शुद्ध-शुद्ध किताबी हिन्दी में कहती है वह, फिर आगे की बात अंग्रेज़ी में… “बाहर चॉकलेट की दुकानें बन्द थीं, दोपहर के कारण, सो यहीं से जलेबियां दिलवा दी. आप भी चलिये, भोजन लग चुका है.”
मैं पहले शर्मिन्दा होती हूं फिर धीरे-धीरे तटस्थ – “शुक्रिया.”
रात हम मां बेटी जब घूम-फिर कर कमरे में आती हैं तो अनी सोते-सोते मेरे गले में बांहे डाल कर पूछती है, “मम्मा, आप इतना डरती क्यों हैं?”
मैं बहुत देर तक चुप रहने और सोचने के बाद कहती हूं…” पता नहीं बेटे.”
अनी सो चुकी है. मैं धीरे से उसे अलगा कर उसे उसके बिछावन पर रख आती हूं. तकिया कंबल सब लगा कर.
बत्तियां बन्द कर चुकी हूं मैं. कोई है जो अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे कहीं ले जा रहा है, सीढ़ी-दर-सीढ़ी जैसे अपने भीतर ही उतर रही हूं मैं… अन्धेरे में कई दृश्य गड्डमड्ड हैं… क्या उस ‘पता नहीं’ के जवाब में…?
अनी का प्रश्न, अपना यह एकांत और अंधेरा सब मिलकर जैसे मुझे सामना करने का साहस देते हैं, अपने भीतर की उन अंधी बावड़ियों का जहां जाने से मैं खुद डरती हूं… जिससे नजरें चुराते-चुराते भागती हूं मैं और अनी के लिये अपने भय के लाख-लाख दूसरे कारण और तर्क ढूंढ़ती हूं…
नन्हीं सी मैं घर के उस ड्राइवर की गोद में हूं जो सबका प्रिय है. जो अक्सर मुझे गोद में बिठा कर रखता है, जांघों पर अपनी पूरी ताकत से दबा कर – जहां मेरा दम घुटता है…
ट्यूशन पढ़ाने वाले भैया की वो गंदी सी चुम्मियां जिसमें वो होठ गालों से नहीं सटाते, होठों पर रगड़ते हैं, कस कर…
उस दूर के अधेड़ जीजा जी का पांव दबबाने के बहाने जगह-जगह उंगलियां फिराना…
मैं चुप थी और चुप होती गई थी. कोई प्रतिरोध नहीं करना स्वभाव का एक हिस्सा बन गया हो जैसे. बस दुख… भीतर तक पसरता एक अजनबी, अनचाहा और अनजाना सा दर्द.
मैं सोचती हूं, घर में इतने-इतने लोग… किसी को तो समझना था, किसी को बचा लेना था मुझे… खास कर मां को. पर उतने भरे-पूरे परिवार में किसी को इतनी समझ नहीं थी. किसी के पास इतना वक्त नहीं था. सबके अपने हिस्से के काम, सबकी अपनी एक दुनिया. मैं फूट-फूट कर रोती हूं, सिसकती हूं, सिसकती रहती हूं…
मैं उठ कर अनी के पास चली जाती हूं. सुबकते-सुबकते मैं कब सो गई हूं, अनी को अपनी बांहो के घेरे में लिये हुए मुझे पता नहीं.
...नींद में फिर वही सपना आया है लेकिन अबकि कुछ बदले रूप में. सपने में वैसी ही कोई बावड़ी है, कोई नीचे उतर रहा है चुपचाप, उदास… धीरे-धीरे… ध्यान से देखती हूं, यह मैं हूं और बावड़ी है, गंधक वाली बाबड़ी, जिसे सुल्तान इल्तुतमिस ने कुतुबुद्दीन एबक के इस्तेमाल के लिये बनवाया था.. कहते हैं, इसकी पानी में गंधक की मात्रा बहुतायत में है और यह चर्मरोगों और बहुत से अन्य रोगों के लिये रामबाण का काम करता है…नीचे उतरकर उलीच-उलीच कर उसके पानी से अपना अंग-अंग धोती हूं, सोचती हूं मन-ही-मन – शायद मेरे भीतर के तलगृह में छुपे इन यादों को भी धो कर मिटा सके यह… मै निर्मल हो लूं ऐसे कि मन में कुछ भी न बचा रह जाये, कुछ भी नहीं.
हंस – सितंबर, २०१२ में प्रकाशित
