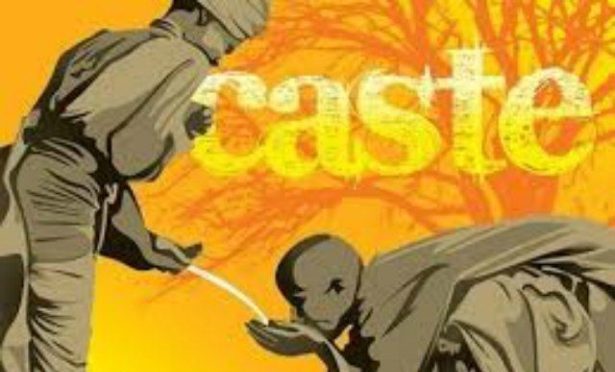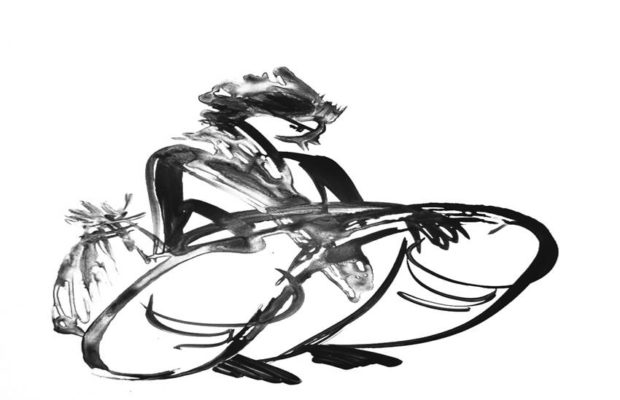रेखा सेठी
 हिंदी विभाग, इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली वि वि, में एसोसिएट प्रोफेसर. विज्ञापन डॉट कॉम सहित आधा दर्जन से अधिक आलोचनात्मक और वैचारिक पुस्तकें प्रकाशित
हिंदी विभाग, इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली वि वि, में एसोसिएट प्रोफेसर. विज्ञापन डॉट कॉम सहित आधा दर्जन से अधिक आलोचनात्मक और वैचारिक पुस्तकें प्रकाशित
विमर्शों की दुनिया में सुशीला टाकभौरे की कविता दोराहे पर खड़ी प्रतीत होती है.दलित व स्त्री अस्मिता की स्वतंत्र राहें जैसे एक-दूसरे से होकर गुजरें…हिंदी के दलित साहित्य में जिन महिला रचनाकारों ने दलित और स्त्री अस्मिता के लिए ज़मीन तैयार की उनमें सुशीला टाकभौरे का सक्रिय हस्तक्षेप रहा.वे लंबे समय से कविता, कहानी, उपन्यास, विचारात्मक लेख, आत्मकथा जैसी विधाओं में अपनी रचनात्मकता का परिचय दे रही हैं.1970 में अम्बेडकरवादी चेतना के प्रभाव से दलित साहित्य की जो अलग पहचान बनी उसमें स्त्री स्वर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया.(ऐसा तब है जब सावित्री बाई फुले जैसी रचनाकार पहले से ही दलित साहित्य की ऊर्जा-स्रोत रही हैं ) नब्बे के दशक में यह स्थिति बदली और पत्र-पत्रिकाओं में दलित स्त्री रचनाकारों ने अपनी उपस्थिति के महत्व का एहसास कराया.अब उसे अनदेखा करना नामुमकिन था.स्त्री-साहित्य के इस उन्मेष में सुशीला टाकभौरे, साहित्य की सभी विधाओं में, एक महत्वपूर्ण नाम बनकर उभरीं किन्तु जितनी चर्चा उनकी आत्मकथा ‘शिकंजे का दर्द’ तथा उनके कहानी संग्रहों की हुई है, उतनी कविताओं की नहीं हुई.अब तक उनके चार कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं – ‘स्वाति बूँद और खारे मोती’ (1992 ), ‘यह तुम भी जानो’ (1994), ‘तुमने उसे कब पहचाना’ (1995), ‘हमारे हिस्से का सूरज’ (2005).दलित और स्त्री प्रश्नों पर केन्द्रित ये रचनाएँ सामाजिक न्याय की गुहार हैं.
भारतीय सामाजिक संरचनाओं का इतिहास आज़ादी के बाद (भी) और कहें तो आज़ादी के बावजूद (भी) नहीं बदला.दलित-जीवन के अंधकारमय पृष्ठों से यातना और संघर्ष की इबारत मिटाई नहीं जा सकी.इस स्थिति का विवरण देते हुए सुशीला जी लिखती हैं. “दलित शोषण आज भी जारी है.प्रतिदिन ऐसी घटनाएँ घट रही हैं.सवर्ण जातियाँ आज भी दलितों को भयभीत रखने के लिए अमानवीय अत्याचार करती हैं कहीं उन्हें ज़िन्दा जलाया जाता है तो कहीं उनकी बस्तियों में आग लगा दी जाती हैं. कानून और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सवर्णों की मदद करती है.दलितों को कहीं न्याय नहीं मिलता.ऐसा कब तक चलेगा ? इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं दे सकता |” (स्वाति बूँद और खारे मोती पृ .17) यह अनुभव सुशीला टाकभौरे के समस्त साहित्य की पृष्ठभूमि है और सिर्फ सुशीला जी के ही नहीं समस्त दलित साहित्य की पृष्ठभूमि है.यह साहित्य अवहेलना और अपमान के कष्टकारी अनुभव की पीड़ा से रचा गया है जिसकी सामाजिक अंतर्ध्वनियाँ बेहद त्रासद हैं. ‘दुख हमें, सुख उन्हें / कैसी यह विडंबना’—यही विचार, भिन्न शब्दों में पंक्ति-दर-पंक्ति उतर आया है.असमानता के ब्यौरे, यातना की स्मृति, प्रत्यालोचना का रूप धरने लगती है.यह नए किस्म का सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है जिसमें सवर्ण जातियाँ सत्ता और साधनों पर कब्ज़ा किये बैठी हैं.जिस अभिशाप को दलितों ने जीवन-भर भोगा वह उनकी नियति नहीं बल्कि कुछ लोगों की धोखाधड़ी है जो बहुजन समाज को हाशिए पर धकेले हुए है.लगातार उन्हें शिक्षा और सुविधाओं के अभाव में, शहरों से बाहर, उतरन व जूठन पर जीने को विवश किया जाता है.बरसों से ठहरा समाज ऊँच-नीच के सामंती ढाँचे से स्वयं को मुक्त करने में अक्षम रहा.
स्वाधीनता और राजनीतिक अधिकारों के बावजूद जड़ मानसिकता को कोई मिटा नहीं पाया.सुशीला जी की अनेक कविताओं में दलित जीवन का यह दर्द उभरता है.उनके यहाँ स्मृति अपमान का पर्याय बन गई है.पूर्वजों की पीड़ा का संताप तथा वर्तमान में बार-बार जाति के नाम पर भोगा गया अपमान स्थायी सत्य है.‘यातना के स्वर’ कविता में उन्होंने साफ लिखा कि वर्तमान स्थिति में अन्याय के प्रतिकार की चेतना सबल न होने के कारण ही पी एच. डी तक शिक्षा प्राप्त प्राध्यापिका भी झाड़ूवाली कही जाती है.शोषण के ये सन्दर्भ अपमान की पीड़ा को जीवित रखते हैं.ऐसी सभी स्थितियाँ घोर अपमानजनक एवं अस्वीकार्य हैं.पीड़ा के इन अनगणित चिन्हों को झेलते हुए, अब सीधे सामने की लड़ाई का संकल्प है.दया और सहानुभूति के पर्दे गिराकर, पूरे वर्ग पर किए अत्याचारों का हिसाब माँगा जा रहा है.कुछ व्यक्ति या जातियाँ ही कटघरे में हैं, पूरे समाज को जवाब देना होगा कि कैसे उसने अपने जनसमूह के एक बड़े भाग को शताब्दियों तक असंख्य यंत्रणाओं की अग्नि में जलने को विवश किया.
हम दलित
आदम रूप होकर / आदम भाषा में पूछना चाहते हैं सवाल
मानव सभ्यता-संस्कृति का इतिहास क्या है ? / भारतीय संस्कृति का आधार क्या है
क्यों किया अब तक / हम पर अत्याचार ?
(हम दलित, यह तुम भी जानो पृ.87 )
दलित साहित्य जिस नए सौन्दर्यशास्त्र की पैरवी करता है उसमें साहित्य का संबंध संघर्ष और जागृति से है.कविता का लक्ष्य न्याय की पुकार है.सुशीला टाकभौरे की इन कविताओं की सृजन भूमि यही है.जातीय उत्पीड़न तथा स्त्री जीवन का दोहरा अभिशाप— अधिकांश कविताओं का विषय-बोध बार-बार इसी घेरे में घूमता है.शायद अनेकश: कहने पर भी पीड़ा पूरी तरह चुकती नहीं.वे बार-बार अपनी कविताओं में उपेक्षित दलित समुदाय की जड़ मानसिकता पर चोट कर, उन्हें स्वयं को पहचानने का संदेश देती हैं.उनके अनुसार कविता की सार्थकता इसी बात में हैं कि सोये हृदयों को आंदोलित किया जा सके.जागृति एवं संघर्ष के बिना, समता-पूर्ण सामाजिक संरचना की आकांक्षा स्वप्न ही रहेगी.‘हमारे हिस्से का सूरज’ काव्य-संकलन के मनोगत में सुशीला टाकभौरे अपनी कविताओं के उद्देश्य व दलित-कविता की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती हैं––“इनका आधार अम्बेडकरवादी विचारधारा है इनमें शोषण, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और दुश्मनों को ललकारने की चेतना है, इसमें कहीं यातना के स्वर हैं, कहीं चेतना के स्वर हैं.कहीं शोषकों को धिक्कार है तो कहीं अन्याय के विरुद्ध अत्याचारियों से बदला लेने की हुंकार है.दलित कविता के विषय, भाव एक जैसे होने के बाद भी, वे अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दलित वर्ग की भोगी हुई पीड़ा की अभिव्यक्ति हैं |” (स्वाति बूँद और खारे पानी पृ.17 )
सामाजिक स्थितियों की जड़ता के पीछे, धर्म व संस्कार के नाम पर होने वाले अनुकूलन की विशेष भूमिका है.रामायण-महाभारत जैसे आदि ग्रन्थ ऐसे असुविधाजनक प्रसंगों के साक्षी हैं. रामायण में बालि-वध, राम द्वारा शम्बूक की हत्या, केवट, निषाद, शबरी की समर्पणशील भक्ति—ऐसे प्रसंग हैं जिनका पाठ-पुन:पाठ नए विमर्शों की गुंजाइश पैदा करता है.
महाकाव्यात्मक अन्विति में ये प्रसंग कथानायक राम के महिमा-मंडन के लिए रचे गए.इनके रचयिता वाल्मीकि आज दलितों के आइकॉन भी हैं.इससे उस साहित्य के पुन:पाठ की और भी सम्भावना बनती है.सुशीला टाकभौरे की निगाह इस ओर भी गयी. वाल्मीकि को ‘बाल्या’ कहकर, उन्होंने अपना बहुत क़रीबी बना लिया लेकिन सवालों के घेरे से वे भी बाहर नहीं हैं.अपने इस ‘बाल्या’ से वे पूछती हैं कि क्यों उनकी दृष्टि राम पर ही रही, वे शबरी और शम्बूक के सम्मान और प्रगति का नया रचना-विधान क्यों नहीं रच सके? दलित मुक्ति के लिए इन प्रश्नों से जूझना ज़रूरी है.इतिहास को धर्म-ध्वजा के रूप में उठाये चलना जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म देता है, दलित कविता उस वितंडा के प्रति सावधान करती हैं.सुशीला जी की शैली अपनी सरलता में सामाजिक अंतर्विरोधों को प्रश्नांकित करने की रही है. रामायण ही नहीं, महाभारत में भी भील एकलव्य की कथा सवर्ण जातियों के षड्यंत्र-रूप में दोहराई जाती है.कवयित्री के मन की फाँस कहीं और है.वह पूछती है —
भील एकलव्य / तुम्हारा तो सिर्फ
एक अँगूठा कटा था, / पर क्या
पूरे समाज के हाथ भी / काट दिये गये थे ?
(भील एकलव्य, यह तुम भी जानो पृ. 35 )
यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है.एकलव्य ने विरोध नहीं किया लेकिन क्यों नहीं किया, यह सवाल विमर्श का हिस्सा होना चाहिए.यहाँ कवयित्री बड़ी बारीकी से उस सामाजिक प्रक्रिया का अनावरण करती है जहाँ अन्याय और अपमान के विरुद्ध पूरे वर्ग की सहिष्णुता, विरोधी स्वर का अभाव उस समाज के भयंकर अनुकूलन का बोध कराता है.एकलव्य की गुरु-भक्ति, मन ही मन जिसे गुरु माना हो उसके प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है या उसके कारण कुछ और रहे.किन्हीं अर्थों में यह पूरी जाति की नपुंसक वीरता का प्रमाण भी है.क्यों ये जातियाँ अपने अधिकार या सम्मान के लिए खड़ी नहीं हो सकीं.न्याय के लिए धर्म-युद्ध करने वाले समाज में इतिहास क्यों इन घटनाओं को इस रूप में दर्ज नहीं कर पाया यह आज भी पूरे युग की बड़ी चुनौती है.यातना की स्मृति जिस पृष्ठभूमि का निर्माण करती है उसका अगला स्तर सामाजिक विमर्श की शुरुआत करना है.समाज के स्थापित ढाँचे का अस्वीकार, उसे प्रश्नांकित कर उससे टकराने की कोशिश, दलित साहित्य का नया सौंदर्यशास्त्र रच रही है.ऐसे स्थलों पर कवयित्री का स्वर काफी उत्तेजित और चुनौतीपूर्ण हो जाता है –
नहीं रहेंगे अब नत मस्तिष्क / विद्रोह की भावनाएँ
उठने लगी हैं / तूफान बनकर
बढ़ने लगा है आक्रोश / संघर्ष की दिशा में
अब तक वे ही / करते रहे विषपान
सागर मंथन फिर से होगा / अब तुम्हें करना होगा विषपान
(व्यंग्य आघात और विषपान, हमारे हिस्से का सूरज, पृ 142)
इस कवितांश की अन्तिम पंक्तियाँ साभिप्राय हैं.संघर्ष का रास्ता सिर्फ उनके प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति नहीं है.आमूल परिवर्तन की राह जातिगत समीकरण में प्रत्यावर्तन चाहती है.ओमप्रकाश वाल्मीकि ने ‘बस्स बहुत हो चुका’ की जो गुहार लगाई थी वह इन कविताओं में भी प्रतिध्वनित होती है.पीड़ा जितनी अधिक है विरोध उतना ही आक्रामक.यातना के स्वर हुँकार में बदल जाते हैं. सुशीला एक ओर दलितों को अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी अस्मिता के प्रति सचेत होने का आह्वान करती हैं तो दूसरी ओर सवर्णों को शर्मसार भी करती हैं.वे जताती हैं कि जिन सवर्णों ने दलितों को अछूत माना, जिनकी छाया से भी परहेज़ किया वे जब तुम्हारी बराबरी में कुर्सी पर आ बैठे तो तुम्हारा हृदय क्यों फटता है.ऐसे छोटे-छोटे विवरण सामाजिक ताने-बाने पर एक बहस खड़ी करने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की पहल भी बनते हैं. इस दृष्टि से ‘सुनो विक्रम’ महत्वपूर्ण कविता है. विक्रम और बेताल के कथासफ़र की तर्ज पर प्रचलित न्याय, प्रेम की कहानियों की दिशा को अपनी नज़र से देखने को प्रेरित करती यह कविता, विक्रम को ललकारती है —
अब तुम सुनाओ कथा बेताल को / सवार होकर उसके ही कंधों पर
और पूछो सवाल / अधिकतम कितना मूल्य है
एक निरीह महिला को / सरेआम नंगा करने का ?
एक इन्सान को बेबसी की / अन्तिम सीमा तक
पहुँचा देने का ?
कब बदलेगें कर्मकाण्ड / कब मिलेगा सामाजिक न्याय !
पूछो उससे,/ अन्यथा / कर दो उसके टुकड़े टुकड़े !
(सुनो विक्रम, यह तुम भी जानो, पृ 38-39)
आहत मन और आक्रोश की चिंगारी के साथ-साथ कवयित्री बार-बार याद दिलाती है कि दलितों को स्वयं रूढ़ियो को तोड़ने का साहस दिखाना होगा.यह पूरी प्रक्रिया दोरुखी है, एक ओर उच्च वर्ग की श्रेष्ठता को चुनौती, उनके विरोध में संघर्ष का शंखनाद तथा दूसरी ओर दलितों का उद्बोधन, मुक्ति की आकांक्षा.जिस विचारधारा के प्रति निष्ठा एवं प्रतिबद्धता सुशीला की कविताओं को ऊर्जा देती है वह प्राय: उसे दृष्टि के विस्तार का अवसर नहीं देती.हाँ, कुछ कविताएँ अपवाद स्वरूप ही सही ऐसी अवश्य हैं जिनमें कवयित्री का विज़न विस्तृत होता दीख जाता है जैसे दलित संघर्ष को वे बिरसा मुंडा के संघर्ष से जोड़ लेती हैं.बुद्ध, कबीर, फुले, अम्बेडकर दलित चेतना के युगपुरूष हैं.अनेक कविताओं में उनका आवाहन किया गया है.उगते अंकुर की तरह जीने, ज्योति दूत बनने की प्रेरणा इनके माध्यम से दी गई है.यातना से विद्रोह तक और विद्रोह से भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न तक—ये कविताएँ एक वृत्त पूरा करती हैं.
फिर चाँद मुस्करायेगा / हवा गुन गुनायेगी
अश्रु फूल बनकर / राहों में बिछ जायेंगे
टूटे हुए सपने / फिर से सज जायेंगे !
(सपने सज जायेंगे, हमारे हिस्से का सूरज, पृ 154)
इस दृष्टिबोध के सुखद अहसास के साथ दलित चेतना का ग्राफ पूरा होता है.दलित साहित्य के सभी प्रमुख रचनाकारों की भांति ‘यातना, संघर्ष और दृष्टिबोध’ के तीन सोपान सुशीला टाकभौरे की कविता में भी बड़ा इलाका घेरते हैं.
दलित अभिव्यक्ति यथार्थ के जिस खुरदरेपन को सतह पर लाती है, सुशीला जी की कविता उसी राह का अनुगमन कर रही है.अनेक स्थलों पर ऐसा हुआ कि कविता वर्तुलाकार स्थितियों में लगभग फँस कर रह गयी.ऐसा इसलिए भी होता है कि यह कविता सामाजिक बदलाव की दिशा में क्रांतदर्शी भूमिका निबाहना चाहती है.अपने इस उद्देश्य में, अनेक दिक्कतों का सामना करते हुए भी कवयित्री ने निभाया है.दलित आन्दोलन के सभी मुद्दे यहाँ अभिव्यक्ति पाते हैं.जाति का सवाल हमारे यहाँ देश-काल की दिशा को परिभाषित करने वाला है.इसीलिए समतापूर्ण समाज की संकल्पना में जातिगत-उत्पीड़न से मुक्ति का प्रश्न सबसे अहं है.सुशीला टाकभौरे की कविता पीड़ा और प्रतिरोध के विकल्प को सामाजिक प्रत्यावर्तन के अस्त्र रूप में प्रस्तावित करती है.इस देश में यह व्यापक क्रांति का आह्वान है, लोकतान्त्रिक व्यवस्था में बराबर की हिस्सेदारी का प्रश्न.सार्थकता की दृष्टि से ये कविताएँ स्त्री-प्रश्नों की अपेक्षा दलित अस्मिता के सवालों को अधिक शिद्दत से उठाती हैं.जाति और लिंग-परक अस्मिताओं के बीच द्वंद्व की स्थिति नहीं है बल्कि जाति, लिंग की असमानताओं को और भी तीव्र कर देती है.
स्त्री-पक्ष दलितों में दलित, पिछड़ों में पिछड़ी, समाज में सबसे संवेदनशील स्थिति स्त्री की ही है.स्त्री रचनाकार, स्त्री जीवन की विंडबनात्मक स्थितियों, उसकी पीड़ा व संघर्ष से विमुख रहे ऐसा संभव नहीं.सुशीला टाकभौरे भी अपनी कविताओं में स्त्री-जीवन की द्वन्द्वपूर्ण, मारक स्थितियों की धारदार अभिव्यक्ति करती हैं.ऐसी कविताएँ स्वयं को पहचानने की कोशिश भी हैं और अपनी स्थिति से ऊपर उठने का संकल्प भी.वे मानती हैं कि मनुप्रणीत नारी-धर्म, स्त्री को पुरूष पर निर्भर बनाए रखने का उपक्रम है.उनकी कविताओं का उद्देश्य स्त्री को प्रोत्साहित करना है.उन्होंने दलित वर्ग के भीतर भी लिंग आधारित अंतर्विरोधों को गहराई से महूसस किया और बेझिझक होकर बयान किया.
दलित जीवन में जाति और लिंग के अंतर पर रजनी तिलक लिखती हैं – “दलित स्त्रियों की दो दुनिया हैं.एक दुनिया में वह अपने भाई, पति, पिता, साथी, मित्र के साथ जाति-व्यवस्था के खिलाफ साथ खड़ी है, दूसरी दुनिया में अपने ही घर में, समाज में, आन्दोलन में हाशिये से फिसल गयी है, फिर भी वह इसी क्रम में दलित चेतना की सावित्री फुले, अम्बेडकर और बोधिसत्व की विचारधारा से प्रभावित हैं.वह ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता, पूंजीवाद, सामन्तवाद व फासीवाद के विरुद्ध संघर्षरत है, अत: समूचे दलित वर्ग में स्त्री स्वर ने अपनी अलग प्रखर अभिव्यक्ति की दस्तक दी है.दलित कवियत्रियों ने न केवल दलित कविता में बल्कि हिंदी कविता में अनेक ऐसे बिंदुओं को छुआ है जिसमें वर्ण, वर्ग, जाति, लिंग, रूप, के भेदभाव को नकारकर नये समतामूलक समाज की कल्पना को साकार करने का आह्वान है |” (समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन-2 (कविता खंड) पृ. 91-92 ) इस स्त्री की व्यथा-कथा के बिम्ब सुशीला टाकभौरे की कविता में मिल जाते हैं.साथ ही स्त्री-प्रश्न को भाषा, धर्म, जाति, लिंग सम्बन्धी भेदभाव से जोड़कर देखा और उनकी जड़ों को पहचानकर उन पर प्रहार किया यानी जैसी लड़ाई जाति और वर्ग को लेकर है वही लिंग को लेकर भी है, सुशीला टाकभौरे की कविता इस संघर्ष में शामिल है.यह संघर्ष हर स्तर पर समतामूलक समाज की माँग को लेकर आगे बढ़ रहा है. दलित लेखन के शुरूआती दौर में स्त्री साहित्य को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति रही.समस्त स्त्री-वर्ग को दलित मानने की पैरवी करने वालों के बरक्स यह चिंता बनी हुई थी कि स्त्री-पीड़ा की अभिव्यक्ति पर अतिरिक्त बल, दलित आग्रहों को कमज़ोर कर सकता है. एक तर्क यह भी था कि सभी स्त्रियाँ दलित नहीं हैं, क्योंकि दलित-स्त्री, जाति के नाम पर जो मान-अपमान झेलती है वह स्वर्ण स्त्रियों को नहीं झेलना पड़ता.
दलित स्त्री का एक अपना वर्ग है जो उसे समस्त स्त्री समाज में सबसे अशक्त बनाता है.सवर्ण स्त्रियों का व्यवहार भी दलित स्त्रियों के प्रति कम क्रूर नहीं है.इसलिए लैंगिक समानता उन्हें एक वर्ग में नहीं बाँधती.उनकी लड़ाई अलग-अलग है.दलित साहित्य का मुख्य मुद्दा जातिगत असमानता के दंश का प्रतिकार का था.कुछ विचारकों को लगता रहा कि इसमें लैंगिक अस्मिता के सवालों को जोड़ देने से यह संघर्ष बिखर सकता है.उनका आग्रह स्त्री-पुरुष विवाद के परे सबको जातिगत संघर्ष में शामिल रखने का रहा.दलित वर्ग में लैंगिक असमानता को वे अंदरूनी मसला मानते हैं. विमल थोरात तथा अनीता भारती ने तो लगातार इस सरलीकरण का विरोध किया और दलित स्त्री के दोहरे, तीहरे शोषण की तरफ ध्यान दिलाया.ओमप्रकाश वाल्मीकि ने भी अपने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि ‘स्त्री, दलितों में भी दलित है |’ स्त्री जीवन के दोहरे संताप के लिए उन्होंने पूरे समाज में फैली लैंगिक असमानता की पारंपरिक सोच को उत्तरदायी बताया––‘इसके लिए व्यवस्था जनित परंपरावादी सोच उत्तरदायी है, जो स्त्री को दूसरे दर्जे का नागरिक ही नहीं, पाँव की जूती समझती है’ इसे स्वीकारते हुए उन्होनें कहा––“दलित वर्ग में भी इस व्यवस्था की घुसपैठ है.” (दलित दखल पृ. 26-29). इस सारे विवाद को सुशीला टाकभौरे किस तरह देखती हैं, इसकी समीक्षा महत्वपूर्ण है.उनका काव्य–संकलन ‘तुमने उसे कब पहचाना’ मूलतः स्त्री-स्वतंत्रता के विचार को केंद्र में लाता है.यहाँ ‘दलित’, ‘स्त्री’, या फिर ‘दलित-स्त्री’ जैसे वर्गीकरण का कोई ज़िक्र नहीं है.हाँ, प्रस्तावना सरीखी ‘मन की बात’ की पहली पंक्ति में ‘दलित पीड़ित अबला’ का संकेत अवश्य है जो स्त्री की सामान्य स्थिति के लिए प्रयुक्त हुआ है.यहाँ वे बार-बार संपूर्ण समाज में स्त्री की परतंत्र स्थिति पर चिंता व्यक्त करती हैं.
इस परतंत्रता का कारण ‘पितृसत्ता’ तथा ‘मनुप्रणीत नारी धर्म’ है.वे जिरह करती हैं कि स्वाधीनता आन्दोलन में भाषण-जलसों, विरोध–प्रदर्शनों में शामिल स्त्री ‘देश के गुलामों की गुलाम’ थी और आज जबकि अंग्रेज़ों से देश स्वतंत्र है तब भी स्त्री स्वतंत्र नहीं हो पाई है. पारिवारिक संबंधो में पुरुष के समक्ष वह अब भी गुलाम है.“उसकी यह स्थिति तब तक यथावत है, जब तक कि समाज में पुरुष प्रधानता को निर्बाध्य मान्यता प्राप्त है.” उनकी कविताएँ स्त्री में आत्मविश्वास व आंतरिक प्रेरणा जगाने की आकांक्षी हैं और ऐसा करने में वे जाति के आधार पर कोई भेद नहीं करती.‘जानकी जान गयी है’ में वे पुरुष के वर्चस्ववादी व्यवहार को झेलती स्त्री का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती हैं.सीता की पीड़ा समस्त स्त्री-जाति की पीड़ा है.
ओ शबरी के राम ! / आँखे चुराकर / संवेदना न दिखाओ / तुम्हीं ने सीता को / धरती में समाया था.
(जानकी जान गयी है, यह तुम भी जानो, पृ.65) स्त्री की जीवन-स्थितियों का यथार्थ तथा मुक्ति का उद्बोधन उनकी सभी स्त्री सम्बन्धी कविताओं का मुख्य स्वर है.‘मासूम भोली लड़की’, ‘औरत नहीं मजबूर’, ‘आज की खुद्दार औरत’—-सभी कविताएँ स्त्री चेतना की रचनाएँ हैं जिनमें यह स्वर उभरता है कि स्त्री किसी पर निर्भर नहीं, उसे आगे बढ़कर स्वयं को पहचानना है, अपना अधिकार प्राप्त करना है, और नई भोर के सपने को सच करना है.वह ‘नवनीत की पुतली’ नहीं ‘विद्रोहिणी’ है जो स्वयं शक्ति है, पूर्ण महायज्ञ है.स्त्री की विवशता व आकांक्षा की दूरी को पार कर वे स्त्री जीवन का नया ताना-बाना बुनती हैं.
मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, / छत का खुला आसमान नहीं,
आसमान की खुली छत चाहिए / मुझे अनंत आसमान चाहिए |
(विद्रोहिणी, यह तुम भी जानो पृ.86)
स्त्री की स्थिति का कंट्रास्ट भी कई कविताओं में है.समाज के रूढ़ ढाँचे में परंपरा-प्रदस्त जीवन की जकड़नें, स्त्री को तयशुदा रास्तों पर ले जाती हैं—
वह सोचती है / लिखते समय कलम को झुका ले
बोलते समय बात को संभाल ले / और समझने के लिए
सबके दृष्टिकोण से देखे, / क्योंकि वह एक स्त्री है |
(स्त्री, यह तुम भी जानो पृ.31)
बहुत-सी कविताओं में ऐसा हुआ है कि एक ही कविता में अनेक भाव एक-साथ चले आते हैं.स्त्री-जीवन की सीमाएँ और उनसे मुक्ति की आकंक्षा, प्रतिकार के लिए उद्बोधन, शक्ति का अहसास सबके संश्लेषण से सुशीला टाकभौरे विषम-भावों का समकोण रचती हैं.उनके यहाँ केवल स्त्री का ही उद्बोधन नहीं है, पुरुष का भी आह्वान है.सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जैसे साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी, वह आदर्श अनुकरणीय है.सभी पुरुषों को ज्योतिबा फुले के समान समाज का अग्रदूत बनने की प्रेरणा दी जा रही है.यह उदाहरण विशेष महत्व रखता है चूँकि पितृसत्ता को चुनौती, पुरुष–विरोध नहीं है.स्त्री सम्बन्धी अधिकांश कविताओं का ग्राफ आगे-पीछे होता हुआ उसी दायरे में चलता रहता है.‘स्त्री’ व ‘कितने करीब’ जैसी कुछेक कविताओं में संवेदना का घनत्व विशेष महसूस होता है. इस सबके बीच, ‘वह मर्द की तरह जी सकेगी’, ऐसी कविता है जो समस्या उत्पन्न करती है.यद्यपि कविता निश्छल भाव से लिखी गयी है और उस स्थिति को सामने लाती है जहाँ यह पैरवी की जा रही है कि औरत यदि स्वयं को सजी-सँवरी मानना छोड़ दे, आत्म-निर्भर बने तभी वह पुरुष के समान स्वावलंबन एवं सम्मान के साथ जी सकेगी.इस स्थिति को उन्होंने लिखा ‘मर्द की तरह’ जीना.क्या स्त्री-मुक्ति, स्त्री का पुरुष हो जाना है ? ऐसा मानने से अनेक समस्याएँ खड़ी हो जायेंगी.जिस स्वामित्व के बड़प्पन से स्त्री संघर्ष कर रही है वह स्वयं उस वर्चस्ववादी ढाँचे में कैद हो जायेगी.मर्द होना मर्दवाद के अहं से भी जुड़ा है.स्त्री आन्दोलन की सार्थकता इसी में है कि वह स्वयं को इस अहं से बचाए रख सके. इस सारे चित्रण में हैरानी की बात यह है कि शोषण के इतने चित्रों के बावजूद, इनमें दलित-स्त्री के शोषण का अलग से कोई चित्र नहीं हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार दलित महिलाएँ अमानवीय व्यवहार के कई रूप झेलती हैं. अपहरण, दैहिक-शोषण, नंगा करके घुमाना, अभद्र भाषा जैसी अनेक स्थितियाँ उनके जीवन को और भी विकट कर देती हैं.
दलित स्त्रियों के शोषण का बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अपनी सत्ता या ताकत का आभास देने के लिए सवर्ण जातियों के पुरुष इन स्त्रियों को हथियार बनाते हैं.पूरे वर्ग को दंडित करने हेतु दलित स्त्रियों का दैहिक शोषण आम बात है.इस पर घरेलू हिंसा और पारिवारिक दमन की स्थितियाँ दलित-स्त्री के लिए अस्मिता व अस्तित्व का संकट बन जाते हैं.सुशीला टाकभौरे अपने एक वैचारिक निबंध में लिखती हैं “स्त्री सर्वप्रथम स्त्री होने के कारण शोषित होती है.इसके साथ दलित स्त्री होने के कारण दोहरे रूप में शोषण-पीड़ा का संताप भोगती है.” (दलित साहित्य, स्त्री-विमर्श और दलित स्त्री, सामाजिक न्याय और दलित साहित्य सं डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन पृ. 132) आर्थिक दृष्टि से भी दलित स्त्रियों का संघर्ष कई गुना अधिक है.वे सदा से कठोर श्रम में संलग्न रहीं.यहाँ तक की मैला ढोने का अमानवीय कार्य भी उनके हिस्से रहा.दलितों में पुरुष-वर्ग जब भी पारिवारिक दायित्वों से विमुख हुआ, इन स्त्रियों ने कड़ी मेहनत से सब ज़िम्मेदारी संभाली लेकिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो पाईं.
वैचारिक स्तर पर दलित स्त्री की इस पीड़ा का अनुभव होने पर भी अपनी कविता में सुशीला टाकभौरे दोहरा संताप झेलती इस स्त्री की अलग से कोई छवि प्रस्तुत नहीं करती.अधूरे स्वावलंबन तथा सशर्त स्वतंत्रता ने दलित स्त्री को जिस वंचित स्थिति की ओर धकेला ये कविताएँ उस स्वर को उजागर नहीं करतीं.प्रतिरोध का स्वर ‘दलित स्त्रीवाद’ की अलग कोटि को प्रस्तावित या संपुष्ट नहीं करता.‘यह तुम भी जानो’ संकलन में, ‘आस्था’ शीर्षक से एक कविता है जिसमें अपने पिछड़े होने की स्थिति का स्वीकार है.‘मैं अनभिज्ञ थी / पिछड़े होने के कटु अपमान से’.इसी में कली मौसी द्वारा किसी को चप्पलों का उपहार देने और उस घटना पर समाज में हंगामा मचने का ज़िक्र भी आता है.ये छोटी-छोटी घटनाएँ संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं, आस्था को जन्म देती हैं, ऐसा कवयित्री ने स्वीकार किया है.
इसी तरह ‘मील का पत्थर’ कविता में अपनी हीनता का बोध और एक नया आत्मविश्वास एक साथ स्वर पाते हैं. अब मैं शर्मिंदा नहीं होती / क्योंकि मुझे लगने लगा है,
मैं भी मील का एक पत्थर हूँ / जो टेकरी ही नहीं.
पहाड़ों से भी / अधिक महत्त्व रखता है ! (मील का पत्थर, यह तुम भी जानो, पृ 24). इन पंक्तियों जैसे कुछ सन्दर्भ स्त्री और दलित होने की पीड़ा को एकमेक कर देते हैं लेकिन सांकेतिक रूप में ही.संभवत: इसका एक कारण तो यह है कि कविता में जीवन सन्दर्भों के लिए अवकाश कम है.कथा साहित्य के पात्र अपनी दलित पहचान तथा जीवन सन्दर्भ जोड़कर रचे जाते हैं.उनकी पीड़ा की लकीरें ज्यादा भास्वर हैं जो सुशीला जी के कथा-साहित्य में दिखता भी है.कविताओं में यह पीड़ा व्यापक स्त्री-सन्दर्भ में जज़्ब हो जाती है.
पुरुष-प्रधान समाज में / चाहे समर्पण हो
या विद्रोह, / दुर्गुण का दोष नारी पर है !
पुरुष के दुर्गुणों पर हमेशा / मनु नाम की चादर डाली जाती है. (गाली, यह तुम भी जानो, पृ 30) मनु की व्यवस्था दलित स्त्री पर क्यों कायम होनी चाहिए ? संभवत: स्त्री-पुरुष सन्दर्भ में दलित पुरुष भी उसी व्यवस्था के शिकंजे से बाहर नहीं.यही संकट दलित स्त्री के संघर्ष को तीव्रतर करता है.जिस पुरुष ने दलित जीवन का अपमान झेला है वह क्या स्वयं अपने वर्ग में लैंगिक सन्दर्भों में स्त्री-पुरुष के पदानुक्रम को निरस्त कर पाया है ? दलित स्त्रीवाद इस प्रश्न से लोहा लेता है और अधिक मानवीय समाज की संकल्पना में अस्मिताओं की टकराहट की बीच मानवीयता का वरण करता है.
अपनी कविताओं में सुशीला टाकभौरे की कविता सीधे इन सवालों से भले ही न टकराती हो, उनकी सार्थकता इस बात में है कि वे उन रचनाकारों की पंक्ति में हैं जिन्होंने इस सारे चिंतन की पृष्ठभूमि तैयार की है .दलित और स्त्री दोनों ही सुशीला टाकभौरे की कविता और चिंतन के केंद्र में हैं.समाज में दोनों की हाशियाकृत स्थिति उनकी प्रतिबद्धता को दृढ़ करते हैं.दोनों की लड़ाई अपने ‘बाहर और भीतर’ समान रूप से चल रही है.सामाजिक न्याय के लिए जितना बाहरी ताकतों से लड़ना ज़रूरी है, उतना ही अपने भीतर पड़ी सांकल को खोलना भी.कवयित्री दोनों अस्मिताओं को अलग-अलग रखते हुए, दोनों के शोषण और उद्बोधन का सटीक बिम्ब प्रस्तुत करती हैं.इस कविता में उद्बोधन का स्वर भीतरी गाँठें खोलने को सन्नद्ध है.सुशीला टाकभौरे के यहाँ, यही चेतना सक्रिय हस्तक्षेप की प्रस्तावना बनती है.अस्मिता की लड़ाई सामाजिक न्याय की उद्भावना से बंधी है.यह कविता प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष से आँख नहीं चुराती लेकिन अपना असली पारितोषक इस बात में मानती हैं कि कविता ‘स्वयंपूर्ण’ होने में मदद कर सके. सामाजिक स्थितियाँ आर्थिक अवस्था पर निर्भर है.सुशीला टाकभौरे की कविता में दलित और स्त्री की दारुण स्थितियों का बहुत बड़ा कारण आर्थिक है.भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों ने स्थिति को और विकट कर दिया.यह विकास का ऐसा मॉडल था जिसमें समाज का एक तबका पूंजी के बाज़ार में खरबपतियों की सूची में शामिल हो रहा था जबकि व्यापक जन-समाज, महंगाई की मार झेलते हुए भूख, गरीबी और लाचारी की ज़िन्दगी जीने को विवश था.दलित और स्त्रियाँ इसी वंचित जन-समाज का हिस्सा हैं.
सुशीला टाकभौरे एकाध कविता में ही सही इस स्थिति की ओर संकेत करती हैं और मानती हैं कि उदारीकरण की नीतियाँ अस्मिता के संकट को अस्तित्व के संकट में बदल रही हैं.
उदारीकरण / निजीकरण
भूमंडलीकरण के दौर में / श्रम का अवमूल्यन
शिक्षा बहुमूल्य / रोज़गार में स्पर्धा
पहचान मिटने का खतरा
(महंगाई, स्वाति बूँद और खारे मोती, पृ.75-76) सुशीला टाकभौरे के यहाँ इन मुद्दों को उठाने वाली बहुत-सी कविताएँ नहीं हैं लेकिन जो हैं वे इस दृष्टि से आश्वस्त करती हैं कि कवयित्री की साझेदारी परिस्थितियों से हारते मनुष्य की पीड़ा से है.सामाजिक जीवन व सामाजिक विडंबना के और भी पक्ष हो सकते हैं लेकिन उतने विस्तार या विविधता में जाने का अवकाश कवयित्री के पास नहीं है.उनका सारा ध्यान असमानता की पीड़ा झेलते व्यक्ति पर है, फिर वह विषमता चाहें जाति की हो, लिंग की या अर्थ की, उनका चित्रण एवं उनके प्रतिकार की राजनीति, अपने प्रेरक सक्रिय रूप में यहाँ मौजूद है. इन कविताओं की असली ताक़त अभिव्यक्ति की साफ़गोई में छिपी है.सुशीला टाकभौरे जिस भावातिरेक के साथ अपनी बात रखती हैं उसमें एक सच्चाई झलकती है.यह सच्चाई दलित साहित्य की सार्थकता का सबसे बड़ा प्रतिमान है.अस्मितामूलक विमर्श से उसकी शुरुआत अवश्य होती है किन्तु सार्थकता उन मानवाधिकारों को प्राप्त करने में है जो मानवीय जीवन के लिए आधारभूत हैं.यह कवितायें उस आन्दोलन को दिशा देने का काम करती हैं जो व्यापक जन-समुदाय के स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए आगे बढ़ता है.आज देश के अलग-अलग हिस्सों से समता की मांग करने वाले आन्दोलनों के तीव्र होने की सूचनाएँ आ रही हैं, सुशीला टाकभौरे की कविताओं का मूल्य यही है कि इनके माध्यम से उस सामाजिक विमर्श की बुनियाद रखी गई जो अब परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है |