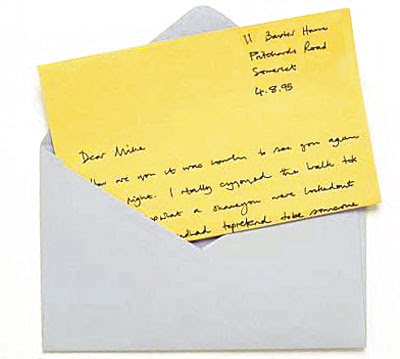प्रिय नन्ना
इन दिनों आपकी बहुत याद आ रही है. पिछले कई दिनों से मन बेचैन है, लगता है आपसे खूब बात करूँ, आपको छू सकूं , पास बैठकर कांपते झुर्रीदार हाथों को पकड़ कर, चीनी मिट्टी के सफेद प्लेट में थोड़ी-थोड़ी चाय डाल कर पिला सकू, आपके नहाने से पहले और बाद भी पीठ में तेल लगा सकूँ और…. ढेरों इच्छाएँ… अनगिनत चाहतें?यह सब अभी संभव होता नहीं लग रहा. हमारे बीच रेलसफर के दस-ग्यारह घंटों की बिसात बिछी है जिसे पार किए बिना इच्छाओं का कोई भी को ना छू पाना कैसे मुमकिन होगा? बस इसलिए यह भूला-बिसरा तरीका खोज बैठी चिट्ठी लिख रही हूँ.
चिट्ठी लिखते हुए याद आता कि आठवीं कक्षा पास कर नवमीं पढऩे जब मैं माँ-पापा के पास जा रही थी. लगभग बारह साल बाद आपसे दूर जाना बेहद कठिन था. बहुत कठोर सी मानी जाने वाली लड़की रो रही थी, खूब रो रही थी. आपने बस में बैठ जाने के बाद कहा था- चिट्ठी लिखना, अभी तुम ग्रेजुएट नहीं हुई हो.सुनकर पापा मुस्कुराए थे. उन्हें पता था यह तंज किया गया है और उन्हीं के लिए किया गया है. और मैं हर पंद्रह-बीस दिनों में चिट्ठी लिखने लगी. कोशिश करती कि अंतर्देशीय-पत्र के तीनों पन्ने भर लिखूँ… लेकिन तब मेरी चिट्ठियाँ आगे बढ़ती ही न थीं! बस पैट्रन राइटिंग पर…. हम सब यहाँ बहुत खुश हैं. आपकी कुशलता की कामना…. मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है….. फिर छोटी बहनों, भाई की पढ़ाई….. फिर हम सब नानी को , आपको याद करते हैं…. कभी-कभी मौसम की बातें भी होती हैं…. चिट्ठी का जवाब देने का अनुरोध और बस विराम.
उन दिनों मेरे पास लिखने लायक बातें ही नहीं थी या निश्चित न था कि कौन सी बात किससे कही जाय. ठीक आज इसके उलट है. मेरे दिल के हरेक कोने में ठूँस-ठूँसकर शब्द भरे हैं. चरखा, चक्की , कैंची, सिलाई मशीन और कलम सब कुछ बारी-बारी चल रहा है भीतर. स्मृतियों का पूरा का पूरा थान लपेट रखा है मैंने.
जिक्र चिट्ठियों का आया तो आपकी ही एक बात याद आई. ससुराल जाती बेटियों को नसीहत की तरह एक पंक्ति पकड़ा दी थी- मुझे कभी भी चिट्ठी मत लिखना. उन्होंने अच्छी बेटियों की तरह पालन किया. आखिर बेटियाँ किसकी थीं? आपकी तरह ही थीं. आपने भी तो अपने पिता को तीन वचन दिये थे… एक – ताउम्र पेड़ पर नहीं चढऩे का , दूसरा- साइकिल नहीं चलाने का और तीसरा कि नदी-तालाब में तैरेंगे भी नहीं. आज मैं आपको यह चिट्ठी लिखते हुए सोच रही हूँ कि यदि मेरी माँ और दोनों मौसियाँ चिट्ठी लिखती तो क्या-क्या लिखतीं…. कितने पन्ने भर लिखतीं…. क्या कभी खत्म होती उनकी चिट्ठियाँ …?
मेरी माँ ने कभी चिट्ठी नहीं लिखी. पिता को नहीं, पति को भी नहीं और किसी प्रेमी को भी नहीं. मुझे भी नहीं.
माँ और उनकी बहनों का चिट्ठियाँ न लिखने का वचन पिता के साथ-साथ पूरी कायनात के लिए था. कभी-कभी मुझे लगता है वह ‘वचन’ न था क्योंकि वचनों में प्रतिपक्ष की सहमति भी होती है. यहाँ प्रतिपक्ष की प्रतिध्वनि कहाँ सुनी गई थी. यदि सुनी जाती तो वे शायद कहतीं- बाबूजी हम आपको चिट्ठी लिखे बिना कैसे रह सक ती हैं, आखिर हम अपने सुख-दुख और किससे कहेंगी, दुख विपत्ति के बखत आखिर किसे पुकारेंगी?…. लेकिन नहीं…. यह बारीक प्रतिध्वनि गूँजी होगी जरूर, पर सुनता कौन? यहाँ वचनों जैसा विश्वास न था… अपनी जबरदस्ती की हुंकार थी. धमकी-सी थी… जिसने ताउम्र उन बेचारियों को स्वप्न में भी डराये रखा.
अब बातों को थोड़ा दूसरी ओर मोड़ देते हैं. 1993 का साल, आप रिटायर हुए. मैंने उसी साल दसवीं की परीक्षा दी थी. 30 मार्च को आपके रिटायर होने के दिन आपके पास ही थी. यहाँ से आपके स्वभाव का , विचारों का दूसरा अध्याय भी शुरू हुआ. अब हम नातिनें, खासकर मैं (सबसे बड़ी होने की वजह से शायद) धीरे-धीरे खुद को व्यक्त क रने का अवसर पाने लगी. अब शारीरिक और मानसिक दूरियाँ सिकुडऩे लगी थीं. अब आप साइकिल पर, पापा की स्कूटर-मोटर साइकिल पर बैठने लगे थे. एक वचन का टूटना बहुत चीजों को नरम क र रहा था. धीरे-धीरे स्वभाव की हुंकार भी टूट रही थी. वे रिश्तों की , बहुएँ, कभी जिनकी आवाज़ सुनना तक असामाजिक मानदंड थे आपके लिए, आज 70 पहुँचते-पहुँचते उन्हें पास बुलाकर हालचाल पूछते, उनके सुख-दुख सुनते और सलाहें भी देते. बहुत सी अकड़ी हुई चीजें टूट रही थीं, बेआवाज़. जैसे तनी हुई रस्सी धीरे-धीरे मुलायम होती जाए और एक दिन रेशम की मानिंद स्निग्ध हो जाए, वैसे ही तो मुलामियत आ गई थी आप में. दिनों-दिन नरम और सहज होते जा रहे थे और कीमती भी. इसीलिए शायद सबसे छुपाया, बचाया आपसे कह सक ने की हिम्मत हो रही है. आज दिल पर हाथ रखकर सौ फीसदी सच कह सकती हूँ कि आप वह पुरुष हो जिसकी वजह से कैसी भी परिस्थिति हो, मैं नहीं कह पाऊँगी कि ‘दुनिया के सारे मर्द एक से होते हैं’ मैं सारे मर्दों से घृणा करने की बात भी नहीं कह सक ती. मुझे हरेक में कुछ खूबियाँ दिखती हैं, बेहद उजड्ड और लंपट किस्म का सहकर्मी भी सहानुभूतिपूर्ण दिखता है मुझे. मैं अपनी उस दोस्त को -जो पुरुषों से घृणा करती है, उसकी सोच को बदलने की कोशिश करती रहती हूँ. उसे स्त्री-पुरुष के स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं की , सामाजिक मानसिकता में दुरूह से पगी परवरिश के अंतरों का हवाला दे-देकर समझाने की कोशिश करती हूँ. वह सचमुच बदल भी रही है….. ये सारी बातें आपके साथ साझा करने की इच्छा आज चरम पर है. चिट्ठी के पन्ने भरते ही जा रहे हैं.
यह सब कहते-सुनते घड़ी एक बजानेवाली है. समय कहाँ रुकता है कभी. मैं स्मृतियों का लपेट रखा थान धीरे से खोलना शुरू करती हूँ तो समय पीछे की ओर तेज गति से गोल-गोल घूमने लगता है. वह थोड़ा सा रुक ता है तो कुछ न कुछ पकड़ ही लेती हूँ. अभी एक चिट्ठी पकड़ में आ गई है. वह छोटी बहन की चिट्ठी है. एक दिन सोते समय तकिया के नीचे एक चिट्ठी निकलती है. यह जानकर कि चिट्ठी बहन की है, एक अनजानी आशंका जाग उठी. क्यों, किसलिए चिट्ठी लिखी….? और एक दम से उगीं आशंकाएँ सच होती हैं. उस चिट्ठी के एक -एक हरफ तो अब मुझे याद नहीं. तब भी सबकुछ कहाँ पढ़ पाई थी? बस कुछ ही पंक्तियाँ ही… कुहरे की तरह दिमाग में छा गई थीं. हरफ याद रखने की जरूरत भी नहीं थी. और क्या किया?… कुछ नहीं. उस कोहरे को फूँक कर हटाने की जरा सी भी कोशिश न की . बस चारों ओर बिखरे रिश्तों के ताने-बाने को सहेजे रखने की खातिर किसी से कुछ भी नहीं कहा अब तक … तो आज आपसे भी क्यूँ कहूँगी? याद है तो बस उस चिट्ठी के आशय, नतीजे. हमारे आसपास के झूठे, दोगले रिश्ते. वह घर, वह परिवार जिसे हम सुरक्षा घेरा मानते हैं, उसके दिखाये तर्कों- कुतर्को को बेप्रश्न कबूल करते हैं, यह सोचकर कि वे हमारे अपने हैं, जो कुछ भी कहते-सुनते हैं हमारे अच्छे आज और कल के लिए? उन्हीं के बीच कोई मुखौटा लगाए हम पर घात लगाने बैठा होता है. आज समझ में आ रहा है कि लड़कियों को तर्क क्यों नहीं करने दिया जाता? ऐसे अनुभव विरले नहीं हैं, हर औरतजात के पास होते हैं. चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, चचेरे-ममेरे भाई, किसी न किसी की लोलुपता की शिकार वे होती हैं पर अपनी छोटी बहनों-बेटियों को वे आगाह नहीं करतीं. हालांकि यह भी उतना ही खरा सच है कि स्त्री का रणक्षेत्र उसका अपना अकेले का होता है. यहाँ कोई भी उसके साथ नहीं होता. बाहर की एक उंगली उठते ही आसपास की वो लकीरें जिन्हें पिता, भाई, पति यहाँ बेटा सब… जो अब तक उसकी रक्षा का दम भरते रहे… उन उठनेवाली उंगलियों में शामिल हो जाते हैं. आज भी यह प्रश्न कतई महत्वपूर्ण नहीं होता कि अपराधी कौन है? केवल लड़कियों के मामले में. यहाँ अपराध कोई भी करे, अपराधी केवल और केवल वे ही होती है और सजा भी उन्हें ही मिलती है.
मुझे इस सत्य का आभास था तभी तो मैंने उस युवा होती लड़की के प्रश्नों, जिज्ञासाओं, आकुलताओं का जवाब चिट्ठी में ही दिया. यहाँ मैं यथार्थवादी बन गई थी, आपकी तरह और बहुत कुछ माँ की तरह. उसे समझाया, चुप करवा दिया था और उस समय तो उस रिश्ते को बचा ले गई. आज भी प्रयासरत हूँ. उस अल्हड़ लड़की ने भी, जो कुछ भी बकती-बोलती रहती थी, आज भी मेरा साथ दे रही है. हमारे आसपास के सभी रिश्ते ऐसे ही खोखले हैं, ऐसे ही बचते हैं वे. एक प्रश्न जब तब बेचैन करता रहता है कि हम आखिर क्यूँ बचाकर रखते हैं इन्हें?
नन्ना पर उस एक रिश्ते के कटघरे में खड़े होने से आप भी खुश नहीं रह पाते? इसीलिए अन्याय का साथ देने का अपराध मैं ताउम्र करूँगी? मैं नहीं चाहती कि इस घटना के अक्स आपकी समझ में आएं. इसे मैंने माँ से भी छुपाया हुआ है… अभी तक . जब कभी संवेदना या आक्रोश की अति होने लगती है और हिम्मत बेकाबू होती है कि कह दूँ… किसी से तो? तभी चुनौती देती हुई वह पंक्ति कानों में शीशे की तरह तीव्रगति से प्रवेश करती है- ‘औरत के पेट में कोई बात नहीं पचती’ और मैं दोनों हाथ से पेट को दबोच, पैरों को तानकर खड़ी हो जाती हूँ… देखो- मैंने आपसे भी कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया.
हाँ एक ख्याल जरूर आता है कि ऐसे अनुभव तो मेरे पास भी थे यदि मैंने माँ को चिट्ठी लिखकर साझा किया होता तो वे क्या करतीं? कैसा जवाब देतीं…? यदि वे आपके वचनों में बंधी न होतीं तो जरूर उनके पास भी मुझे बताने को कोई न कोई अनुभव तो जरूर ही होता. हर औरत की एक मात्र पूँजी है शायद ऐसे अनुभव, जो उसे सपनों में भी पुरुष नामक प्राणी से डराते हैं और हद तो यह कि इन्हीं में से कोई एक को वह आजीवन सहन क रती है. हाँ इतना तो जरूर तय है कि अगर मैंने माँ को चिट्ठी लिखी होती तो उनका तीखा-कडुवा अनुभव संसार भी आज मेरे पास होता. ऐसा ही कोई मासूम सा दिखनेवाला सगा-पराया रिश्तेदार, जिस पर आपको भी भरोसा रहा हो. लेकिन आपकी बेटियों ने तो चिट्ठी न लिखने की कसम खाई थी. इसी वज़ह से मैंने अपना भोगा उनसे साझा किया ही नहीं. मैंने खुद को खुद ही समझा लिया था. अपना रास्ता चुन लिया था. और उस छोटी उमर में एक बड़े कडुवे सच को लगभग सहन करने की क्षमता ओढ़ ली थी कि इस परिवार रूपी भग्नावेषों की संरचनाएँ खोखली जरूर लेकिन सर्पीली भुजाओंवाली हैं. अपने आडंबरों में वे किसी को भी लपेट लेंगी. औरतें यहाँ शापग्रस्त आत्माओं की तरह भटकती काया मात्र हैं. यहाँ उनके मन की रत्तीमात्र परवाह नहीं होती. आपने भी नहीं की थी वरना अपनी बेटियों से उनकी रचनात्मकता और सच कह सकने का अधिकार नहीं छीनते.
मैंने न तो अपने पिता को कोई ऐसा वचन दिया न ही उन्होंने कभी मुझे ऐसे मुखर-अमुखर वचनों में बांधने की चेष्टा की . मेरे लिखे पर तो आपको भी प्रसन्नता होती है. अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी कविताएँ सुनते हुए आपने कहा भी था- ‘मुझे तुम पर गर्व है’ ओह पहली या शायद दूसरी बार सुने शब्द थे ये. पर औचक नहीं, पूरे सोच-विचार के बाद ही निकले होंगे कुछ शब्द… मेरे जीवन भर की पूँजी. पापा भी मेरा लिखा, छपा देखकर मन ही मन खुश होते हैं. चाहते हैं कि मैं कविताएँ लिखूँ, किताबें लिखूँ. यह तो परदे के बाहर का चित्र है और परदे के भीतर वही नानी, दादी हैं जिन्हें पितृसत्ता ने पढऩे का ही मौका न दिया. अपराध कि वे लड़कियाँ थी, उन्हें चौका -चूल्हा ही तो संभालना था… सो किसलिए पढ़ाना? नानी तो बेहद सरल स्वभाव की महिला हैं, उन्होंने कभी असंतोष, कोई माँग जताई ही नहीं, लेकिन दादी एक आत्मस्वाभिमानी व्यक्तित्व की , तेज-तर्राट महिला… उनकी बातों में ऐसे असंतोष झलक ते हैं. केवल पढ़े-लिखे न हो पाने की वज़ह से जब कभी किसी को साथ ले जाने की बाध्यता सामने आती तो उनका असंतोष मुखर हो जाता है. माँ की पीढ़ी पढ़ी-लिखी होकर भी पिता के विचारों की शिकार. दोनों मौसियों का अखबारों और किताबों की दुनिया से भी नाता लगभग शून्य है. माँ किताब, अखबार, पत्रिका एँ जो मिलता है सब पढ़ लेती हैं. को ई चुनाव नहीं. खूब उपन्यास भी पढ़े उन्होंने. एक समय उन्होंने, मनोज पॉकेट बुक्स वाले और भी जाने क्या-क्या प्रकाशनों वाले. मैंने भी पढ़े हैं उनमें से कुछ… अब याद नहीं आ रहे. न जाने क्यों यहाँ आप बार-बार कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं. किताबों के अच्छे जानकार, कलाकार स्वयं, साहित्य-संस्कृति से गहरे वाकिफ होते हुए भी आपने उन्हें पढऩे का सलीका नहीं दिया. अपने सारे हुनर अपने पास रखकर खत्म कर दिये. बेटा न होने से वसीयत तो बेटियों को मिली और कुछ वंशानुगत मनोवृत्तियाँ भी, लेकिन वह संचित किया हुआ जिसे ‘ज्ञान’ या ‘कला’ कहते हैं, उसे देने लायक आपने अपनी बेटियों को नहीं समझा. हालाँकि इसके पीछे भी आपका एक तर्कशास्त्र था कि- व्यक्ति अपनी-अपनी रुचि, मनोवृत्ति का खुद अर्जित करता है. मुझे भी आपने कहाँ- कुछ सिखाया? जबकि ढाई साल की उम्र से आपके पास रहती थी.
लेकिन मुझे लगता है और जैसा कि आप कहते रहे कि रुचियों के अनुसार, मनोवृत्तियों के अनुसार… तो मैंने आपकी परछाई का थोड़ा सा हिस्सा खुद पर ओढ़ लिया. रुचियाँ तो ओढ़ी-ढांकी ही, मनोवृत्तियों की चादर भी तान ली, कितना? अभी निश्चित नहीं कह सकती, समय के द्वार-दालान थोड़े और पार करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
आज, अब जब आपको चिट्ठी लिखने बैठी हूँ तो सोचा तो यही था कि सबकुछ लिखूँगी, जो सामने नहीं कह पाती पर अब आगे समझ में ही नहीं आ रहा कि और क्या लिखूँ? एक प्रश्न बार-बार कौंधता है कि माँ-मौसियों ने जिस तरह आपको कभी चिट्ठी नहीं लिखी, इसी तरह वचनों के बिना भी मैंने पापा को कभी चिट्ठी नहीं लिखी! क्यों नहीं लिखी मैंने चिट्ठियाँ? हम भारतीय और खासकर ग्रामीण, कस्बाई लड़कियाँ, पिता से इतनी दूर कैसे हो जाती हैं? जैसे-जैसे हम बड़ी होती हैं, हमारी दूरियाँ बढ़ती जाती हैं… हमारे कपड़ों की तरह, बालों की तरह. लगभग बारह-तेरह साल के बाद, बड़ी होने के बाद मैं पापा के गले नहीं लगी? क भी-क भार ही उनके बगल में, सटकर बैठती हूँ. अभी पिछले महीने जब माँ-पापा मेरे पास आए थे, तब का किस्सा आपको सुनाती हूँ- एक दिन मैं बेहद थकी हुई थी, बुखार- सा भी लग रहा था. मैं पापा के बगल के सोफे पर बैठी थी, थका न और संवेदनाओं के किसी बबंडर से आहत हो उनके बगल से, सोफे के हत्थों पर सिर औंधाकर बैठी-बैठी ही लगभग लेट गई. उस समय बेहद जरूरत लग रही थी कि पापा मेरे सिर पर हाथ रख दें. पीठ पर भी हाथ फेर दें. उन्होंने ऐसा नहीं किया. अलबत्ता मुझे बार-बार कहा जरूर कि भीतर जाकर बिस्तर पर सो जाऊँ, दवा ले लूँ, डॉक्टर को दिखा आऊँ. उन्हें चिंता थी मेरी, लेकिन उनका हाथ मेरे सिर तक क्यों नहीं पहुँचा? आप जरूर ही इसे संस्कार कहोगे… भारतीय संस्कृति जैसा महान- मायावी कुछ! मैं इसे नैतिकता के डर कहूँगी, जबरन सिखाये गए सामाजिक भय-संकोच! आपने खुद इनका खूब पालन किया है मगर सुखद है कि अब आप बदल गए. आप तो परिवर्तित हो गए, जैसे बर्फ की शिला पानी बनकर बहने लगे, लेकिन हर कोई नहीं बदल पाता.
आप बदल सके इसीलिए अब आपसे दुराव-छिपाव नहीं रहा.
चिट्ठी जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे नजरें पीछे घूमती हैं. वह लोक गीत आपको याद होगा जिसमें विदा होती बेटी, कहार से नीम के नीचे डोली रोकने का आग्रह करती है-
निमिया के नीचे डोला रोक देक हरवा
देखि लेऊँ गाँव की ओर…..
बाबुल दिहै मोर नौ मन सोनवा
मैया लहंगा-पटोर…
नौ मन सोनवा, नौ दिन चलिहै
फटि जइहै लहंगा-पटोर…..
जाते हुए सब कुछ आँख भर देख लेने की इच्छा, कि घर-दुआर, पुर-परिजन सभी आँखों में बस जायें. चिट्ठी लिखते हुए मेरा मन भी जहाँ-तहाँ रुक -रुक जाता है, कुछ जीवंत सा तलाशने लगता है. मेरी अपनी जड़ें, अपनी पहचान टटोलने लगती हूँ. और जब किसी नीम के नीचे सुस्ताने ठहरती हूँ तो आप मेरे बगल में बैठे कोई गीत छेड़ देते हो-
नदिया के तीरे तीरे चर बोक्की (बकरी)
नदिया सुखा जाय त मर बोक्की …..
बचपन से इस गीत को सुनती आ रही हूँ… कुछ भी समझ में नहीं आता था… बस नदिया के किनारे हरी-हरी, को मल घास चरती बक री और वही पतली सी धारवाली अपनी गाँव की बलुई नदी का चित्र उभरता था. कभी-कभी तो डर भी लगता कि रात में जंगल से निकलकर कोई बाघ उस अकेली भोली-भाली बकरी को मारकर खान खा जाय. आज भी इस लोक गीत का अर्थ पूरा का पूरा नहीं खुल पाया. आज भी बकरी का अकेलापन याद आते ही डर लगने लगता है. ऐसा महसूस होने लगता है कि जंगल में दूर कहीं से बाघ-भेडिय़ों के गरजने-गुर्राने की आवाज़ें आ रही हैं. सभी उसकी ओर लपक ती जीभें लिए खड़े हैं. ओफ्हो… हद! इस गीत की मात्र दो पंक्तियाँ मुझ पर इस हद तक हावी हो जाती हैं कि मैं बकरी के अक्स में खुद को देखने लगती हूँ… आईने में देखती हूँ कि मेरे गले में एक तख्ती लटकी है और उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है- ‘नदिया के तीरे तीरे चर बोक्की … नदिया सुखा जायत मर बोक्की …’