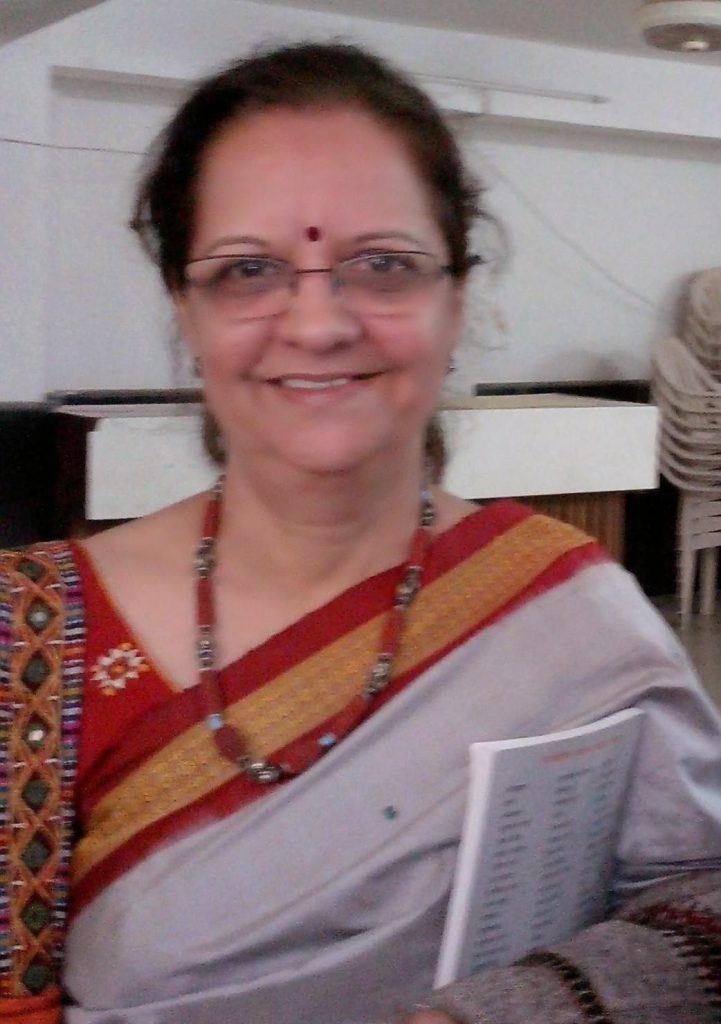
सुधा अरोडा सुप्रसिद्ध कथाकार और विचारक हैं. सम्पर्क : 1702 , सॉलिटेअर , डेल्फी के सामने , हीरानंदानी गार्डेन्स , पवई , मुंबई – 400 076
फोन – 022 4005 7872 / 097574 94505 / 090043 87272.
सिनेमा की पहुंच समाज के बहुत बड़े वर्ग तक है इसीलिये मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक दायित्व निभाने का सवाल भी यहां जुड़ जाता है.जब कोई फिल्म रोचक अंदाज़ में सामाजिक विसंगतियों के चित्र और कुछ सकारात्मक संदेश सही सही संप्रेषित करने में समर्थ होती है तो उसे व्यापक स्तर पर सराहना भी मिलती है.
हिन्दी सिनेमा में नायिका एक ऐसा मिथक है जिसकी अनुपस्थिति में कोई फिल्म बन ही नहीं सकती लेकिन अब तक जिसकी उपस्थिति नायक समेत पेड़ों और फव्वारों के चारों ओर चक्कर लगाने के लिये ही होती रही है.नायक की नायिका और कहानी का मूलाधार होने के बावजूद सिनेमा की नायिका को बार-बार कंडीशंड किया जाता रहा.स्वयं नायिका ही इस मिथक को बार-बार तोड़ती रही.अगर कभी कहानी ने उसे घेरे में जकड़ने की कोशिश की तो उसने एक विद्रोह भी रचा.यह अलग बात है कि बॉक्स ऑफिस के भूत के डर से फिल्मकारों ने स्त्री को परम्पराओं से बाहर निकलने ही नहीं दिया क्योंकि दर्शक वैसी ही सहनशीला नारी की छवि देखना और उस पर सहानुभूति जताना चाहता है जो उसके मानदंडों पर सही ठहरती हो.दर्शक सब कुछ पचा सकता है – एक अकेला नायक सौ-पचास गुंडों को धराशायी कर दे, कोठे पर लगातार बुरी नज़रों की शिकार ‘पवित्र तवायफ’ बड़े बड़े डायलॉग मारे, सबकुछ धड़ल्ले से चल जाएगा .हिंदी फिल्मों की नायिकाओं ने एक लंबे अरसे तक अपनी महिमामंडित छवि को पुष्ट करने के लिये त्याग, ममता और आंसुओं से सराबोर अपनी तस्वीर दिखाई और बाॅक्स आॅफिस पर खूब वाहवाही बटोरी.
भारतीय सिनेमा लंबे समय तक पुरुष वर्चस्व का सिनेमा रहा है.निर्माता से दर्शक तक यहां पुरुष की केन्द्रीयता रही है और ऐसे में जाहिर है पुरुष को एक सहचरी ही चाहिए, स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं .नायिका पति को आगे बढ़ने का मौका देती हुई नौकरी और अपना फलता फूलता कैरियर होम कर देती है .अभिमान वाली जया भादुड़ी इसकी मेटाफर है.‘अल्लाह तेरो नाम’ और ‘ना मैं धन चाहूं , ना रतन चाहूं’ की बीते समय की नायिकाएं हों या ‘दिलवाले दुलहनियाँ’ की और ‘कुछ कुछ होता है’ की लंदन रिटर्न, गाती वह ‘ओम जय जगदीश हरे’ ही है.यही उसकी भारतीयता है! भारत का दर्शक ऐसी ही पराश्रित नायिकाओं का मुरीद रहा है.
शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि नायिकाएं हीरो को बचाने के लिए खलनायक के सामने नाच-गाना, समर्पण और कभी-कभी धोखा देकर नायक को छुड़ा लेने तक के लटके झटके बरसों से सिनेमा में करती रही है और दर्शकों का जी नहीं ऊब रहा क्योंकि उसे ऐसी ही स्त्रियाँ रुचती हैं .उसे परंपरा में लिथड़ी नायिकाएँ पसंद हैं.परंपरा का नाम सिंदूर, करवाचैथ और मंगलसूत्र ही होता है क्योंकि इन्हीं में पुरुष होता है और ये ही वे बंधन हैं, जिसे स्त्री तोड़ना नहीं चाहती .ये ही वे हथियार हैं जिससे वह अपनी इच्छाओं का गला घोंट लेती है .चाहे महल में वह भूखी सो जाय, चाहे पति के लात-घूंसों को खाकर ही अपने को बचाए रखे लेकिन वह मर नहीं पाती क्योंकि उसके पास अपने नाम से न कोई घर होता है , न संपत्ति .लिहाजा वह खलनायक या जालिमों के हाथ से बचाई जाती है, नायक उसका संरक्षक हो जाता है और वह उसके पाँवों पर गिर जाती है.साहब बीवी और गुलाम की छोटी बहू को देखिये – शराबी पति के लिये शराब तक पीने को तैयार हो जाती है और उसके पैरों पर गिरकर गाती है – न जाओ सैंया , छुड़ा के बैयां , कसम तुम्हारी , मैं रो पड़ूंगी ! फिर भी वो जमींदार पति ही क्या जो पसीज जाये ! वह सिंदूर भरी मांग से लिथड़ी रोती-कलपती , मिन्नतें करती , सुरीले सुर में गाती सुंदरी नायिका को छोड़कर, तवायफ़ के कोठे पर चला ही जाता है .नायिकाएं तब भी ‘तुम्हीं मेरे मंदिर, तुम्हीं मेरी पूजा, तुम्हीं देवता हो’ गा गाकर, गले में मंगलसूत्र भरपूर दिखातीं रहीं .मूक फिल्मों से शुरु होकर अछूत कन्या और मदर इंडिया से गुज़रते हुए सुजाता, बंदिनी, दिल एक मंदिर, मैं चुप रहूंगी तक सिंदूर से मांग भरी नायिकाएं दशकों तक बड़े परदे पर सबकी आराध्य बनी रहीं.
पुरातनपंथी मध्यवर्गीय परिवार के दमघोटू माहौल में ताने बाने से छलनी अपने नसीब को कोसती और विधि के विधान को स्वीकारती ‘‘मैं चुप रहूंगी’’ वाली फिल्मों का दौर भी हमने देखा है जब ऐसे संयुक्त परिवार में जाकर अपनी सहनशीलता के सुपर पावर की बदौलत झुकी आँखों वाली बहू दर्शकों की चहेती होती थी! घर के सबसे क्रूर सदस्य को अपनी जान की बाज़ी लगा कर बचा लेती नायिका के कंधे पर फिल्म की ‘‘हैप्पी एंडिंग’’ का दारोमदार था ! वह खुद ही गले में रस्सी बाँध कर उसके सिरे को खुला छोड़ देती थी फिर संयुक्त परिवार में जिसका जी चाहे, उसे हाँक लेता था ! ऐसी फिल्मों की एक लंबी कतार है जिनमें स्त्री का ममतामयी मां, पत्नी, बहन और बेटी का उजला धुला रूप दशकों तक दर्शकों को लुभाता रहा.
पांच दषक पहले गीत भी ऐसे ही रचे गये –
‘‘ तुम्हीं मेरे मंदिर, तुम्हीं मेरी पूजा, तुम ही देवता हो !
कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो! (फिल्म – खानदान में नूतन और सुनील दत्त)
‘‘ कैसा मुझे वरदान मिला है, तुम क्या मिले भगवान मिला है! अब तो जनम भर संग रहेगा, इस मेंहदी का रंग रहेगा तेरे चरण की मैं दासी रे दासी ….जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी !’’
सौ साल के हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि निरंतर बदल रही है.दर्शक और महिलाएं बरसों तक फिल्में देखने के बाद अपने आंसुओं से भरे रुमालों को निचोड़ने में ही फिल्म की सफलता को आंकते रहे.मेंहदी, सिंदूर, टिकुली और मंगलसूत्र में सजी दासी बनी इस नायिका ने प्रेम भी किया और घर से विद्रोह भी ! पर करवाचैथ का सारा ताम-झाम , जेवर और जरीदार साड़ियों से लंदी फंदी नायिकाओं ,भव्य रंगीन दृष्यों और गीतों की संभाव्यता के कारण , बागी आधुनिक नायिका को भी, सिनेमा अपने पारंपरिक और समर्पित खांचे में दिखाता रहा.‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगें’ से लेकर ‘हम दिल दे चुके सनम’ में करवाचैथ के सुहावने मंजर देखे जाते रहे .भारतीय सिनेमा के इतिहास पर समग्रता में एक नज़र अगर डाली जाय तो हम ऐसी नायिकाओं को भी पाएंगे जो इस मिथक को तोड़ भी रही हैं और अपनी स्थितियों में मुक्ति का एक आख्यान भी बनती रही हैं.बेशक सिनेमा का मनोरंजनशास्त्र जनमानस में पैठी हुई प्रवृत्तियों के संदोहन पर टिका हो.सबसे पहले हंटरवाली नाडिया को हम एक ऐसी स्त्री के रूप में सिनेमा के पर्दे पर पाते हैं जो अब तक पुरुष के लिए आरक्षित और स्त्री के लिए वर्जित क्षेत्र में दखल देती है .जो हंटर अभी तक स्त्री की पीठ पर बजते थे नाडिया ने उससे पुरुष की पीठ रंग डाली .वह कल्पना के नहीं बल्कि वास्तविक घोडे दौड़ाती थी और जिस दौर में पूरब से पश्चिम , उत्तर से दक्षिण तक की भारतीय स्त्रियाँ घूँघट और ओढ़नी-चुनरी में लिपटी थीं , निडर नाडिया ने ‘फीअरलेस’ बनकर सिर खोलकर लोगों को चुनौती दी और उन मूल्यों को बचाया जो आमतौर पर पुरुषों की बपौती माने जाते थे .पर यह एक औसत नहीं , अपवाद स्वरूप चरित्र था जो बाॅक्स आॅफिस की संभावनाओं को देखते हुए रचा गया .
इसके बाद आता है नरगिस का दौर .भारतीय सिनेमा की इस नायिका ने अपनी लंबी पारी में मध्यवर्गीय स्त्री के सपनों और आकांक्षाओं के साथ-साथ उसकी चारित्रिक दृढता को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया .कम खाकर ईमानदारी से जीना और अपनी एक सामाजिक भूमिका तलाशना इस नायिका का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है .नरगिस का केवल एक दौर नहीं था बल्कि उसका एक व्यापक उत्तर काल भी है जब दामिनी , लज्जा , मृत्युदंड , प्रतिघात , ज़ख्मी औरत , अंजाम , खून भरी मांग , अस्तित्व की नायिकाओं ने दयनीय और सहने वाली इमेज को धराशायी कर अपनी सारी वल्नरेबिलिटी सहित पुरुष सशक्त को चुनौती दी और समाज के सामने कुछ सवाल रखे .पांच दशक पहले तक नायिकांए मीनाकुमारी और नरगिस जैसी सलज्ज थीं जो भारतीय पोशाक साड़ी में लैस होती थीं और सारी रूमानियत अपनी आंखों से ज़ाहिर कर देती थीं .अपनी देह, ज़ीरो फ़िगर और यौनिकता के प्रति सचेत नायिकाएं तब स्वीकार्य नहीं थीं.इसके लिए तो हेलेन, बिन्दु या अरुणा ईरानी ही काफी थीं और वे फिल्म की नायिका कभी नहीं रहीं.आज नायिका और खलनायिका के बीच सिर्फ कपड़ों का ही नहीं, मानसिकता का भी अंतर मिट गया है.आज कम कपड़ों में आइटम साॅन्ग करने के लिये हेलेन और बिंदु की तरह सिर्फ़ राखी सावंत या मलाइका खान की भी ज़रूरत नहीं रही .उसके लिये करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ़ या विद्या बालन तक, जो अपनी शर्तों पर किसी भी रोल को अस्वीकार करने की कूवत रखती हैं, चालू किस्म के आइटम साॅन्ग – ‘चिपका ले सैंया फेविकाॅल से’ और ‘कारे कजरारे’ से लेकर ‘शीला की जवानी’ ‘चिकनी चमेली’ और ‘मला जाउ दे’ की उत्तेजक लावणी तक के लिये अपने को सहर्श प्रस्तुत कर देती हैं.
ग्रामीण नायिकाएँ खासतौर पर उन समस्याओं से जुडी रहीं जो आमतौर पर ग्रामीण नायकों से सम्बद्ध थीं , मसलन कृषि की समस्याएँ, शोषण और घरेलू कलह आदि लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ग्रामीण नायिकाएँ एक खुले माहौल में सांस लेती प्रतीत होती हैं .वे शहरी नायिकाओं की तरह कठपुतली नहीं बल्कि सहनायक की तरह मौजूद होती हैं .आर्देशिर ईरानी की ‘किसान कन्या’ से महबूब खान की ‘औरत’ और ‘मदर इंडिया’ और जे. पी. दत्ता की गुलामी में रीना रॉय को भी इसे बेहतर ढंग से देखा जा सकता है.‘मदर इंडिया’ तो स्त्री अस्मिता का एक माइलस्टोन ही है जहां एक मां, दूसरी स्त्री का सम्मान बचाने के लिए अपने सगे को भी नहीं बख्शती और अपने बेटे को बंदूक का निशाना बना लेती है .विभाजन के तौर पर हम ग्रामीण नायिकाओं को श्रम-संस्कृति और शहरी नायिकाओं को मांसलता और यौनिकता के प्रतिनिधि के तौर पर रख सकते हैं.ऐसा इसलिए भी है कि एक उत्पादन के आदिम चरण पर खड़ी है तो दूसरी बाज़ार और वितरण के आधुनिक और प्रचलित चरण पर .शोषण से दोनों को निजात नहीं है पर अधिकांश फ़िल्म निर्माताओं का मक़सद सामाजिक नहीं, शुद्ध व्यावसायिक है.
सत्यम शिवम सुंदरम की उस नायिका को देखें ,जो अपने जले हुए चेहरे को पल्लू से छिपाकर नायक से मिलती है .उसमें उसकी अपनी त्रासदी से लड़ने की चाहत , एक युवा शरीर की आवश्यकताएँ , स्त्री यौनिकता का एक अलग आख्यान है लेकिन वह अंत में अपराधिनी ही साबित होती है क्योंकि उसका पति ‘अर्धसत्य’ से प्यार करता है , ‘पूर्णसत्य’ उसके लिए स्वीकार्य नहीं होता .स्त्री की सहनशीलता और यातना से जूझते चरित्र के बरअक्स एक विद्रोही रूप भी गढ़ा गया – सीता के सामने गीता और चालबाज की अंजू के सामने मंजू .पर ये भी वास्तविक चरित्रों से ज्यादा बाॅक्स आॅफिस के आंकड़ों को भुनाने के लिये थे .
आज स्थितियां बदल रही हैं.दरअसल बदलती हुई स्थितियों में स्त्री की जद्दोजहद अपने अस्तित्व को तलाशने की एक अनवरत प्रक्रिया पर्दे पर भी देखी जा सकती है.इसे ‘गॉडमदर’ , ‘फायर’ ,‘मृत्युदंड’ और ‘इश्किया’ से लेकर ‘डर्टी पिक्चर’ तक और अब लिव इन और मुक्त स्वच्छंद प्रेम के समय में ‘लव आजकल‘ और ‘शुद्ध देसी रोमांस’ और ताज़ा फिल्म ‘क्वीन’ में देखा जा सकता है.यहां आज के समय में पैदा हुई नये किस्म की त्रासदियाँ हैं लेकिन मुक्ति के अपने रास्ते और आज़ादी की अपनी पहचान भी हैं.जैसे-जैसे कहानियाँ स्त्री की तलाश करती जा रही हैं वैसे-वैसे नायिकाएँ बदल रही हैं.जैसे-जैसे स्त्री की उपस्थितियों और उसकी भूमिकाओं का मूल्यांकन होता जाएगा वैसे-वैसे नयी स्त्रियाँ आती जाएंगी और नायिकाओं का चेहरा और चरित्र बदलता जाएगा.इसकी आज सख्त ज़रूरत भी है.दरअसल नये माहौल में स्त्री के बदलते चेहरे को पहचानने की कोशिश की जा रही है और इसमें अनंत संभावनाएं हैं, इसमें संदेह नहीं।
त्याग और सहनशीलता के विलोम के रूप में ‘सीता और गीता’ में ऐसी दबी सहमी दासीनुमा सीता के बरअक्स हंटरवाली छाप गीता की ज़रूरत महसूस हुई जो पुरुषनुमा मैनरिज़्म और प्रतिशोध के दमनकारी तेवर के साथ उपस्थित थी ! धीरे धीरे स्थितियां बदलीं और इसका एक बेहतर और विश्वश्नीय आकलन हुआ ‘गाॅडमदर’ में जहां वह अपने आत्मसम्मान और प्रखर मेधा और कूटनीति के साथ उपस्थित थी ।गंभीर फिल्में तब भी बनीं, सामाजिक मुद्दों से तब भी मुठभेड़ की गयी! ‘धूल का फूल’ में भी क्वांरी मां के बच्चे को स्वीकृति दी गई, ‘क्या कहना’ में वही स्वीकृति कुछ और मुखर हुई.‘भूमिका’ में अपनी अस्मिता तलाषती स्मिता पाटिल, ‘अर्थ’ में पतिप्रेम से उबरती षबाना और ‘अस्तित्व’ में अपनी आकांक्षाओं को स्वीकारती तब्बू कुछ स्वतंत्रचेता स्त्रियों की छवि बनाती रहीं.
दरअसल बदलती हुई स्थितियों में स्त्री की जद्दोजहद अपने अस्तित्व को तलाशने की एक अनवरत प्रक्रिया पर्दे पर भी देखी जा सकती है.इसे ‘गॉडमदर’, ‘फायर’ ,‘मृत्युदंड’ और ‘इश्किया’ से लेकर ‘डर्टी पिक्चर’ तक और अब लिव इन और मुक्त स्वच्छंद प्रेम के समय में ‘लव आजकल‘ और ‘शुद्ध देसी रोमांस’ और ताज़ा फिल्म ‘क्वीन’ में देखा जा सकता है.आज के बदले हुए माहौल में ऐसी नायिका का स्वागत है जो न मिमियाती हुई सीता है और न भृकुटियां तरेरती चाबुक फटकारती गीता ! आज वह अपने को पहचान रही है.अपने खिलाफ़ बारीक साजिशों और प्रताड़ना से वाकिफ़ होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के चलते स्त्री पर थोपी हुई पाबंदियों को देखती है, अपनी आज़ादी की हवा को पहचानती है।तीन दशक पहले क्या हमने कभी सोचा था कि ‘‘अजीब दास्तां है ये ….’’ और ‘‘ दिल एक मंदिर है ….’’ जैसे गीत गाती स्त्रियों के देश में कभी हाइवे, क्वीन, पिंक और पाच्र्ड जैसी फ़िल्में भी बनेंगी ? बेषक भारतीय सिनेमा में यह एक बड़ा बदलाव आया है।
यह दौर निश्चित रूप से नायिकाओं की स्टीरियोटाइप इमेज से बाहर स्त्री की अस्मिता को पहचानने और उसकी आकांक्षा को तरजीह देने का है.हिन्दुस्तानी जनता द्वारा इस छवि को स्वीकार्यता देना भारतीय सिनेमा के लिये गर्व की बात है.भला हो निर्माताओं – निर्देशकों का जिन्होंने समय रहते यह पहचान लिया कि सामूहिक नृत्य के नाम विदेशी बालाओं की बिकनी पहने परेड अब दर्शकों को लुभा पाने में कामयाब नहीं है इसलिये ‘लुटेरा’ फ़िल्म में साठ के दशक की रूमानियत दिखाई गई और ‘क्वीन’ में बिना किसी के प्रेम में पड़े एक लड़की की अपने आप से पहचान करवाई गई.फिल्मों में नायिका का रूप रंग, ज़ीरो फिगर आज पीछे छूट गया है.‘इंगलिश विंगलिश ’ की नायिका एक अधेड़ गृहिणी है जो अपने बच्चों और पति की मेधा से अपने को पीछे छूटता देखती है, तो इस उम्र में अंग्रेज़ी भाषा सीखने की कोशिश करती है और अपने बूते पर अपने लिये सम्मान हासिल कर दिखाती है.‘कहानी’ में एक गर्भवती नायिका अपने पहरावे और बिखरे हुए बालों से बेखबर अपने पति के अपराधी को पकड़ने के मिशन में जुटी है और पूरी फिल्म अपनी चुस्त पटकथा और निर्देशन के बूते पर बग़ैर किसी ग्लैमर और नाच गाने के दर्षकों को बांधे रखती है.
‘क्वीन’ फिल्म में एक दक़ियानूसी मध्यवर्गीय परिवार से आयी एक लड़की, जिसे उसके होने वाले पति ने रिजेक्ट कर दिया है, अकेले ही हनीमून पर विदेश जाने का फैसला लेती है.अब उसके सामने उसके छोटे से कस्बे के बरक्स कहीं बड़ी आज़ाद ख़याल दुनिया है जो पहले उसे चैंकाती है, फिर अपनी ज़द में ले लेती है.वह अपनी आंकाक्षाओं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पहली बार पहचानती है और अपना निर्णय ख़ुद लेने का साहस दिखाती है.फिल्म ‘हाईवे’ सिर्फ़ एक खुले लंबे रास्ते का विस्तार ही नहीं है, वह खुली हवा और आज़ादी का प्रतीक भी है.यहां एक रईस परिवार की लड़की अपने आलीशान बंगले और संभ्रांत दिखने वाले लोगों की वहशी कैद और जकड़न से निकलकर बेरोकटोक हवा में सांस लेने का सुकून पाती है.यह फिल्म एक मिथ को तोड़ती है कि एक अपराधी सिर्फ़ अपराधी ही नहीं होता ! कई बार परिस्थितियां उसके मानवीय और संवेदनात्मक पक्ष को कुंद कर देती हैं.जहां रिश्तों का संभ्रांत मुखौटा लगाये चेहरे एक कमउम्र लड़की को भी सिर्फ़ जिस्म के रूप में देखते हैं, वहां एक मुजरिम उसे एक मासूम इंसान की तरह देखता है, जिंस की तरह नहीं.यह फिल्म रोचक अंदाज़ में यह संदेश देने में भी समर्थ है कि घरों की चहारदीवारी के भीतर चल रहे शोषण को आखिर कब तक लड़कियां घर की झूठी इज़्जत के नाम पर छिपाती रहेंगी ? एक ऐसा घर-घर का सच जिसे अब तक कहा नहीं गया था।
लड़कियां चुस्त कपड़ों और ज़ीरो फ़िगर से आगे एक ज़हीन दिमाग़ और सोच भी रखती हैं बेशक उनकी काया मोटी और रंगरूप बहुत आकर्षक न हो -‘दम लगाके हईशा ’ फिल्म से बेहतर तरीके से इसे नहीं बताया जा सकता.यह भी हमारे समाज की एक रूढ़िगत सोच है जिसके कारण हर लड़का अपने लिये गोरी चिट्टी काया वाली सुंदर कन्या चाहता है बेशक वह दिमाग़ से शून्य हो.यहां एक स्थूल काया और ज़हीन दिमाग़ है.सदियों से सुनाई जाती हिदायतों को सुनने से बरजती बीस साल पहले के माहौल में आज की लड़की निश्चित रूप से जानती है कि उसके मोटापे और उसके साथ बीती रात के लिए अपने दोस्तों के बीच उसे ज़लील करता पति सिर्फ तमाचे का ही हक़दार है ! आहत होकर अपने अगले कदम के बारे में भी मज़बूती से फैसला लेती है और पति को अपनी गलती महसूस करते देख अपना जुड़ाव जताने में भी दूसरी बार नहीं सोचती -‘‘मैं वहां जाना नहीं चाहती ! मुझे रोक लो!’’ बिना किसी क्लाइमेक्स और मेलोड्रामा के, सीट पर टेंशन में आगे की ओर खिसक कर फिल्म देखने के बजाय, अपनी सीट पर पसर कर मुस्कुराते और शाखा बाबू की आचार विचार की कार्यशाला में विशुद्ध हिंदी और ठसकेदार पुरबी पर ठहाके लगाते हुए दर्शक फिल्म देखते और सराहते हैं !
धीरे धीरे हमारे फिल्म निर्माताओं को भी समझ में आने लगा है कि सिर्फ़ आइटम सांग और द्विअर्थी संवाद किसी फिल्म के चलने की गारंटी नहीं देते.‘पीकू’ देखते हुए लगा जैसे हमारे घर के डाइनिंग टेबल पर होने वाला वार्तालाप सीधे हमारे खाने की मेज़ से उठा लिया गया है.फ़िल्मी चकाचौंध , ग्लैमर, हिंसा, नायिका का ज़ीरो फिगर और एक गाने में दस बार बदलते कॉस्ट्यूम की जगह सुंदरता के प्रतिमानों को ध्वस्त करती ये नायिकाएं आज की सामान्य लड़की का प्रतिनिधित्व करती हैं.रंगीन फूल पत्ते वाले कुर्ते और साडी़ पहने या राजस्थानी घाघरा और ढीला ढाला टाॅप पहने अंग्रेज़ी गाने पे बेलौस नाचती आत्मविश्वास से भरपूर एक नॉर्मल लड़की पहली बार फिल्म की हीरोइन बनी है!
हाल ही में रिलीज़ हुई दो फ़िल्में अपने विषय के कारण भरपूर चर्चा में रही हैं.दोनों फ़िल्मों में तीन तीन लड़कियां हैं – ज़ाहिर है, तीन प्रतिनिधि चरित्र .पिंक में महानगर में नौकरी करती तीन लड़कियों में एक पंजाबी, एक मुस्लिम और एक नाॅर्थ ईस्ट की .पर्चेड में एक विधवा, एक पति की प्रताड़ना से त्रस्त बांझ और एक अपनी देह को अपनी मर्ज़ी से जीने वाली बिंदास लड़की.दोनों फ़िल्में आधुनिक दौर की हैं.पिंक फ़िल्म में जहां मनोरंजन, व्यवसाय और मुनाफ़े का नज़रिया अहम है, ‘पर्चेड’ एक कला फ़िल्म की श्रेणी में रखी जा सकती है हालांकि उसमें भी अन्तराष्ट्रीय बाज़ार को ध्यान में रखा गया है.एक स्त्री के अपनी यौनिकता पर अधिकार और प्रताड़ना या वंचना से बाहर आकर अपनी तरह से जीने के उल्लास को फ़िल्म रेखांकित करती है.फ़िल्म ‘पर्चेड’ में आया गांव और ग्रामीण स्त्री कितनी वास्तविक है और कितनी सिनेमाई, यह लंबी बहस का मुद्दा है।
पिंक फिल्म बाॅक्स आॅफ़िस पर सफल फ़िल्म है क्योंकि वह दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है.आज की कामकाजी लड़कियों की अलग फ़लैट लेकर रहने की आज़ादी, एक छोटे से क़दम से उन्हें परेशानी में डाल देती है.एक घटना को कोर्टरूम ड्रामा बनाकर पिंक फिल्म दर्शकों को उलझाए रखती है.फिल्म ‘‘तलवार’’ की अप्रत्याशित सफलता के बाद निर्देशक निर्माता ने दर्शकों की नब्ज पहचान ली और अमिताभ जैसे कलाकार को फिल्म का नायक बनाकर आधुनिक लड़कियों की समस्या पर एक कहानी बुन दी गई.फ़िल्म का सबसे बढ़िया संवाद — ‘‘नो एक शब्द नहीं, पूरा वाक्य है!’’ भी उसी नायक के हवाले कर दिया जिसने फिल्म की मार्किट वैल्यू बेशक बढ़ा दी पर स्त्री चरित्रों को कमजोर और असंतुलित कर दिया.यह मेसेज फिल्म के वकील महानायक की जगह अगर विक्टिम लड़की देती तो बात में कुछ ज़्यादा वज़न होता .बेशक उसे वकील साहब अपने पुरअसर अंदाज़ में दोबारा घोषित कर देते.
फिल्म हिट है इसमें कोई शक नहीं ! एक महत्वपूर्ण मेसेज की अति नाटकीय अदायगी के सारे झोल इसकी वजह से छिप गए हैं.अमिताभ की स्क्रीन वैल्यू से निर्माता निर्देशक इस कदर आक्रांत न होते तो फिल्म में तीन लड़कियों के किरदार सलीके से इस मेसेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों तक पहुंचा पाते ! जितनी मशक्कत इस फिल्म के लेखक ने वकील दीपक सहगल के चरित्र का ग्राफ बनाने और धीमी आवाज से सप्तम के सुर तक संवाद लेखन का रिदम तैयार करने में लगाई, उससे चौथाई भी कहानी की मुख्य विक्टिम मीनल के मनोविज्ञान और उसकी दुविधा का ग्राफ बनाने में लगाते, तो उसे हकलाते हुए ‘‘न न… न्नो’’ बोलते तो न दिखाते.पुलिस स्टेशन जाने की शुरुआती हिचक से गुजर चुकने और कोर्ट केस एक बार शुरू हो जाने के बाद कोई भी सच्ची लड़की इतना डरते हुए नहीं बोलेगी.वास्तविकता बेशक भयावह है और आज गांव की या शहरी , कामकाजी या घरेलू किसी भी लड़की के साथ कहीं भी हादसा हो सकता है, बलात्कारी तक छूट जाते हैं, उनका पूरा परिवार कोर्ट कचहरी से जूझता थक जाता है और न्याय तब भी नहीं मिलता .लेकिन फ़िल्म में निर्माता निर्देशक का पहला सरोकार फ़िल्म में लगाई गई पूंजी आौर उससे मुनाफ़ा कमाना होता है .फ़िल्म अगर कोई संदेश देने में सफल हो पाती है तो यह मनोरंजन के साथ एक अतिरिक्त बोनस है.पिंक फ़िल्म लड़कियों के ‘नहीं’ कहने और ‘नहीं’ को ‘नहीं’ समझे जाने के अधिकार के संदेश को दर्शकों तक बखूबी पहुंचा देती है.
बाॅक्स आॅफ़िस पर भी कामयाब होती ये फ़िल्में इस धारणा को पुख़्ता करती हैं कि आज हिंदी फिल्मों में उभरती नयी नायिकाओं के किरदार को और अपनी ज़मीन पहचानती लड़कियों की अलग किस्म की मानसिकता को आम दर्शक अपनी स्वीकृति देता है !जैसे-जैसे कहानियाँ नयी स्त्री की तलाश करती जा रही हैं, वैसे-वैसे नायिकाएँ बदल रही हैं.जैसे-जैसे स्त्री की उपस्थिति और उसकी भूमिकाओं का मूल्यांकन होता जाएगा, वैसे-वैसे नयी स्त्रियाँ आती जाएंगी और नायिकाओं का चेहरा और चरित्र बदलता जाएगा.इसकी आज सख्त ज़रूरत भी है.दरअसल नये माहौल में स्त्री के बदलते चेहरे को पहचानने की कोशिश की जा रही है और इसमें अनंत संभावनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं.






