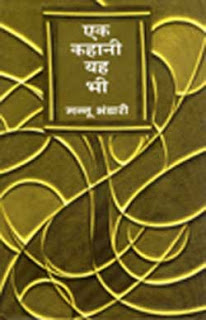रोहिणी अग्रवाल स्त्रीवादी आलोचक हैं , महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं . ई मेल- rohini1959@gmail.com
रोहिणी अग्रवाल स्त्रीवादी आलोचक हैं , महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं . ई मेल- rohini1959@gmail.com
चारो ओर से कीलती अपनी ही सीमाओं में घिर कर अवाक स्तब्ध खड़ा है व्यक्ति! वक्त का प्रवक्ता और सर्जक बनने का अकूत हौसला है उसके भीतर, लेकिन निजी जीवन-सत्यों और सम्बन्धों के संश्लिष्ट संजाल को देखने की निःसंग दृष्टि नहीं। क्या सचमुच बींधती अजनबी नजर से अपने को देखना इतना कष्टकर होता है? क्या इसलिए कि यह अपनी उन सब उपलब्धियों, निष्पत्तियों, निर्णयों और जीवन-दर्शन की क्रूर जांच की अनिवार्य प्रक्रिया है जहां आज तक स्वयं ’अपने को ’ केन्द्रीय एवं मानक इकाई मान कर वह व्यक्ति, सम्बन्ध, समाज – सब को अपने संदर्भ में बांचता आया है? या इसलिए कि जानने-पहचानने-स्वीकारने की इस प्रक्रिया में जिस अपेक्षित ईमानदारी और निर्भीकता की जरूरत होती है, वह आत्ममुग्धता के रेशों से सिरजी मानवीय फितरत में है ही नहीं? हैं तो लंगड़े पूर्वग्रह या उद्धत अहं जिनके तहत अपनी खूबियों और शहादत के बरक्स दूसरों की खामियां और टुच्चापन रख कर, काटती-छीलती नुकीली सच्चाइयों के बरक्स सहलाती-पुचकारती आत्मछलनाएं रख कर अपने और दूसरे को उतना भर देखा जाता है जिससे अपना ’देखना’ और ’निर्द्वंद्व जीना’ सुभीते से चल सके। आत्मछलनाओं का अनवरत सिलसिला जोे सच को बयान करने की छटपछाहट के सघन दबाव तले सच उगलता है तो कोई न कोई कलात्मक आड़ लेकर – चित्र, संगीत, कहानी कविता। समग्र दृष्टि अर्जित ही नहीं कर पाता आदमी! वह विडंबनाओं में जीने को अभिशप्त है और कतरा-कतरा छुपाने-उघाड़ने की आंखमिचैली में अपने को ’साबुत’ पाने को व्याकुल भी। लेखिकाओं से आत्मकथाएं लिख कर पुरुष तंत्र का पूरक पाठ प्रस्तुत करने का अनुरोध करने वाले राजेन्द्र यादव हों या अपने ही खोल में सिमटी मासूम मन्नू भंडारी – आत्मकथा लिखने के नाम पर दोनों चौककर न-न कर उठते है. राजेन्द्र यादव हिचकिचाती ईमानदारी के साथ कि ’’जिसे हम अपराध कहते हैं, वह कहीं जाने-अनजाने गलत हो जाने का दूसरा नाम है। वह हम सबके साथ है। जो चीजें मुझसे गलत हो गईं, या दूसरों के प्रति जो गलतियां मैंने की हैं, उन सबको स्वीकार करने की या स्वयं अपने सामने देख सकने की मानसिकता मेरी नहीं है। सामाजिक प्रतिष्ठा या तथाकथित मर्यादाएं ऐसी हैं जो मुझे रोकती हैं।’’ (हमारे युग का खलनायक: राजेन्द्र यादव, पृ0 620) और मन्नू बेहद पारदर्शी ढंग से कि ’’ आत्मकथा कथाकार को नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि वह अपनी कथाओं में ही बहुत कुछ लिख चुका होता है। अपने ही जीवन का कोई न कोई अंश उसमें जरूर आता है। कहानी भले ही दूसरे की हो, लेकिन जब तक मैं उसे अपनी नहीं बना लेती हूं (मेरा भी कोई आयाम जुड़ ही जाता है) तब तक लिखूंगी कैसे!’’ (आजकल, सितंबर 2004) जाहिर है जब मन्नू भंडारी ’एक कहानी यह भी’ में इसे व्याकुल भाव से आत्मकथा न मानने का आग्रह करती हैं तब प्रश्न उठाने को मन नहीं करता कि फिर निजी जीवन के प्रसंगों, तनावों, विश्वासघातों, आरोपों और शिकायतों से भरपूर इस आत्मकथात्मक रचना को क्या कहा जाए? बस, भूमिका और प्रस्तावना में जहां-तहां टंकी आत्मस्वीकृतियों को आधार बना कर मान लिया जाता है कि यह उन पूरक प्रसंगों और सच्चाइयों को ’थ्री डाइमेंशनल इमेज’ देने का प्रयास भर है जिनकी निजता को अनायास ’मुड़ मुड़ के देखता हूं’ ने उघाड़ कर सार्वजनिक कर दिया है। तो क्या यह प्रतिवादी की ओर से दाखिल जवाबदावा है?
स्त्री का समाज और समाज में स्त्री‘अकेली’
लेकिन क्या साहित्य की देशकालातीत उदात्त सर्जनात्मकता को अदालत या अखाड़े के देशकालाबद्ध टुच्चे दांवपेंचों में रिड्यूस किया जा सकता है?
‘एक कहानी यह भी’ आत्मकथा न होकर आत्मस्मरण या सैल्फ जस्टीफिकेशन ही क्यों न हो, यह तय है कि एक साहित्यिक कृति के रूप में इसका पाठ लेखिका सहित तमाम नामी-गरामी लेखकों और जीवित व्यक्तियों को साहित्यिक पात्रों में तब्दील कर देता है जो एक-दूसरे की संगति और अन्विति में एक-दूसरे को काटते-संवारते अपनी निजता और संपूर्णता ग्रहण करते हैं। अनायास नहीं कि तब स्मृति में कौंध उठता है अमृतलाल नागर का उपन्यास ’सुहाग के नूपुर’ – कन्नगी, कोवलन, और माधवी के त्रिकोण के साथ! प्रेम की टीस, पछाड़ने और छीनने की जिद, पा कर भी ठगे रह जाने की प्रतीति, समर्पण-शहादत के साथ घुलमिल गया कुट्टनी धर्म, प्रेम की उद्दाम लहरों के वेग से रेत के घरौंदों की मानिंद बिखर-बिखर जाती मर्यादा, नैतिकता, पतिव्रत्य और शील की सुपरिचित परिभाषाएं। न, तीनों में गलत कोई भी नहीं और शायद सौ फीसदी सही भी कोई नहीं। न कन्नगी के लाचार आंसू, न माधवी का बेलगाम रोष और न कोवलन की निस्सहाय विवशता। अनुष्ठानमूलक पतिव्रत्य मे जकड़ी कन्नगी एकबारगी क्लीन चिट पा भी ले, लेकिन माधवी की निष्ठा और समर्पण, प्रेम और प्रिय के जरिए अपने भीतर की मनुष्यता और शास्त्र के कुत्सित सत्य को खंगालने का सामर्थ्य क्या उसे वेश्या और वंचिता बनाए रखने का ही आग्रह करते हैं? कोवलन की उद्दाम वासना कब भीतरी राग से आपूरित हो सम्बन्धों के मकड़जाल से परे अपनी दैहिक-सामाजिक इयत्ता के बोध से परे हृदय पर कब्जा कर बैठी, वह स्वयं नहीं जान पाता। उसका कसूर है कि माधवी के साथ मिल कर उसने समाज का कानून तोड़ा है, और सामाजिक जकड़बंदियों के बीच जीवित-शोभित कन्नगी की त्रासदी यह कि इस फ्रेमवर्क के बाहर उसकी कोई निजी इयत्ता ही नहीं। त्रासदी कहर बन कर नहीं बरपेगी क्या? ’एक कहानी यह भी’ के मन्नू-राजेन्द्र यादव-मीता त्रिकोण चित्रण में बेशक कोवलन-कन्नगी-माधवी सरीखी संवेदना की गहराई, नैतिकता के सनातन सवाल पर बहस का आह्वान या निजी संदर्भों को वृहद् सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देने की लेखकीय अकुलाहट नहीं है, फिर भी पुनर्परीक्षण की मांग लेकर विवाह-संस्था तो कटघरे में आ ही खड़ी हुई है और साथ ही विवाह संस्था द्वारा अनुमोदित पति-पत्नी के रोल माॅडल भी। शायद विवाह-संस्था का पुनरीक्षण मन्नू भंडारी को पसंद नहीं क्योंकि इस रचना सहित अपने समूचे कथा साहित्य में वे विवाह-संस्था की ’पवित्रता’ तोड़ने वाली बेहयाइयों से संत्रस्त रही हैं, विवाह-संस्था से बाहर निकल कर इसके स्वरूप केा विकृत और संकीर्ण करती ’नैतिकताओं’ और वर्चस्ववादी सामाजिक संरचनाओं के हस्तक्षेप पर विचार नहीं करतीं। इसलिए हथियार छोड़ कर ’आत्मकेन्द्रित आत्मलिप्त’ पति पर यही आरोप लगाती हैं कि ’’वैवाहिक सम्बन्ध की गरिमा का निर्वाह न कर पाने वाले व्यक्ति के लिए विवाह-संस्था के विरुद्ध झंडा उठाए फिरना वाजिब ही नहीं, अनिवार्य भी है। लेकिन फिर विवाह किया ही क्यों?’’ (पृ0 218) इस अभियोग के साथ अपने एकनिष्ठ पत्नी धर्म के प्रति क्षोभ भी है कि ’’क्यों मैं सबके सामने एक सुखी संतुष्ट गृहिणी का मुखौटा ओढ़ कर यह सब झेलती रही जिसे किसी भी स्त्री के लिए झेल पाना बहुत दुष्कर है’’ और वह भी तब जब ’’न मैंने राजेन्द्र का दिया कभी खाया.. न पहना बल्कि घर और बच्ची की सारी जिम्मेदारियां भी मैं खुद ही ढोती रही।’’ (पृ0 213) बेशक वे दावा करती हैं कि यह रचना उनकी लेखकीय यात्रा पर ही केन्द्रित है किंतु इसका मूल स्वर और लक्ष्य खलनायक के तौर पर राजेन्द्र यादव की फजीहत करना है। गुनाह? एक नहीं, अनेक! पत्नी के प्रति एकनिष्ठ समर्पण का अभाव! दाम्पत्येतर प्रेम सम्बन्ध जीने की सीनाजोरी! पत्नी की अस्मिता को खंडित करता पुरुष अहं! लेकिन इसमें नया क्या है? अभियोगों को विशेषण का रूप देकर पुरुष आज तक अपने पतित्व केा वर्चस्व की निरंकुशता और क्रूरता तक हांकता आया ही है। तो क्या हाशिए से बाहर धकेली पत्नी अन्याय के खिलाफ गुहार न लगाए? मान ले कि अपनी जड़ता में जड़ीभूत स्त्री या तो अहिल्या की तरह शिला बन जाने को अभिशप्त है या भीत कातरता में मुक्ति द्वारों की सांकल खोलने में असमर्थ?
नहीं! मन्नू भंडारी अपना प्रतिरोध दर्ज करना चाहती हैं।
तो सबसे पहले कटघरे में पति यानी राजेन्द्र यादव!
राजेन्द्र यादव के ‘पेंचदार गुट्ठल’ व्यक्तित्व की एक-एक गांठ उघाड़ते हुए वे जिस तरह उन्हें प्रस्तुत करती हैं, तब वहां राजेन्द्र यादव नहीं, ’मेरे आका’ का मुस्तफा खार अपनी तमाम सामंती क्रूरता और सम्मोहन, निरंकुशता और नृशंसता के साथ आ विराजता है। बच्ची और परिवारियों के सुख-दुख से उपरत; अंतरंग मित्रता को गहरी संवादहीनता के कगारों तक ले आने वाला अहंवादी (’’किसी का भी वर्चस्व स्वीकार करना तो इनके अहं को गवारा ही न था’’, पृ0 82); सहजीवन के नाम पर पत्नी को ’समानांतर जिंदगी का आधुनिकतम पैटर्न’ थमाता हिपोक्रेट ताकि उसकी ऐयाशियों और विश्वासघातों का सिलसिला बदस्तूर चलता रहे (पृ0 48); पत्नी के संदर्भ में सामान्य सी इंसानियत को भी दरकिनार करता, अपनी शर्तों पर जीता पौरुषीय अहं जिसके लिए पत्नी का अर्थ है मूक समर्पिता नर्स (पृ0 88)। न, पत्नी के विशिष्ट आत्मनिर्भर व्यक्तित्व की अकुंठ स्वीकृति नहीं। बल्कि वही तो कलह-क्लेश की मूल जड़ क्योंकि मन में कहीं यह संस्कार जड़ें जमाए बैठा है कि ’’परिवार में वर्चस्व और प्रभुत्व केवल उसी का हो सकता है जो परिवार का भरण-पोषण करे।’’ (पृ0 208) इसलिए बच्ची की देखभाल को ’आयागिरी’ के साथ जोड़ने की मर्दवादी मानसिकता जो अपने आर्थिक निठल्लेपन के कारण मर्माहत हो पत्नी को बुरी तरह चींथ डालती है तो पत्नी द्वारा अलग रहने के निर्णय पर फूट-फूट पड़ती कातर रुलाई – ’’मन्नू, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्लैक स्पाॅट है… तुम्हीं मुझे इससे उबार सकती हो….देखो, तुम मुझे छोड़ कर मत जाना… तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगी।’’ (पृ0 205) छल और झूठ की गंध से शून्य इस आग्रह पर कौन पत्नी न बलिहारी जाए? तहमीना हो या मन्नू – पत्नियों की जमात कमोबेश एक सी होती है – सुरक्षा के नाम पर ब्रीदिंग स्पेस देता बाड़ा और सम्बन्धों के नाम पर संवरी लता की तरह फैलने की स्वतंत्रता! बेड़ियों से बंध कर उड़ने की लालसा! पत्नी की परंपरागत रूढ़ छवि क्या आज भी इस द्विधा से मुक्त हो पाई है?
राजेन्द्र यादव की स्वीकरोक्ति और स्त्रीवादी प्रतिबद्धता के सवाल !
जाहिर है सारी सहानुभूति मन्नू भंडारी की झोली में। मन्नू जिसने पूरे पैंतीस साल रोते-झींकते ’बहुरूपिए’ के साथ जिंदगी काटी, मन्नू जिसने घर के भरण-पोषण के लिए अपने को नौकरी और व्यावसायिक लेखन में झोंका (पता नहीं क्यों अपनी ही किरचों से लहूलुहान मन्नू के बरक्स बार-बार ’आधे-अधूरे’ की सावित्री महेन्द्रनाथ की लाचारगी के साथ संपृक्त होकर याद आती रही?) ; मन्नू जिसने अकेले दम दोहरी-तिहरी व्यस्तताओं के बीच बेटी और नातेदारियों को सम्हाला; मन्नू जिसने हर टूटन को हथियार बना कर लेखन को धारदार किया। क्या इसी सहानुभूति, स्तुति और सतीत्व के लोभ में कोढ़ी पतियों को कंधे पर लाद वेश्यालयों तक ले जाती पत्नियों का मिथ आज भी जीवित नहीं समाज में? पत्नी की मानवीयता को खंड-खंड कर उसे रूढ़ छवियों, दायित्वों, विसर्जन एवं स्थगन की अमूर्त प्रक्रिया में तब्दील करता हुआ! लेकिन किशोरावस्था से मन्नू जिस वक्त की उंगली पकड़ कर चली हैं, वह ’’मूल्यों के मंथन का युग था… पाप-पुण्य, नैतिक-अनैतिक, सही-गलत की बनी-बनाई धारणाओं के आगे प्रश्नचिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था।’’ ( पृ0 22) स्वाभाविक है कि ’सुनीता’, ’त्यागपत्रा’, ’शेखर: एक जीवनी’, ’चित्रलेखा’ आदि के जरिए उन्होंने जो संस्कार, दृष्टि और मूल्यबोध अर्जित किया, वह न परम्परावादी हो सकता है, न यथास्थितिवाद का पोषक। इसकी झलक उनके काॅलेज जीवन की कुछ घटनाओं में भी मिलती है जहां स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने का निर्द्वंद्व निर्भीक भाव एक ओर काॅलेज के प्रांगण में हक की लड़ाई के लिए हड़ताल, हुड़दंग और सार्थक नेतृत्व में लक्षित होता है तो दूसरी ओर प्रगतिशील पिता से चलने वाली लम्बी लड़ाई में भी। लेकिन विवाह के बाद मानो कायान्तरण ही। स्वयं चकित हैं मन्नू भी कि ’’किशोरावस्था में मेरी जिन रगों में लावा बहता था, उनमें क्या अब निरा पानी बहने लगा है?’’ (पृ0 213) कहां से आ जाती है पत्नी में मिमियाती-झींकती आत्मदयाग्रस्त स्त्री जो उसकी निरीहता में दादी-नानी की तरह पति को पालतू बना लेने का अटूट विश्वास नत्थी कर युद्ध-सन्नद्ध बनाती है कि ’’मेरा समर्पण एक न एक दिन राजेन्द्र को जरूर बदल देगा’’ (पृ0 52)। विश्वास दरकने का दंश पराजय बोध को गहराता है ’’एक स्वच्छंद और मनमाने ढंग से जीवन जीने की इनकी जिद जिसमें सारे प्रयत्नों के बावजूद मैं जरा सा भी परिवर्तन नहीं ला सकी थी’’ (पृ0 188) तो ’किसी का कंधा, किसी की गोद’ तलाश कर वहीं लिथड़े रहने की कातरता एक अवश आदत बन कर निष्कृति के सारे द्वार बंद कर देती है। ऐसा नहीं कि आत्मपड़ताल की प्रक्रिया में आत्मधिक्कार से भर कर मन्नू ने अपनी रीढ़विहीन कातरता पर क्षोभ प्रकट न किया हो, लेकिन अपने को कटघरे में खड़ा कर चीन्हने की बजाय वे बार-बार लक्ष्यभ्रष्ट सैल्फ जस्टीफिकेशन की लीपापोती में जुट जाती हैं। मसलन, पिता से विद्रोह के रूप में की गई शादी को सफल बनाने (या दिखाने) की चुनौती; घर को बनाए रखने का विशुद्ध स्त्रियोचित दायित्व जो भावना के उच्छ्ल आवेग में अहं और आत्माभिमान को भी बहा ले जाता है – ’’सोचने पर आज तो यह भी लगता है कि कौन जाने तीन दिन तक ऊपर से भले ही मैं अपने संकल्प पर दृढ़ता की परतें चढ़ाती रहीं, पर भीतर ही भीतर मैं भी तो ऐसे ही किसी बिंदु की, छोर की, संकेत की प्रतीक्षा में ही थी जिसे थाम कर मैं अपने संकल्प से डिग सकूं।’’ (पृ0 205) ; सामंत पति के लबादे के ठीक नीचे सहयोगी-प्रेरक साहित्यकार मित्र की निर्दोष मैत्री को न खोने की दूरंदेशी – ’’कैसी विडम्बनापूर्ण सच्चाई है कि राजेन्द्र के व्यक्तित्व का एक पक्ष जहां मेरी हीनता ग्रंथि पर परत दर परत चढ़ा कर मेरे आत्मविश्वास को खंडित करता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायक ही नहीं रहा बल्कि लिखने के लिए मुझे बराबर प्रेरित-प्रोत्साहित भी करता रहा है। नई से नई पुस्तकों और पत्रिकाओं का आना, सभी तरह के साहित्यकारों के जमावड़े… उत्तेजक बहसें.. गप्प गोष्ठियां, मेरे जैसे लेखक के लिए बड़ा प्रेरक था यह वातावरण… मेरा मूल प्रेरणा स्रोत! इसीलिए जब तक मेरे व्यक्तित्व का लेखक पक्ष सजीव-सक्रिय रहा, चाह कर भी मैं राजेन्द्र से अलग नहीं हो पाई।’’ (पृ0 215) एकाएक यहां लेखिका की दो स्वीकारोक्तियों को उद्धृत करने का मन हो आता है। एक, ’’राजेन्द्र से विवाह करते ही लेखन के लिए तो जैसे राजमार्ग खुल जाएगा और उस समय यही मेरा एकमात्र काम्य था’’ (पृ0 10 ) और दूसरी, ’’ठेठ यथार्थ की भूमि पर खड़े होकर ही मैंने यह निर्णय लिया है क्योंकि अब मुझे जिंदगी से जो चाहिए, वह एक लेखक के साथ ही मिल सकता है।’’ (पृ0 201) साथ ही एक प्रश्न भी अंकुराता है कि यशस्वी लेखक को साबुत पा जाने की हड़बड़ी ने ही कहीं उन्हें राजेन्द्र यादव की विवाह करने की टालमटोलू अन्यमनस्कता को नजरअंदाज करने को मजबूर नहीं किया? आखिरकार एक अपंग, आर्थिक दृष्टि से आधारहीन व्यक्ति के साथ सहजीवन शुरु करने के पीछे मूल जज्बा क्या थ? प्रेम की प्रगाढ़ता? लेखक राजेन्द्र यादव के पेचदार गुट्ठल व्यक्तित्व की महीन परतों के नीचे छिपे व्यक्ति राजेन्द्र यादव से अभिन्नता? या एक-दूसरे को समृद्ध करने के प्रयास में स्वयं समृद्धतर होते चले जाने की सहज मानवीय अभिलाषा जिसके मूल में विश्वास और सौहार्द दोनों की समान उपस्थिति अनिवार्य है? लेकिन क्या किसी एक भी विकल्प पर निश्चयपूर्वक उंगली रखी जा सकती है? ’’अंतरंग परिचय से बिल्कुल अपरिचय की दुनिया में लौट जाने की तकलीफ’’, अपनी ’’दुखती रगों और खाली कोनों’’ को लेखन से पूरा करने की मुआवजी कोशिशें; जुबान पर ’छुरी-कांटे’’ उगा लेने की आवेश भरी प्रतिक्रियाएं या हर तालाबंद गोपनीयता को जान लेने की जासूसी हरकतें – सम्बन्धों को खोखला कर देने को काफी हैं। सम्बन्ध जो नकार का प्रत्युत्तर नकार में नहीं चाहते, नकार को निर्विकार तक लाने के लिए अपनी मनुष्यता के बरक्स दूसरे की मनुष्यता को छूते-उद्वेलित करते हैं।
यहीं चारों खने चित्त हो जाती हैं मन्नू! रिक्तियां और गैप्स..किंवदंतियों और विवादों से गर्माए राजधानी के प्रभावक्षेत्र से दूर कस्बे में बैठा आतुर पाठक तथ्य की तह में छिपे सत्य का साक्षात्कार कर अपनी निजी राय बनाना चाहता है, किंतु जगह-जगह तथ्यों के नाम पर बंद चुप्पियां! या ’’..फिर कुछ ऐसा घटा कि मुझे निर्णय लेना ही पड़ा कि बस, बहुत हुआ’’ (पृ0 163) जैसी छुपाती-भरमाती अ-पारदर्शिता! क्या सच्चाई को छुपाने का एक अर्थ किसी दूसरे को विकृत और विद्रूप करना नहीं?
हालांकि मन्नू भंडारी ने दावा किया है कि ’एक कहानी यह भी’ लिखते समय उन्होंने निःसंगतापूर्वक अपने अतीत को उधेड़ा है – ’’अपने को अपने से काट कर बिल्कुल अलग’’ कर देने की ’डाॅक्टरी’ कुशलता के साथ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है कि शब्द दर शब्द वे हर प्रकरण में इन्वाॅल्व हैं। न, अनजाने नहीं, जानती-बूझती हैं, अपनी हरकत पर शर्मिंदा भी हैं और शिकायतों की लम्बी फेहरिस्त तहा कर अपने को संयमित भी करती हैं कि ’’आत्मदया में लिपटी यह गाथा अब बिल्कुल बंद क्योंकि मुझे खुद इससे बड़ी चिढ़ है। पर क्या करुं, लाख कोशिशों के बावजूद जब-तब इसके दौरे पड़ ही जाते हैं।’’ (पृ0 169) मन्नू की समस्या यह है कि पूरी पुस्तक में ’चुप्पी’ के बावजूद एक खास किस्म के बड़बोलेपन का शिकार वे होती रही हैं जिसका मूल कारण है आवेशभरी प्रतिक्रियात्मक मुद्रा में अपने को ’देखने’ की अनिवार्यता को निरंतर स्थगित करने रहने का जनून। इससे उनके व्यक्तित्व में एक ओर आत्मरक्षा और आत्मगौरव की मिश्रित सजगता आई है -’’स्वभव से ही मैं बहुत तनावग्रस्त हूं। लेकिन यदि अनुकूल परिस्थितियां मिलती… अपनत्व भरा साथ मिलता तो निश्चित रूप से मेरे ये सारे तनाव ढीले ही नहीं होते , बल्कि समाप्त हो जाते’’ (पृ0 169); तो दूसरी ओर औसत स्त्री की ’संतुष्ट’ नियति का सामान्यीकरण करते हुए अपने दुख का महिमामंडन – ’’यह मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आज की हर स्त्री घर-परिवार के अतिरिक्त और भी न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभाती है, उसमें अपनी ऊर्जा खर्च करती है लेकिन अपने साथी का सहयोग प्यार भरा लगाव निरंतर उस ऊर्जा की क्षतिपूर्ति भी करता रहता है… मेरे साथ क्या हुआ कि मैं सिर्फ खर्च ही करती रही और एक ऐसी स्थिति आई कि मैं बिल्कुल खाली-खोखली हो गई… रोगग्रस्त शरीर.. निष्क्रिय जीवन और खंडित आत्मविश्वास की किरचों में लिपटा व्यक्तित्व!’’ क्या एक संवेदनशील उद्बुद्ध लेखिका से ऐसे मोहाविष्ट एकांगी निष्कर्षों की अपेक्षा की जा सकती है जिनका सारा लेखन मध्यवर्गीय औसत स्त्री के परिवार और मन के कोने-अंतरे में झांक कर उसके कहर, क्लेश और सपनों को जीता रहा है? पत्नी, गृहिणी और व्यक्ति के रूप में क्या हर स्त्री कमोबेश टूटने-सहने की त्रासदी के बीच अखंड बनी रहने की जिजीविषा से प्रदीप्त नहीं होती रहती?
तो क्या दुख का अतिरेक व्यक्ति को संकुचित और आत्मकेन्द्रित बना देता है – पूरे फलक से काट कर एक निर्जन द्वीप में कैद करता? शायद! लेकिन मन्नू लेखिका हैं और कहानियों में उनके भीतर की सर्जनात्मकता पूरी ऊँचाई के साथ सारे विस्तार को बांहों में समेट लेना चाहती है। चूंकि कहानियों में जहां-तहां टुकड़ा-टुकड़ा आत्मकथा निबद्ध कर देने का दावा करके वे ’बंद दराजों का साथ’, ’एक बार और’, नायक खलनायक विदूषक, करतूते मरदां, स्त्री सुबोधिनी जैसी कहानियों का नामोल्लेख करती हैं तो यह कहना आसान हो जाता है कि भगिनीवाद विस्तार की नारीवादी अवधारणा ही उन्हें अंतःशक्ति प्रदान करती है। बेशक मीता पहले दिन से ही उनके दाम्पत्य सम्बन्धों में विघटन का अहम कारण बनी है और एक स्वाभाविक सौतिया डाह के कारण दाम्पत्य सम्बन्ध के विघटन की इस महागाथा में उन्होंने मीता के पक्ष और पीड़ा को उभारने की तिल भर कोशिश भी नहीं की है लेकिन कहानियों में पुरुष-प्रवंचिता प्रेयसियों का चित्र उकेरते हुए वे मानो मन्नू नहीं, मीता हो जाती हैं जहां पति-पत्नी के बीच ’वो’ बन जाने की अभिशप्त नियति हिंसक बना कर वस्तुतः उसकी लस्त-पस्त बेचारगी को ही उघाड़ती है। कुचला आत्मसम्मान सांप बन कर फन लहराता हुआ कुंज और मधु के बीच आता जरूर है लेकिन बार-बार डंसता उसे ही है। अंधी गली का रूप लेकर भावुकता कब तक मन्नू-मीताओं को भरमाती रहेगी – मन्नू नहीं जानतीं क्योंकि वे दोनों बैताल सी इन्हीं गलियों में भटक रही हैं – निरंतर! लेकिन पाठक जानता है कि विवाह के सुरक्षित दुर्ग में बैठी पत्नी की धाक, अधिकार और गरिमा को अंगूठा दिखा कर अधिकारविहीना अकिंचन प्रेयसी स्मृति पर हावी हो जाती है। वंचित-प्रवंचित, कमजोर-तिरस्कृत के प्रति सहानुभूति के कारण? या इसलिए कि निर्बंध प्रेम और अनुशासन में पुराना बैर है?
क्या पुरुष अपने समदुखी ‘मीत’ की व्यथा -कथा समानुभूति से लिखेंगे ?
आत्मकथाकार/निजी जीवन की आख्यानकार के रूप में मन्नू से अपेक्षा थी कि निजी जीवन की लव-हेट गुंजलक (जिसका उल्लेख वे इससे पूर्व 1964 में लिखे संस्मरणात्मक आलेख में भी कर चुकी हैं) से निकल कर वे दाम्पत्य सम्बन्धों के विश्लेषण के बहाने उन नई संकटापन्न स्थितियों का विश्लेषण करेंगी जो स्त्री को शिक्षित, स्वावलम्बी एवं आधुनिक बना कर उसे वक्त से आगे ले जाती हैं और वक्त की दौड़ में पिछड़े अहंनिष्ठ पुरुष को अपेक्षाकृत अनुदार और संकीर्ण बना कर सामंती मूल्यों की पुनप्रतिष्ठा में जुट जाती हैं। आखिरकार वे स्वयं स्वीकारती हैं कि उनका युग मूल्यों की मीमांसा का युग था, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने किन दिशाओं और मूल्यों को एक्सप्लोर करने के लिए स्त्री छवि गढ़ी? आत्मकथा शिकायतों-प्रत्यारोपों का पुलिंदा मात्रा नहीं होती, एक साहित्यिक कृति के रूप में वस्तुनिष्ठ चरित्र ग्रहण कर वह शब्दों और घटनाओं, मनःस्थितियों और मनोद्गारों के जरिए स्वयं लेखक के व्यक्तित्व की महीनतर एवं संश्लिष्ट परतें उघाड़ने लगती है। तब ऐसा क्यों लगता है कि उनके कथा साहित्य की नायिकाओं के व्यक्तित्व का पैटर्न – निरंतर द्वंद्वग्रस्तता, निरंतर निर्णय-दुर्बलता, स्वार्थपरक शाइस्तगी और यथास्थितिवाद में परित्राण पाती उदारता – ’एक कहानी यह भी’ में भी ज्यों का त्यों उभर कर आ रहा है? कहीं सर्जनात्मकता का अभाव तो नहीं? सर्जनात्मकता वह नहीं जो साहित्य रच कर ही हो। सृजन विचार और क्रिया के स्तर पर कुछ नया सोचने/करने में भी निहित है। संवेदना के साथ जुड़ कर सृजन जब मिशन का रूप लेता है तो सक्रियता और सकारात्मकता, प्रतिकूलताओं से टकराने का जज्बा और जिजीविषा व्यक्तित्व को अद्भुत ओज और ऊर्जा दोनों देते हैं। सृजन शांतिकाल का मनोविलास है ही नहीं, प्रसव पीड़ा के दौरान बीहड़ पगडंडियों पर दौड़ते-गिरते अपने को ’नया’ करते रहने की अनवरत प्रक्रिया का नाम है। इसलिए चाहे वे अपनी लंबी निष्क्रियता और न लिख पाने के कारणों को ’मन में रचे-बसे तनाव’ के मत्थे मढ़ दें, लेकिन सवाल तो उन्हें भी मथता रहा है कि उज्जैन में प्रेमचंद विद्यापीठ पर रह कर दो बरस उन्होंने किया क्या? क्या यह एक लेखक की भीतरी ऊर्जा, संवेदन और अंतर्दृष्टि के ’चुक’ जाने की पूर्वसूचना नहीं जो ’एक कहानी यह भी’ में घटनाओं का सपाट ब्यौरा बन कर आती है – साहित्यिक औदात्य से छूंछी? क्या वजह है कि इसी रचना में मन्नू के यशस्वी लेखकीय व्यक्तित्व की ऊँचाई को अंगूठा दिखा कर अपनी पोतियों के लिए मराठी रचनाओं का टूटा-फूटा हिंदी अनुवाद करती अ-लेखक वृद्धा सर्जनात्मक ऊँचाइयों का संस्पर्श करने लगती है? दरअसल अपने आवेश और भावाकुलता को थिरा कर अंतर्दृष्टि से संगुम्फित न कर पाने की दुर्बलता मन्नू को उन सिरों को एकान्विति में जांचने की नजर नहीं दे पाई जो हताशा और पराजय के बाद ही आशा और जिजीविषा के अदम्य आवेग से आपूरित होती है। तहमीना का विद्रोह, तसलीमा की उद्दंड निर्भीकता, भंवरीबाई की संकल्पदृढ़ता और मुख्तार माई की सिर पर कफन बांध कर मौत की आंख में धूल झोंकने की चतुराई – निजी दुखों की शिकायती पोटलियों को परे फेंक देने के बाद की ही उपलब्धियां हैं। हां, परे फेंकने की इस प्रक्रिया में संवेदनशून्य होने की प्रतिक्रियात्मकता नहीं, अपने जैसी प्रताड़िताओं के आंसू पोंछ कर सह-अस्तित्वपूर्ण साझी दुनिया रचने की स्वप्नशीलता है।
साहित्यिक कृति के रूप में ‘एक कहानी यह भी’ मन्नू भंडारी के समकालीन साहित्यिक परिदृश्य की भीतरी नग्न सच्चाइयों का भी पर्दाफाश करती है जहां इमरजेंसी के दौरान सरकारी भोंपू बन कर रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जैसे दिग्गज अपनी भौतिक लोलुपताओं के साथ निर्वसन हो जाते हैं तो राकेश-राजेन्द्र-कमलेश्वर की तिकड़मी तिकड़ी साहित्य में माफिया के बीज बोती दीखती है। लेकिन इस रचना का तात्कालिक महत्व न मन्नू की लेखकीय यात्रा का हमसफर बनने की चाहत में है, न अन्य लेखकों के टुच्चेपन का रस लेने में। यह सिर्फ और सिर्फ राजेन्द्र यादव को घेर-घार कर दुरदुराने-मारने का महानुष्ठान है। फलतः साहित्यिक रचना से अधिक वैयक्तिक राग-द्वेष की अभिव्यक्ति! लेकिन जो परिदृश्य में अपनी ठोस उपस्थिति के बावजूद अनुपस्थित है, उसके खलनायकत्व को आंख मूंद कर क्यों स्वीकारा जाए? कटघरे में है तो बयान देने का अधिकार तो है इस लोकतंत्रा में उसे भी। इसलिए मैं नहीं समझती कि ’मुड़ मुड़के देखता हूं’ के बगैर ’एक कहानी यह भी’ के कोई मायने हैं। बकौल मन्नू घुन्ना व्यक्तित्व है राजेन्द्र यादव का, हर झूठ, हर जिद, हर नाजायज हरकत को ढांपने के लिए विश्वसनीय तर्क गढ़ने में माहिर आत्ममुग्ध-आत्मरतिग्रस्त व्यक्ति जो अपने से इतर अन्य किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। यहां तक कि मीता सहित अनगिन प्रेम सम्बन्धों में अधिकार और समर्पण (जिसे मन्नू प्रेम का विस्तार मानती हैं) का भाव नहीं, ’वर्चस्व के बोध से छके हुए एक कुंठाहीन पूर्ण पुरुष’ का अनुभव जीने का दर्प है। बेशक अपनी इस ’लम्पटता’ का संज्ञान लेते हैं राजेन्द्र यादव लेकिन साथ ही कुछ इस तरह की जिज्ञासा भी करते हैं कि क्या कोई भी मनोविकार या मनोवृत्ति अपने परिवेश की उपज नहीं होती? मन्नू क्षुब्ध हैं कि ’या.. या.. या.. के विकल्प लगा कर यह बहुरूपिया ऐयार पाठकों को भरमा कर हर बार अपनी असली सूरत छुपा ले जाता है लेकिन क्या ऐसा नहीं कि प्रश्न के रूप में दिए गए सारे विकल्प राजेन्द्र यादव एवं पूरी पुरुष जाति के मनोविज्ञान को खंगालने की श्रृंखला बन जाते है? ’’यह अपनी रचनात्मक ऊर्जा और वैचारिक स्वाधीनता के लिए बार-बार किया जाने वाला नवीनीकरण है या अधूरे होने की हीनता-ग्रंथि से उत्पन्न दमित सेक्स की विकृत अभिव्यक्ति जो बार-बार दूसरे से अपनी पूर्णता का आश्वासन चाहती है? यह मेरी निजी कुंठा है या प्राक् ऐतिहासिक आदिम पुरुष-वृत्ति जहां वह अपने कक्षों में शत्रुओं और शिकारों के सिर सजा कर विजय के गर्व को बार-बार जीवित रखता है? या वह सामंत जिसे हरम में अनगिनत भोग सामग्री चाहिए?’’ या फिर इसलिए कि ’’हर नई स्त्राी के साथ सम्पर्क पुरुष-व्यक्तित्व के उन अनुद्घाटित आयामों को खोलता है जिन्हें उसने पहले कभी आविष्कृत नहीं किया था।’’ ठीक शरतचंद्र के नायकों की सी स्थिति जो राजलक्ष्मी, अभया, सावित्री, पारो, चंद्रमुखी के बिना अपनी अस्मिता को पा ही नहीं सका। राजेन्द्र यदि जीते-जागते व्यक्ति न होकर कथानायक होते तो मीता, दीदी, मन्नू के संदर्भ में उनके विकसित अहं और स्निग्ध अंतःप्रकृति के तीन अंतरंग खूबसूरत चित्रों के साथ-साथ व्यक्ति और लेखक के अंतर्सम्बन्धों की महीन पड़ताल की जा सकती थी। अब बेशक वे लाख कहते रहें कि उनकी जिंदगी में ’’मीता संगीत के निःशब्द अंतरे की तरह बनी रही तो जिस तार ने सुर संभाले रखा या लगभग संचालित करती रही, वह तो दीदी है। उधर मन्नू न होती तो जमीनी सच्चाइयों की यह अनुभव-सम्पन्नता कहां से आती – ठहराव और गहराई तो मन्नू ने ही दी’’ (मुड़-मुड़के देखता हूं’, पृ0 131) , मन्नू के नजरिए ने ढर्राबंद जिंदगी न जी पाने की उनकी असफलता को ’लम्पट’ की उपाधि तो दे ही दी है।
बहुपठित राजेन्द्र यादव के अर्जित ज्ञान और मौलिक उद्भावनाओं को लेकर कहीं दो राय नहीं। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के हर लम्हे और स्थिति का विश्लेषण कर उसे कहानी का रूप देने को सन्नद्ध रहे, वह सामान्य तो है ही नहीं। विशिष्ट भी नहीं क्योंकि बोहेमियन के लिए सांसारिक मूल्यांकन कोई मायने नहीं रखते। वे क्रांतिदर्शी, स्वप्नजीवी, स्वतंत्रचेता ही नहीं हुआ करते, बेहद जिद्दी, महत्वाकांक्षी और उन्मादी भी होते हैं और कठोर आत्मालोचक भी। आंतरिक बुनावट में बेहद संश्लिष्ट और जटिल। स्वयं अपने को समग्रता में न पहचान पाएं, लेकिन यथार्थ के नाम पर चौहद्दियां बुनती जड़ता का अतिक्रमण करने को व्याकुल; देश-काल को नए सिरे से सिरजने को आतुर – मनुष्य की आदिम मनोवृत्तियों के साथ जहां पाप-पुण्य, मर्यादा-अश्लीलता की चोर निगाहों तले लहूलुहान होती मनुष्यता सिर धुनती कुंठाओं में तब्दील होने की त्रासदी न भोगती हो, वरन् अंतर-वैयक्तिक सम्बन्धों का संजाल रच कर एक एक सा ब्रीदिंग स्पेस जुटाने में संलिप्त हो; जहां निजता और पारस्परिकता दोनों की रक्षा होती रहे, सदा। यकीनन एक यूटोपिया! इसलिए सात्र-सीमोन की मित्रता से प्रभावित राजेन्द्र यादव जब दम घोंटती विवाह संस्था के विकल्प रूप में लिव इन रिलेशपशिप की वकालत अपने उपन्यास ’उखड़े हुए लोग’ में करते हैं तो हिंदुस्तानी वक्त से बहुत आगे निकल जाते हैं। दूर, दुर्बोध और मुजरिम! एक ऐसी स्थिति जिसे ’आते जाते यायावर’ में पूरी आंतरिकता से चित्रित कर देने के बावजूद मन्नू रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन में संभव मान ही नहीं पातीं। ’घर’ और ’निर्बंध उत्तरदायित्वहीनता’ दोनों को साथ-साथ पा लेने की औसत ललक उन्हें कहीं बौना भी बना देती है लेकिन ’आत्मसंतुष्टि की दुहराव भरी जिंदगी’ भीतर के बुद्धिजीवी को एकदम स्वीकार्य नहीं। फलस्वरूप विद्रोह और नकार – अपने को साबुत पाने के प्रयास में अपने को तोड़ना और गढ़ना। विश्व क्लासिक साहित्य के नायक के सनातन द्वंद्व का साक्षी हूक, कसक भरी अनवरत तोड़-फोड़ हांफते-जूझते नायक को एक खास किस्म का औदात्य और आह्लाद अवश्य देती है। निस्सीम को बांहों के घेरे में बांध लेने का आह्लाद! राजेन्द्र यादव का दुर्भाग्य कि वे क्लासिक रचना के पात्रा नहीं!
उल्लेखनीय है कि जहां ‘एक कहानी यह भी’ में मीता प्रसंग आतंक और अनैतिक भाव से आया है, वहीं मुड़-मुड़के देखता हूं’ में परिपूर्णता, श्रद्धा और अपराध बोध के मिले-जुले भाव में। ’तपस्वी सा जीवन बिता रही’ मीता के प्रति एक कोमल भाव (साॅफ्ट काॅर्नर) है जिसे वे छिपाते नहीं। हां, उसके साथ किए गए विश्वासघात के कारण आत्म-निर्मम जरूर हो गए हैं। लेकिन मोहन राकेश, मनमोहन ठाकुर के संस्मरण हों या ’देखा तो इसे भी देखते’ शीर्षक के अंतर्गत मन्नू का जबाव – मन्नू से विवाह के संदर्भ में मीता को लेकर एक खास किस्म की दुविधा उनमें देखने को मिलती है, मित्रों से मन्नू तक अपनी कमजोरी को सम्प्रेषित करने का आग्रह और न-नुकर की भाषा में मन्नू को कहा गया यह वाक्य -’’सोचता हूं पहले मीता सैटल हो जाती तो…’’। न, छल और बेईमानी का सवाल ही नहीं। है तो दुविधा और निर्णय-दुर्बलता जो ’यही सच है’ की ढुलमुल दीपा को हिंदी साहित्य का यादगार पात्रा बना देती है। यानी जिंदगी से जीवनीशक्ति पाने के बावजूद साहित्य और जीवन के मूल्यांकन के मानदंड एक नहीं हैं? बेशक! साहित्य लार्जर दैन लाइफ है, जिंदगी के द्वंद्वों और क्षुद्रताओं का समाधान-उन्नयन करता एक प्रेरणा-पुंज; वर्तमान की कंटीली जकड़न से मुक्ति की स्वप्निल उड़ान; अंतःशक्ति और स्फूर्ति, ऊर्जा और ओज को संवेदना और दृष्टि के साथ निबद्ध कर ’कल’ को मनचाहे ढंग से जीने की हौंस को साकार करता स्वप्न! लेकिन जिंदगी के तलछट में सिर्फ घोंघे और कीचड़ नहीं, न ही विशाल टाइटैनिकों को डुबोते आइसबर्ग! बल्कि जिंदगी का आदिम स्रोत तो वही है जहां नौ बटे दस हिस्से पर कब्जा करते आइसबर्गाें के खौफ से मुक्त एक बटा दस हिस्से पर ही संवाद और सृजन की संभावनाएं जगाई जाएं। ’मुड़-मुड़के देखता हूं’ में ये संभावनाएं हैं और इसीलिए बकौल मन्नू भंडारी यह एक साहित्यिक कृति भी बन गई है जबकि ’एक कहानी यह भी’ घटनाओं और ब्यौरों की सपाटबयानी। दोनों में फर्क यह भी है कि सारे आरोपों और गलतियों को स्वीकारते हुए राजेन्द्र यादव जहां आत्मविश्लेषण करते हुए अपनी मानसिक संरचना में देश-काल, समाज-संस्कृति-इतिहास की वाजिब हिस्सेदारी को रेखांकित कर आम आदमी की संरचना को समझने का अहम फार्मूला अनायास उपलब्ध करा देते हैं, वहीं मन्नू भंडारी ’’एक-एक बात, एक-एक ब्यौरा, एक-एक पंक्ति सही’ होने के दावे के बावजूद ’एक कहानी यह भी’ के महत्व को रोजमर्रा की घरेलू लड़ाइयों से ज्यादा नहीं बढ़ा पातीं। अतः अपनी अंतिम परिणति में यह कांता भारती के उपन्यास ’रेत की मछली’ जैसी औसत रचना बन कर रह जाती है – चटखारेदार! अलबत्ता एक सवाल जरूर टंगा रहता है कि पुरुष के सामंती चरित्रा पर उंगली उठाने वाला सुधी समाज उसके सामंती व्यक्तित्व से शक्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा लेकर सामंतवाद को जिलाए रखती स्त्रिायों की अनदेखी क्यों कर जाता है? क्या इस समूचे प्रकरण में कृष्णा सोबती की यह पंक्ति ज्यादा सटीक और मानीखेज नहीं हो जाती कि ऐसी स्त्राी ’’पहले अपनी दया से पुरुष की हिंसा पकाती है और फिर पुरुष की हिंसा से अपनी दयनीय स्थिति मजबूत करती है।’’
स्त्रीकाल का संचालन ‘द मार्जिनलाइज्ड’ , ऐन इंस्टिट्यूट फॉर अल्टरनेटिव रिसर्च एंड मीडिया स्टडीज के द्वारा होता है . इसके प्रकशन विभाग द्वारा प्रकाशित किताबें ऑनलाइन खरीदें :
दलित स्त्रीवाद , मेरा कमरा, जाति के प्रश्न पर कबीर
अमेजन पर ऑनलाइन महिषासुर,बहुजन साहित्य,पेरियार के प्रतिनिधि विचार और चिंतन के जनसरोकार सहित अन्य
सभी किताबें उपलब्ध हैं. फ्लिपकार्ट पर भी सारी किताबें उपलब्ध हैं.
दलित स्त्रीवाद किताब ‘द मार्जिनलाइज्ड’ से खरीदने पर विद्यार्थियों के लिए 200 रूपये में उपलब्ध कराई जायेगी.विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थान के आईकार्ड की कॉपी आर्डर के साथ उपलब्ध करानी होगी. अन्य किताबें भी ‘द मार्जिनलाइज्ड’ से संपर्क कर खरीदी जा सकती हैं.
संपर्क: राजीव सुमन: 9650164016,themarginalisedpublication@gmail.com