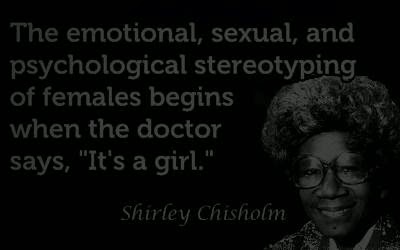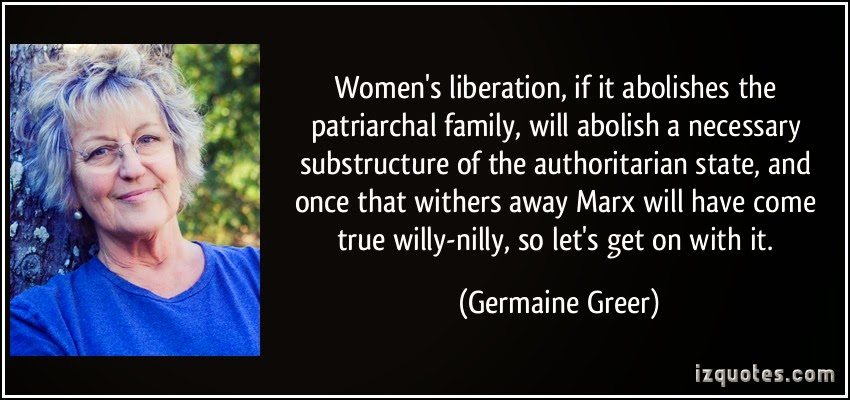( अरुण कुमार प्रियम की सद्य प्रकाशित पुस्तक ‘ पितृसत्ता और साहित्’ की समीक्षा कर रहे हैं डा. आम्बॆडकर विश्वविद्यालय के शोधार्थी अनंत विजय पालीवाल )
पितृसत्ता और साहित्य अरुण कुमार प्रियम की पहली पुस्तक है। पहली उपलब्धि अनुभव के पायदान पर प्रथम प्रयास होता है, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। पितृसत्ता और समाज में उसके अलग-अलग चेहरों की पहचान करते हुए अरुण इसे जाति और वर्गों की परिधि तक ले जाते हैं। समाज, साहित्य से लेकर परिवार जैसी छोटी इकाई तक में इसके स्तरीकरण पर चर्चा को वे गंभीरता से उठाते हैं। सामाजिक संस्थाएँ पितृसत्ता का पाठ कैसे पढ़ाती हैं; पितृसत्ता के अभिकर्त्ता कौन-कौन है; परिवार में इसकी घुसपैठ या बुनियाद कैसे गढ़ी जाती है? आदि पर संक्षिप्त किन्तु असरदार बहस को उठाने का प्रयास यह पुस्तक करती है। पुस्तक की भूमिका ‘धूमिल’ और ‘सुभद्रा कुमारी चौहान’ जैसे शीर्षस्थ साहित्यकारों के परंपरावादी नजरिए की आलोचना से आरंभ होती है। अरुण ने इन रचनाकारों की जिन पंक्तियों को उठाया है व समय के साथ उनका जो तुलनात्मक विश्लेषण किया वह उचित है। लेकिन यहाँ यह कहना कि “साहित्य इसका अनुकूलन करता है, जिससे यह मूल्य आगे भी इसी रूप में आने वाले समाज को दिया जाता रहा” (पृ. 11), पूरे ‘साहित्य’ पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देता है। डॉ. अंबेडकर के समय से ही साहित्य के विभिन्न रूप सामने आने लगे थे। दलित आंदोलन, स्त्री आंदोलन व इसी प्रकार के अन्य आंदोलनों ने साहित्य को और इससे संदर्भित साहित्य ने इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई थी। आज स्त्री-साहित्य, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य व उनसे संबन्धित पत्र-पत्रिकाओं का साहित्य जगत में एक अलग स्थान है। इस तरह उपरोक्त वक्तव्य सम्पूर्ण साहित्य को एक साथ कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता।
अरुण की इस पुस्तक का आधा भाग सीधे-सीधे पितृसत्ता जैसे सामाजिक विमर्श पर केन्द्रित है और आधा भाग पितृसत्ता के नजरिए से साहित्य की पड़ताल करता है। ‘पितृसत्ता की सार्वभौमिकता’ अध्याय में परिवार, धर्म, समाज, संस्था, संविधान, विवाह, मीडिया, शिक्षा प्रणाली, आर्थिक क्षेत्र और यौनिक नियंत्रण जैसे मुद्दों पर खुली बहस को प्रस्तुत किया गया है। शायद सभी मुद्दों को एक साथ उठाने के कारण इस बहस में कई पक्ष अवश्य छूट गए हैं, फिर भी इनसे एक संक्षिप्त समझ जरूर पैदा होती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम यहाँ ‘मीडिया’ पक्ष को ही लें तो अरुण धारावाहिकों में ‘अच्छी औरत’, ‘बुरी औरत’ और मीडिया संस्थानों में उनके ‘पद’ तक ही बहस को सीमित कर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि यह पितृसत्ता का केवल प्रत्यक्ष पक्ष है। दरअसल यहाँ मार्केटिंग की उन परोक्ष नीतियों को भी उठाना चाहिए था जो बड़ी बारीकी से पितृसत्ता को स्थापित करती हैं। जैसे विज्ञापनों को ही लें यहाँ विज्ञापन चाहे मेंस-डियो-परफ्यूम का हो या बाइक का; पुरुष के पीछे आकर्षित होती या उसकी पिछली सीट पर चिपके औरत होती है। बाइक के विज्ञापन में ड्राईविंग सीट उसे शायद ही कभी नसीब हुई हो लेकिन वॉशिंग पाउडर से लेकर स्कॉच ब्राईट तक के विज्ञापनों में वह जरूर कपड़े धोते मिल जाएगी। टॉयलेट क्लीनर बेचने वाला सेल्स मैन भले ही पुरुष हो लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाली महिला ही दिखाई जाती है। इस तरह यह सोच कि विज्ञापनों के जरिये स्त्रियों को रोजगार मिल रहा है, उनकी भागीदारी बढ़ रही है; दरअसल एक धोखा है। जिसका मूल्य और प्रस्तुतीकरण दोनों पितृसत्तात्मक है।
यहाँ यह कहना भी उचित है की पितृसत्ता एक विचार है; एक मानसिकता है जो किसी भी जाति और धर्म में समान रूप से घुसी हुई है। चूंकि धर्म पुरुष प्रणीत है और पुरुष प्रभुत्व वाला है अत: यह संस्थाएँ महिलाओं को नियंत्रित करने का एक पारंपरिक हथियार है जिनकी वैधता को चुनौती देना आसान नहीं है। यहाँ अरुण यह कहने में बिल्कुल नहीं झिझकते की “सभी धर्म पितृसत्तात्मक हैं। धर्म अपने चरित्र में ही स्त्री विरोधी है और पुरुष प्रभुत्व को सर्वोपरि मानता है” (पृ. 27)। इस संदर्भ में वे धर्मों से तथ्यात्मक उदाहरण भी पेश करते हैं। कुछ ऐसे ही संदर्भ वे जातियों से भी उठाते हैं जहाँ एक ही जाति व्यवस्था में होने के बावजूद भी पितृसत्ता हावी रहती है। यहाँ वर्ग व्यवस्था का वाहक पितृसत्ता बनती है। आर्थिक वर्गीकरण में निचले पायदान के लोग भी इसका शिकार होते हैं। “सल्लन की पत्नी खुद एक दलित स्त्री है, लेकिन वह प्रमिला, जयवंती और नीलम के वर्ग की स्त्री नहीं है। वह आर्थिक रूप से ऊँचे दर्जे की स्त्री है। जयवंती, प्रमिला और नीलम आर्थिक रूप से निचले और कामगार वर्गों की स्त्रियाँ हैं। इसलिए सल्लन की पत्नी का वर्चस्व उन पर बना रहता है”। वह पितृसत्ता के वर्गीय चरित्र की वाहक है। इस प्रकार अरुण ने पितृसत्ता के वर्गीय भेद को भी कई उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है।
पुस्तक के द्वितीय भाग ‘पाठ-अंतर्पाठ’ में कुछ स्त्रीवादी कविताओं की समीक्षा व ‘मीरा’ और ‘सुभद्रकुमारी चौहान’ जैसे भिन्न युग की कवियित्रियों की रचनाओं का विश्लेषण है। स्त्रीवादी कविताओं में ‘रंजना जायसवाल’ और ‘शायक आलोक’ की कविताओं की जो समीक्षा अरुण ने प्रस्तुत की है मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। कविता के शब्दार्थ, भावार्थ और व्यंग्यार्थ भिन्न होते हैं। दरअसल ‘सेक्स रैकेट की लड़कियाँ’ कविता पितृसत्ता पर व्यंग्य है न कि उसका समर्थन जैसे यह पंक्ति ‘चेहरा यूं ढाँपे खड़ी हैं / मानो रही ही न हों / मुँह दिखाने के काबिल / या फिर चेहरा विहीन / सिर्फ देह ही हैं’। अरुण ने यहाँ चेहरे का आशय ‘दिमाग’ से लगाया है। उनका आशय है कि “लड़कियों के पास दिमाग नहीं है सिर्फ दिमाग विहीन (चेहरा विहीन) शरीर है” जबकि पंक्तियों में कवियित्री का तीखा व्यंग्य है कि सेक्स रैकेट की इन लड़कियों का चेहरा इनकी पहचान नहीं होती है बल्कि समाज द्वारा केवल एक सिंबल (प्रतीक) ‘वेश्या’ ही इनकी अस्मिता के लिए गढ़ा जाता है। इसके लिए दलालों द्वारा कोई नाम, नंबर या वस्तुओं के नाम तक की कोडिंग इनके लिए की जाती है। अत: समाज इन्हे केवल देह मात्र तक सीमित कर देता है। इस प्रकार इनका चेहरा (अस्मिता) केवल ‘सेक्स रैकेट की लड़कियों’ तक सीमित रह जाता है। इसी तरह के कई अन्य पक्ष इस कविता और शायक आलोक की कविताओं में भी हैं जहाँ मैं खुद को इस समीक्षा से सहमत नहीं पाता हूँ। खैर समीक्षा में अरुण का अपना अलग नजरिया हो सकता है जिसे उन्होने बिना झिझके रखा भी है।
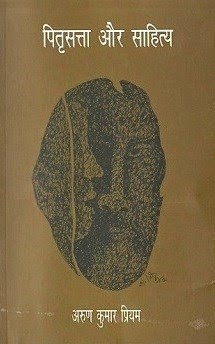 |
| पितृसत्ता और साहित्य, अरुण कुमार प्रियम (लेखक ) प्रथम संस्करण -2013, आरोही प्रकाशन, नई दिल्ली मूल्य : 100 रुपये |
‘मीरा और आधुनिक साहित्य’ में अरुण ने स्त्रीवादी नजरिए से मीरा के व्यक्तित्व और उनके काव्य को जांचा-परखा है। मध्ययुगीन समाज में पितृसत्ता के सभी बंधनो को तोड़ने वाली मीरा को उन्होने पुन: प्रतिष्ठित किया है। साहित्य में मीरा केवल ‘भक्तिकाल’ की गढ़ी-गढ़ाई छवि में पेश की जाती रही हैं। सूर, तुलसी, मीरा केवल सगुण (ईश्वरपरक) भक्ति धारा के एक कवि के रूप में याद किए जाते हैं। इनके सामाजिक संदर्भों पर हुए शोध भी ज़्यादातर भक्ति तक ही सीमित हैं। लेकिन वहाँ भी नजरिया स्त्रीविरोधी और पितृसत्तात्मक रहा है। मीरा पर एक संक्षिप्त लेकिन मुकम्मल नजरिया रखते हुए अरुण ने इस बहस को आगे बढ़ाया है। उनका यह प्रयास सराहनीय माना जाएगा।इसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान को केंद्र में रखते हुए अन्य समकालीन रचनाकारों के साथ एक तुलनात्मक विश्लेषण यह पुस्तक प्रस्तुत करती है। इसके लिए उन्होने कविता, कहानी दोनों विधाओं का चयन किया है। अरुण की दृष्टि इस संदर्भ में पक्षपात रहित कही जा सकती है, जहाँ शुरू में उन्होने सुभद्रा कुमारी चौहान के ‘मर्दानी’ शब्द पर आपत्ति जताई थी वहीं उनकी अन्य रचनाओं और व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पक्षों के स्त्रीवादी संघर्ष को सराहा भी। बाद में वे इन समकालीन महिला साहित्यकारों के पितृसत्ता के विरोध में स्त्रीवादी नजरिए पर मुकम्मल शोध किए जाने की जरूरत पर भी ध्यान दिलाते हैं। जिससे इस संदर्भ में उनकी जिजीविषा और गंभीरता को पहचाना जा सकता है।
कुलमिलाकर यह पुस्तक पितृसत्ता के विरुद्ध एक स्पष्ट और मुकम्मल बयान दर्ज करती है। यहाँ यह जरूर है कि पुस्तक के संक्षिप्त कलेवर के कारण कई महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार नहीं दिया जा सका है; लेकिन यह भी सही है कि पितृसत्ता के विषय में यह पुस्तक एक जरूरी समझ विकसित करती है। शायद यही अरुण और इस पुस्तक का पहला ‘हासिल’ भी है। आगाज़ के तौर पर लेखनी में अरुण ने धीमी लेकिन ‘असरदार’ दस्तक दी है। यह देखना और भी कौतूहलपूर्ण होगा कि उनकी अगली दस्तक ‘कब’ और कितनी ‘तेज़’ आती है।