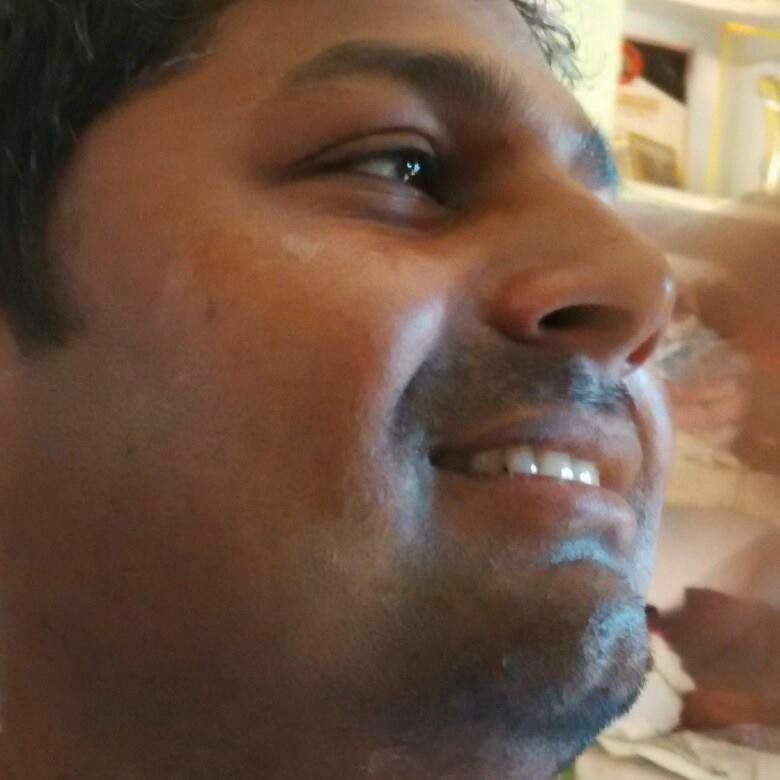 कर्मानन्द आर्य मह्त्वपूर्ण युवा कवि हैं. बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हिन्दी पढाते हैं. संपर्क : 8092330929
कर्मानन्द आर्य मह्त्वपूर्ण युवा कवि हैं. बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हिन्दी पढाते हैं. संपर्क : 8092330929
इक्कीसवीं सदी संक्रमण के दौर से गुजर रही है. भारतीय समाज में पहले आधुनिकता और फिर उत्तर आधुनिकता को लेकर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है. विमर्शों का जन्म कहीं इसी कोख से हुआ है.विमर्श चाहे वह किसी भी तरह का हो अब लगातार अपनी धुरी प्राप्त कर रहा है. समय का सातत्य यह है कि चाहे साहित्य हो अथवा समाज चारो तरफ उथल पुथल मच रही है. यही कारण है कि आधुनिक भारतीय समाज अब ज्यादा प्रजातान्त्रिक और लोक उन्मुख हुआ है. सबको अपना हक मिल पा रहा है और लोग बिना झिझक के खुद सबके सामने ला पा रहे हैं. ‘सिगमण्ड फ्रायड का यह बयान मशहूर है कि मनोविश्लेषण के क्षेत्र में इतने वर्ष काम करने के बाद भी मैं यह नहीं समझ पाया कि स्त्री आखिर चाहती क्या है?’ शायद इसीलिए स्त्री को ‘अंतिम उपनिवेश’ कहा गया है. स्त्री के लिए जो भी जगह छोड़ी गई है उसका वृतांत निश्चय ही कारुणिक है. लेकिन यह वृतांत हमेशा डराने वाला नहीं होना चाहिए. नहीं तो स्त्री अपनी वाजिब जगह ढूंढने से हमेशा खौफ खाती रहेंगी.’
साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य की कल्पना असंभव है. समाज एक सामूहिक इकाई है और साहित्य भी बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनता है. यह तथ्य सृजन के हर क्षेत्र में लागू होता है. हिंदी साहित्य का अपना सात-आठ सौ वर्षों का इतिहास है. लेखन की एक बड़ी संख्या में इसमें आमद रही है. साहित्य की बहुत सी विधाओं का अब तक जन्म हो चुका है और कुछ काल के गाल में खुद को समाहित करने से नहीं रोक पायी हैं. प्रतिरोध के इस साहित्य ने वैसे अनेक मुकाम हासिल किये हैं पर साथ की एक जाति विशेष की कृपा के कारण इस का समुचित विकास नहीं हो पाया. साहित्य उन अर्थों में प्रजातान्त्रिक नहीं हो पायी जहाँ उसे समाज के अन्य वर्गों का भी समुचित योगदान प्राप्त होता. अपनी पुस्तक ‘आलोचना और विचारधारा’ में डॉ. नामवर सिंह लिखते हैं कि आलोचना की दुनिया विचारों की दुनिया है. और विचार के लिए चाहे गुरु-शिष्य परंपरा हो या विदग्ध लोगों का समुदाय, उनके बीच बातचीत और शास्त्रार्थ जरुरी है. बहस के जरिये एक पीढ़ी में जो सवाल उठते हैं उनके जबाब अगली पीढ़ी को देने होते हैं . यह सच है कि हिंदी आलोचना का विकास पश्चिम की तरह नहीं हुआ. यहाँ आलोचना का विकास
कुछ आलोचों के द्वारा नहीं वरन संस्थाओं के द्वारा हुआ है. वह संस्था चाहे कोई पत्र, पत्रिका, प्रतिष्ठान के रूप में हो चाहे शिक्षणसंसथान के रूप में. साहित्य और समाज का रिश्ता द्वंदात्मक है.
बात आलोचना की है. यह कला की वह कसौटी है जिसपर साहित्य का ढांचा जांचा परखा जाता है. आलोचना साहित्य के सौन्दर्य को निखारने का कार्य करती है. शब्द अर्थ के निहितार्थों से अलग यह विधा साहित्य के उन तत्वों की बात करती है जो साहित्य सौन्दर्य के कारक हैं. आलोचना की यह परम्परा मनुष्य को सीखने सिखाने पर नहीं अपितु जीवन निर्माण करने की प्रक्रिया स्वरूप प्राप्त हुई. आलोचना के क्षेत्र में जब हम हिंदी पट्टी की स्त्री आलोचकों पर बात करते हैं तो एक शून्य स्थिति दिखाई देती है. आज भी स्त्री आलोचकों की संख्या अँगुलियों पर गिनाने लायक है. स्त्री सैधान्तिकी के लिए आज भी हिंदी जगत कोई ऐसी समीक्षक, आलोचक नहीं पैदा कर पाया जिसको तथाकथित मुख्यधारा बेझिझक उल्लेख कर सके. छिटपुट प्रसंगों को छोड़ दें तो एक खालीपन नजर आता है. यह खालीपन बहुत गहरा है और इसकी लतरें बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देती है. क्या कारण है की जहाँ रचनात्मक साहित्य में स्त्री रचनाकारों का बोलबाला है वहीँ वे अपने रचनात्मक साहित्य का मूल्यांकन स्वयं नहीं कर पायीं. आज भी वे नामवरों, नामचीनों के द्वारा पददलित हैं. हिंदी की आलोचना आज भी कहने पर केवल पुरुष का ही नाम सामने आता है. क्या पुरुष आलोचकों ने उन्हें हासिये पर नहीं धकेल दिया.
क्या यह सच नहीं है कि जिन्होंने कुछ काम किया वे भी पुरुष के संरक्षण के बदौलत ही. क्या यही कारण नहीं है उनकी रचनाधारा का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया. भारत में स्त्रीविमर्श लगभग अपने चौथे दशक में है इसपर भी इतिहास में उनका नाम कहीं हासिये पर चला गया. हिंदी के इतिहास ग्रंथों में उनके लिए मात्र कुछ पन्ने लिखे गए. आधी आबादी वहां एक सिरे से गायब नहीं तो दबाई अवश्य गई है.
कुछ काम हुआ है पर उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता. क्योंकि पुरुष रचनाकारों का ही प्रभुत्व चारो तरफ रहा है अतः आलोचना भी इससे अछूती नहीं रही है. यहाँ उन पुरुषों के योगदान को कमतर आंकने का आशय नहीं है अपितु उनकी सदाशयता को बार बार प्रणाम है. पुरुषों ने भी स्त्री आलोचना को काफी आगे बढ़ाया है. स्त्री आलोचना के विकास में समकालीन पत्रिकाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है. पत्र-पत्रिकाओं, महिला-लेखन विशेषांक निकाल कर पुनर्जीवन देती रही हैं. विमेन्स स्टडीज विश्वविद्यालयों का एक अलग विषय बन गया है. जगह-जगह विद्यार्थी महिला रचनाकारों के कृतित्व पर शोधकर्ता में संलग्न है. यह हक और दर्जा पाने के लिए महिला रचनाकारों ने अथक परिश्रम और निरंतर साधना की है. महिला लेखन की जमीन तैयार होने में लाखों अनाम स्त्री रचनाकारों की मेधा लगी है. जिनमें बहुत बड़ी संख्या उनकी भी है जिन्होंने लिख-लिखकर अपना साहित्य कॉपियों में दबा दिया, खुद भी कभी दुबारा निकालकर नहीं देखा कि शब्द की यह मौन सम्पदा उनसे छिन न जाए.
प्रजातान्त्रिक मूल्यों में लगातार स्त्री की सहभागिता बढ़ रही है. आज भारतीय राजनीति में स्त्रियों को केवल प्रतीक रूप में ही नहीं वाकई उनकी यथार्थ सहभागिता है. स्त्रियों ने लगभग उन क्षेत्रों में प्रवेश पा लिया है जो आज तक उनके लिए प्रतिबंधित था. अब वह केवल आत्मकथा, संस्मरण या कविता तक ही सीमित नहीं है अपितु वाब साहित्य के हर क्षेत्र में उसकी धमक महसूसी जा सकती है. समकालीन हिंदी आलोचना में स्त्री
आलोचना के उभार को कुछ इन्हीं विन्दुओं के माध्यम से जाना परखा जा सकता है. आजकल की आलोचना की तरह खुद को पुरुष के आईने में देखे कि वह अच्छी दिखाई दे रही है की नहीं, उसे कोई देखेगा कि नहीं. पुरुष ने अपने स्वार्थ के लिए कैसे प्रकृति या स्त्री के दोहन की शब्दावली रची है. वह गाय से दूध निकाल कर ही रहेगा. माँ के शोषण के लिए बस उसपर कोमलतम कवितायें ही लिखता रहेगा उसका शोषण रोकने के लिए उसे अपने संपत्ति में भागीदार नहीं बनाएगा. जैसा कि हम ‘इकोफेमिनिज्म’ में देखते हैं. यहाँ मुझे गोदान में प्रेमचंद की वह पंक्तियाँ याद आती हैं जहाँ पुरुष समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचंद स्वयं को प्रस्तुत करते हैं ‘जब पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं तब वह देवता बन जाता है और जब स्त्रियों में पुरुषों का गुण आ जाता है तो वे कुलटा हो जाती हैं. यह कैसी पुरुष विडम्बना है. वह कैसे अपने स्वार्थ के लिए स्त्री के मन का अनुकूलन करता है. आज हम इसे साहित्य का गोपी भाव कह सकते हैं. पुरुष जैसे चाहे उसे नचाये, घुमाये और जब काम निपट जाए तो वह उसे योग मार्ग की शिक्षा दे या सन्यासी का चोला पहना कर उसके मन में यह भाव भर दे कि ‘मेरो को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई’. यह मनःस्थिति रखते हुए स्त्री आलोचना का विकास कदापि संभव नहीं है. उसे अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व में महादेवी का अक्स दे दिया जाय जो ‘मैं नीर भरी दुःख की बदरी’ की करुना जनित पीड़ा से बाहर न निकल पाए. बस जिन्दगी भर वह केवल स्यापा ही रोती रहे. ‘हूम-हूम करे’ का आपाद मस्तक भजन कीर्तन करती रहे. क्या यह सच नहीं है कि पुरुष वादी आलोचना और स्त्री मस्तिष्क में घुसी हुई वही पुरुषवादी आलोचना है.
अन्तराष्ट्रीय महिला-वर्ष के बीस बरस से अधिक बीत जाने के बावजूद भी भारत में अभी तक कोई ऐसा मुखर स्त्री विमर्श नहीं आया जिसे हम भारतीय स्त्री विमर्श मान सकें. जो कुछ उपलब्ध है उसे केवल प्रॉक्सी द्वारा ही हिंदी का अपना विमर्श कहा जा सकता है. बकौल अर्चना वर्मा ‘’हिंदी के अपने स्त्रीविमर्श का अर्थ क्या हो सकता है इसकी कोई साफ़ तस्वीर भी हमारे पास नहीं थी और इस सन्दर्भ में शुद्ध हिन्दीनुमा किसी वैचारिक साम्पदायिकवाद या बौद्धिकजातीयतावाद जैसा कोई खास दुराग्रह भी नहीं था’’ . अब प्रश्न पैदा होता है जब स्त्रीवाद को लेकर ही बहुत गहरे प्रश्न हैं तो वहां स्त्री आलोचना को ढूढ़ पाना थोड़ा कठिन कार्य अवश्य है. यह देखा जाना यहाँ लाजिमी है की आज हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में स्त्री रचनाकारों की संख्या संतोषजनक है. वह कविता कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी आदि का काम तो प्रचुर मात्रा में कर रही है पर आलोचना जो वैचारिकी को स्थापित करने का मुख्य और सशक्त विन्दु है वह वहां पिछड़ रही है. यह स्त्री आलोचना की महज एक पंक्ति है. माया एन्जेलों कि उन पंक्तियों को संबोधित करती हुई जिसमें वह कहती हैं ‘मैं रोज उदित होती हूँ’.हिंदी ने पचास वर्षों ने पचास से भी अधिक महत्वपूर्ण महिला रचनाकार दीं. जिनमें महादेवी वर्मा, सुमद्राकुमारी चौहान, चंद्र किरण सोनरिक्सा, कृष्णा सोबती, मन्नू भण्डारी, उषा प्रियंबदा, मंजुला भगत, मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्गल, मृणाल पाण्डेय, नमिता सिंह, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, मधु काँकरिया, अनामिका, अनीता भारती, रजतरानी मीनू, गीतांजलि श्री, पद्मा सचदेव, मीराकांत, चन्द्रकांता राजा सेठ, सूर्यबाला और सुधा अरोड़ा, ने अपनी स्वतंत्र छवि बनाई है. इनकी मौलिकता पर कोई शंका नहीं की जा सकती. कुछ लेखिकाओं ने तो इस विषय पर बहुत बार और निरंतरता में लिखा है.
स्त्री स्वाभाविक आलोचक होती है और प्रकृति ने उसे स्वभावतः जो गुण दिया है वह उसमें ही कहीं पीछे दिखाई देती है. उसका रचनात्मक फैलाव बहुत विशाल है पर जब उसके साहित्य की परिधि का निर्माण करना होता है तो वह कहीं बहुत पीछे रह जाती है. यह सब जानबूझ कर और साजिसन किया गया है क्योंकि इससे पुरुष आलोचकों का एकाधिकार टूटेगा. अनेक खेमों में बंटा हुआ आज का हिंदी आलोचक ग्यारह वर्षों के लम्बें अंतराल में कुछ ऐसी स्त्री आलोचकों को नहीं पैदा कर पाया जिसे मुख्यधारा गर्व से धारित करती हो. आज भी भारतीय पुरुष समाज उतना ही बर्बर और क्रूर है जितना सामंती युग में था. स्त्री का लेखन उसे दोयम दर्जे का लगता है, उसकी आलोचना भी पुरुष को सुहाती नहीं है. यही कारण है कि जब हम हिंदी आलोचन की बात करने चलते हैं तो वहां से स्त्री पक्ष गायब मिलता है. कुछ नाम हम अपनी अँगुलियों पर रखने के सिवा कोई विकल्प नहीं ढूढ पाते. वह हजारो वर्षों से पुरुष की कृपा पर जीती आ रही है. जब पुरुष की इच्छा होती है तब वह रोटी डाल देता है नहीं तो सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देता है. देश के और भागों में अमूमन स्त्री की दशा-दिशा भले अच्छी हो पर आज जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं वहां की स्थितियां बहुत ही ख़राब हैं. समाज और साहित्य दोनों में वह आज भी बर्बरता ही झेल रही है. उन्हीं की कृपा है जो स्त्री विमर्श आज विमर्श की जगह अपनी मनोग्रंथियो को सहलाने का उपक्रम भर हो गया है.
मृणाल पांडे की ‘स्त्री लंबा सफर’ अनामिका की ‘स्त्री विमर्श की उत्तर-गाथा’ चारू गुप्ता की ‘स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक’ तथा ‘मौसम बदलने की आहट’ तथा सुधीरचन्द्र की ‘रमाबाई: स्त्री अधिकार और कानून’देह की राजनीति से देश की राजनीति तक -मृणाल पांडे, दुर्ग द्वार पर दस्तक – कात्यायनी, स्त्रीत्व का मानचित्र – अनामिका, उपनिवेश में स्त्री – प्रभा खेतान, औरत के लिए औरत-नासिरा शर्मा, स्वागत है बेटी – विभा देवसरे, स्त्री पुरुष कुछ पुनर्विचार – राजकिशोर, स्त्री के लिए जगह – सं. राजकिशोर, स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य – क्षमा शर्मा, स्त्री : मुक्ति का सपना – सं. प्रो. कमला प्रसाद, राजेन्द्र शर्मा, अतिथि सं. अरविन्द जैन व लीलाधर मंडलोई, स्त्री उपेक्षिता – सीमोन द बुआ, विद्रोही स्त्री – जर्मन ग्रेयर, स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन – मेरी, वोल्स्टनक्राफ्ट, औरत की कहानी – सं. सुधा अरोड़ा’ अपना कमरा – वर्जीनिया वुल्फ, एक स्त्री की ज़िंदगी के चौबीस घंटे – स्टीफन ज्विग इस संदर्भ में पठनीय पुस्तकें है. आज वैचारिक परिपक्वता की भी कमी नहीं है.
आज जहाँ पश्चिम के विषद साहित्य ने भारतीय मानस को झकझोरा है वहीँ पर भारतीय भाषाओँ में कैद ज्ञान भी एक दूसरे के बहुत निकट आया है. दरवाजे अब लोग अपने पड़ोसियों के लिए खोल रहे हैं. फिर भारतीय साहित्य और हिंदी का पूरा परिक्षेत्र भी इससे कैसे अछूता रह सकता है. यदि हम हिंदी आलोचना के प्रथम पुरुषों पर ध्यान दें तो हम पायेंगे कि हिंदी में आलोचना के पुरस्कर्ता आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आरम्भ के सवा सौ पृष्ठों में एक जगह स्त्री प्रसंग की चर्चा की है कि सास-ननद के लाख समझाने के बाद भी स्त्रियाँ कापालिकों के प्रति उसी तरह से आकर्षित होती थीं जैसे कृष्ण के प्रति गोपियाँ. आचार्य के इस मत से कम से कम तीन तथ्यों पर बात होने की गुंजाइश बनती है – स्त्रियों का कापालिकों के प्रति आकर्षण एक समस्या थी. कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम इस कापालिक प्रेम के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया. आकर्षण के बाद इन स्त्रियों का क्या हुआ? सिद्धों की सूची में लगभग सभी प्रमुख इतिहासकारों ने कुछ योगिनियों के नाम दिए हैं. मजेदार बात है कि ये सिद्ध अधिकतर कवि हैं और कोई भी योगिनी कविता करना नहीं जानती. किसी की भी एक पंक्ति उदाहरण के रूप में आज तक सामने क्यों नहीं आई?मूल्यांकन का मसला आरक्षण के मसले की तरह ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है. दरअसल हिंदी के पेशेवर आलोचक की रणनीति और राजनीति महिला लेखन को मुख्यधारा का अविभाज्य अंग मानने से सशंकित हो उठती है. स्त्री रचनाकारों की रचनाओं ने अपनी सहजता, सरसता और शालीनता से एक विशाल पाठक-वर्ग तैयार किया है. यह कोई कम बड़ा योगदान नहीं है.
बड़ी बात यह नहीं है कि आज भी हिंदी पट्टी में स्त्री आलोचना का अभाव है. इधर के कुछ वर्षों में कुछ नई स्त्री आलोचकों का आगमन तेजी से हुआ है या यह कहें कि अमूमन आजकल की आलोचिकाएं मुख्यतः रचनाकार हैं और प्रकरांतर से आलोचना के कार्य में प्रवृत्त हुई हैं. अपितु बड़ी बात यह है की बहुत सारी स्त्री आलोचना पुरुषवादी आलोचना का विस्तार भी है. कथादेश का जून, 2012 का अंक ‘औरत के नजरिये से’स्तंभ में ‘व्याधि पर कविता या कविता की व्याधि’नामक लेख में शालिनी माथुर ने पवन करण की कविता ‘स्तन’ और अनामिका की ‘ब्रेस्ट कैंसर’ को सटीक विश्लेमषण के ऑपरेशन थिएटर में बुद्धि की मेज पर रख अपने अचूक तर्कों के पैने औजारों की मदद से दोनों कविताओं के रोगग्रस्त अंग/अंगों – उपमानों/रूपकों – की सफल शल्यक्रिया कर दी है. इस आलेख ने मानो हिंदी आलोचना में स्वयं तहलका मचा दिया. उन्हीं का ‘तहलका’ में प्रकाशित एक अन्य आलेख ‘मर्दों के खेला में औरत का नाच’ ने भी बहुत सनसनी फैलाई और साथ में समकालीन स्त्री आलोचकों को आगाह भी किया. आलेख कहता है कि स्त्री आज भी सच्चे अर्थों में पुरुष की चेरी मात्र है. हालाँकि यह लेख स्वयं भी विशुद्धतावादी और स्त्री की छवि को एक विशेष घेरे में खड़ा करने वाला ताब पर साथ ही इस आलेख ने पुरुषवादी स्त्रीआलोचना पर जमकर प्रहार किया. इसमें उन स्त्रियों की भी खोज खबर ली गई है जो आज भी पुरुषवादी आलोचना से बाहर नहीं निकल पायीं.अर्चना वर्मा आज की हिंदी आलोचना में एक बड़ा समादृत नाम है. आलोचना और तीखी आलोचना करने वाली अर्चना वैसे तो समग्रतः रचनाकार हैं पर आलोचना में भी उनका कोई सानी नहीं है. उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर स्त्री की एक अलग दुनिया की स्थापना की है. ‘हंस’ में 1986 से लेकर 2008 तक निरंतर संपादन सहयोग रहा है. उनके रचनात्मक साहित्य में कविता संग्रह : कुछ दूर तक, लौटा है विजेता, कहानी संग्रह : स्थगित, राजपाट तथा अन्य कहानियाँ, आलोचना : निराला के सृजन सीमांत : विहग और मीन, अस्मिता विमर्श का स्त्री-विचार आदमी की निगाह में औरत – राजेन्द्र यादव, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य – अर्चना वर्मा, औरत उत्तरकथा – राजेन्द्र यादव के साथ मिलकर उन्होंने बड़ा काम किया है. आज के भी रचना जगत में वे इस फलक को और मजबूत ही कर रही हैं.
व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि स्त्री स्वयं में आलोचकीय प्रतिभा से युक्त होती है. जितना सही और सटीक मूल्यांकन वह कर सकती है वैसा कहीं संभव नहीं है. हिंदी के तथाकथित बड़े विचारक यह मानते हैं हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य को हम लिंग, जाति, समूह में बांटकर नहीं देख सकते. ‘आलोचना और विचारधारा’ सम्पादित डॉ. आशीष त्रिपाठी के माध्यम से नामवर सिंह एक बड़ा प्रश्न उभरते हैं. वे कहते हैं कि ‘ साहित्य में मुख्यधारा जैसी कोई चीज नहीं होती, धाराएँ होती हैं. काशी में मिश्रबंधुओं ने नवरत्नों में कबीर को शामिल नहीं किया था तो क्या हो गया? जिस समय साहित्य में जिस सौंदर्यशास्त्र और आलोचना सिद्धांत का वर्चस्व होता है, वह अपने से अलग साहित्य को हासिये पर डाल देता है.’’ स्त्री ने स्वयं को इतना आबद्ध पाया है कि वह पुरुष के बिना अपना अस्तित्व स्वीकार ही नहीं पाती है. आलोचना करने वालों में रोहिणी हैं, अच्छी आलोचना करती हैं. निर्मला जैन, सुनीता जैन, राजी सेठ हैं, इनकी आलोचना भी आती है. मगर ये मात्र आलोचक नहीं हैं, रचनाकार भी हैं. हिन्दी में किसी रचना की आलोचना उसे खांचों में बांट कर किया जा रहा है. स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श ये और वो, इन्हीं खांचों में रचनाओं को देखा जाता है. दूसरी बात जब महिला रचनाकारों की लेखनी को ही स्वीकृति नहीं मिली तो फिर वे आलोचना के क्षेत्र में कैसे जातीं. उनकी रचनाओं का न तो ढंग से मूल्यांकन होता, न जिक्र होता, न ही किसी तरह का पुरस्कार दे कर प्रोत्साहित किया जाता, तो उनमें आत्मविश्वास कैसे आएगा. अपने लेखन पर उन्हें कैसे विश्वास होगा.
स्त्री अपनी दुर्गति के लिए स्वयं जिम्मेदार है. आज भी हमें ऐसी स्त्रियाँ मिल जायेंगी जो स्वयं को पुरुष से अलगाकर नहीं देखतीं. जैसे वे दो स्वतंत्र नहीं एक शरीर हों. हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान राजेन्द्र यादव लिखते हैं कि ‘ इधर महिला लेखिकाओं की ओर से यह आग्रह बार-बार किया जा रहा है कि उनके लेखन को जनाना या मर्दाना कहकर न अलगाया जाय. लेखक सिर्फ लेखक होता है. उसके साथ महिला विशेषण लगते ही हम उसे ऐसे वर्ग में आरक्षित कर देते हैं जहाँ उसका लेखन ‘ कुछ ऐसा ही’ सा हो जाता है और लिहाज या प्रोत्साहन से देखे जाने वाली वस्तु की गंध देने लगता है…..यानि यह विभाजन एक षड़यंत्र है.’ कहते हैं समय अपने आलोचक स्वयं पैदा करता है. समकालीन रचना विमर्श में यदि रोहिणी अग्रवाल का नाम न लिया जाय तो सब कुछ अधूरा सा रहेगा. रोहिणी अग्रवाल समकालीन हिंदी आलोचना में उभरता हुआ एक दूसरा बड़ा नाम है. खासकर विमर्श और समकालीन हिंदी उपन्यासों पर उनके आलेख बहुत रोचक और ग्रहणीय हैं. वे अपनी बात बहुत अलग ढंग से रखने वाली आलोचक है. कहानी संग्रह : घने बरगद तले, आओ माँ हम परी हो जाएँ. आलोचना : स्त्री लेखन : स्वप्न और संकल्प, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, एक नजर कृष्णा सोबती पर, इतिवृत्त की सरंचना और संरूप (पंद्रह वर्ष के प्रतिमानक उपन्यास), समकालीन कथा साहित्य : सरहदें और सरोकार ‘साहित्य की ज़मीन और स्त्री-मन के उच्छवास’संपादन : प्रतिनिधि कहानियाँ (मुक्तिबोध) आदि. इधर के कुछ वर्षों में रचनाशीलता और व्यावहारिक आलोचना का एक बड़ा नाम है सुधा अरोड़ा. एक औरत की नोटबुक, जिस हिंसा के निशान दिखाई नहीं देते, स्त्री-शक्ति की भूमिका से उठते कई सवाल, आदि कृतियों ने लगातार स्त्री होने के अस्तित्व को चेताया है. अनामिका भी स्त्री विषयों को लगातार अपनी रचनाओं में उठा रही हैं. वे एक कवि ह्रदय के साथ एक समर्थ आलोचिका भी हैं. इधर आई उनकी पुस्तक स्त्रीत्व का मानचित्र – अनामिका ने काफी ख्याति अर्जित की है. हाँ कभी कभी वे अपनी आलोचना में उस पुरुष वादी परंपरा का नकार नहीं कर पातीं.डॉ. सुमन राजे लिखती हैं कि ‘समकालीन समीक्षा में डॉ. निर्मला जैन का नाम उल्लेखनीय है. यद्यपि ‘रस सिद्धांत और सौंदर्यशास्त्र’ उनकी डीलिट की थीसिस है, परन्तु तुलनात्मक सैद्धांतिक समीक्षा की एक दुर्लभ कृति है. आगे चलकर लेखिका ने मुख्यरूप से नयी समीक्षा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया. नाट्य समीक्षा के सन्दर्भ में डॉ. गिरीश रस्तोगी का नाम महत्वपूर्ण है. उन्होंने एक सीमित क्षेत्र का चयन करके उसपर जमकर लिखा है.’’ इस क्षेत्र में स्वयं सुमन राजे का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है. उनकी पुस्तक ‘ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास’ ने स्वयं एक इतिहास की रचना की. उन्होंने अपने पुस्तक में स्त्री इतिहास के उन पन्नों को उजागर किया जो आजतक कहीं दबकर रह गए थे.
इक्कीसवीं सदी के आगमन के साथ हिंदी आलोचना में दलित आदिवासी आलोचकों की आमद बढ़ी है. वे विमर्श के सरोकारों को तो उठा ही रही हैं साथ ही हिंदी आलोचना के प्रतिमानों को नकार कर नए प्रतिमानों का गठन भी कर रही हैं. आदिवासी साहित्य की नामचीन रचनाकार रोज केरकेट्टा कहती हैं ‘स्त्री को स्कूल के दिनों में ही हमें संक्षेपण करना सिखाया जाता है. स्त्रियों के बारे में समाज भी हमें ऐसा नजरिया देता है. हम जीवन के हर क्षेत्र में स्त्रियों का संक्षेपण करते हैं. हमारा लेखन ऐसे संक्षेपण के खिलाफ है’. उनकी नई किताब ‘स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति’इसी स्थापना का विश्लेषण है.अभी हाल ही में ‘स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति’ का लोकार्पण झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा द्वारा रांची के सूचना भवन सभागार में आयोजित किया गया था. पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के तीन पीढ़ी की प्रमुख स्त्री लेखिकाओं ने सामूहिक रूप से किया. समारोह में झारखंड के बौद्धिक समुदाय सहित युवाओं ने अच्छी-खासी भागीदारी थी. ‘पुरुष जगत में बराबरी का दर्जा मांगती स्त्री-लेखिकाएं और अधिकांश नामवर समीक्षक मासूम विनोभाई वक्तव्य देकर तालियाँ बटोरते हैं कि लेखन में स्त्री पुरुष विभेद गलत है: रचना सिर्फ रचना है. ईमानदारी से कहा जाय तो यह समानता बारीक पुरुष साजिस है.’
भारतीय भाषाओं में दलित स्त्री लेखन को रूपाकार लिए हुए दो दशक से ज्यादा गुजर चुके हैं. यह पूरा दौर दलित स्त्रीवादी कार्यकर्ताओं, रचनाकारों के लिए कठिन संघर्षों का रहा है.दलित स्त्रीवादी आन्दोलन का जन्म भले ही अस्मितावाद की जमीन पर हुआ मगर जल्दी ही इस आन्दोलन ने अपने को अस्मितावाद की अनुदार चौहद्दी से मुक्त कर लिया.अब यहाँ दलित स्त्रीवाद की आलोचना का भी जन्म हो रहा है.गंभीर अध्येता और चिंतक अनीता भारती की रचनाएँ उनके वैचारिक संघर्ष का ही हथियार है. यहाँ वही जद्दोजेहद और उत्पीडक सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ वही क्रोध से भरा, लेकिन तार्किक प्रतिरोध है जो उनके गद्य में दिखता है. अभी हाल ही में दलित स्त्रीवाद पर अनीता भारती की महत्वपूर्ण पुस्तक ‘समकालीन नारीवाद और दलित स्त्री का प्रतिरोध” पुस्तक आई है., स्त्रीकाल पत्रिका का “दलित स्त्रीवाद” पर विशेषांक ने भी स्त्री आलोचना को नया आयाम दिया है.‘स्त्रीकाल’ पत्रिका और उसके संपादक लगातार स्त्री आलोचकों को एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं. हां जहाँ अभी तक शून्य पसरा हुआ था वहीँ पर सैकड़ो स्त्री रचनाकार अपनी रचनाओं, विमर्शों और आलोचना से हिंदी साहित्य को अनवरत समृद्ध कर रही है.











