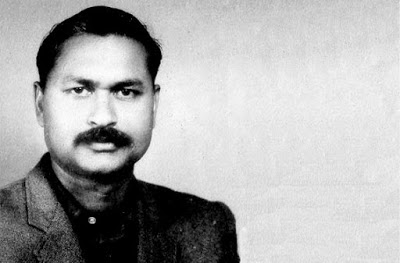हिन्दी विश्वविद्यालय में स्त्री अध्ययन विभाग में प्रोफ़ेसर. सम्पर्क : ई मेल- shambhugupt@gmail.com, मोबाइल: 8600552663
हिन्दी विश्वविद्यालय में स्त्री अध्ययन विभाग में प्रोफ़ेसर. सम्पर्क : ई मेल- shambhugupt@gmail.com, मोबाइल: 8600552663
सेक्सिज़्म भाषा के ढाँचे में नहीं, तत्वतः लेखक के अन्तर्मन में होता है
पहली क़िस्त पढने के लिए लिंक पर क्लिक करें :
धूमिल और स्त्री : अर्थात् वक़्त की चैकी पर बैठा अधेड़ मुंशी: पहली क़िस्त
देखने की बात यहाँ यह है कि लोहिया ऐसा तब लिख रहे हैं जब कि स्वदेशी भाषा (हिन्दी) और संस्कृति से उन्हें बेइन्तहा प्यार है और किसी भी हद तक वे उसके समर्थक हैं। उनका तर्क है कि दिल्ली जो ‘‘विश्व-इतिहास की अत्यंत हृदयहीन वेश्या’’ बनी है तो ‘‘इसका सबसे बड़ा कारण भाषा की शक्ति रहा है। किसी भी राजधानी ने इतने लंबे समय तक विदेशी और सामंती भाषा में काम नहीं किया है। गगग वेश्या आम जनता से एक हद तक ही संबंध रखना चाहती थी और इसलिए उसने अपना काम ऐसी भाषा में चलाया जिसे जनता नहीं समझती थी।’’ (राममनोहर लोहिया रचनावली, भाग-8, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि. नई दिल्ली (प्र. सं. 2008), पृ. 194)। अन्तर्वस्तु के लिहाज़ से तो लोहिया यहाँ एकदम चैकस हैं। लेकिन जो उपमान-विधान उन्होंने बनाया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। क्या किसी और उपमान द्वारा यह बात नहीं कही जा सकती थी? और फिर यह भी क्या ज़रूरी है कि बात को किसी अप्रस्तुत-विधान में ही कहा जाए? बात को सीधे-सीधे वर्णनात्मक या अनलंकृत तरीक़े से भी तो कहा जा सकता है। यह कथित काव्यात्मकता ज़बर्दस्ती घुसेड़ने की ज़रूरत भला क्या है? जो हो। लेकिन लोहिया यहाँ पकड़े जाते हैं। एक और बात जो संज्ञान में आती है वह यह है कि लोहिया जब कि स्वदेशी और आम जनता की भाषा में यह सब लिख रहे थे तो स्वदेशी भाषा से काम लेने पर भी यह सैक्सिस्ट उपमान-विधान कहाँ से चला आया? क्या सैक्सिज़्म स्वदेशी भाषा की अन्तस्संरचना में निहित है? आखि़र अनजाने या अचेत भाव से ही सही, पुरुष लेखक की रचनाओं में यह यौनवाद आता कैसे है? क्या यह यों ही स्वभावतः चला आता है? क्या हमारी भाषा की संरचना ही पक्षपातपूर्ण है? अभयकुमार दुबे ने अपने उसी लेख में एक जगह लिखा है ‘‘(क्योंकि उसका मैस्क्युलिन जेंडराइज़ेशन या मर्दानाकरण पहले ही हो चुका है) गगग स्त्री के पक्ष में सोचते और लिखते समय भी अगर सतर्क न रहा जाए तो मर्दाने लिंग में ढली भाषा ही स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है।’’ (वही, पृ. 405 एवं 406)। मेरा ख़याल है कि सारा का सारा दोष भाषा के मत्थे मँढ़ देना एक उचित तार्किकता नहीं है। यह ठीक है कि भाषा मूलतः मर्दाने लिंग में ढली है, वह स्त्री के प्रति दुराग्रहों से भरी है लेकिन यह भी देखा ही तो जाता है कि इसी भाषा में अनेकानेक पुरुष-लेखकों ने स्त्री को पूरा सम्मान और स्पेस देते हुए अपनी रचनाएँ लिखी हैं। निश्चय ही यहाँ उन्हें बेहद सतर्क रहना पड़ा होगा और कोई वैकल्पिक जेंडर-न्यूट्रल या जेंडर समानतामूलक भाषा विकसित की होगी। इसका एक अर्थ यह भी है कि दरअसल सैक्सिज़्म व्यक्ति के अन्तर्मन में निहित होता है। मर्दाने लिंग में ढली भाषा तभी उसे स्वाभाविक लगेगी, जब वह ख़ुद मर्दाना यौन-मानसिकता में ढला होगा। सैक्सिज़्म की जड़ इसी मानसिकता में धँसी होती है। किसी की भाषा तभी सैक्सिस्ट होती है जब उसकी मानसिकता पर सैक्स हावी हो। अतः यह क़तई नहीं माना जा सकता कि कोई पुरुष है तो वह स्त्री के प्रति यौनवादी होगा ही और कोई स्त्री है तो वह पुरुष के प्रति यौनवादी होगी ही। इसे इस तरह सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। देखना यह होगा कि अपनी वस्तु, अन्तर्वस्तु और अभिव्यक्ति तीनों में वह जेंडर के हिसाब से सतर्क और समतामूलकतावादी है या नहीं! क्या लोहिया मर्दाना यौन-मानसिकता में ढले थे? जो हो।
वक़्त की चैकी पर बैठा (और निष्क्रिय) अधेड़ मुंशी
इस सैद्धान्तिकी के आलोक में धूमिल की कविता पर विचार करने पर हम पाते हैं कि उनमें बहुत सारी चीजें गड्डमड्ड हैं। वे, जैसा कि कहा गया, अपनी वस्तु और अन्तर्वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए स्त्री-देह के अंगों, उसकी जैविक कार्य-प्रणाली, विभिन्न गतिविधियों इत्यादि को उपमान के रूप में स्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे अपनी बात ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कह पा रहे हैं। धूमिल के इस विशिष्ट शिल्प-विधान के उत्स पर बात की जाए तो इसका असल स्रोत वही है जिसकी ओर विद्यानिवास मिश्र ने संकेत किया था; जिसका कि ऊपर उल्लेख किया गया; हालाँकि एकदम उस अर्थ में नहीं, जिसका तर्क उन्होंने दिया है। विद्यानिवास मिश्र का तर्क था कि ‘‘गगग धूमिल के गाँव वाले मन को बात सीधी तौर पर कहने के लिए लाचारी से इतना आक्रामक होना पड़ा है। गगग जो कवि फरेब से, हर तरह के फरेब से एकदम अफना गया हो वह शहरी नारी गरिमा के फरेब को भी दूर फेंक देता है, गगग’’। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, विद्यानिवासजी का कहना था कि ‘‘शायद उसका उत्साह विस्थापित है’’ लेकिन उनका यह भी कहना था कि ‘‘उसका ईमान अपनी जगह पर है’’। (सुदामा पाँडे़ का प्रजातन्त्र, पृ. 12)। इस तर्क-शृंखला पर विचार किया जाए तो एक अज़ीबोग़रीब विमर्श पैदा होने लगता है। विद्यानिवास यह तो मानते हैं कि यह नारी-गरिमा के खि़लाफ़ बात है। लेकिन साथ ही यह भी जोड़ देते हैं कि शहरी नारी ही इस तरह की बातों पर उज्र करती है, देहाती औरतों को इससे कोई परेशानी नहीं है। विद्यानिवासजी का आखि़र मन्तव्य क्या है? क्या वे यह कहना चाहते हैं कि इस तरह की बातों पर ऐतराज़ करना एक तरह का फरेब है और चूँकि देहाती स्त्रियाँ तो सीधी-सादी होती हैं, फरेब शहरी औरतों का ही चरित्रोपलक्षण है अतः वे ही इन पर आपत्ति करती देखी जाती हैं? यानी कि यह जो धूमिल या कोई भी लेखक स्त्री को अपनी अन्तर्वस्तु के उपनिवेश या उपमान या अप्रस्तुत-विधान के रूप में स्तेमाल करता है, वह शहरी स्त्रियों को ही चुभता है, ग्रामीण स्त्रियाँ तो यह सब न तो जानती हैं और जानती भी हों तो उनके लिए यह कोई आपत्ति या आश्चर्यजनक बात नहीं है, यह लगभग उनके रोज़मर्रा जि़न्दगी का हिस्सा है, अत्यन्त स्वाभाविक और सहज उपक्रम है! विद्यानिवास मिश्र के विषय में यह कहा जाता है कि वे अत्यन्त ही लोकवादी थे, लोक/ग्राम्य जीवन में उनकी आत्मा बसती थी। पता नहीं यह कैसा लोकवाद है जो स्त्री को इस क़दर डि-ग्रेड करके चलता है। और फिर यह मानना कि धूमिल या किसी और ने जो किया, वह उसकी गरिमा के खि़लाफ़ नहीं है और वह उसे सह्य है, पूरी तरह पुरुष-मन की गढ़न्त है। स्त्री के बारे में यह पुरुष-मानसिकता का इकतरफ़ा फ़ैसला है। चूँकि गाँव में अभी भी, और आज से चालीस साल पहले तो- जब धूमिल यह सब लिख रहे थे- और भी ज़्यादा सामन्ती माहौल था अतः स्त्री के पास चुप रहने के अलावा और क्या चारा था! इस चुप्पी को उसकी स्वीकृति और यहाँ तक कि गरिमा कहकर परिभाषित करना हद दजेऱ् की चालाकी (अगर कोई ‘धूर्तता’ शब्द को गै़र-साहित्यिक मानने पर कटिबद्ध न हो तो दरअसल धूर्तता) है। विद्यानिवास मिश्र की यह तार्किकता धूमिल को कठघरे से निकालने के बज़ाय और गहरे उसमें धँसा देती है। हो सकता है, धूमिल का ईमान अपनी जगह पर हो और इसके महत्व से किसी को इनकार भला क्यों होगा? लेकिन एक ईमान की आड़ में दूसरी बेईमानी करने की इज़ाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती। जिस तरह से धूमिल स्त्री को लाते हैं, उसके आधार पर निर्विवाद रूप से यह कैसे कहा जा सकता है कि धूमिल के काव्य में काम नहीं है, या कामुकता के प्रति वितृष्णा है? स्त्री सम्बन्धी यौन-बिम्ब क्या काम-भावना के बिना आ सकते हैं। ऊपर लोहिया के सन्दर्भ से यह स्पष्ट किया गया कि इस तरह के बिम्ब या प्रतीक या उपमान तभी आते हैं जब मन पर सैक्सिज़्म हावी होता है। जब मन में स्त्री को लेकर लगभग इसी तरह का चिन्तन-अनुचिन्तन चलता रहता है। ग्रामीण सांस्कारिकता के साथ तो इस मामले में और भी दिक़्कत है क्योंकि उसमें सामन्ती तत्व किसी न किसी रूप में लगातार मौज़ूद रहते हैं। विद्यानिवासजी कहते हैं कि यह कवि फरेब से, हर तरह के फरेब से अफना गया था इसलिए लाचारी में आक्रामक हुआ। लेकिन आक्रामक होने के लिए स्त्री का इस तरह यौनवादी स्तेमाल क्यों? क्या इसलिए कि वह उस समय इस स्थिति में नहीं थी कि आपकी क़लम पकड़ सके और कहीं मिल जाएँ तो आपका भी वही हाल करे जो इधर कुछ स्त्री को निशाना बनाने वाले लेखकों का हुआ। यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनसे सब परिचित हैं। आज तो हालत यह है कि अभी म. गां. अं. हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के ‘हिन्दी का दूसरा समय’ (01-05 फरवरी 2013) के मीडिया वाले सारांश सत्र में एक वक्ता ने जब धूमिल के इस जुमले का किसी प्रसंग में इस्तेमाल किया कि ‘जिसकी पूँछ उठाई, वही मादा निकला’ (‘‘मैंने जिसकी पूँछ उठायी है उसको मादा पाया है।’’-संसद से सड़क तक, पृ. 126) तो विरोध की ऐसी लहर उठी कि वक्ता को तत्काल अपने शब्द वापस लेने पड़े। आज धूमिल की कैसी भी पुनव्र्याख्या कर ली जाए, यह कलंक उन पर लगेगा ही। और फिर उस समय भी क्या और दूसरे कवि नहीं थे, जो फरेब से एकदम अफना गए थे; जैसे कि मुक्तिबोध या रघुवीर सहाय या और बहुत-से अन्य कवि, जिनके यथार्थानुभवों में कई समानताएँ भी हैं, जैसे कि ‘पटकथा’ का यह अंश, जिसकी तुलना मुक्तिबोध की कविता ‘अँधेरे में’ (मुक्तिबोध, ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’/भारतीय ज्ञानपीठ) के प्रोसेशन में शामिल विभिन्न सत्तोन्मुख षड्यन्त्रकारियों से की जा सकती है: ‘‘वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषिये हैं।/वे वकील हैं। वैज्ञानिक हैं।/अध्यापक हैं। नेता हैं। दार्शनिक/हैं। लेखक हैं। कवि हैं। कलाकार हैं।/यानी कि-/कानून की भाषा बोलता हुआ/अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है।’’ (वही); इन लोगों का उपमान-विधान स्त्री के यौनिक स्तेमाल से कैसे बचा? क्या इनके सामने भी एकदम वही परिदृश्य नहीं था? आखि़र धूमिल और उनके जैसे कुछ और कवियों को ही स्त्री-देह इतना परेशान क्यों किए थी? इसका उत्तर सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि यह दरअसल स्त्री के बाबत हमारी कुल मानसिकता से ही तय होता है कि हमारे लिखे में वह कैसे आएगी और आएगी भी या नहीं? आलोचकों ने धूमिल का बचाव करते हुए और उनकी दूसरी-दूसरी कविताओं का हवाला देते हुए यह सिद्ध करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है कि स्त्री के प्रति धूमिल की दृष्टि वस्तुवादी नहीं है, उनका यह कथन कि औरत एक देह है, ‘‘उपभोक्तावादी सोच से अलग है। जहाँ स्त्री-शरीर एक माल है, वस्तु अथवा माल बेचने का औजार’’ (श्रीराम त्रिपाठी, धूमिल और परवर्ती जनवादी कविता, रंगद्वार प्रकाशन अहमदाबाद/द्वितीय संस्करण, 2002; पृ. 66)। इस सन्दर्भ में धूमिल की ‘नौ मादा कविताएँ’ शृंखला की आठवीं कविता ‘स्त्री’ का हवाला दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर धूमिल विज्ञापन में स्त्री के इस्तेमाल पर टिप्पणी करते हैं। (वही; पृ. 67)। यह तो किसी हद तक ठीक है। लेकिन इससे पहले की इन आप्तवाक्यमूलक पंक्तियों की व्याख्या कैसे की जाएगी जिनमें धूमिल वक्तव्य देते हैं कि-
मुझे पता है
स्त्री-
देह के अँधेरे में
बिस्तर की
अराजकता है।
(सुदामा पाँडे़ का प्रजातन्त्र, पृ. 130)।
क्या यह वक्तव्य स्त्री के बारे में किसी पुरुष का इकतरफ़ा अभिमत नहीं है? यह ठीक है कि इस तरह के विचार-निर्णय के मूल में कवि का आम तौर पर अनुभव किया हुआ यथार्थ और उसका सामान्य पर्यवेक्षण होता है लेकिन देखने की बात यही तो होती है कि कवि अनुभव की हुई बातों को ज्यों का त्यों उल्था कर दे रहा है या उसमें अपनी अन्तर्दृष्टि के कुछ सूत्र भी मिलाकर उसे कोई सम्भावनाशील मोड़ दे दे रहा है या नहीं। कवि की अन्तर्दृष्टि की पहचान और परीक्षा दरअसल इसी बिन्दु पर होती है कि यथार्थ को कोई नया अग्रगामी आयाम वह दे रहा है या नहीं? इस दृष्टि से धूमिल पर विचार करते हैं तो और भी ज़्यादा निराशा होती है क्योंकि प्रतीत यह होता है कि धूमिल समकालीन राजनीति, राज्य-व्यवस्था, उससे जुड़े लोगों, उनकी गतिविधियों और इस सबसे बने परिदृश्य की घनघोर आलोचना करते हैं, उस पर बहुत ही तीखी, चुनौतीपूर्ण और काटकर रख देने वाली टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन ख़ुद कहीं किसी अँधेरे में खड़े कहीं से रोशनी चले आने का इन्तज़ार-भर करते रहते हैं और इस पर तुर्रा यह कि इसे वह ‘सहज’ होना भी कहते हैं-
मैं यहाँ, इस अँधेरे में खड़ा हूँ।
यहीं,
मेरे देश ने
मुझे रोशनी देने को कहा है। (सुदामा पाँडे़ का प्रजातन्त्र, पृ. 61-62)।
देखा जा सकता है कि देश यहाँ किस तरह अमूर्तता ग्रहण करता जाता है। इसमें कोई शक़ नहीं कि एक व्यक्ति/कवि के तौर पर धूमिल यहाँ व्यवस्था का दंश झेलने को तत्पर हैं लेकिन जबकि आप एक चेतना-सम्पन्न कवि हैं, लोग आपकी तरफ़ एक अन्तर्दृष्टि के लिए टकटकी लगाए खड़े हैं; आप इससे आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं दिखाते-
वक्त की चैकी पर बैठे हुए अधेड़
मुंशी की तरह
मैं अपने बहते हुए खून में
तुम्हारे दाँतों की रपट पढ़ता हूँ। (वही, 62)।
भगतसिंह पैदा तो हो, लेकिन पड़ौसी के घर में!
धूमिल की विशेषता यह है कि वे जो कुछ देखते हैं, उसे अन्दर तक अनुभव करते हैं। उनके आत्मानुभव और यथार्थ की वास्तविकता लगभग एक है, उसमें कोई विभेद नहीं है। यथार्थ की वास्तविकता और उसके उनके अनुभव के बीच कोई तीसरी चीज नहीं है। इसीलिए दरअसल ऐसा हुआ है कि वे आम को आम और चाकू को चाकू कह सके हैं। आम को आम और चाकू को चाकू कह सकना एक कवि की सबसे बड़ी सहजता कही जा सकती है-
मैं चाहता हूँ मैं वह सब कुछ
अनुभव करूँ जो कुछ देखता हूँ।
मैं साहस नहीं चाहता
मैं सहज होना चाहता हूँ
ताकि आम को आम
और चाकू को चाकू कह सकूँ! (वही, 61)।
आम को आम और चाकू को चाकू कह सकना उस समय आसान नहीं था और समय की यह एक भारी ज़रूरत थी। यह एक चुनौती थी जिसे धूमिल ने न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे एक उल्लेखनीय मुक़ाम तक पहुँचाया भी। लेकिन कवि की सहजता के अन्तर्गत यह भी आता है और नहीं आता तो आना चाहिए कि उसके पास आने वाले समय का, समय की सम्भावनाओं का एक नक़्शा/ब्लू प्रिंट भी हो। धूमिल यहाँ मात खाते हैं। वे लगभग इस शैली में बात करते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन मेरे नहीं, पड़ौसी के घर में! वे ख़ुद कुछ पहल करने की स्थिति में नहीं हैं, सिर्फ़ दूसरों को ललकारने में उनकी शक्ति लगी रहती है-
गगग अपनी दुविधाओं में
लहूलुहान एक गद्दीनशीन औरत
टाँगों में धमाका दबाए बैठी है
और सारा हिन्दुस्तान
जबड़े में भिंची हुई
कलेजी की तरह बमक रहा है
क्या तुम निहत्थे हो? (वही, 68)।
जैविक तत्ववाद का ज़बर्दस्त अभ्यास अर्थात् धूमिल का सैक्सिस्ट देहाती माइंड-सेट
इस कविता में धूमिल नक्सलवाद के न केवल समर्थक/सिम्पैथाइज़र, बल्कि एक निगूढ़ प्रवक्ता की तरह पेश आते हैं। बाद की उनकी बहुत-सी कविताओं में उनका यह रूप हमें देखने को मिलता है। आलोचकों ने उनके इस पक्ष की सराहना भी ख़ूब की है। लेकिन मेरा ऐसा ख़याल है कि धूमिल में नक्सलवाद एक आवेगी वैचारिकता की तरह आयत्त होता है। मूलतः वैचारिकता आवेगी नहीं होती, उसका स्वरूप चिन्तनपरक और दर्शनात्मक ही होता है। लेकिन धूमिल चूँकि आधारभूत रूप से एक आवेगी कवि हैं अतः अन्य विचारों के साथ नक्सलवाद भी एक आवेग की तरह ही उनकी कविताओं में आता है। यह आवेगशीलता बहुत आकर्षक और टटकी है तो इसके कई पाश्र्व ऐसे भी हैं जो सारे किए-कराए पर पानी फेर देते हैं। जैसे कि यदि इसी अंश में देखा जाए तो जिस ‘औरत’ का जि़क्र यहाँ किया गया है, वह औरत बाद में है, एक डरा हुआ तानाशाह पहले, बल्कि मूलतः है। यह कोई पुरुष भी हो सकता था। जिस औरत का जि़क्र यहाँ है, वह अपने औरतपन से काफ़ी पहले पीछा छुड़ा चुकी थी और अब वह सिर्फ़ एक शासक-वर्ग की नेता थी। भारतीय राजनीति का यह समय बहुत ही नाकस रहा है। लोकतन्त्र के संसाधनों से ही लोकतन्त्र के संसाधनों को ही जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया, वह अपने-आप में एक हौलनाक परिदृश्य था। इस स्थिति पर हिन्दी के उस समय के बहुत-सारे कवियों-लेखकों ने क़लम चलायी। बाबा नागार्जन की कविताएँ इस सन्दर्भ में याद की जा सकती हैं। लेकिन धूमिल ‘औरत टाँगों में धमाका दबाए बैठी है’ जैसा सैक्सिस्ट बिम्ब लाकर सारा ध्यान दूसरी जगह भटका देते हैं। पाठक चाहे स्त्री हो या पुरुश, उसका ध्यान सबसे पहले इसी जगह जाता है और अटका रह जाता है। ‘सारा हिन्दुस्तान जबड़े में भिंची हुई कलेजी’ के बिम्ब में जो तेजी, तुर्शी और प्रहारात्मकता थी, उसे इस यौनवादी बिम्ब ने मटियामेट कर दिया और पाठक भौंचक देखता रह जाता है कि कवि ने आखि़र यह किया क्या? इसके अलावा एक बात यह भी उसके दिमाग़ में आती है कि नक्सलवाद की कवि की यह कैसी समझ है कि वह एक राजनीतिक तानाशाह को जैविक तत्ववाद की निगाह से देख रहा है! धूमिल इस जैविक तत्ववाद के इतने ज़्यादा अभ्यस्त हैं कि लगभग हर जगह यह एक स्वाभाविक संस्कार की तरह उनके सिर चढ़कर बोलने लगता है। यह दरअसल स्त्री के प्रति एक ख़ास कि़स्म का देहाती ‘माइंड-सेट’ है, जो सैक्सिस्ट है, सैक्स से शुरू होकर सैक्स पर ही ख़त्म होता है। यहाँ यह सवाल नहीं है कि जैसा कि विद्यानिवासजी ने बहस उठाई थी कि धूमिल के काव्य में काम है कि नहीं है या कामुकता के प्रति वितृष्णा है या नहीं है। हो सकता है कि वहाँ काम न हो, कामुकता के प्रति गहरी वितृष्णा हो; लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता है कि आप लगातार यौन-प्रतीक और बिम्ब लाएँ और कहें कि नहीं, कामुकता से इसका कोई लेना-देना नहीं। हो सकता है कि आपका न हो, लेकिन पाठक तो पाठ और भाषा से ही आप तक पहुँचेगा, क्या आप उसे मना करने आएँगे कि भाई, इसका यह अर्थ मत लेना जो यहाँ निकल रहा है, बल्कि मैं बताउँगा कि क्या अर्थ लेना है! लेकिन यह सब दरअसल एक ख़ामख़याली है। असल बात यह है कि कवि ख़ुद यह चाहता है कि इसका यही अर्थ लिया जाए! वह स्वयं यथार्थ को इस तरह पेश कर रहा है कि वह इतना ही अश्लील और भदेस है, जितना उसका यह उपमान! इस पर ऊपर हमने बात की। यानी कि कवि मूलतः यह मानता है कि स्त्री पर्याय है यौन का और यौन का अर्थ है, अश्लीलता! इस तरह दुनिया-भर का सारा बोझ आप औरत के कन्धों पर डाल देते हैं और उस पर अबोधता यह कि आप कहते हैं कि मैं तो कामुकता से कोसों दूर हूँ। होंगे आप दूर, व्यक्तिगत तौर पर आप काम से परहेज़ भी करते होंगे लेकिन आपका अन्तर्मन तो वहीं चक्कर काटता रहता है, जब भी आप कुछ लिखने का मन बनाते हैं, आपका यह अन्तर्मन आपकी अभिव्यक्ति पर क़ब्ज़ा कर लेता है। धूमिल का यह दरअसल सबसे बड़ा अन्तर्विरोध है कि वे ख़ुद कामुकता से बहुत-बहुत दूर हैं लेकिन उनकी कविता बरबस इसी में अपनी सार्थकता तलाशती है। निश्चय ही, जैसा कि मैंने कहा, यथार्थ-निरूपण की कवि की क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है, पर यह यथार्थ विरूपित और अन्यथाकृत होकर पाठक तक पहुँचता है। जहाँ धूमिल स्त्री को उपमान की तरह नहीं लाते, उसका वस्तुकरण नहीं करते, उसे एक जीते-जागते अस्तित्ववान व्यक्ति के रूप में/मुख्य विषयवस्तु के रूप में लाते हैं, वहाँ वे बहुत ही संयत और दृष्टि-सम्पन्न रूप में सामने आते
हैं।
धूमिल की काव्य-प्रविधि अर्थात् प्रकरी-पताका रूप में स्त्री
धूमिल के पास ऐसी बहुत-सी कविताएँ हैं, जिनमें स्त्री एक स्वायत्त काव्यवस्तु के रूप में आती है। धूमिल ने आधारभूत रूप में भी इस काव्यवस्तु को लिया है और इस पर केन्द्रित कुछ स्वतन्त्र कविताएँ लिखी हैं। इसके अलावा अन्य विषय-सन्दर्भ-केन्द्री कविताओं में भी प्रसंगवश इस मुद्दे को लिया है और नायाब टिप्पणियाँ की हैं। इनमें एक अतिमहत्वपूर्ण विषय तो यही है कि भारतीय-विशेषतः हिन्दू-समाज में औरत की वास्तविक स्थिति क्या व कैसी है। इस मामले में धूमिल एकदम बेबाक और दो-टूक हैं। इस मामले में वे किसी को नहीं बख़्शते; यहाँ तक कि ख़ुद को भी, अपने कथित पुरखों को भी, समाज के ठेकेदारों को भी। ‘नौ मादा कविताएँ’ की पाँचवीं कड़ी ‘पाँचवें पुरखे की कथा’ में वे लिखते हैं-
उनके लिए पूजा-पाठ:
केवल ढकोसला था
ऐसे अहिंसक कि-
उनकी बन्दूक में
बया का घोंसला था
ऐसे थे संयमी कि-
औरत जो एक बार
जाँघ से उतर गई
उनके लिए मर गई
चतुरी चमार की
लटुरी पतौह को (सुदामा पाँडे़ का प्रजातन्त्र, पृ. 124)।
यहाँ जाति और जेंडर के अन्तर्सम्बन्ध देखे जा सकते हैं, जहाँ दलित जातियों की स्त्रियाँ सदियों से कथित उच्च वर्ण-विशेषतः ब्राह्मण-के पुरुषों के निशाने पर रहती आई हैं। इसी तरह वर्ग और जेंडर के अन्तर्सम्बन्धों का खुलासा इन पंक्तियों में होता है-
यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा
उस महरी की तरह है, जो
महाजन के साथ रात-भर
सोने के लिए
एक साड़ी पर राज़ी है (संसद से सड़क तक, पृ. 13)।
यहाँ बेशक़ धूमिल उपमान-विधान में सैक्सिस्ट हैं और व्यंग्य की उनकी धार नैगेटिव है क्योंकि यह महरी एक साड़ी के एवज़ में यह सब करने के लिए ख़ुद राज़ी नहीं है, उसके सामने ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की गई हैं कि ऐसा करने के लिए वह विवश है। कोई भी स्त्री यदि उसके सामने कोई और विकल्प होता है तो इस विकल्प को कदापि नहीं चुनती। वह ख़ुद राज़ी है, यह कहने का अर्थ तो यह होता है कि इस तरह बिक जाना स्त्री-मात्र की आम प्रवृत्ति है और वह मूलभूत रूप से ऐसी होती है। धूमिल अन्यत्र कहीं ऐसा कहते भी हैं। बावज़ूद इस सब के यह बिम्ब-जिसे कि यहाँ उपमान के रूप में लाया गया है-महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय इसलिए है कि इसके मार्फ़त धूमिल अपने अनजाने स्त्री-सम्बन्धी एक भीषण यथार्थ को उजागर कर सके हैं। जैसी कि धूमिल की काव्य-प्रविधि है, स्त्री का यह यथार्थ उनका मूल कथ्य नहीं है, यह एक प्रकरी-पताका ही है, लेकिन जिस रूप में भी है, वस्तुगत रूप से हमारे काम का है।
धूमिल का प्रिय विषय: दाम्पत्य अर्थात् अतृप्त यौन-संवेदना का परावर्तन
आम हिन्दू दाम्पत्य पर धूमिल की काव्यात्मक टिप्पणियाँ इतनी मारक और काटकर रख देने वाली हैं कि ताज़्ज़ुब होता है कि यह कवि इन अनुभवों को कहाँ से लाया! हो सकता है, इनमें उनके अपने व्यक्तिगत जीवनानुभव भी शामिल हों। और न भी हों तो इतना तो निश्चित है कि कवि की पर्यवेक्षण-शक्ति इतनी तीव्र और मर्मभेदी है कि वह सिर्फ़ असलियत को निकालकर बाहर लाती है। हिन्दी के आम कवि की तरह दाम्पत्य के इर्द-गिर्द वह कोई ग्लैमर-जिसे दरअसल घटाटोप कहना चाहिए-, नहीं बुनता बल्कि इतने निर्मम और बेलौस तरीक़े से उसे तार-तार करता है कि सहसा विश्वास नहीं होता कि अपने स्थापत्य में स्त्री को खिलौने की तरह बरतता यह कवि उसके प्रति हद दजऱ्े तक सहानुभूतिशील भी है। उसका लगभग यह स्पष्ट और अन्तिम निष्कर्ष है कि भारतीय दाम्पत्य-व्यवस्था में स्त्री के लिए कोई स्वतन्त्र-स्वायत्त स्पेस नहीं है। विद्यानिवास मिश्र की तरह उनके बारे में यह क़तई नहीं कहा जा सकता कि धूमिल के काव्य में काम नहीं है या कामुकता के प्रति गहरी वितृष्णा है। धूमिल के काव्य में काम-भावना है और बहुत ही सघन और प्रकृष्ट रूप में है। कामुकता-दरअसल इसे यौनिकता कहना चाहिए-भी ख़ूब है। हाँ, कह सकते हैं कि लम्पटता नहीं है। नारी की गरिमा जैसे मुहावरे का यहाँ कोई अर्थ नहीं है बल्कि यह वस्तुस्थिति को बरगलाने/अन्यथाकृत करने का एक उपागम है। इसके पीछे मर्दवादी मानसिकता की बू आती है। जो हो। हमें कहना यहाँ यह है कि धूमिल दाम्पत्य में स्त्री की दोयम दजऱ्े की स्थिति से बेहद चिन्तित और परेशान दिखाई देते हैं। वे बार-बार यह दिखाते हैं कि समाज ने औरत की यह क्या हालत कर रखी है कि न वह इधर की है न उधर की। न उसे एक पत्नी के रूप में ही ठीक से रहने दिया गया है, न एक माँ के रूप में ही। एक स्त्री के रूप में तो ख़ैर ठीक से रहने का सवाल ही कहाँ उठता है! हर तरफ़ से जि़न्दगी-भर वह बेहद दबाव में रहती आती है।
धूमिल ने स्त्री को जो अपने अप्रस्तुत-विधान के एक अवयव के रूप में लिया है तो इसकी एक ध्वनि यह भी है कि भारतीय समाज में औरत की हैसियत एक ‘अप्रस्तुत’ की तरह ही है, वह समाज का केन्द्रीय सन्दर्भ नहीं है, मुख्यधारा में नहीं है। ध्यान रहे कि हम कविता में एक अप्रस्तुत की तरह स्त्री के स्तेमाल के औचित्य पर विचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ धूमिल के सन्दर्भ में उसकी कैफि़यत की सम्भावनाओं पर बात कर रहे हैं। धूमिल को यह दुनिया जैसी मिली, उसमें उसने कोई तब्दीली नहीं की, तब्दीली करने की इच्छा उसकी रही होगी लेकिन उसने ख़ुद को इस पर रिएक्ट करने, इसकी लानत-मलामत करने, इसकी बखिया उधेड़ने तक सीमित रखा; यह ऊपर हम कह चुके हैं। यह काम भी हालाँकि कोई कम महत्व का नहीं था। यह काम समय की ज़रूरत थी। धूमिल की उल्लेखनीयता यह है कि उसने इसे एक ऐसी ऊँचाई तक पहुँचाया कि बहुत-सारे कवि स्वतः उसके आगे फीके पड़ गए। ‘आलोचनात्मक यथार्थवाद’ धूमिल की सीमा भी रही और शक्ति भी। इसका कारण शायद यह रहा हो कि एक ग़ज़ब तटस्थता या कहें कि यथातथता धूमिल में पाई जाती है जो पर्यवेक्षणात्मक आनुभविकता से आगे उन्हें नहीं बढ़ने देती। सम्भवतः इसीलिए ज़्यादातर वे ग़ुस्से, तानाक़शी, लानत भेजने, चोट पहुँचाने जैसी मानसिकता में देखे जाते हैं। इसका काव्यात्मक प्रतिफल यह हुआ कि यथार्थ बहुविध और बहुआयामी रूप में उभरकर सामने आया। वस्तुस्थिति बहुत मारक और लगभग संहारक प्ररूप में नमूदार हुई। जैसे कि शायद ही किसी हिन्दी-कवि के यहाँ ऐसी पंक्तियाँ मिलेंगी-
नेकर में नाड़े-सी पड़ी हुई पत्नी का प्यार
रिश्तों की तगार में ऊँघती हुई
एक खास और घरेलू किस्म की थू
आक् ! (सुदामा पाँडे़ का प्रजातन्त्र, पृ. 26)।
धूमिल बहुत निर्मम तरीक़े से एक परम्परागत समाज में पति-पत्नी के कथित प्यार की वास्तविक अन्दरूनी तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि प्यार के नाम पर वहाँ केवल स्त्री का उपनिवेशीकरण है-
प्यार-
मैं। सुनता हूँ खून में
अन्धाकुप का साइरन अपनी शिराओं में
सुनता हूँ मगर नहीं जानता-
यह साइरन
अन्धाकुप खुलने का है या शुरू
होने का। मैं प्यार को नहीं जानता।
सिर्फ जानता हूँ कि हम दोनों
ज्यादातर चुप हैं या जब भी हम बोलते हैं
मेरे शब्द तुम्हारे शब्दों को
ढक लेते हैं। (वही, पृ. 128)।
यह कितना विचित्र है कि भारतीय-विशेषतः देहाती-परिदृश्य में पति-पत्नी का प्यार इकतरफ़ा क्रिया है। कुछ इस तरह का दृश्य है कि स्त्री यहाँ अकर्मक क्रिया की तरह है। वह ऐक्टिव नहीं पैसिव रूप में ही है। सक्रियता सिर्फ़ पुरुष के हिस्से में है। ज़रा सोचा जाए कि कालान्तर में इस इकतरफ़ापन के क्या-क्या नतीज़े सामने आ सकते हैं? इसके कम से कम चार नतीज़े तो ख़ुद धूमिल ने ही गिनाए हैं, जो उनकी ‘गृहस्थी: चार आयाम’ कविता में निबद्ध हैं। इनमें पहले दो आयाम तो ये हैं-
1. स्त्री का उसकी भावनाओं, संवेदनाओं, अन्तरात्मा से रहित होकर केवल एक देह में तब्दील हो आना (कल सुनना मुझे, पृ. 81),
2. स्त्री का धीरे-धीरे सारी क्रिया के प्रति उदासीन और रुचिहीनता की स्थिति में पहुँच जाना। (वही)।
और बाक़ी के दो आयाम ये-
3. पुरुष का भी इस स्थिति से संक्रमित हो आना; दोनों के बीच एक बेहिसाब ठसपन पैदा हो आना (रात की प्रतीक्षा में/हमने सारा दिन गुजार दिया है/और अब जब कि रात/आ चुकी है/हम इस गहरे सन्नाटे में/बीमार बिस्तर के सिरहाने बैठकर/किसी स्वस्थ क्षण की/प्रतीक्षा कर रहे हैं) (वही, पृ. 81-82) और;
4. पति-पत्नी का पूरी तरह एक यौन-मशीन में बदल जाना (न मैंने/न तुमने/ये सभी बच्चे/हमारी मुलाकातों ने जने हैं/हम दोनों तो केवल/इन अबोध जन्मों के/माध्यम बने हैं।) (वही, पृ. 82)।
इसकी एक पाँचवीं स्थिति और है-जि़न्दगी से यौनिकता का हमेशा-हमेशा के लिए तिरोहित हो जाना-‘‘अन्त में हमने तय किया अपनी टाँगें/अब शरीक नहीं करेंगे हम अपनी/दिनचर्या में अपने बिस्तर की/सेहत के लिए/ /प्रार्थना करेंगे/चमड़े की जिल्द में बँधी हुई अपनी मुहब्बत/का मजा/रोजमर्रा के खर्च में जमा करते हुए।’’ (सुदामा पाँड़े का प्रजातन्त्र, पृ. 131)। कोई चाहे तो कह सकता है कि यह प्यार का उदात्तीकरण है या देह की भौतिकता से उठकर जि़न्दगी की आधिभौतिक व्यापकता में उसका रवाँ हो जाना है! जो लोग इस तरह का भ्रम पाले हुए हैं, उन्हें यह वैचारिकता मुबारक़। लेकिन हक़ीक़त यह है कि यह दाम्पत्य का पूरी तरह असफल हो जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि यौनिकता एक ऐसी मूलाधार-भूमि है, जिस पर दाम्पत्य टिका होता है। इस ज़मीन के तिड़कने का अर्थ है, भवन का भरभराकर गिर जाना; हम चाहे उसे कितना भी अन्यथागत रूप में व्याख्यायित करते जाएँ! यह देखकर दुखद आश्चर्य होता है कि परम्परागत समाजों में दाम्पत्य के बिखरने की यह प्रक्रिया विवाह के दिन से ही शुरू हो जाती है। धूमिल की ‘नौ मादा कविताएँ’ की सातवीं कड़ी ‘प्यार’ का यह अंश देखा जाए-‘‘मैं/छोटी-छोटी सुविधाओं के मोर्चों पर/मारा गया/कुल का एक बटा सात/ब्याह के दिन मारा गया मैं/मेरी सुहागरात/उस सितारे की चीख थी/जो सागर में चमकी और बिना किसी/भाषा के बुझ गई।’’ (वही, पृ. 128-29)।
यह सचमुच कितना विचित्र है कि जिस देश में दाम्पत्य को इस क़दर महिमामंडित किया गया हो कि वह सात जन्मों का बन्धन तक कह दिया गया हो, वहाँ पहले ही जनम में पति-पत्नी की यह हालत है! दरअसल सात जन्मों वाली बाध्यता केवल स्त्री के लिए थी, पुरुष के लिए नहीं। और स्त्री की हालत तो हमने देखी ही। पुरुष की स्थिति भी उससे कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। सामाजिक रूप से वर्चस्व के बावज़ूद पुरुष की यह हालत है! दरअसल दाम्पत्य की गाड़ी समानता, संवेदनशीलता और इन दोनों से पैदा सहअस्तित्व से चलती है। परम्परागत सामाजिकीकरण और सांस्कृतीकरण की प्रथा इसे सामन्ती सम्बन्धों में बदल देती है। यह प्रथा हमारे अनजाने हमारे अन्दर प्रवेश करती है और सारा गुड़-गोबर कर देती है। धूमिल ने हिन्दी-कविता में सम्भवतः पहली बार इस यथार्थ को इस गहराई से पकड़ा। मेरा अनुमान है कि धूमिल के यहाँ यौन प्रतीकों, बिम्बों इत्यादि का जो इतना घटाटोप छाया है, इसी अतृप्त यौन-संवेदना का परावर्तन (पर्वर्जन) है। अन्य शब्दों में इसे यौन-कुंठा भी कहा जा सकता है। एक तरह से धूमिल ख़ुद दाम्पत्य में घुसी सामन्ती सांस्कारिकता से क्षुब्ध दिखाई देते हैं।
नक्सलवादी आन्दोलन में भाग लेती स्त्रियों के बहाने कुछ गतिशील विचार
यह एक सुखद आश्चर्य ही है कि धूमिल अपनी काव्य-यात्रा के क्रम में ही अपनी इस कुंठा को काबू में करते हैं और नक्सलवादी आन्दोलन में भाग लेती आदिवासी या और दूसरी स्त्रियों के बहाने स्त्री के प्रति अपने गतिशील विचारों को प्रकाश में लाते हैं। अब यह जाँचने या मापने का साहित्येतर कोई पैमाना हमारे पास नहीं है कि सचमुच धूमिल अपनी कुंठाओं से उबर पाए थे या नहीं या नक्सलवाद जैसा डि-क्लास वे हो पाए थे कि नहीं? हिन्दी में एक अज़ीब स्थिति यह पाई जाती है कि आप मंच पर अच्छा-अच्छा बोलते चलिए, अच्छी-अच्छी धाँसू क्रान्तिकारी कविताएँ लिखते चलिए, जुलूसों में गला फाड़-फाड़कर नारे लगाते चलिए लेकिन जब कतल की रात आए तो चुपचाप अपने दड़बे में घुस जाइये या आप लाख ढूँढ़ने पर भी कहीं न मिलें तो अगले दिन पता चले कि आप तो दूसरे शिविर में अपने कुछ सजातियों के साथ बैठे चमगोइयाँ करते देखे गए थे! अमूमन यह देखने-सुनने में आया है कि वे लोग जिन्होंने स्त्री की स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता इत्यादि पर शानदार कविताएँ लिखी हैं, लेख लिखे हैं, घर पहुँचते ही शराब या शक़ के नशे में पत्नी को पीटते-प्रताडि़त करते पाए गए हैं। स्त्री व्यावहारिक तौर पर कभी भी स्वतन्त्रता-योग्य उन्हें नहीं लगी! अपने मर्दवाद को वे कभी भी जीत नहीं पाए। साहित्य ही नहीं प्रायः हर कला-क्षेत्र में ऐसी विभूतियाँ देखने को मिलेंगी। प्रसिद्ध कथाकार सुधा अरोड़ा ने अपने एक लेख ‘कलाकार के सौ गुनाह माफ हैं’ (आम औरत: जिंदा सवाल; सामयिक प्रकाशन, न. दि. 2009; पृ.129-132) में नामज़द रूप से उदाहरण सहित इसके ब्यौरे दिए हैं। और कुछ नहीं तो चुप्पी और उपेक्षा-अवहेलना की हिंसा से तो आप उसे क़ाबू में कर ही सकते हैं। ‘सेंस आॅफ नाॅन बिलांगिंग’ और ‘चुप्पी की हिंसा’ एक ऐसा हथियार है, जिससे अच्छी से अच्छी पढ़ी-लिखी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और दमदार महिला को भी आप नाकों चने चबवा सकते हैं। या तो वह आपसे पीछा छुड़ाकर भाग जाए या आपकी बाँदी बन जाए; दोनों स्थितियों में आपका ही आपका फायदा है। (द्रष्टव्य, सुधा अरोड़ा का ‘जिसके निशान नहीं दिखते… मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ’ शीर्षक लेख, वही, पृ. 147-65)। मुझे नहीं मालूम कि धूमिल ऐसे थे कि नहीं, उनकी कविताओं से तो यही लगता है कि स्त्री की इस दोयमता से वे बहुत परेशान थे और उनका विचार था कि स्त्री अपनी मादा सीमाओं और असुरक्षा-बोध से ऊपर उठ ले तो उसके सामने एक नई और बेहतर दुनिया खुल सकती है। जैसे कि कुमारी रोशनारा बेगम की आत्म कुर्बानी के वाक़ये पर लिखी अपनी कविता ‘आतिश के अनार-सी वह लड़की’ में एक जगह वे लिखते हैं-
मुमकिन था यह भी कि अपने देशवासियों की गरीबी से
साढ़े तीन हाथ अलग हटकर
एक लड़की अपने प्रेमी का सिर छाती पर रखकर
सो रहती देह के अँधेरे में
अपनी समझ और अपने सपनों के बीच
मुमकिन यह भी था कि थोड़ी-सी मेंहदी और
एक अदद ओढ़नी का लोभ
लाल तिकोने के खि़लाफ़ बोलता जिहाद
और अपने ‘वैनिटी बैग’ में छोड़कर बच्चों की एक लम्बी फेहरिस्त
एक दिन चुपचाप कब्र में सो जाती हौवा की इंकलाबी औलाद
(कल सुनना मुझे, पृ. 58)।
इन पंक्तियों के बीच यह अंश और आता है-‘‘मैं उसे कुछ भी न कहता सिर्फ कविता का दरवाज़ा/उसके लिए बन्द रहता लेकिन क्या समय भी उसे/यूँ ही छोड़ देता ?/ /वह उसके चुम्बन के साथ बारूद से जले हुए गोश्त का/एक सड़ा हुआ टुकड़ा जोड़ देता/और हवा में टाँग देता उसके लिए/एक असंसदीय शब्द-नीच !’’ (वही)। यानी कि जिसका जूता उसी का सिर! समय यानी कि समाज और उसकी परम्परा। पहले तो स्त्री को यही उसका कर्तव्य-कर्म और आदर्श बता-बताकर यहीं तक सीमित कर दिया कि वह सिंगारदान, आईने, केश-सज्जा यानी कि देह-केन्द्रिकता में फँसी रहे (वही, पृ. 59), और फिर इसी देह-केन्द्रिकता के आधार पर उसका अवमाननीकरण (डि-ग्रेडेशन)! यह हमारे यहाँ ही है कि पहले तो स्त्री को उसकी दैहिकता में गौरवान्वित और महिमामंडित किया और फिर उसी देह के चलते उसका उपनिवेशीकरण हुआ! धूमिल की एक और कविता है-‘कल’। इस कविता में वे इस प्रक्रिया पर इस तरह प्रकाश डालते हैं-‘‘कल तुम ज़मीन पर पड़ी होगी और बसन्त पेड़ पर होगा/नीमतल्ला, बेलियाघाट, जोड़बगान/फूलों की मृत्यु से उदास फूलदान/और उगलदान में कोई फर्क नहीं होगा।’’ (वही, पृ. 78)। फूलदान से उगलदान बन जाना; कुल यही नियति भारतीय समाज ने स्त्री को दी है। धूमिल कथित तौर पर इसका निषेध करते हैं और एक ज़्यादा खुला आसमान उसके लिए उपस्थित घोषित करते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि अब जनता को ही नहीं कविता को भी अपनी मुक्ति का एक शानदार रास्ता मिल गया है-
जैसे वह आदिवासी औरत झाड़ी की ओट से
जलते हुए झोंपड़ों को देखती उतरती चली गई
वो जंगली ढलान-
जहाँ फौरी कार्रवाई के लिए हमलावर दस्ता
पेटियाँ कस रहा था।
इसके बाद
तुम जानते ही हो शब्द शस्त्र बन गए हैं
और अगवा बन्दूक की निशानदेही पर
कविता ने ढूँढ़ लिया है अपनी मुक्ति का रास्ता
दुश्मन की छाती के खून भरे छेद से । (सुदामा पाँडे़ का प्रजातन्त्र, पृ. 76-77)।
वामपंथी विचार का आवश्यक चरण: जेंडर-संवेदनशीलता
यह तो ठीक है। लेकिन रोशनआरा बेगम के लिए लिखी कविता में धूमिल आदतन फिर कुछ ऐसे भाषा-प्रयोगों से बच नहीं पाए हैं, जो स्त्री के प्रति पुरुष की एक ख़ास मानसिकता से पैदा होते हैं। जैसे यह कि ‘‘बाबुल के देश का चुटिहल धड़कता हुआ टुकड़ा था सीने में’’ (कल सुनना मुझे, पृ. 57) या जैसे यह कि ‘‘एक हाथ जो नाजुक जरूर था’’ (वही) या यह कि ‘‘और लोग चकित थे देखकर कि एक नंहा गुलाब’’ (वही, पृ. 58) या यह कि ‘‘बीस सेबों की मिठास से भरा हुआ यौवन’’ (वही, पृ. 59)। ये शब्द-प्रयोग उसी जैविक तत्ववाद के प्रतीक हैं, जिसका यहाँ ऊपर हमने जि़क्र किया और जिससे धूमिल जीवन-भर मुक्त नहीं हो पाए। सम्भवतः जिस माहौल में वे थे, इनसे मुक्त हो सकते नहीं थे। जहाँ तक सतर्क रहे आने(अ. कु. दु.) की बात है तो कम से कम धूमिल से तो यह उम्मीद करना बेकार है। यहाँ ध्यान देने की बात एक यह भी है कि यदि नक्सलवाद या (मोटे तौर पर) वामपंथी विचारधारा को मात्र लबादे या दिखावटी आवेग की तरह ओढ़ा न जाए और सचमुच में इसे आत्मसात् किया जाए तो इस आत्मसात्करण की प्रक्रिया का एक आवश्यक चरएा है- जेंडर-सेंसिटाइज़ेशन यानी जेंडर-सचेतनता या संवेदनशीलता। नक्सलवादी सन्दर्भों पर कविता लिखते समय भी यदि कोई भाषा के मर्दवादी ढाँचे के प्रति सतर्क नहीं है तो इसका सिवाय इसके और क्या अर्थ हो सकता है कि कवि अपने स्वयं के कठघरों से मुक्त नहीं हो पाया है और उसकी यह काव्यगत वैचारिकता सिर्फ़ एक शाब्दिक कलाकारी है। यह बात धूमिल ही नहीं, हिन्दी के और भी कई नामचीन कवियों के बाबत जाँचने योग्य है।