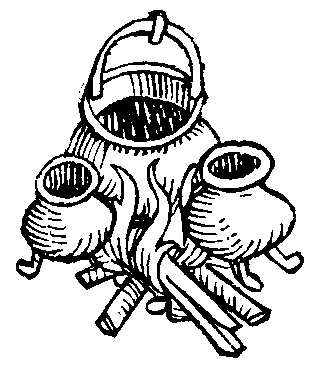रोहिणी अग्रवाल स्त्रीवादी आलोचक हैं , महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं . ई मेल- rohini1959@gmail.com
रोहिणी अग्रवाल स्त्रीवादी आलोचक हैं , महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं . ई मेल- rohini1959@gmail.com
वाया
रवींद्रनाथ टैगोर)
होता है, इसलिए इसके मूल्य भी कुछ हद तक वास्तविक जीवन के मूल्य होते हैं. लेकिन यह स्पष्ट है कि औरतों के मूल्य मर्दों द्वारा निर्मित मूल्यों से अक्सर
भिन्न होते हैं. स्वभावतः मामला ऐसा ही है. फिर भी मर्दाना मूल्य ही प्रभावी होते
हैं. अगर बिना किसी लाग-लपेट के कहा जाए तो फुटबाल और खेल ’महत्वपूर्ण’ है ,
फैशन
की पूजा और कपड़ा खरीदना ’महत्वहीन’ है. और ये मूल्य
अनिवार्यतः जीवन से कथा-साहित्य में स्थानांतरित हो जाते हैं. आलोचक मान लेता है
कि यह महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि यह युद्ध से संबंधित है. यह एक महत्वहीन किताब
है क्योंकि इसमें ड्राइंग रूप में बैठी औरतों की अनुभूतियों का वर्णन किया गया है. किसी दुकान के दृश्य के मुकाबले युद्धभूमि का कोई दृश्य अघिक महत्वपूर्ण है.’’
(वर्जीनिया
वुल्फ, अपना कमरा, पृ0 78). मैं बड़े-बड़े हरफों में पहले ही अपनी बात खोल कर
साफ कर देना चाहती हूं कि आपसी प्रतिदुंदिता और वैपरीत्य के अभाव में दोनों
कहानिया ’पत्नी’ (जैनेंद्रकुमार)
और ’उनकी व्यस्तता’ (अल्पना मिश्र) एक ही भावभूमि का
विस्तार हैं; नैरेटर के भीतर तक उतर कर दूसरे पक्ष को एक
प्रामाणिक ईमानदारी के साथ उकेर देना चाहती हैं, और सदा के अ-डोल
और जल-जल कर राख हुए जा रहे सवालों को अजस्र ऊष्मा से तमतमाए विकसनशील
विचार-प्रवाह के बीचोबीच रख देना चाहती हैं कि घर-परिवार में क्या सब कुछ ठीक चल
रहा है? इस सवाल में यदि नकारात्मक उत्तर की निश्चयात्मक गूंज सुनाई पड़ रही
है तो तय है कि तलवार लेकर मच्छर के पीछे भागने से मलेरिया के स्रोत के सफाया नहीं
होगा.
इसलिए क्यों न तलवार को म्यान में रख कर कुछ देर को छुट्टी दे दी जाए;
और
खुद को मिट्टी के किनारों से उमग कर प्रकाश फैलाते दीए के हवाले कर दिया जाए?
न,
भीतर
के तहखानों में बिजली की फिटिंग का आडंबर नहीं रचाया जा सकता कि खट से खटका दबा कर
सब कुछ जगर-मगर कर दिया जाए. वहां तो अपने ही चाक पर दीया गढ़ कर अपनी ही चेतना की
बाती से टिमटिमाता आलोक फैलाना पड़ता है. लेकिन यह जो ऊपर वर्जीनिया वुल्फ कह गई हैं,
सुन
कर कैसे कोई स्थितप्रज्ञ भाव से अपनी प्रज्ञा-जोत जलाए रखे ? पाखंड पर
जतनपूर्वक ओढ़ाई गई चादर को कोई बेशर्मी से उघाड़ दे तो क्यों नहीं ’नग्न’
होने
की लाज अपने अहं और ताकत को गूंध-सान कर आतंक में फूट पड़े ? मैं जानती हूं
पिछले अस्सी बरस से दीवार से लग कर द्वार की ओट में खड़ी ’सुनंदा’ से
कभी किसी ’कालीचरण’ ने खौफ नहीं खाया है, बल्कि अदृश्य
सुनंदा की ठोस उपस्थिति ने उसे सुख ही दिया है – एक पुकार की दूरी पर खड़ी कामधेनु
की तरह. वह ’अपने पुराने बक्से से अब तक जोड़ी पूंजी निकाल
कर’ बस-स्टेशन की ओर लपकती पत्नी की ’गति’ से
भी भयभीत नहीं. जानता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सरीखी कहावतें यूं ही नहीं
बनतीं. इसलिए लक्ष्मण-रेखा के भीतर कितना ही कूद-फांद ले स्त्री, खूंटा
तुड़ा कर ज्यादा दूर तक भागना आसान नहीं रहता.
लिए मृणाल (रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानी ’पत्नी का पत्र’) की निःशब्द
टंकार में जाने ऐसा क्या था कि हुआं-हुआं की जमात बौखला-बिलबिला कर अपनी-अपनी
खोहों में दुबक गई.
से सुनंदा और पत्नी (अल्पना मिश्र की कहानी की मिसेज सुदामाप्रसाद, या
शैलजा की अम्मा ? अहा! कितनी भाग्यवती है यह स्त्री कि पति-सेवा
का पुण्य लूटते-लूटते अपना नाम भी विसर्जित कर दिया उसने! ) के बीच क्यों आ बैठी है?
इन
दोनों की सीधी-सपाट कहानी का सीधा-सतही इकहरा विश्लेषण करने के मेरे मंसूबों पर
पानी फेरने के लिए ? लेकिन देख क्या रही हूं कि मृणाल की तेजस्विता
के स्पर्श मात्र से ये दोनों सूखी-मुरझााई स्त्रियां मानो जी उठी हैं. न, वे
सत्यनारायण की कथा की कलावती-लीलावती नहीं है कि कोई दैवीय (या लौकिक) शक्ति
सत्यनारायण का नाम धर कर मिट्टी के लोंदों की तरह उन्हें घड़ी-घड़ी बनाता-मिटाता
रहे. मृणाल की उपस्थिति ने मुझे भी छूकर स्पंदित कर दिया है. अपनी बात कहने के लिए
वर्जीनिया वुल्फ के शब्दों को चुरा कर मैं यह जो आंख-मिचैली का खेल खेल रही थी,
उसे
बनाए रख कर क्यों देर तक अपनी आंख में घूल झोंकती रहूं ? हां, मैं
स्वीकार करती हूं कि आज की इक्कीसवीं सदी के इस ’चेतन’ युग
में भी स्त्री, स्त्री-प्रश्न और स्त्री का वजूद हाशिए पर हैं. अस्पतालों की तर्ज पर साहित्य में भी ’गाइनी वार्ड’ की परिकल्पना कर
ली जाती है ताकि स्त्रियां अपने सुख-दुख और सवालों को लेकर बतियाती-उलझती रहें. मर्दानी दुनिया स्त्री को चैपाल की चकल्लस देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि
स्त्रियों के तंग दायरे और वही तीन सवाल – प्रेम, पति और परिवार. वे मानते हैं, पुरुषों की दुनिया बड़ी है और बेहतर भी, जहां घर के बाड़े
से बाहर निकल कर समय और समाज को आंदोलित करने वाले बड़े-बड़े सवालों से सिर खपाने के
बड़े-बड़े कुलाबे हैं.
स्त्रियां क्या जानें कि राजनीतिक मसलों पर देश-दुनिया और
भविष्य की तरक्की टिकी है; कि सांप्रदायिक विद्वेष और आतंकवादी
गतिविधियों के अलावा किसान-कामगार आंदोलन, दलित आंदोलन, नक्सली हिंसा,
बाजार
की संस्कृति और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उन्हें हर पल सिर पर कफन बांधे
रखना पड़ता है. घर की महफूज चारदीवारी पुरुष के ’नसीब’ में
कहां ? इसलिए जिस अहं भाव से पुरुष (लेखक-पाठक दोनों) इन तथाकथित ’बृहत्तर’
सवालों
से जूझता है, उतनी ही हेय दृष्टि से स्त्री-लेखन और
स्त्री-प्रश्नों को बिना टकराए खारिज कर देता है. बिना पढ़े ही खारिज कर दिए जाने
की आशंका के बावजूद मैं घर-परिवार और स्त्री-पुरुष संबंध से जुड़े तमाम सवालों से
बार-बार जूझते रहना चाहती हूं क्योंकि
जानती हूं कि आतंकवाद, सांप्रदायिक विद्वेष, घृणा और अलगाव
की राजनीति, गुटबंदी जैसी परिणतियां भयावह रूप लेकर एकाएक आसमान
से नहीं आतीं. वे बरसों-बरस घर की दुनिया और मनुष्य के अंतस के भीतर चुपचाप
पलती-सुगबुगाती हैं. पुरुषों की दुनिया के इन बड़े-बड़े मुद्दों की विभीषिका को
स्त्री देह के साथ-साथ आत्मा के स्तर पर भी झेलती है, इसलिए चाहती है
पुरुषों की भीड़ से नहीं, अपने घर के पुरुष के साथ अपने भय,
दुःस्वप्न,
अपमान
और अरमान साझा करे; उसे बताए कि स्त्री को हीन समझे जाने का भाव
पुरुष का कभी अपनी हीनता (जिसे श्रेष्ठता के गुब्बारे में फुला कर वह आंखों में
धूल झोंकने के मद में उन्मत्त रहता है) से मुक्त कर दूसरे के भीतर पैठने की विवेकशील
संवेदना नहीं देगा.
बहुत छोटी इकाई है घर, लेकिन निजता की महीन परत के नीचे वह
विषमता, विभाजन, आतंक, हिंसा, अपराध और
राजनीति से खदबदाता एक समूह भी है. भीड़ में नजर बचा कर अपराध करने और नजर आ जाने
पर फरार हो जाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है. जाहिर है वहां रक्तरंजित हाथ और
पाक-साफ दामन साथ-साथ चल सकते हैं. लेकिन घर साफ-सुथरा पारदर्शी आइना है जो धब्बे
को एनलार्ज कर पूरे व्यक्तित्व के दागदार हो जाने की चेतावनी देता है. घर बड़े-बड़े
मुद्दों को लघु स्तर पर सफलतापूर्वक सुलझा लेने की प्रयोगशाला है जहां फैसले
अदालती कार्रवाइयों की तरह लंबे नहीं टलते चलते। चूंकि यहां फौरी तौर पर सुनवाई और
कार्रवाई होती है, इसलिए कठघरे में खड़े होने की अप्रीतिकर अनुभूति
’बड़े मुद्दों’ की ओट में रिहाई पा जाना चाहती है.ठीक कहते हैं विचारक कि स्त्री की स्थिति ही
समाज के विकसित होने की पहली कसौटी है क्योंकि घर समाज का आंगन है, ’समाजसेवियों’
का
रैन-बसेरा नहीं.’’मेरे लिए तो दुनिया है ही नहीं. मैं तो बस मन
के सहारे ही रहती हूं’’ (’दृष्टिदान’, रवींद्रनाथ
टैगोर) बनाम ’’घर और दफ्तर को अलग-अलग रखना चाहिए’’ (’उनकी
व्यस्तता’ अल्पना मिश्र) शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की तरह जैनेंद्रकुमार
से अपने को संबंध को लेकर मैं सदा असमंजस में बनी रहती हूं. दोनों अपने पात्रों के
साथ अनायास मन के भीतर गहरी पैठ बनाते हुए मुझे अपने रंग में रंगने लगते हैं,
लेकिन
जैसे ही अपनी शख्सियत पर मृणाल-सुनीता या सावित्री-किरणमयी-राजलक्ष्मी का लबादा
ओढ़ने को होती हूं कि जाने कहां से वितृष्णा तैर कर आती है और सम्मोहन जाल छिटका कर
मुझे अपने में लौटा लेती है. विश्लेषण करने पर पाती हूं कि विद्रोह के सब्जबाग
दिखा कर स्त्री की पीड़ा और त्याग का महिमामंडन करते हुए वे भी तो स्टीरियोटाइप्स
को पुख्ता कर रहे हैं. अलबत्ता आधा सच पूरी ईमानदारी से बयान करने की दृढ़ता तो
उनमें है ही.
’पत्नी’ कहानी को ही लूं तो वह पति के भोजन की
प्रतीक्षा में अस्त-व्यस्त सामान्य स्त्री की सामान्य दिनचर्या का आख्यान नहीं है,
व्यवस्था
द्वारा एक भरी-पूरी शख्सियत को प्रतीक्षा और जड़ता के दो खूंटों से बांध कर बधिया
कर दिए जाने की पड़ताल है. उल्लेखनीय है कि बधिया कर दिए जाने का क्षोभ मौन हाहाकार
बन कर कहानी की नायिका सुनंदा को जब-तब जकड़ लेता है. तब वह ’भीतर ही भीतर
गुस्से से घुट कर रह’ जाती है, या पति का जी
दुखाने के लिए उसकी उपस्थिति का नोटिस न लेकर ’कठोरतापूर्वक
शून्य को ही देखती रहती’ है; या ’हाथ
की बटलोई को खूब जोर से फेंक’ देना चाहती है ताकि बता सके कि ’किसी
का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं’ है. लेकिन इस सारे मानसिक ऊहापोह के
बाद अपने में लौटने पर पाती है कि वह ’जहां थी, वहां’ अब
भी है – गीली लकड़ी की तरह धुंआती हुई या अंगीठी की आग की तरह राख हुई जाती हुई. घटनाओं की न्यूनता, स्थितियों की
गतिहीनता एवं पात्रों के विकास की संभावनाओं का अभाव – जैनेंद्रकुमार की कहानी-कला
की कुछ विशेषताएं हैं जो कहानी में स्फूर्ति, उत्साह और आशा
जैसी सकारात्मक चटखदार रेखाओं को उभरने नहीं देतीं. लेखक व्यक्ति की मनःस्थितियों
के जरिए सामाजिक विडंबनाओं और पाखंड का उद्घाटन करते हैं और इस प्रक्रिया में
पात्र के अंतद्र्वंद्वों या दो पात्रों को आमने-सामने रख कर कहानी को खुद अपनी
यात्रा तय करने का अवसर देते हैं. ’पत्नी’ कहानी में
जैनेंद्रकुमार एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्विता में तन कर खड़े दो विरोधी पात्रों या
स्थितियों को नहीं गढ़ते, बल्कि उनकी संवादहीनता के भीतर बोलती
चुप्पियों के जरिए उनके मानसिक गठन को उद्भासित करते हैं.
अपनी नित्यक्रमिकता को
यांत्रिक भाव से जीती सुनंदा कहानी में शुरु से अंत तक अवरुद्ध कर दी गई लहर के
बिंब की सृष्टि करती है, मानो लेखक कहना चाह रहा हो कि जीवन की
गत्यात्मकता के भीतर जीवन का क्षरण करने वाली स्थितियों को चीन्हने के लिए हमें
स्वयं उनके भीतर उतरना होगा. इस अवरुद्ध लहर के धु्रवांत पर है कालिंदीचरण जो
मित्र-मंडली के साथ हवा के झोंके की मानिंद घर और समाज में बेरोक-टोक मनचाही गति
और समय के साथ घूमता है. उसके पास संवारने को संघर्ष-संकुल वर्तमान है, और
विचरण के लिए भविष्य का आसमान। सुनंदा के पास न वर्तमान है, न भविष्य. बस,
उसकी
थाती है अतीत – पुत्र की अकाल मृत्यु के कारण चोट खाया, बिलबिलाती
स्मृतियों से भरा अतीत. यह अतीत उसे खाली देखते ही गहरे सख्य भाव से बतियाने हेतु
उसके पास आ पहुंचता है. लेकिन दोनों जैसे ही मिल-बैठ कर साझा भाव से अपने-अपने
जख्म चाटने लगते हैं, सुनंदा अश्रुपूरित नेत्र लिए उसे जहां का तहां
छोड़ वर्तमान में लौट आती है. वह जानती है वर्तमान का स्वामी उसका पति कालिंदीचरण
है और वह स्वयं उसकी छाया या अनुगूंज. वर्तमान उसे पलायन की सुविधा देता है
क्योंकि यहां उसे विचारशून्य सेवादारिन की भूमिका निभानी है. सुनंदा पाठक के भीतर गहरे भावोद्वेलन की सृष्टि
करती है, लेकिन लेखक उसके चरित्र की बारीक परतों को एक निश्चित अंतराल में
उठने वाली परस्पर विरोधी विचार-लहरियों के जरिए बुनता-उकेरता है. एक ओर किसी भी
सामान्य स्त्री की तरह सतीत्व उसकी पूंजी है और पति-सेवा सौभाग्य. यही उसके
दायित्व की जमीन है और सपनों का आसमान भी.
मन में उठती टीस और हुलसते अरमान दोनों की ’भू्रण हत्या’ करने के लिए वह किसी न किसी ’व्यस्तता’
की
तलाश में अपने स्वत्व और ऊर्जा को क्षरित करती चलती है. लेकिन इसके बावजूद पढ़-लिख
कर भारतमाता को स्वतंत्र कराने जैसे ’बड़े’ और ’पुरुषेचित’
मुद्दों
को समझने की ललक सुनंदा को निरी छाया या अनुगूंज नहीं रहने देती. उसमें अपनी कमतरी
पर ग्लानि है तो उसी सांस में कमतर बनाए रखने वाले घटकों की शिनाख्त की तमीज भी. ’’उसने
बहुत चाहा है कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे. उसमें बुद्धि तो जरा कम है,
फिर
धीरे-धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी ? सोचती है, कम पढ़ी हूं तो
इसमें मेरा ऐसा कसूर क्या है? अब तो प़ढ़ने को मैं तैयार हूं, लेकिन
पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है.’’ आत्मविस्मरण से आत्मान्वेषण की उत्कंठा
के बीच निरंतर दोलायमान सुनंदा की विचार-यात्रा दरअसल यथास्थितिवाद के अभिशाप से
उबरने के लिए स्पेस पाने की चाहत है जिसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिनिधि
पुरुष/पति कालिंदीचरण ने पूरी तरह घेर लिया है. ’माथे को
उंगलियों पर टिका कर’, ’बैठी-बैठी सूनी सी’ अदृश्य को ताकती
सुनंदा ऊपरी तौर पर लकड़ी के कुंदे सी ठस्स भले ही दीखती हो, वक्त से पिछड़ने
की पराजय ने उसके भीतर क्षीणकाय संघर्ष-चेतना अवश्य भरी है. बेशक ’’उत्साह
उसके लिए अपरिचित है’’ और ’’जीवन की हौंस उसमें बुझती जा रही है’’,
पर
फिर भी वह ’जीना चाहती है’ रेंग-रेंग कर
नहीं, पति के साथ कंधे से कंधा मिला कर भारतमाता की स्वतंत्रता के यज्ञ में
आहुति डाल कर.
दुबकी-सिमटी सुनंदा को दयनीयता में ढाल कर विघटित नहीं करते, उसमें
सेवा, त्याग, नैतिकता का बल गूंध कर आक्रांता सरीखे
कालिंदीचरण के सामने खड़ा कर देते हैं. निश्चय ही यह शेर और मेमने की लड़ाई है. सुनंदा के पास आत्म-बलिदान के तेज से परिपूर्ण आत्मबल है तो कालिंदीचरण के पास
पुरुष होने के दंभ से उपजा अहं भाव. एक ओर अपने मान की रक्षा की मूक मिन्नतें हैं,
दूसरी
ओर सब कोमल चकनाचूर कर देने की उद्धत लापरवाही. दोनों ओर बिना कहे अपने को समझे
जाने की चाहतें हैं, और दोनों ओर समझबूझ कर भी अनजान बने रहने की
भंगिमाएं हैं. संभवतया इसलिए कि बरसों से पसरी संवादहीनता संबंध को कुतरते-कुतरते
दो व्यक्तियों को परस्पर अजनबी बना देती है. पति के पास यदि क्रुद्ध होकर बाहरी
दुनिया में जा रमने का विकल्प है तो पत्नी के पास और अधिक कड़ाई से अपने दायित्व को
निभाए चलने की विकल्पहीनता. अलबत्ता खाना न परोसने के हुक्म का उल्लंघन करते हुए
वह खाना परोसने के साथ-साथ अपने आहत अभिमान को भी अनबोले ठसके के साथ परोस आती है. लेकिन यह क्षणिक उत्तेजना की तात्कालिक प्रतिक्रिया भर है. अपने-अपने खांचों में
बंधे सुनंदा और कालिंदीचरण जानते हैं कि स्त्री की कमजोरी ही पुरुष की ताकत है. इसलिए आंख में आंख डाल कर पंजा लड़ाने की यह क्षणिक प्रक्रिया अंततः पति-पत्नी की
समाजानुमोदित भूमिकाओं की पारंपरिक लय-ताल में विलीन हो जाती है, जहां
अपनी छोटी से छोटी जरूरत की पूर्ति के लिए हांक लगा कर पत्नी को हड़का देने के
विशेषाधिकार हैं तो दूसरी ओर अपनी भूख और जरूरतों को मुल्तवी कर पति के लिए जान की
बाजी लगा देने की दीनता. लेकिन जैनेंद्रकुमार का लक्ष्य ऊबड़खाबड़ जमीन पर स्थित
दांपत्य संबंध की कथा कहना नहीं है.
वे इस तथ्य की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करना
चाहते हैं कि सृष्टि के विकास- क्रम को निरंतर बनाए रखने के लिए स्त्री और पुरुष
की दो पूरक इकाइयां कैसे समाज व्यवस्था के हत्थे चढ़ कर एक-दूसरे की
प्रतिद्वंद्विता में तनी दो लैंगिक इकाइयां बन जाती हैं। चूंकि एक पक्ष को श्रेष्ठ
अथवा कर्ता मानते ही अपने आप दूसरा पक्ष हीन और अनुकर्ता की भूमिका में आ
विराजता है, इसलिए दमनकारी तंत्र में सहभागिता की बात
बेमानी हो जाती है. यह व्यवस्था के आंतरिकीकरण की मनोवृत्ति ही है कि सुबह के
उपासे पति की प्रतीक्षा में अंगीठी की आग लहका कर बैठी सुनंदा की चिंता और चेतना
में पति की भूख ही जब-तब आ विराजती है, अपनी नहीं. ’’कुछ हो, आदमी
को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए’’ खीझ में वात्सल्य भर कर सुनंदा सोचती
है तो उसकी सोच में ’आदमी’ यानी कालिंदीचरण ही है, अपनी
आदमियत नहीं. यह स्त्री द्वारा अपनी देह (अस्तित्व) को नकार कर स्वत्वहीन हो उठने
का संस्कार है जो देह के भीतर स्थित दिमाग और देह पर आच्छादित व्यक्तित्व दोनों से
पिंड छुड़ाने के अभ्यास में उभरता है. लेखक ने एकाधिक बार सुनंदा को अपनी देह के
प्रति असावधान दिखाया है और कालिंदीचरण की देह के प्रति ममत्वपूर्ण, मानो
देह जैविक संरचना न होकर ठोस व्यक्तित्व हो. ’’उन्हें न खाने
की फिक्र है, न मेरी फिक्र. मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर
अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए’’ सुनंदा की यह आत्म-दीनता एक ऐसी
स्त्री-छवि की रचना करती है जो चोट खाकर आत्माभिमान में फुफकार उठती है और फिर
आत्मपीड़न में ढल जाती है. इसके विपरीत देह के स्वीकार के साथ अनिवार्य रूप से
व्यक्तित्व के स्वीकार और संवार का भाव व्यक्ति में पनपता है जो स्वाभिमान के
सहारे अपनी परिधि का विस्तार करता चलता है.
व्यस्तता’ कहानी की ओर बढ़ती हूं। देखती हूं अब वह कुछ बुढ़ा गई है. उम्र ने शरीर
को कहीं से फुला कर, कहीं से ढीला कर बालों में चांदी के तार बुनते
हुए अपनी दस्तक दे दी है. अब वह चौके में अंगीठी के सामने नहीं, छोटे
से स्टूल पर बैठी जाने क्या-क्या सोच रही है. एक नहीं, तीन-तीन बेटियों
की मां बन चुकी है. बेटा न पाने का दुख बड़ा है या बेटियों को सही भविष्य न दे पाने
की कचोट -विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता क्योंकि बोलना तो वह अब तक नहीं सीखी. भाषा के नाम पर वही एक गहरा निःछ्वास और शून्य को ताकती आंखें. या शायद बेटा न
होने के ’लाउड’ दुख को पति के मुंह से इतनी बार सुन चुकी है कि
दुख ने अनुभूति की तरह नहीं, ग्रंथि की तरह उसके भीतर घर कर लिया
है. पति के लिए वह कभी उसकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने वाला स्वचालित रोबो है,
कभी
हड़का दिए जाने वाला ढोर-डंगर. पति की डांगरी से ग्रीस के दाग छुड़ाते हुए वह अक्सर
सोचती है, आज उनके दफ्तर, कामकाज और अफसरों-सहकर्मियों के बारे
में जरूर पूछेगी. घर रहने की मजबूरियों के बीच बाहर की बातें सुन-सुन कर बाहर घूम
आने का वर्चुअल सुख तो हासिल कर ही सकती है. लेकिन सुदामाप्रसाद हैं कि बात करने
का कोई मौका पनपने ही नहीं देते. घर में घुसते ही टी वी के रिमोट पर कब्जा करके
चारों ओर खबरों की दुनिया ऐसे फैला लेते हैं कि दुनिया-जहान की विपदाओं के बीच
अपने निजी सुख-दुख की बात करते भी शर्म आती है. शर्म तो तब भी आती है जब उसके
एकमात्र व्यसन – सास-बहू के धारावाहिक देखने का चाव को हिकारत भरी नजर से देख वे
क्रोध में भर कर बुड़बुड़ाने लगते हैं – मूढ़मती, भई, मूढ़मती.
गुस्सा करने का शऊर नहीं है उसके पास, लेकिन चाहती है कभी फुर्सत हो पति के
पास तो वह उन्हें बताए कि इन धारावाहिकों को देख-देख कर ही उसे समझ आया है क्यों
कोई भी स्वस्थ, संतुलित, कर्मठ और
लक्ष्योन्मुख व्यक्ति तिकड़मों और जालसाजियों के फंदे नहीं बुनता। जाल बिछा कर घात
लगाने की टोह में वे ही बैठते हैं जिनसे सब कुछ छीन कर अपनी मौत मरने के लिए
निहत्था छोड़ दिया जाता है या वे जिन्हें अपनी लंबाई के मुताबिक बढ़ने के अवसर नहीं
दिए जाते. जिसके हिस्से की जमीन छीन ली जाती है, वह रो कर अपने
को खत्म कर सकता है या दूसरे को खून के आंसू रुला कर अपने टीसते जख्मों पर
प्रतिशोध के गर्म-दहकते फाहे रखता है. लेकिन असंतुष्टि की बात वह कहे कैसे ?
सुनते
ही आसमान सिर पर न उठा लेंगे कि घर बैठे आराम की रोटी तोड़ने से ही ’औरतों
का दिमाग खराब हो गया’ है. बाहर जाकर इतना-इतना खटना पड़े तो अक्ल
ठिकाने आ जाए. उन्होंने नहीं पढ़ी वह कहानी, लेकिन ब्याह से
पहले शैलजा ने ही पढ़ कर सुनाई थी, किन्हीं शिवरानीदेवी प्रेमचंद की कहानी
थी शायद – ’समझौता’. उसमें भी यही सब – पति-पत्नी की
चखचख. औरतें ऐसी और मर्द वैसे. बहस के दौरान तमक कर बोली थी नायिका, हां,
ललिता
नाम ही था उसका कि बाहर की दुनिया की ज्यादा ऐंठ तो दिखाओ मत. जो मूसलों की परवाह
किए बिना घर की ओखली में चैबीसों घंटों सिर दिए रहती हैं, वे दफ्तर के
कामों से क्या डरें. बस, जरा हमारे हाथ-पैर खोल दो, मजबूती
से दोनों मोर्चे संभाल कर मर्दों को पटकनी न दे दें तो कहना
जीवन-यात्रा. इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंघी हुई बोली,
बंधी
हुई मार’’ (रवीन्द्रनाथ टैगोर, ’पत्नी का पत्र’) लेकिन यह क्या ! लेखिका की पकड़ से मुक्त कर मैं
खुद ही मिसेज सुदामाप्रसाद को ग़ढ़ने बैठ गई. लेखिका ने तो तीन-चार वक्तव्य दिलवाने
के अतिरिक्त मिसेज सुदामाप्रसाद की ओर झांका भी नहीं. वे सुदामाप्रसाद में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं और ऐसे दबे पांव उनके अंतर्मन में घुस गई हैं कि शब्दों को
नहीं, शब्द को जन्म देने वाले विचार या अनुभूति की कौंध को उसकी प्राथमिक
अपरिपक्व अवस्था में पकड़ सकें. शब्दों की पोशाक पहन लेने पर अनुभूतियां अपनी निजता
खो देती हैं और वाचक अपनी स्वतःस्फूर्त वास्तविकता. मैं कालिंदीचरण के किसी हमशक्ल
को कहानी में पाने की प्रत्याशा में पृष्ठ-दर-पृष्ठ आगे बढ़ रही हूं और विस्मय में
घिरती जा रही हूं. ’’यह कैसा आदमी है, स्त्रियों सरीखा
कि हमेशा द्वंद्वग्रस्त ! हमेशा अपराधबोध से पीड़ित ! हमेशा अपने को दिलासा देता हुआ !
दफ्तर की फाइलों और गप्प-गोष्ठियों को छोड़ कर घर भर की फिक्र में दुबला होते किसी
और को तो अब तक देखा नहीं कभी!’’
होने की मांग करती हैं. तो क्या (प्रतिपक्षी पर) तमाम तरह के आरोप लगाती भंगिमाओं
या (प्रतिपक्षी द्वारा लगाए गए) आरोपों का उत्तर देती सफाइयों से भरे स्टीरियोटाइप
लेखन को छोड़ अल्पना मिश्र ’उनकी व्यस्तता’ तक आते-आते इतनी
परिपक्व हो गई हैं कि अभियुक्त के कठघरे से निकाल कर पुरुष के साथ सहानुभूतिपूर्वक
संवाद करने को तैयार हैं ? मेरी दिलचस्पी भी सुदामाप्रसाद में बढ़
गई है, लेकिन साथ ही आशंका और उपेक्षा से भर कर लेखिका की ओर भी देख रही
हूं.
सच कहूं तो आशंकित ज्यादा हूं कि पुरुष को सहानुभूति देते-देते यह संवाद
अर्धनारीश्वर का दर्जा देने की हड़बड़ी में स्तवन-गान में ही विघटित न हो जाए. मेरी
आशंका निराधार नहीं है क्योंकि जैसे पुरुष के लिए स्त्रियां भोग्या या देवी की दो
कोटियों में विभाजित ’जीव’ हैं, उसी प्रकार
अधिकांश स्त्री-लेखन अब तब पुरुष को ’सम्मानपूर्वक’ खलनायक का दर्जा
देता आया है, या अपनी ही कथा-रूढ़ि से अघा कर उसे स्त्री के
उद्धारक (अर्धनारीश्वर) के रूप में प्रस्तुत करता रहा है. जहां पुरुष के मन से
अचानक जेंडर बोध समाप्त हो जाता है और संबंधों की ऊबड़खबड़ जमीन समान रसधारा से
सिंचित समतल जमीन बन जाती है. मिसेज सुदामाप्रसाद के मूक गिले-शिकवों को छोड़
दूं तो सुदामाप्रसाद सुनंदा की निकटवर्ती प्रजाति के जीव जान पड़ते हैं. फर्क यह है
कि अपने मृत शिशु की याद में आंसू बहा कर सुनंदा जी हल्का कर लेती है (स्त्री होने
का सुख! ), और सुदामाप्रसाद ’जीवित’ ब्याहता बेटी की
चिंता में भरे-भरे बैठे हैं. पत्नी से देह और जरूरतों का गहरा रिश्ता है, मन
की बात का कोई मार्ग नहीं. न, मोहन राकेश जितने आत्मसंकुचित नहीं कि
मानें मन की बात कह कर आदमी छोटा हो जाता है, लेकिन इतना जरूर
जानते हैं कि ’’जो वे कहना-बताना चाहते हैं, उसे
अपने ही घर में कोई समझता क्यों नहीं?’’ पत्नी सोचती है, घर घुसते ही
खबरों की दुनिया ओढ़-बिछा कर वे उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन वे ही
जानते हैं कि चारों ओर शोर का सैलाब फैला कर वे अंदर के खदबदाते सन्नाटे को चीर
देना चाहते हैं. उस सन्नाटे में शैलजा उन्हें जोर-जोर से पुकार रही है, और
वे हैं कि हर पुकार पर कन्नी काट जाते हैं. सुदामाप्रसाद के लिए शैलजा का बेटी से
क्रमशः अपराध-ग्रंथि में तब्दील होते चलना कहानी को एकाएक ऐसे मोड़ पर ले आता है
जहां पूर्ववर्ती परंपरा से हाथ छुड़ा कर उसे अपनी यात्रा आप तय करनी है.
शैलजा चाहे
और जो भी हो, अन्नपूर्णा मंडल (सुधा अरोड़ा की कहानी ’अन्नपूर्णा
मंडल की चिट्ठी’ की हतभागी नायिका) नहीं है. शायद हो भी सकती थी,
लेकिन
लेखिका ने दृढ़तापूर्वक उसकी शहादत देने से इंकार कर दिया है. क्यों परिवार-समाज
की उपेक्षा पाकर हर बार स्त्रियां ही दम तोड़ती रहें? क्यों न अपराधी
के भीतर पलते अपराध-बोध की पड़ताल की जाए? अपराधी मनुष्य है तो मन की भीतरी
कंदराओं में आत्मसाक्षात्कार के वक्त अपनी ही आंख में आंख डालने का नैतिक साहस
नहीं जुटा पाएगा. फिर क्यों न तभी वार किया जाए जब वह निहत्था है और ईमानदार भी? अल्पना मिश्र की विशेषता है कि वे खबर की
तटस्थता को पारिवारिक परिप्रेक्ष्य देकर मानवीय बनाती हैं और इस प्रक्रिया में
कहानी को एकाधिक स्तरों पर कई चरित्रों के मार्फत घटित होते दिखाती हैं. खबर मामूली-सी
है. दिल्ली के किसी एक परिवार में सात साल से बहू को ताले में बंद रखा गया है. बेटी को ब्याह कर सुर्खरू हुए मां-बाप अपने में मग्न हैं कि ’नो
न्यूज मींस गुड न्यूज’, और ससुराल पक्ष सप्ताह में एक-दो बार खिड़की के
रास्ते खाना पहुंचाकर ’सभ्य’ ढंग से उस कंकाल की मौत की बाट जोह रहा
है. नाराजगी का कारण कुछ भी हो सकता है. बहू द्वारा ’सम्मानजनक’
दहेज
न लाने से लेकर अपमानजनक व्यवहार करने तक. खबर की विभीषिका बड़ी है या भीतर का
अपराध-बोध कि सुदामाप्रसाद बेसाख्ता कह उठते हैं . ’’ये कैसी
व्यस्तता है हमारे समाज की कि लड़की को ससुराल में छोड़ कर निश्चिंत हो गए?’’ विश्लेषण के बिंदु को यहीं फ्रीज कर मैं पहले
अपने भीतर फूटते क्रोध के लावे को बाहर निकाल लेना चाहती हूं क्योंकि जानती हूं
आवेश पूर्वाग्रहों की आंच को लहका कर विवेक को जला देगा.
एक खांटी औरत बन कर मैं
सुदामाप्रसाद को कठघरे में खींच लाती हूं और दन्न से सवाल दाग देती हूं कि पांच
साल से ससुराल में उत्पीड़न झेल रही शैलजा की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम
उठाया. मेरा आवेश सुदामाप्रसाद को गरिया कर ही शांत नहीं हुआ. वह शैलजा सरीखी सभी
लड़कियों की ओर मुड़ गया है कि जिंदा रहने की लालसा में लड़कियां क्यों इतना उत्पीड़न
झेलती हैं? ’मूक भाव से उत्पीड़न न झेलें तो क्या करें
लड़कियां, जबकि उनके समर्थन में समाज में एक भी आवाज नहीं है?’ आवेश
की झाग बैठने लगी तो विवेक सक्रिय होना शुरु हो गया. तब अपने ही सवालों की अनुगूंज
इतनी खोखली लगी कि दिखाई पड़ा साड़ी का पल्लू मुंह में ठूंस कर अपनी आवाज घोटते-घोंटते भी मृणाल कटाक्ष करने से नहीं चूकी है . ’’हां लड़कियों का
कपड़ों में आग लगा कर मर जाना तो अब फैशन सा हो गया है.’’ (टैगोर, ’पत्नी
का पत्र’) कायदे से मुझे सुदामाप्रसाद की पीठ ठोंकनी
चाहिए थी कि उनके अवचेतन में ससुराल में यंत्रणा भोग रही बेटी की याद है, और
चेतन में बेटी का बाप होने की हताशा. सुदामाप्रसाद ऐसा व्यक्ति है जो एक ही समय
बेटी को दुलार और दुत्कार देना चाहता है. वह देख रहा है ’पिता’ को
धकिया कर कोई एक घनघोर पितृसत्ताक पुरुष उसके भीतर आ बैठा है. जब-जब पिता शैलजा की
लड़कों-सी निर्भींकता पर खुश होता है, तब-तब पितृसत्ताक पुरुष उसे तरेर कर
चुप करा देता है कि ’’लड़का ही चाहिए था उन्हें, पर
ईश्वर की कृपा होते-होते रह गई थी.’’ पिता शैलजा के मर्दाने गुणों पर लट्टू
है, लेकिन पितृसत्ताक पुरुष मानता है कि एक उम्र के बाद ’’मैदान
में दौड़-दौड़ कर, उछल-कूद कर हल्लागुल्ला करते हुए खेलना’
लड़कियों
को नहीं सोहता.
पिता खुश है कि अन्याय के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए रणचंडी सरीखी
पुत्री से डर कर भी वह कैसा मीठा-मीठा सा गर्वीला सुकून महसूस कर रहा है, लेकिन
पितृसत्ताक पुरुष लड़कियों की नाक में नकेल डालने का कोई भी मौका नहीं गंवाना
चाहता. उसके पास सदियों पुरानी स्त्री-सुबोधिनी है कि ’सब सह लो.’
पिता
चाहता है भारतीय विवाह अधिनियम, क्रिमिनल लाॅ, मुस्लिम पर्सनल
लाॅ जैसी तमाम बातों की जानकारी रखे, लेकिन पितृसत्ताक पुरुष एक लंबी सांस
भर कर उसे लहरों के सुपुर्द कर देता है. ’’देखो, सबकी
कैसी-कैसी किस्मत होती है. लड़कियां भी अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं.’’
विरोधी को देखना और उसके परंपरावादी दबंग व्यक्तित्व से घबरा कर अपने खोल में आ
दुबकना सुदामाप्रसाद को कमजोर चरित्र नहीं बनाता, बल्कि
पितृसत्तात्मक व्यवस्था की कार्यशैली को रेखांकित करता है जो स्त्री को स्त्री
बनाने के अभियान के साथ पुरुष को पुरुष बनाने का अनुष्ठान भी रच रही है. विचार के
स्तर पर बेटियों की चिंता ने उसे व्यवस्था की हृदयहीनता को समझने का विवेक दिया है,
लेकिन
व्यवहार के स्तर पर व्यवस्था से टकराने का माद्दा अपने भीतर नहीं पाता. मीडिया
जब-जब स्त्रियों के उत्पीड़न और विद्रोह की खबर देता है, वह
उत्सुकतापूर्वक उसकी परिणति को जानना चाहता है, शायद अपने भीतर
अंगड़ाई लेती प्रतिरोधी ताकत का पुनर्गठन कर बेटियों के साथ साझी लड़ाई लड़ना चाहता
हो, लेकिन पाता है कि अधबीच काल-कवलित हो गई खबर के अलावा उसके पास पैर
टिकाने को कोई जमीन नहीं. वास्तविकता यह है कि किसी भी बड़ी निर्णायक लड़ाई को लड़ने
का हौसला उसके पास नहीं है. बाकी लड़कियों को ’निबटा’ कर
पांच साल से ससुराल की कैद में जकड़ी शैलजा को लिवा लाने का इरादा आत्मप्रवंचना की
ही एक रूप है.
लेने
को उत्सुक सुदामाप्रसाद को अल्पना मिश्र ने व्यंग्य की तीखी चुटकियों और सहानुभूति
की तेज बौछारा के साथ रचा है, मानो चोर-सिपाही का कोई खेल चल रहा हो
दोनों के बीच.लेखिका के साथ गहरा सख्य भाव स्थापित होते ही सुदामाप्रसाद उनके
सामने अपना अंतर उलीचने को होते ही हैं कि वहीं कहीं कोने में दुबका चोर आत्मरक्षा
के प्रयास में भाग कर सामने आ खड़ा होता है
और चैतन्य हो सुदामाप्रसाद लेखिका के चेहरे में सिपाही का अक्स चिपका देते हैं. इस
सारे आयोजन में वे एक बात स्वीकार करते हैं कि लड़कियों को ’ठिकाने लगाने,
सहनशील
(दब्बू) बनाने और घर के आंगन में खुलने वाले आसमान तक महदूद रखने का प्रशिक्षण
उन्हें किसी ’अज्ञात शक्ति’ ने दिया है,
लेकिन
यह अज्ञात शक्ति पितृसत्तात्मक व्यवस्था है और इसे उन जैसे सुदामाप्रसादों की घुटी
चुप्पी ने बनाया संरक्षित किया है, नहीं मानते. इसलिए हर दुखद अनुभूति के
साथ आश्चर्य और असहायता का भाव उन्हें जकड़ लेता है. वे दबे-दबे ढंग से स्वीकार
करते हैं कि स्त्री को उन्होंने पत्नी और बेटियों के साथ जिए जा रहे संबंध के
मार्फत नहीं जाना; औरतों के स्वभाव के बारे में प्रचलित ’सूक्तियों’
के
जरिए पत्नी और बेटियों को ’समझने’ का प्रयास किया
है. इसलिए चकित और आहत हैं कि ’’पत्नी अपना एक विचार भी रखती थी,
और
उनकी बात के एकदम उलट भी कह सकती थी.’’ सुदामाप्रसाद ने इतना झन्नाटेदार तमाचा
शायद जिंदगी में नहीं खाया कि छाया समझ कर जिसके प्रति बेपरवाह रहे, वही
उनके कदमों तले बैठ कर अपना कद-बुत बढ़ाती रहीं.
पुरुष के रूप में नहीं उभारतीं, संवेदनशीलता को व्यक्तित्व में रचा-बसा
कर संवाद के लिए तड़पती बेचैनी के रूप में रचती हैं. लेकिन संवाद किससे? पत्नी
से? जिस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। बेटियों से? जो बोझ के अलावा
और कोई भाव मन में नहीं उठातीं. ’’ये कैसी दूरी रह गई उनके रिश्ते में?
कैसी
दुनिया में रह रहे हैं वे लोग? बदलना होगा यह सब।’’ जैसा
चारित्रिक गठन है सुदामाप्रसाद का, उससे लगता तो यही है कि उमड़ का विलीन
हो जाने वाली लहर की तरह वे फिर उसी ’अभ्यस्त’ ढर्रे को जीने
लगेंगे, लेकिन यह भी सच है कि रोशनी के ऐसे बिंदु ही अंधेरे की काली चादर में
सूराख बनाते हैं। शायद इसीलिए वे अपनी अंतिम परिणति में कालिंदीचरण की तरह ’आतंक’
को
हथियार बना कर आत्मरक्षा में नहीं फुंफकारते, बल्कि सुनंदा की
तरह दुर्बलताओं की धंसी जमीन में दबे भविष्य और व्यक्तित्व का लेखाजोखा करने लगते
हैं। जाहिर है तब यह स्थल स्त्री-मुक्ति की लड़ाई को लैंगिक पूर्वाग्रहों के
इर्दगिर्द बुनी गई स्त्री और पुरुष दोनों की मुक्ति की साझा लड़ाई का रूप देने की
संभावनाओं से युक्त दिखाई पड़ता है.
गई है. सबसे पहले दोनों लेखकों ने लैंगिक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान को भुला कर ’मनुष्य’
होने
का विश्वास अर्जित किया है. फिर इतरलिंगी चरित्र के भीतर प्रवेश करते हुए लैंगिक
विषमता के कारण भीतर के द्वंद्वों और अंतर्विरोधों को पहचानने का प्रयास किया है. इस कारण दोनों सिमोन द बउवा की इस मान्यता को झुठला पाए हैं कि पुरुष (स्त्री) कभी
स्त्री (पुरुष) का विश्वसनीय चित्रण नहीं कर सकता. यही नहीं, दोनों
लेखकों की विचार-यात्रा एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुख हुई है और वह है युग के भीतर
खदबदाती उन गोपन सच्चाइयों को सामने लाना जो स्टीरियोटाइप्स के रक्षा-कवच को तोड़े
बिना बाहर लाई ही नहीं जा सकती. बेशक जैनेंद्रकुमार अपने विपुल साहित्य, विशेषकर
’सुनीता’, ’त्यागपत्र’, ’सुखदा’ उपन्यासों
तथा ’जाह्नवी’, ’नीलम देश की राजकन्या’ कहानियों
में स्त्री के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का भ्रम देते हुए बरकरार रखते हैं, लेकिन
पत्नी (स्त्री) के भीतर अपनी स्थिति (जड़ता) और संभावना (वैचारिक गत्यात्मकता पाने
की अभिलाषा) को चीन्हने का विवेक पैदा करते हैं. यह ऐसी छटपटाहट है जो क्रमिक भाव
से एक-दूसरे में गड्डमड्ड हुए सही और गलत को अलग-अलग पहचानने और पुनव्र्याख्यायित
करने की तमीज देती है. इसी कारण साहित्य में अनुकरणीय चरित्र के रूप में गढ़ी गई
भाग्यवती (श्रद्धाराम फिल्लौरी) समय बीतने के साथ-साथ समाज में ’सीमंतनी
उपदेश की रचयिता अज्ञात हिंदू महिला, शिवरानीदेवी प्रेमचंद, महादेवी
वर्मा और सुभद्राकुमारी चैहान (उल्लेखनीय है कि सुभद्राकुमारी ’झांसी
की रानी’ की गायिका के रूप में नहीं, कहानीकार के रूप में मूल्यांकन की मांग
करती हैं) के रूप में दिखाई देने लगती हैं.
स्त्री की अस्तित्व और व्यक्तित्व संपन्न होने की क्रमिक लड़ाई का चित्रण करता है,
वहीं
पुरुष सामंतवाद की उन्हीं कंदराओं में बैठा हिंसक, आत्मकेद्रिंत,
संवेदनहीन
एवं रूढ़ रूप में दिखाई देता है. स्वयं जैनेंद्र कालिंदीचरण को पितृसत्ताक सामंत से
इतर अन्य कोई पहचान नहीं दे पाते. इसके विपरीत अल्पना ने निर्ममतापूर्वक दोनों
स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश की है. इसलिए ’पत्नी’ कहानी
में कालिंदीचरण को पत्नी की भूख से ज्यादा अपनी और मित्र-मंडली की भूख की फिक्र है,
जबकि
सुदामाप्रसाद पत्नी को हड़का देने के बाद अपराध-बोध से भर उठते हैं. यह ’अभ्यास’
बार-बार
उनके मानसिक बौनेपन की ओर इशारा करते हुए अहसास कराता है कि पत्नी का स्पेस घेरकर
वे अपनी ही मर्यादा घटा रहे हैं. यही वजह है कि जैनंद्र की कहानी विचार के स्तर
पर खुलती है, और वहीं कहीं ठिठकी खड़ी रह जाती है. सारी
जद्दोजहद स्वतंत्रता का अर्थ समझे बिना ’भारतमाता’ को स्वतंत्र
कराने की परोक्ष लड़ाई में केंद्रित हो जाती है. अल्पना शब्दों के जरिए विचार का
आस्वाद नहीं करतीं, स्टूल पर बैठ कर सोचती पत्नी को एकाएक
जिम्मेदारी के बोध और कर्मठता से भर कर एक नई चारित्रिक गढ़त देती हैं. इसलिए कहानी
आखिरी पंक्ति के साथ खत्म होकर भी खत्म नहीं होती. कहानी से बाहर समाज में निर्भीक
भाव से नागरिक दायित्व निभाती नई स्त्री को प्रकाश में लाती है तो एक बार फिर
कहानी के भीतर प्रविष्ट हो पाठक से मिसेज सुदामाप्रसाद की सोच को परिप्रेक्ष्य
देने और सोच का खाका खींचने का अनुरोध करती है. उल्लेखनीय है कि जैनेंद्र
सुनंदा-कालिंदी को अपनी-अपनी परिधि में घूमती दो इयत्ताओं की तरह चित्रित करते हैं
जहां संवाद की कोई गुंजाइश नहीं.
अल्पना के पात्र अपनी-अपनी परिधि में घूमने के
अभ्यास और अभिशाप दोनों से त्रस्त हैं, इसलिए संवाद के जरिए जब पल भर को
टकराते हैं, तब उस टकराहट से उनके मनोजगत में भारी उथल-पुथल
मचती है. देख रही हूं कि ’उनकी व्यस्तता’
कहानी
’पत्नी’ कहानी के इकहरे चरित्र से काफी दूर हुए जा रही
है. चरित्र-चित्रण में स्याह-सफेद रंग का इस्तेमाल तो जैनेंद्रकुमार ने किया है –
सुनंदा को भरपूर सहानुभूति देकर ही नहीं, सुनंदा के परिपाश्र्व में कालिंदीचरण
की बदनीयतियों को उघाड़ कर भी. अल्पना एक के सहरे दूसरे को उघाड़ती नहीं, कथा-परिदृश्य
से अनुपस्थित सूच्य पात्र शैलजा को रचने लगती हैं. महारत ऐसी कि शैल-पुत्री (दबंग,
निर्भीक,
ऊर्जावान
चरित्र) को अपने ही कूलों से क्षरित करके रेतीले बियाबान में खो जाती बरसाती नदी
के रूपक में बांधते-बांधते मां-बेटी दोनों को एक-से त्रास की दो हमशक्ल परिणतियां
सिद्ध कर देती हैं. हां, स्त्री के पत्नीत्व (सुहाग-गाथा) पर
भरपूर प्रकाश डाला है उन्होंने (महादेवी वर्मा के निबंध ’हिंदू स्त्री का
पत्नीत्व’ का स्मरण हो आया न!), लेकिन फिलहाल मेरे सामने सुदामाप्रसाद
का मुखर चिंतन है और उसी के समानांतर विचार-यात्रा करते हुए मिसेज सुदामाप्रसाद
द्वारा बोले गए तीन वाक्य हैं.’’कुछ चीजों के लिए थोड़ा पहले सोचना पड़ता है’’,
’’भाग्य
क्या होता है? सोचने-समझने की जरूरत होती है’’ तथा
’’जब-जब बोली, आप व्यस्त रहे’’ – ये
तीनों वाक्य संदर्भ से जुड़ कर (शैलजा की नवविवाहिता सहेली रूबीना का आगमन और
वधू-उत्पीड़न की खबरें) ससुराल में बेटी की दुर्दशा के लिए मां-बाप की परोक्ष
भूमिका को सामने लाते हैं.
शैलजा की मां की सोच में दबंग लड़की को तिलचट्टा बना दिए
जाने की स्मृतियां हैं. वह देखती है हर अनाचार-अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली
उस लड़की ने जब बैडमिंटन के कोच को बदतमीजी के जवाब में थप्पड़ मारा, तो
वे सब कितने खुश थे कि अपनी संतान को उन्होंने देश का जिम्मेदार नागरिक बनाया है. लेकिन उसी लड़की ने, ससुरालवालों द्वारा बतौर सजा खाना-पीना बंद किए
जाने पर जब रात को रसोई के सारे बर्तन पटक कर अपना विरोध जताया तो वे जरा भी
उत्फुल्ल नहीं हुए. अपने भीतर पलती आशंकाओं को उन्होंने शैलजा के भीतर दहशत बना कर
रोप दिया कि उसकी जिंदगी उस घर से बाहर कहीं नहीं. तिल-तिल कर मरने की यातना को
बेटी के माथे पर लिखते हुए शायद मां को क्षीण-सा विश्वास रहा हो कि ’सयानी’
होकर
बेटी भी गृहस्थी की गाड़ी को खींच ले जाएगी. लेकिन यह तो सच को अनदेखा करने का
पाखंड है. मरने का संत्रास भोग कर जीने का आह्लाद कैसे पाया जा सकता है ? हो
सकता है तब मृणाल उसके पास चली आई हो और कहा हो कि बचने के लिए मरना नहीं पड़ता,
जीवन
की लगन से लौ लगा कर ही जिया जा सकता है.मृत्यु यदि दोनों तरफ है तो जीवन को पाने
के लिए क्यों न जूझा जाए? हाथ पर हाथ धर कर बैठने से तो हम
आततायी का पाला ही मजबूत करते हैं. अल्पना मिश्र ने मिसेज सुदामाप्रसाद की ’सोच’
का
चरित्र गढ़ने के लिए शैलजा को पृष्ठभूमि के तौर पर और टी वी खबर को उद्दीपक के तौर
पर प्रयुक्त किया है. मीडिया में लगातार आती खबरों ने मानो उसे चेताया है कि गले
में अपराध-बोध का पत्थर बांध कर दरिया पार नहीं किया जा सकता.
अपराधी के पक्ष में
खड़ी अपनी भागीदारी को पहचान कर प्रायश्चित करना जरूरी है. अब वह जमाना नहीं कि
गोबर और गौ-मूत्र को मुंह में रखकर आत्मिक शुद्धि का ढिंढोरा पीटा जाए। कर्म इंसान
की चेतना के उद्घाटक हैं. इसलिए मौत की बाट जोहती तालाबंद वधू की खबर फ्लैश करने
के बाद अल्पना ’’दिल्ली की सड़कों पर पैंटी और ब्रा में भागी जा
रही’’ लड़की की खबर ठीक उस समय दिखाती हैं जब धीरे-धीरे रिस-रिस कर आता
बदलाव कहानी में एकाएक बड़ी उलट-फेर कर देने की ताकत पा लेता है. नेपथ्य में बित्ता
भर जगह लिए खड़ी पत्नी क्रमशः केंद्र में आ रही है – कत्र्ता की भूमिका के साथ,
और
सुदामाप्रसाद नेपथ्य में जा रहे हैं. चेतना और आत्मपड़ताल उसके व्यक्तित्व का
मानवीय पहलू बुनते हैं जिन पर परंपरा, संस्कार और दुनियादारी हावी है। इसलिए
सुदामाप्रसाद के पास बाकी बेटियों के लिए आनन-फानन में वर ढूंढने की दुश्चिंता है
तो पत्नी के पास सदियों की चुप्पी और निर्णयहीनता से बुनी निष्क्रियता को तोड़ने का
एकमात्र विकल्प. इसलिए आश्चर्य नहीं कि अंतिम खबर सुदामा की गैरमौजूदगी में घटती
है और पत्नी के सामने एक बड़ी दुष्कल्पना के रूप में आती है. ’नंगी
होने को देख लिए जाने के डर’ को जीत का भाग आई वह अर्धनग्न युवती
शैलजा भी हो सकती थी, यदि डर को वर्जना बना कर खुद को जिंदा दीवार
में चुनने का प्रशिक्षण उन्होंने शैलजा को न दिया होता. वह अविलंब उस बहादुर लड़की
में अपनी और शैलजा की कुचली हुई बहादुरी जोड़ देना चाहती हैं, नहीं
तो कौन जाने इन्हीं लड़कियों को कामोत्तेजना भड़काने के आरोप में समाज एक और जघन्य
दंश देकर अपनी मर्दानगी पर इठलाने लगे.
मैं एक बार फिर कहानी की अंतिम पंक्ति को
दोहराना चाहती हूं. ’’पत्नी चुपचाप भीतर आई और अपने पुराने बक्से से
अब तक जोड़ी पूंजी निकाल कर उस सड़क की तरफ भागी, जिधर से दिल्ली
जाने वाली बस मिलती है.’’ बेशक सुनंदा से बहुत अलग है यह पत्नी, लेकिन
सुनंदा का विलोम नहीं. यदि बेड़ियों की जकड़न के बीच सुनंदा ने पोर-पोर अपने को न
महसूसा होता तो उसकी वंशज बन कर कैसे आती वह? अल्पना का
योगदान इतना है कि जैनेंद्रकुमार की वैचारिक लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया है;
पत्नी
को लक्ष्मण-मूर्छा से मुक्त किया है; और पति को उस उर्वर मनोदशा में ऊभचूभ
करते दिखाया है जिसमें तीन-चैथाई सदी पहले जैनेंद्र ने सुनंदा को रखा था. जिस गति
से समय बदल रहा है, कौन जाने कुछ दशकों में ही मीडिया और समाज
के पितृसत्तात्मक चरित्र को पति-पत्नी
दोनों मिलकर चुनौती दें क्योंकि पितृसत्तात्म्क व्यवस्था स्त्री के स्पेस को ही
नहीं घेरती, पुरुष की अंतःशक्तियों को क्षरित कर आगे बढ़ने
के अवसरों को भी बाधित करती है.