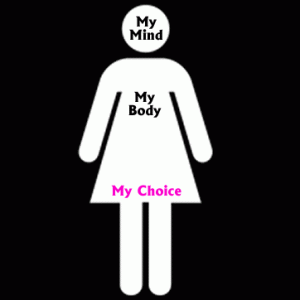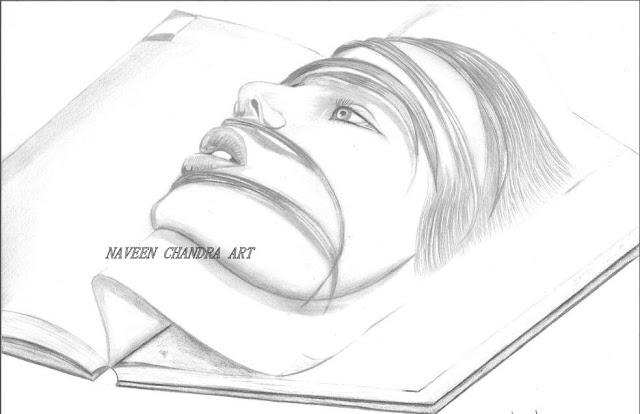अजय कुमार यादव, शोधर्थी , जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली . संपर्क :ajjujnu@gmail.com
Mobile no.8882273975
पिछले कुछ दशकों में विचारधारा और चिन्तन की दुनिया में आए वैचारिक और अवधारणात्मक बदलावों ने ‘अस्मिता’ के प्रश्न को केन्द्र में लाकर खड़ा कर दिया. विचारधारा और चिन्तन के दुनिया में आए इन बदलावों ने कई प्रकार की अस्मिताओं को जन्म दिया, मसलन-राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता, स्त्री अस्मिता, दलित अस्मिता, आदिवासी अस्मिता और अल्पसंख्यक अस्मिता इत्यादि.‘अस्मिता’ पर हुए तमाम शोधों और अनुसंधानों के बावजूद ‘अस्मिता’ की परिभाषा विभिन्न सामाजिक संरचनाओं के द्वारा विभिन्न है. यद्यपि यह सभी जानते है कि इस शब्द का उपयोग वैचारिक विमर्शों और अकादमिक दुनिया में कैसे किया जाय? यह बताना सचमुच कठिन है कि ‘अस्मिता’ की ‘फलाँ’ परिभाषा इसे सम्पूर्णता में परिभाषित करती है लेकिन इस बारे में लोगों की सामान्य और स्पष्ट समझ है कि इस शब्द का प्रयोग कब किया जाए और क्यों किया जाए ? आश्चर्य जनक बात यह है कि किसी भी विद्वान ने इसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं महसूस की और हिन्दी में तो इस पर सामग्री न के बराबर है और इसीलिए सामान्यतः ‘अस्मिता’ के प्रति पाठक की जो अकादमिक समझ है वह भी अस्पष्ट है. अकादमिक दुनिया में फैशन की तरह उभरा यह शब्द आज कुछ विशेष सामाजिक वर्गों की तरफ इंगित करता है और इन सामाजिक संरचनाओं की पहचान की निर्मिति के रूप में रूढ़ हो चुका है और अब यह शब्द संदर्भों के आधार पर अपने अर्थ खोज लेता है.
समकालीन अस्मिता विमर्शों की विचारधारा और मुद्दे अलग-अलग होने के बावजूद सभी आंदोलन अस्मिता आंदोलन का दावा जरूर करते हैं. हालांकि इस अस्मिता का स्वरूप सभी के लिए एक जैसा और सुपरिभाषित नहीं है. जब कोई समुदाय अपने अस्मिता तलाशने की कोशिश करता है तो उसके सामने ये सवाल सहज ही आ जाते है कि ‘हम कौन है?’ और दूसरे समुदायों के मुकाबले हमारी समाज में क्या हैसियत है? या हमारे बीच क्या सह संबंध है? इन सवालों से टकराकर ही व्यक्ति/समुदाय अपनी अस्मिता निर्माण की प्रक्रिया की शुरूआत करता है.
स्त्रियाँ अपने अस्मिता के लिए जिन सवालों से टकराती हैं और परस्पर वाद-विवाद करती हैं उसे ही स्त्री विमर्श के रूप में देखा जाता है. सामान्य शब्दों में कहें तो स्त्री के अस्तित्व को रसोई व बिस्तर के गणित से परे स्थापित करने की मुहिम ही स्त्री अस्मिता है. स्त्री अस्मिता का मतलब है:- स्त्री-पुरुष के बीच घटने वाले संबंधों को बिना नकारे, उसके पारस्परिक संबंध से मुक्ति. नारी तुम केवल श्रद्धा हो, देवी माँ, सहचरि प्राण जैसे ब्रह्म वाक्यों को सुनते हुए होश संभालने वाले इस सामाजिक मानस को परिवर्तित कर देना अकल्पनीय बात थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उभरे सामाजिक अस्मिता के आन्दोलनों ने स्त्री की छवि, स्त्री की सामाजिक स्थिति और स्त्री के बारे में प्रचलित रूढ़िगत और मिथकीय अवधारणाओं को तोड़ा है.
सदियों से उसके जिस ‘स्व’ का अपहरण पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने किया था उसे अब वह वापस पाने के लिए प्रयासरत है.स्त्री मुक्ति की बात करते हुए ये जानना जरूरी है कि स्त्री को किससे मुक्ति चाहिए? किसने उसे अधीन बना कर रखा है? और स्त्री भी अधीन बनी रही, इसके क्या कारण हो सकते है? रमणिका गुप्ता लिखती है कि- “एक साझी व्याख्या तो स्त्री की समझ में आ ही गई है कि पुरुष ने उसके मन को गुलाम बनाने से पहले उसे परिवार, ब्याह, संतान और समाज की लक्ष्मण रेखाओं के बाड़े में कैद करके उसके शरीर को गुलाम बनाया और उसे सभी अधिकारों से वंचित किया. पुरुष को जब जरूरत हो तो प्यार, आलिंगन व चुंबन के हथियार का इस्तेमाल कर या उसके रूप का बखान कर उसे गौरवान्वित किया- सर्वोत्तम करार किया, लेकिन उसके सब अधिकार छीन लिए ताकि वह उसी के प्रति समर्पित रहे. किन्तु, आज समय बदल रहा है, वह इस छद्म को पहचान गई है. आज वह घर, परिवार, पुरुष का सुरक्षात्मक छाता, रिश्तों की भावनात्मक बेड़िया- सभी को नकार अपनी अस्मिता के निर्माण के लिए जूझने लगी है.”1
स्वत्व का बोध होना स्त्री मुक्ति की पहली सीढ़ी है क्योंकि स्वत्व का बोध होने पर ही स्वत्व की रक्षा का सवाल खड़ा होता है. यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ऐसी है जो गोहत्या पर दंगे कर देती है लेकिन भ्रूण हत्या व वधू हत्या पर चूँ नहीं करता. दरअसल दुनिया की ओर पीठ कर बैठ जाने की प्रवृत्ति या सामाजिक सत्ता को अस्वीकार कर अपने ही संसार में मग्न रहने की स्थिति से यहाँ काम नहीं चलने वाला है. इधर के दिनों में तो स्त्री सौंदर्य की प्रशंसा करने का हथकंडा जो पुरुष जाति ने अपनाया, वह वास्तव में स्त्री को व्यक्ति से वस्तु की तरफ गतिशील करता है और स्त्री का ध्यान वास्तविक स्वतंत्रता से अलग हटाता है. दुःखद बात यह है कि पैसे, सत्ता और प्रतिष्ठा के समीकरण वाले इस समाज में स्त्री भी पुरुष की अनुगामिनी हो रही है और यह इन मुक्तिगामी आन्दोलन को सही दिशा में नहीं ले जा रहा है. इससे स्त्री मुक्ति की डोर स्त्री के हाथों से फिसलने का भी डर है. स्त्रियों को यह समझना होगा कि वे कितने विडम्बनापूर्ण समय में जी रही है, जहाँ एक तरफ शक्ति, ज्ञान और सम्पदा के रूप में स्त्रियों (क्रमशः दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी) की पूजा होती है और दूसरी तरफ स्त्रियों को इन्हीं तीन चीजों से हमेशा से वंचित रखा गया. शक्ति का काम तो हमेशा पुरुषों का ही माना गया.
दरअसल यह पूरा का पूरा मामला ‘जेण्डर’ और ‘सेक्स’ का है. सेक्स जो कि जैविक विभेद को इंगित करता है लेकिन जेंडर सांस्कृतिक अर्थ की अभिव्यक्ति है. निवेदिता मेनन ने लिखा है कि- “खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी. इस पंक्ति का क्या अर्थ निकलता है? वास्तविकता में यह उस सूरत में भी जबकि एक औरत ऐसे अपरिमित शौर्य और वीरता का प्रदर्शन कर रही है, उसके इस गुण को ‘नारी सुलभ’ गुण नहीं माना जा रहा है यानि कुल मिलाकर बहादुरी का गुण पुरुषों की ही विशेषता कहलाती है, फिर भले ही कितनी भी औरतें बहादुरी का प्रदर्शन करती रहें और कितने ही पुरुष पीठ दिखाकर भाग खड़े होते रहें.”2 कुल मिलाकर इस संदर्भ में केवल इतना ही कि इस विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का काम केवल रोना है.तैत्तिरीय संहिता के अनुसार उसे किसी प्रकार की शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं, वरन् धन उपार्जन करने या अपने शरीर को अवाहित क्रियाओं तक से बचने का अधिकार उसे नहीं है. प्राचीन काल से ही गार्गी जैसे कुछ उदाहरणों को छोड़ दिया जाय तो शिक्षा स्त्रियों के लिए जरूरी नहीं समझा गया इसलिए उनको उससे वंचित रखा गया.
कुमकुम राय ने लिखा है कि- “एक तरफ हमें गार्गी जैसी महिला दार्शनिकों की चर्चा मिलती है वहीं इस बात के बहुत थोड़े प्रमाण मिलते है कि शिक्षा प्रसार के औपचारिक संस्थानों में बतौर छात्रा या शिक्षिका, महिलाएँ भी उपस्थित थीं. दूसरे शब्दों में, ऐसी महिलाएँ भी संभवतः नियमित बौद्धिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करने के बजाय सिर्फ गाहे-बगाहे ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थीं.”3 इस स्थिति को और इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मनु महाराज कैसे पीछे रहते, उन्होंने स्त्रियों को उपनयन संस्कार में शामिल होने से रोका. चूँकि उपनयन संस्कार पवित्र ज्ञान प्राप्ति का प्रारम्भिक बिंदु था. इसे और गहरे स्थापित करने के लिए उन्होंने कई विकल्प भी सुझाए, जैसे- ‘स्त्रियों के लिए विवाह करना पुरुषों के उपनयन के समकक्ष है, पति की सेवा करना छात्र होने के समान है और घर के कामों को संपन्न करना पवित्र अग्नि की पूजा अर्चना के समान है‘ ( मनुस्मृति प्रकरण 2-67) कुमकुम राय ने लिखा है कि- “ऐसे निर्देशों को स्वीकार कर लेने का मतलब होता है कि कोई भी गैर घरेलू काम को नारीत्वहीन और गैर पत्नी कार्य माना जाता.”4
और जहाँ तक स्त्रियों की सम्पदा पर अधिकार की बात है, आर्थिक स्वतंत्रता जरूर बढ़ी है स्त्रियों में, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का होना स्त्री के शोषित न होने की गारंटी नहीं है. आर्थिक स्वतंत्र होते हुए भी उसका शोषण हो रहा है, क्योंकि यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था उसे पचा नहीं पा रही है. आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर स्त्री को भी दहेज के लिए मार दिया जाता है.
अनामिका ने पितृसत्ता के नजरों में स्त्री की जो छवि निर्मित है उसकी बानगी प्रस्तुत किया है-
‘पढ़ा गया हमको / जैसे पढ़ा जाता है कागज
बच्चों की फटी काॅपियों का / ‘चनाजोर गरम’ के लिफाफे के बनने से पहले
देखा गया हमको / जैसे कि कुफ्त हो उनींदे
देखी जाती है कलाई घड़ी / अलस्सुबह अलार्म बजने के बाद
सुना गया हमको / यों ही उड़ते मन से
जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेंटों पर / ठसाठस्स ठुंसी हुई बस में
भोगा गया हमको / बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुःख की तरह.’
और आखिरकार इन स्थितियों से अफना कर लिखती हैं कि-
हे परमपिताओं / परमपुरुषों-
बख्शो, बख्शो, अब हमें बख्शो!
लेखिकाएं सिर्फ अपने को एक इंसान का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अर्धांगिनी , देवी जैसे फुसलाने वाले शब्दों पर संदेह करने लगी हैं. वास्तव में मोहक शब्दों का यह माया जाल स्त्री को आत्ममुग्धता की ओर ले जाता है और वह इस शब्द खेल में उलझती हुई कठपुतली की तरह नाचती है. इन षड्यन्त्रों को समझते हुए स्त्री अपनी अस्मिता का निर्माण कर रही है. स्त्री अपनी पहचान के लिए बेचैन है, अपनी पहचान पर सिर्फ अपना हक समझती है. अस्मिता निर्माण में यह प्रथम सोपान है ‘स्व’ का बोध. स्त्री को अपने ‘स्व’ का पूर्ण बोध है. तरन्नुम रियाज ने लिखा है कि-“उसे अपनी पहचान पर/ इतना नाज है/ कि वह मुझे नहीं पहचानता है/ वह कहता है/ उसकी पहचान ही है मेरी पहचान / और इसके अलावा / मेरा कोइ वजूद नहीं है मुमकिन / कि/ उसकी माँ की पहचान भी / उसका बाप था / और सबकी माँओ की पहचान/ सबके बाप होते हैं/ मगर मैं अपने आप को पहचानती हूँ/ अपने माँ बनने और/ उसके बाप बनने के बहुत पहले से/ वह भले ही मुझ पर/ अपनी पहचान थोपता है/ मगर मैं उसे/ अपनी पहचान नहीं दूंगी!” ‘सेवा समर्पण और सहनशीलता’ जैसे तीन ‘स’ वाले शब्दों के बीच कैद स्त्री को अपने अस्तित्व का भान है.
“तुम इन्द्रधनुष बनोगे आकाश का
मैं छत के चमगादड़ गिनूँगी
साथी ये नहीं होगा.” ; मेघना पेठे
आज स्त्री मजबूर नहीं है, वह अपना अस्तित्व समझने लगी है. उसे यह पता हो गया है कि उसकी गतिशीलता को बाधित करने के लिए ही पुरुष-सत्तात्मक समाज वर्जनाओं की बेड़ियाँ गढ़ता रहा है. स्त्री की ममता का उसकी कमजोरी मानकर पुरुष ने उसकी ममता ग्रन्थि को बेड़ी बनाकर स्त्री को गतिहीन कर दिया. उसकी कोख, उसकी देह और उसके सेक्स पर किसी एक पुरुष के आधिपत्य का सिद्धांत इसलिए गढ़ा गया कि उन्हें एक ‘वस्तु’ बना दिया जाय और वे खुद भी अपने को वस्तु ही समझें. इसके लिए पितृसत्तात्मक समाज ने रिश्तों का जंजाल बुना और इन रिश्तों की मर्यादा को त्याग और ममता से सींचने का ठेका पुरुषों ने स्त्रियों को दे दिया. पुरुष जब मन करे तो रिश्तों को तोड़ ले लेकिन स्त्री नहीं तोड़ सकती. अगर वह तोड़ देती है तो उसे वाचाल तथा हठधर्मी कहकर, उसे डायन कहकर सरेआम नंगे पूरे गाँव में घुमाए जाने का रिवाज पुरुष जाति ने बनाया. लेकिन स्त्री भी अब खुलकर बोलने लगी है, वह अब ताल ठोंक कर कह रही है कि हाँ मैं बुरी औरत हूँ. निरुपमा दत्त ने लिख है कि-“तुम मेरे शहर आओगे/ तो बुरी औरतों की फेहरिस्त में मेरा नाम भी दर्ज पाओगे/ मेरे पास है वह सब कुछ/ जो एक बुरी औरत के पास होना/ बेहद जरूरी है/ मुँह में जलती आग/ धड़कता दिल/ थिरकती रग-रग/ हाथ में छलकता जाम/ पाँव चले सड़क/ ऊपर खुला आसमान/ सहने का मेरा हौसला बेमिसाल है/
मेरे पास कहने को पूरा आसमान है.”
जब स्त्री के अन्दर इतना आत्मसम्मान आ जाता है तभी वह निर्णय ले पाती है. निर्णय लेने के अधिकार को ही पन्ना नायक ‘स्त्री मुक्ति’ कहती है-
“दो पैरो में से
कौन-सा एक पैर
खौलते पानी में रखूँ
और कौन-सा जमी हुई बर्फ पर
यह निर्णय लेने का अधिकार
यानि ‘स्त्री मुक्ति’.
कविताओं के कई अंदाज और तेवर मिलेंगे. कहीं पर वे पितृसत्ता को चुनौती देती हैं तो कहीं पर प्रेम से बतियाती भी है. अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखकर वे बहस करती है. वाद-संवाद की शैली में कहीं पर मुक्ति का गणित पेश करती हैं तो कही पर घिसे-पिटे पुराने आदर्शों को तोड़कर उसे नए अंदाज में पेश करके पुरानी गं्रथि को तोड़कर ही अपनी अस्मिता की खोज करती हैं.
स्त्रीवादी चिंतकों और विचारकों ने स्त्रियों की मुक्ति में कुछ सार्थक कदम जो बताए हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे- स्त्रियों को अपने अस्तित्व के प्रति बोध कराना, स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान देना, आर्थिक स्वतंत्रता और देह की स्वतंत्रता. यहाँ यह बात भी काबिलेगौर है कि देह की स्वतंत्रता केवल यौन से मुक्ति नहीं है. अनामिका ने कहा है कि- “पागल हैं लोग जो देह मुक्ति का अर्थ देह को ‘मुक्त चरागाह’ बना देना समझते हैं. हमेशा-हमेशा से औरत की देह ही उसके शोषण की प्राइमरी साइट रही है- मार-पीट, गाली-गलौज, बेगार, भावहीन, यांत्रिक सम्भोग, बलात्कार, डायन-दहन, पोर्नोग्राफी, पर्दा-प्रथा और सती, असुरक्षित प्रसव और तद्जन्य बीमारियाँ- सबके मूल में ‘देह’ ही तो है.”5 तो देह की मुक्ति को केवल यौन से मुक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि स्त्री देह से जुड़ी वो सभी शोषक गतिविधियों से मुक्ति ही देह मुक्ति है. स्त्री की देह उसकी अपनी है और उससे जुड़े सभी निर्णय उसके अपने हो. चाहे वह विवाह का मामला हो या सन्तानोत्पत्ति उसके निर्णय का भी सम्मान किया जाय. दूसरी तरफ स्त्री की देह का बाजार द्वारा जो उपनिवेशीकरण किया गया उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है. जो स्त्रियाँ खुद को बाजार को सौंपने के लिए उतावली हैं उन्हें भी यह समझना होगा कि बाजार उन्हें नहीं उनकी देह को खरीद रहा है जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है. लीलाधर मंडलोई ने लिखा है कि- “स्त्री सोच के बदलते आयाम अपनी देह के उपयोग को लेकर सीमित अर्थों में कदाचित सही लगे किंतु नारी मुक्ति आंदोलन के परिपे्रक्ष्य में वे अनुकूल नहीं होंगे.”6
स्त्री विमर्श प्रमुख रूप से पितृसत्तात्मक समाज के विरूद्ध आन्दोलन के रूप में शुरू हुआ. मुख्य मुद्दा था स्त्री को वे सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो अब तक पुरुष सत्ता के कारण नहीं प्राप्त हो सके. पश्चिम में स्त्री विमर्श लेखन का प्रारम्भ 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही शुरू हो गया था. परन्तु हिन्दी में स्त्री विमर्श आन्दोलन बहुत बाद में शुरू हुआ. किन्तु स्त्री-मुक्ति आंदोलन और स्त्रीवादी चेतना के फलस्वरूप नारी जीवन में एक नयी उर्जा दिखाई पड़ी, और एक नया उन्मेष आया. अब वे अपने अधिकारों के लिए पुरुष के समानान्तर अपनी दुनिया देखने लगीं. पुरुष के वर्चस्व को चुनौती देती हुई हिन्दी साहित्य में कई स्त्री-चिंतक देखी जा सकती है. जैसे- महाश्वेता देवी, कृष्णा सोबती, चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, अनामिका आदि.
विशेषकर दलित स्त्री, जाति व पितृसत्ता रूपी दोहरे अभिशापों के तीखे दंशों को झेलने के लिए अभिशप्त है. भारतीय समाज व्यवस्था में स्त्री होने के साथ दलित होना स्त्री के संतापों को कई गुना बढ़ा देता है. भारतीय समाज जाति व धर्म पर आधारित है. पितृसत्तात्मक भी है. पितृसत्ता ने सारे नियम अपनी सुविधा के अनुसार बनाये हैं. दलित स्त्रियां जाति और पितृसत्ता दोनों का उत्पीड़न झेलती हैं. घर के बाहर गैर दलित उन्हें लहूलुहान करते हैं तो घर के अन्दर दलित पुरुषों की वर्चस्ववादी मनोवृत्ति व शारीरिक हिंसा उन्हें तोड़ती है.
आज दलित समाज से दलित महिलाओं को अलग करके देखने की आवश्यकता है आज का दलित समाज मनुवादियों के षड्यंत्रों के कारण हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है. किंतु दलित समाज की महिलाएं उससे भी अधिक पिछड़ी हुई हैं. इस मायने में दलित महिलाएं दोहरी दलित हैं. इसमें दो राय नहीं है कि हमारे समाज में औरत और उसमें भी दलित औरत की स्थिति काफी दयनीय है. दलित स्त्री के शोषण के मुख्य कारण हैं- अशिक्षा, निर्धनता, रूढ़िवादिता, अतः कहना न होगा कि आत्मनिर्भरता और शिक्षा का सवाल दलित स्त्री का भी प्रमुख सवाल है. समाज में पवित्र और उत्कृष्ट समझी जाने वाली प्रचलित मिथकीय संरचनाओं पर कड़ा प्रहार करता हुआ स्त्री आन्दोलन वास्तविक अर्थों में विवेकशील परंपराओं का समर्थन करता है. महान समझी जाने वाली उच्च एवं पितृसत्तात्मक केंद्रित परम्पराओं पर प्रहार करती हुई उनकी विवेकशीलता पर सवाल करत है. ज्ञान के परंपरागत मिथकीय स्थापनाओं को खारिज करती हुई कड़ा प्रतिरोध दर्ज करत है.जर्मेन ग्रीयर ने अपनी किताब ‘द फीमेल यूॅनक’ में इब्सन के डाल हाउस एक्ट के नोरा-हैल्मर संवाद के हवाले से स्त्री मुक्ति संबंधी अपनी मान्यता को प्रस्तावित करती है. “नोरा ने हैल्मर से पूछा- तुम क्या मानते हो मेरा सबसे पवित्र कर्तव्य क्या है? और जब उसने कहा कि- अपने पति और बच्चों के प्रति, तुम्हारा कर्तव्य तो वह असहमत होती है और कहती है कि- मेरा एक और कर्तव्य है, उतना ही पवित्र, अपने प्रति मेरा कर्तव्य…मैं मानती हूँ कि सबसे पहले मैं मनुष्य हूँ…उतनी ही जितने कि तुम हो या हर सूरत में मैं वह बनने की कोशिश करूँगी ही.”7
स्त्री मुक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ही है कि स्त्री को भी एक इंसान के रूप में देखा जाए, उसमें एक इंसान की तरह अच्छाईयाँ व बुराईयाँ भी हो सकती है. स्त्री मुक्ति आन्दोलन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के परम्परागत ढाँचे को तोड़कर एक स्त्री को असफल होने का भी अधिकार देता है और पुनः प्रयास करने का भी.अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह आन्दोलन ‘सामाजिक न्याय’ का भी आंदोलन है. नाओमी वुल्फ ने अपनी किताब ‘फायर विद फायर’ में लिखा है कि- “वृहद स्तर पर नारीवाद को सामाजिक न्याय के लिए एक अनिवार्य आंदोलन समझना चाहिए. इस स्तर पर नारीवादी होने का अर्थ होगा कि- स्त्री होने के कारण कोई मेरे रास्ते में बाधा न बने और किसी की जाति या स्त्री पुरुष होने के आधार पर कोई मतभेद न हो तथा स्त्रियों के पक्ष में काम करने का अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें देवी का दर्जा दे या उन्हें पुरुषों से बेहतर या अलग समझें.”8 अंततः ऐतिहासिक परिवर्तनों की प्रक्रिया में स्त्री इतिहास का साथ बखूबी निभा रही है. इस प्रयास की दिशा सही है या गलत, वादों के नारों के बीच स्त्री अपना स्वरूप खो रही है या तलाश रही है इसका निर्णय काल अपने क्रम में स्वयं कर देगा लेकिन स्त्री अस्मिता के आन्दोलन स्त्री मुक्ति की दिशा में सार्थक है इसमें कोई दो राय नहीं है.
संदर्भ –
संपादकीय ‘खरी-खरी बात’ से, ‘युद्धरत आम आदमी’ संपा. रमणिका गुप्ता पूर्णांक 108, 2011
पृ. 9 निवेदिता मेनन .‘नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एवं मुद्दे’ संपादक: साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता,
पृ. 141 कुमकुम राय,वही
पृ. 141 कुमकुम राय,वही
पृ. 16, ‘सामायिक मीमांसा’ संपा. विजय कुमार मिश्र:अंक 1, वर्ष 4, जनवरी-जून-2011
पृ. 15, वही
पृ. 20, जर्मेन ग्रीयर: ‘द फीमेल यूनक’
पृ. 13, नाओमी वुल्क, ‘फायर विद फायर’