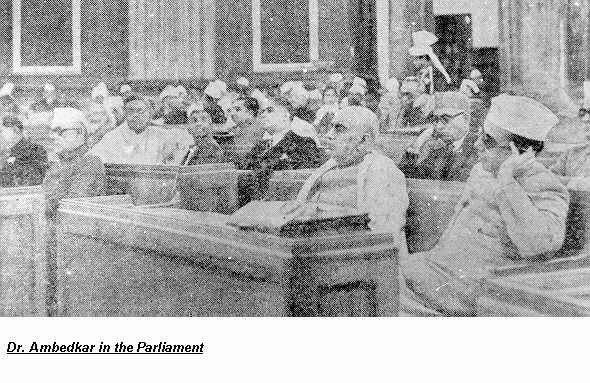( बजरंग बिहारी का यह आलेख ऐतिहासिक तथ्यों , विभिन्न स्रोतों से डा बाबा साहब आम्बेडकर के वकतव्यों के आधार पर मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद में जरूरी साह्चर्य की स्थापना देता है . इस क्रम में वे अस्मितावाद के अगले विकास के रूप में इसे अम्बेडकर चिंतन पर आधारित विचारधारा और राजनीति के रूप में देख रहे हैं , जिसका अनिवार्य रिश्ता मार्क्सवाद से बनता है. )
हिंदी दलित साहित्य में नयी पीढ़ी के हस्ताक्षर राज वाल्मीकि ने पिछले हफ्ते फोन पर हुई अनौपचारिक बातचीत में इस प्रश्न पर मेरी राय जाननी चाही कि क्या दलित लेखन निष्क्रियता के दौर में है. तुरंत जो सूझा वह जवाब मैंने दिया लेकिन संतोष न हुआ. प्रश्न इतना आसान है भी नहीं. जिस पृष्ठभूमि में यह सवाल उठाया गया है उसका ध्यान न रहे तो प्रश्न की व्यंजना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता. अभी कुछ दिन पहले ही नई सरकार की ताजपोशी हुई है. तमाम दलित नेता सीधे तौर पर या पार्टी के स्तर पर अलायंस करके सता में साझीदार हुए हैं. जिसे दलितों की पार्टी के रूप में पहचाना जाता है ,वह पराजय का कीर्तिमान बनाकर किंकर्तव्यविमूढ़ दिख रही है. महाराष्ट्र में दलित पैंथर के उदय की परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी. रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता तब अपने समर्थक-समुदाय को नज़रंदाज़ करते हुए सता में शामिल हो गए थे. मतदाताओं ने उन्हें इसका फल भी भली-भांति दे दिया था. वह युवा दलित पीढ़ी के लिए मोहभंग का दौर था. उस मोहभंग की ऐतिहासिक परिणति ‘दलित पैंथर’ का निर्माण थी. बीस से तीस वर्ष के नौजवानों ने स्वार्थी नेताओं को धिक्कारते हुए ‘विचारधारा’ की ओर रुख किया था.
पैंथर का मैनिफेस्टो इसी का दस्तावेज़ी सबूत है. ‘कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो’ की तर्ज़ पर निर्मित इस घोषणापत्र पर आंबेडकर-चिंतन की नई इबारत रची गयी है. पैंथर के संस्थापकों की दृढ़ धारणा थी कि- “समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना की चेतना से लैस होकर दलित-आंदोलन में ईमानदारी और प्रतिबद्धता से काम किया जाए तो दलित सभी प्रकार के शोषण से मुक्त हो सकते हैं और उनका उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता है.” दोनों ही विचारधाराओं से सामग्री लेते हुए पैंथर के ऊर्जावान युवाओं ने लस्त-पस्त सामाजिक आन्दोलन को एक बार पुनः खड़ा कर दिया था. पैंथर की जन सभाओं में हजारों-लाखों का जन सैलाब उमड़ता था और स्थिति-परिवर्तन की उनकी ईमानदार कोशिश को अपना मुखर समर्थन देता था. उस समय के दलित असंतोष को शब्द देते हुए बेबी कांबले ने लिखा-“अब हमारे नेता भी भ्रष्ट हो गए हैं. उन्हें दिल्ली की गद्दी चाहिए.यह देख मेरा मन रो पड़ता है. अगर भीमदेव न होते तो हम लोग पड़े होते किसी टूटी-फूटी झोपड़ी में और अन्न के लिए जंगलों में भटक रहे होते. पेट की आग बुझाने के लिए मरे जानवर खा रहे होते.” (‘जीवन हमारा’ मूल मराठी 1986, हिंदी अनुवाद 1995, अंतिम अनुच्छेद से) दलित पैंथर अगर संगठित रहता तो वह निश्चय ही वर्चस्ववादी ताकतों को निर्णायक शिकस्त देता. लेकिन बहुत जल्दी ही उसमें फूट पड़ गई. अपने को शुद्ध आंबेडकरवादी कहने वाले एक तरफ हो गए और वामपंथी रुझान वाले दूसरी तरफ.पैंथर के कार्यकर्ताओं में प्रारंभ में यह सहमति बनी थी कि वे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (आरपीआइ) में शामिल नहीं होंगे. यह सहमति टूटी और तमाम पैंथर सक्रिय राजनीति में आ गए.
 |
| धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर डा बाबा साहब आम्बेडकर उपस्थित लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाते हुए |
कई गुटों में बंटी आरपीआइ में दो गुट मुख्य थे- रूपवते गुट और दादासाहेब गायकवाड़ गुट. दादासाहेब गायकवाड़ धड़ा सांस्कृतिक प्रश्नों के साथ आर्थिक मुद्दों को भी तरजीह देता था. उस पर आरोप लगा कि वह मार्क्सवादी है. क्योंकि उस समय इन दोनों गुटों में प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर थी ,इसलिए वे व्यापक राजनीति में अपने प्रतिपक्षियों को पहचानने और उनसे मुकाबला करने की बजाए आपस में ही ज्यादा उलझे रहे. रूपवते गुट की उग्रता और आक्रामक शैली ने दादासाहेब गायकवाड़ गुट के साथ मार्क्सवादी विचारधारा को भी निशाने पर लिया. भीतरी गुटबाजी ने बड़ी कटुता पैदा की. प्रसंग-विशेष में कम्युनिज्म पर डॉ.आंबेडकर की कही बातों को सिद्धांत-कथन मानकर और कई बार उन कथनों में फेरफार कर मार्क्सवाद को घृणा का प्रतीक बनाया गया. महत्त्वपूर्ण आंबेडकरवादी विचारक रावसाहेब कसबे की किताब ‘आंबेडकर और मार्क्स’ (हिंदी अनुवाद उषा वैरागकर आठले, संवाद प्रकाशन, मुंबई, 2009) इस इतिहास का बड़ा मूल्यवान विश्लेषण करती है. कभी रूपवते गुट से सम्बद्ध रहे रावसाहेब कसबे मार्क्सवाद के प्रति गहरे विद्वेष से भरे हुए थे. उन्होंने ज्यों-ज्यों मार्क्स का अध्ययन किया, मार्क्सवादी साहित्य पढ़ा और फिर उसके परिप्रेक्ष्य में पूर्वग्रह मुक्त हो कर आंबेडकर के कार्यों और लेखन पर निगाह डाली, त्यों-त्यों उनका विद्वेषभाव पिघलता गया. यह किताब एक कष्टसाध्य वैचारिक रूपांतरण से गुजरे चिंतक की मार्मिक कथा कहती है. अस्मितावादी विमर्श अभी जिस बिंदु पर आकर ठहर गया है ,वह डॉ. आंबेडकर को कतई स्वीकार्य न होता. वे स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज चाहते थे. जाति-बोध की किसी भी किस्म की निरंतरता उन्हें असह्य थी. एक भिन्न वैचारिक या सामाजिक इयत्ता के रूप में दलितवाद का जड़ीभूत ठहराव उनको मंजूर न होता. दलित जनता की आकांक्षाओं का दोहन करके व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले उनकी नज़र में अपराधी ठहरते हैं. आंबेडकर का मंतव्य पहचानने वाले रचनाकार समय के इस नाजुक मोड़ पर हमारा ध्यान इसी तरफ ले जाना चाहते हैं. बेबी ताई कांबले की वह व्यथाजनित अभिव्यक्ति आज की रचनाकार अनिता भारती की तमाम कविताओं में प्रतिध्वनित हो रही है. बानगी के तौर पर एक कविता का अंश देखा जा सकता है-
तुम ले आए थे बाबा को
बाज़ार में
लगा रहे थे बोली
कह रहे थे देखो-देखो
हमारे बाबा ने झेले थे
दुःख-तकलीफें
जो तुमने दी थी उन्हें
अब तुम्हें भरना पड़ेगा
सबका हर्जाना
तकलीफें सुविधाओं में बदल रही थीं
कर रहे थे तुम विदेश यात्राएं
बोल रहे थे सभा-सम्मेलनों में
धिक्कार रहे थे उन्हें
जो सदियों से कर रहे थे अत्याचार
पर तुम्हारे पास एक अत्याचारग्रस्त
औरत खड़ी थी
लेकिन तुम्हारी आँखे उसकी पीड़ा से दूर
आसमान पर टिकी थीं
जो तुम्हें मिलना अभी बाकी था.
अब तुम बाबा को
घसीट लाए हो
व्यापार में
लोगों को बाबा के अपनाने के
जंतर-मंतर, हानि-लाभ सिखा रहे हो
सिखा रहे हो उनको
सूदखोर की तरह लाभ बटोरना
जबकि तुम्हारे पास
तुम्हारे भाई-बहन
भूख से बिलख रहे हैं.
हासिल की हैं तुमने
बिजनेस यात्राएं
अपने इन्हीं भूखे भाई-बहनों के बूते
गले, हाथ, लाकेट में लटकाए
भीम नाम की माला
ठीक स्वर्णकार की तरह
जो तुम्हारी ही तरह
सिद्धान्तहीन लोगों को चाहिए
पहनने के लिए (‘एक कदम मेरा भी’, अनिता भारती, बुक्स इंडिया, दिल्ली, 2013, पृ. 84-85)
अनिता भारती हिंदी दलित नारीवाद के प्रतिनिधि स्वरों में से एक हैं, अस्मिता-विमर्श की ढलान को पहचान कर और उसके इस तरह अदूरदर्शी सत्ता-विमर्श में बदलते जाने पर सवाल उठाकर दलित नारीवाद ने बड़ा मूल्यवान योगदान किया है. इसे विमर्श की जगह विचारधारा और क्षुद्र वैयक्तिकता की जगह मूल्यनिष्ठ प्रतिबद्धता को प्रतिष्ठित करने के उपक्रम के रूप में देखा जा सकता है. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रासंगिकता और यथास्थिति से टकराने में उनकी अनिवार्यता को महसूस करने का इससे बेहतर तरीका और क्या होगा! घातक विचलनों से आगाह करते हुए दलित आन्दोलन को पुनः उसके मूल स्रोत से जोड़ना विमर्श के निष्क्रिय कर्मकांड से परिवर्तन के सार्थक प्रयासों की रक्षा है. यहाँ इस तथ्य को याद किया जाना चाहिए कि अस्मिता-विमर्श की एक परिणति सत्ता की दिशाहीन दौड़ में दिखी और दूसरी मूलनिवासीवाद जैसे रोमानी भावबोध में. इन दोनों से बचकर ही परिवर्तन की धारा प्रवहमान रह सकती है. आंबेडकर की वैचारिकी इसी अर्थ में अपरिहार्य लगती है. इसे समझने के कारण आलोचक-संपादक डॉ. तेज सिंह दलितवाद त्याग कर आंबेडकरवाद के प्रबल आग्रही हुए थे.
 |
| Add caption |
इस साल आंबेडकर जयंती (14 अप्रैल,2014) पर बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में युवा मराठी लेखक, संपादक और आंबेडकरवादी कार्यकर्ता राहुल कोसंबी को सुनने का मौका मिला. अपने व्याख्यान में राहुल ने यह बात जोर देकर कही कि श्रम और पूँजी के सवालों तथा मजदूर आंदोलन पर डॉ.आंबेडकर की समझ व तमाम अवसरों पर इस संबंध में लिए गए उनके निर्णयों को नए सिरे से देखने की जरूरत है. डॉ. आंबेडकर जब-जब आम श्रमिकों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, संगठन बनाया अथवा चुनाव लड़ा तब-तब उन्हें ज्यादा सफलता मिली. उदाहरण के तौर पर राहुल ने स्वतंत्र मजदूर दल (इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी) की चुनावी सफलता को उद्धृत किया. इस पार्टी का निर्माण आंबेडकर ने 1936 में किया था. इसके बरक्स 1942 में उनके द्वारा स्थापित अखिल भारतीय शिड्यूल कास्ट फेडरेशन की 1946 के प्रादेशिक चुनावों में मिली पराजय की बात राहुल ने उठाई. राहुल ने इस अल्पज्ञात तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि इस फेडरेशन का निर्माण क्रिप्स मिशन के (प्रत्यक्ष) दबाव के नतीजे के चलते हुआ था. स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो केबिनेट मिशन मार्च 1942 में भारत आया था वह धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक प्रतिनिधियों को ही मान्यता देता था और उन्हीं से संवाद करता था. क्रिप्स ने आंबेडकर से पूछा था कि वे अछूतों के प्रतिनिधि हैं या मजदूरों के. (‘आंबेडकर और मार्क्स’, पृ.68) अनुसूचित जाति के हितों की चिंता के चलते आंबेडकर ऐसे फेडरेशन के निर्माण में संलग्न हुए थे. फेडरेशन की स्थापना 18-19 जुलाई 1942 में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय अस्पृश्यवर्गीय परिषद् में मंजूर प्रस्ताव के आधार पर हुई थी. इस अधिवेशन के दूसरे ही दिन आंबेडकर ने वाइसराय के कार्यकारी मंडल में श्रम मंत्री बनने की स्वीकृति दी थी. (वही, पृ.135). उन्होंने आगे इस संगठन को बनाए रखने की बजाए रिपब्लिकन पार्टी की योजना बनाई मगर यह योजना उनके जीवनकाल में साकार न हो सकी. यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर उनके रहते यह पार्टी अस्तित्व में आयी होती तो उसका स्वरूप क्या होता और उसके सरोकार कैसे होते.
इतना निश्चित है कि तब यह जाति-विशेष की पार्टी के रूप में न पहचानी जाती और उसमें इतनी जल्दी तथा इतनी ज्यादा टूट-फूट न हुई होती. इस अनुमान का एक आधार बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्वरूप है. डॉ. आंबेडकर ने यह सभा अपनी आंदोलनधर्मी सक्रियता के शुरुआती दिनों 1924 में स्थापित की थी. सभा की कार्यकारिणी मिश्रित सदस्यों वाली थी. सभा का यह स्वरूप सचेत और सायास तरीके से निर्मित किया गया था. यह सिलसिला बाबासाहेब के पूरे जीवनकाल में कायम रहा. सन् 1927 में महाड़ के अस्पृश्यवर्गीय परिषद् में मनुस्मृति का दहन हुआ. परिषद् ने कई प्रस्ताव पास किए. इनमें दूसरा प्रस्ताव मनुस्मृति को जलाने का था. इसके प्रस्तावक सोशल सर्विस लीग के गं.नी. सहस्रबुद्धे थे. प्रस्ताव का समर्थन पां. ना. राजभोज ने किया था. मनुस्मृति को आग के हवाले करने का काम एक अछूत बैरागी के हाथों संपन्न हुआ. लंबे समय तक बाबासाहेब के सहयोगियों में शामिल रहे सहस्रबुद्धे जन्मना ब्राह्मण थे. राजभोज ग़ैरमहार (चमार जाति से) थे.डॉ. आंबेडकर की बड़ी स्पष्ट समझ थी कि “सामाजिक घटकों के परस्पर योग्य सहयोग पर ही सामाजिक पुनर्रचना निर्भर है.”(‘जीवन चरित’ धनंजय कीर, 1996, पृ. 38) आंबेडकर ने यह बात बर्ट्रेंड रसेल की एक किताब पर अपनी समीक्षा में लिखी थी. राजर्षि शाहूजी महराज की आर्थिक सहायता से उन्होंने ‘मूक नायक’ पत्र निकाला था. इसका पहला अंक 31 जनवरी 1920 को आया. अपनी दूरदर्शिता के चलते ही उन्होंने ‘मूक नायक’ का संपादक पांडुरंग नंदराम भटकर को बनाया था. भटकर महार थे और उनकी पत्नी ब्राह्मण परिवार से थीं. इस दंपत्ति को बहुत सामाजिक अपमान झेलने पड़े थे. प्रवेशांक में लिखा गया था-“अंग्रेजी राज के खिलाफ उठाया गया एतराज ब्राह्मणों के मुंह में यदि एक गुना शोभायमान होता है तो वही एतराज ब्राह्मणी राज के खिलाफ किसी बहिष्कृत व्यक्ति के उठाने पर हज़ार गुना शोभायमान होगा.” (वही, पृ.48) आंबेडकर का यह कथन आज वैश्वीकरण के ज़माने में और भी प्रासंगिक हो गया है. इसे अब यूं कहा जाना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते-फैलते जाल पर व्यक्त की गई चिंता से कई गुना मूल्यवान चिंता दबंग जातियों द्वारा दलितों के उत्पीड़न की है. आंबेडकर का जीवन ताउम्र ऐसे ‘देशप्रेमियों’ की असलियत सामने लाता रहा जिनके देश के दायरे से दलित बहिष्कृत हैं. लोकमान्य तिलक ऐसे ही एक मान्य नेता थे. अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद् का एक आयोजन उन्नीस मार्च 1918 में हुआ. तिलक ने इसमें हिस्सा लिया. अनपेक्षित पोजीशन लेते हुए तिलक ने अस्पृश्यता को मानने वाले ईश्वर को ईश्वर मानने से इनकार किया. लेकिन, परिषद् ने जब अस्पृश्यता के खिलाफ घोषणापत्र तैयार किया और उसे उपस्थित सदस्यों के सम्मुख हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया तो लोकमान्य तिलक ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया! टाइम्स ऑफ़ इंडिया के 16 जनवरी, 1919 अंक में डॉ. आंबेडकर ने लिखा-“स्वराज्य जैसा ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है वैसा ही वह महारों का भी है… जब तक यह नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता का दिन दूर रहेगा.”(वही, पृ.40 ) देश की स्वतंत्रता की चिंता डॉ.आंबेडकर को भी थी और तमाम राष्ट्रवादियों की तुलना में कहीं ज्यादा गहन व पुख्ता थी. ब्रिटिश शासन के प्रति उनका रवैया निर्भ्रांत तौर पर आलोचनात्मक था. इस बात पर काम ही लोगों का ध्यान जाता है कि डी. फिल.उपाधि हेतु लिखे उनके शोध-प्रबंध के सुपरवाइजर एडविन आर.ए. सेलिग्मन थे. सेलिग्मन मार्क्सवादी थे. उनकी कई किताबों में से एक ‘द इकॉनोमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ़ हिस्टरी’ लेखक की वैचारिक रुझान की जानकारी के लिए देखी जा सकती है. आंबेडकर ने इनके मार्गदर्शन में 1916 में डी.फिल. किया था. यह प्रबंध आठ वर्ष बाद 1924 में ‘द इवोल्यूशन ऑफ़ प्रोविंशियल फाइनांस इन ब्रिटिश इंडिया’ शीर्षक से छपा. इस ग्रन्थ में आंबेडकर ने लिखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने देश के धनाड्यों और उनके उद्योगों के हित साधन में लगा हुआ है. यह सही है कि ब्रिटिश नौकरशाही ने देश में शांति और सुव्यवस्था स्थापित की. अब लोग इसका क्या करें? क्या वे इससे संतुष्ट हो जाएं? (वही, पृ.31) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उसकी मूलाधार निजी संपत्ति की अवधारणा को समतामूलक समाज के निर्माण में बाधा मानना आंबेडकर के चिंतन में केंद्रीय मुद्दा है. इसे नज़रंदाज़ कर आंबेडकर की वैचारिकी को समझने का सिर्फ भ्रम पाला जा सकता है. यह बिडम्बना नहीं तो और क्या है कि अपने को आंबेडकर का उत्तराधिकारी घोषित करने वालों ने उनकी मृत्यु के तुरंत बाद समाजवादी विचार-दर्शन से संवाद और सहयोग करने की बजाए उससे शत्रुतापूर्ण रिश्ता बना लिया. इस रिश्ते के निर्माण और विकास में तथाकथित साम्यवादियो/समाजवादियों का भी कम योगदान नहीं है.
रावसाहेब कसबे की किताब उस वैचारिक परिदृश्य को मूर्त करती है, जो आंबेडकर के परिनिर्वाण के तुरंत बाद निर्मित हुआ था. डॉ.आंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की परिकल्पना स्वतंत्र मजदूर दल के विकसित संस्करण के रूप में की थी मगर वह अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की छाया-प्रति बन कर रह गया. दलितों के असली शत्रु कहीं पीछे ओझल कर दिए गए और मार्क्सवाद को दुश्मन की तरह देखा जाने लगा. दो-तीन पीढ़ियाँ इसी माहौल में पली-बढ़ीं. युवा होते रावसाहेब कसबे उन दिनों को याद करते हुए लिखते हैं-“उस समय कम्युनिस्टों के प्रति सहानुभूति रखना आंबेडकर-द्रोह की श्रेणी में आता था.”(आंबेडकर और मार्क्स’ पृ.२०) रावसाहेब इस बात को रेखांकित करते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के रूपवते गुट के नेताओं ने मार्क्सवाद विरोध का ऐसा वातावरण तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी. उनकी पीढ़ी ने बाबासाहेब को देखा नहीं था. “बाबासाहेब के कुछ ही दिन पूर्व हुए महानिर्वाण के बाद हम इसी गुट को उनका सच्चा उत्तराधिकारी मानते थे…उनके विचारों को हम इन नेताओं के माध्यम से ही समझ रहे थे. हमें यह ढृढ़ विश्वास था कि हमारे नेता कभी झूठ नहीं बोल सकते.बाबासाहेब के साथ भावनात्मक तादात्म्य बनाने का एकमात्र रास्ता अपने नेताओं के प्रति निष्ठा रखना था.” (वही, पृ.२१) चीन का आक्रमण भी इन्हीं दिनों हुआ. कम्युनिस्ट चीन के प्रति गुस्सा सहज रूप से कम्युनिज्म के प्रति क्रोध में बदल दिया गया. कुल मिलाकर, “यह विचार हमारे दिल-दिमाग पर हावी था कि कम्युनिस्ट और उनकी विचारधारा ‘मार्क्सवाद’ हमारे देश की दुश्मन हैं…कम्युनिस्ट विरोध हमारे लिए अंतिम सत्य था.”(वही, पृ.२१) कई बार हुए एक ही प्रकार के अनुभव को याद करते हुए रावसाहेब लिखते हैं कि (चीन आक्रमण के समय बने) घोर राष्ट्रवादी माहौल में “जब रक्त संग्रह या चंदे के लिए कोई शासकीय सेवक या स्वयंसेवक उनके (कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के) पास पहुंचता, तो वे डरते-डरते पूछ बैठते थे-“जिनके शरीर में पहले से ही खून की कमी है, उनसे क्यों खून माँगते हैं?” या फिर “जिनके पास दो जून की रोटी नहीं है, उनसे चंदा क्यों माँगते हैं?” सुनते ही उनका गला दबा देने की इच्छा होती.” (वही, पृ.२१) सारांश यह कि “समूचे वातावरण में कम्युनिस्टों के प्रति शत्रुता का भाव भरा हुआ था. इसी वातावरण में मैं बड़ा हुआ.”(वही, पृ.२१) रावसाहेब ने बड़े मार्मिक तरीके से अपने मानसिक रूपांतरण को शब्दबद्ध किया है. राजनीति शास्त्र में एम.ए.करते हुए उन्होंने मार्क्स और मार्क्सवादी सिद्धांतों के बारे में मजबूरन परीक्षा पास करने की गरज से पढ़ा. इससे उनके भीतर थोड़ी उत्सुकता जगी. इसी दौरान अहमदनगर में हुए बौद्ध साहित्य सम्मेलन में उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे धड़े के नेता दादासाहेब गायकवाड़ से मिलने और उनके साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिला. “उन्हें सुनने-समझने के दौरान मेरे अधिकांश पूर्वग्रह धीरे-धीरे पिघलने लगे और उनकी राजनीतिक भूमिका के बारे में पुनर्विचार करने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई.” इस उत्सुकता का विकास बाबासाहेब आंबेडकर के लेखन को परिवर्तित दृष्टि से पढ़ने के क्रम में हुआ.
1916 में आंबेडकर ने जाति-व्यवस्था पर जो शोध निबंध लिखा था उसका आरंभिक वाक्य है- “समूची दुनिया का इतिहास वर्गीय समाजों का इतिहास है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है”. बाबासाहेब के काठमांडू भाषण (जिसका आधा-अधूरा और गलत हवाला देकर मार्क्सवाद के प्रति नफरत में बढ़ोत्तरी की गई थी उसे) लेखक ने मूल रूप में पढ़ा. इसमें आंबेडकर ने बुद्ध की तुलना कार्ल मार्क्स से की है. इस भाषण का प्रास्ताविक अंश है- “भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स की तुलना करना अत्यंत आकर्षक और मार्गदर्शक है. दोनों को पढ़ने और दोनों के दर्शन में गहरी रूचि होने के कारण, इनकी तुलना करने के लिए मुझे बाध्य होना पडा.” आंबेडकर की ‘गहरी रुचि’ से बावस्ता होने के बाद निरंतर अध्ययन के परिणामस्वरूप लेखक के “मन में जमा कट्टर कम्युनिस्ट विरोध और मार्क्सवाद संबंधी नफरत धीरे-धीरे समाप्त होने लगी. इस नई दृष्टि के आलोक में मैंने दीर्घ काल तक ढोए हुए जुए से मुक्ति पाने का संकल्प लिया और आंबेडकर तथा मार्क्स पर एक साथ विचार करना प्रारंभ किया.”(वही, पृ.24) अब जरूरत इस भीतरी परिवर्तन को सार्वजानिक करने की थी. जड़ीभूत परिवेश लेखक को इसकी अनुमति नहीं दे रहा था- “कार्ल मार्क्स के बारे में अनेक वर्षों से जमा हुआ मेरे मन का कलुष धीरे-धीरे घुलने लगा. मगर वह किसी से कहने की हिम्मत मुझमें नहीं थी.”(वही)जब भी किसी (दलित) व्यक्ति से उनकी मार्क्स पर चर्चा होती “तो वह उन्हें इस तरह भला-बुरा कहता कि मुझे कोफ़्त होती कि मैने यह बात छेड़ी ही क्यों!” सभा-संगोष्ठियो-जुलूसों में आते-जाते, अज्ञानजनित नफरत की परतों को जानते-बूझते और ‘लोक आग्रह के स्थान पर आत्मालोचना की आवश्यकता महसूस करने वाले’ दलित और दलितेतर युवकों से मिलते-जुलते क्रमशः साहस आता गया. बाबासाहेब के निकट सहयोगी रहे मिलिंद कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य म.भि.चिटनिस की निकटता ने लेखक को अपने विश्वास के परीक्षण का अवसर उपलब्ध कराया.
रावसाहेब कसबे न तो आंबेडकरवाद को कम्युनिस्ट विचारधारा में शामिल करने की हिमायत करते हैं और न मार्क्सवाद को दलित आंदोलन में घुला देने की वकालत. उनका मानना है कि “दलित और वामपंथी आंदोलन को परस्पर शत्रुता रखकर अपनी सीमित शक्ति का दुरुपयोग करने की बजाए परस्पर सहयोग के द्वारा अपनी-अपनी सामर्थ्य का विस्तार करना चाहिए.” (वही, पृ.31) इस पारस्परिकता का विकास करने के लिए उन्होंने दोनों विचारधाराओं के उन पक्षों को रेखांकित किया जो संवाद और सहयोग में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं. इस संदर्भ में आंबेडकर और मार्क्स के खुद के लेखन से ज्यादा सहायता और किस स्रोत से मिल सकती है! रावसाहेब कसबे की अगाध अध्ययनशीलता और तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक दृष्टि से जन्मी यह किताब मानव-मुक्ति की चिंतनधारा में यादगार योगदान है. किताब का पहला संस्करण 1985 में आया था. सोवियत संघ के विघटन के छः वर्ष पहले. दूसरा संस्करण 2005 में आया. निजीकरण और अमेरिकीकरण की भव्य शुरुआत के डेढ़ दशक बाद. स्वाभाविक रूप से लेखक के सामने वैश्वीकरण एक बड़ा मुद्दा है. रावसाहेब वैश्वीकरण को ‘ऐतिहासिक विकासक्रम की नैसर्गिक व्यवस्था’ मानते हैं. अब उसके अच्छे या बुरे होने पर बहस करने का वक़्त नहीं बल्कि यह प्रयास करने का वक़्त है कि ‘उसे मानव जाति के लिए किस तरह पोषक और उपयोगी बनाया जा सकता है.’ लेखक के इस कथन की अनुगूंज पूरे अध्ययन में व्याप्त है कि “वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया प्राकृतिक नहीं है बल्कि अमरीका जैसी महाशक्ति द्वारा अपने साम्राज्यवादी फैलाव के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है.” सोवियत रूस के विघटन में पूंजीवादी ताकतों की सक्रियता को जिम्मेदार मानने से ज्यादा रावसाहेब ने वहां की खोखली और भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया है. मिखाइल गोर्बाचेव लिखित ‘पेरिस्त्रोइका’ को उन्होंने अपने विवेचन का आधार बनाया है. जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं की रौशनी में अगर बेहतर से बेहतर व्यवस्था अपने को अद्यतन करते रहने को तैयार नहीं होती तो उसका ढह जाना अवश्यंभावी हो जाता है. दुनिया की तमाम क्रांतियों का जिक्र करते हुए रावसाहेब लेनिन के हवाले से यह बात कई बार रेखांकित करते हैं कि क्रांति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है. लेनिन का उद्धरण है- “इतिहास में ऐसी कोई भी क्रांति कभी भी संपन्न नहीं हुई जिसमें विजय पाने के बाद, बिना शस्त्र उठाए, बिना कुछ नया किए, सफलता की ख़ुशी मनाते हुए वह निश्चिन्त रह सकी हो. जिस समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक विकासक्रम में पूंजीवाद से अधिक प्रभावी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिवर्तन करना है,वह अपनी संपूर्ण क्षमता को प्रकट करके, अंततः एक मूलभूत नई रचना को साकार करने के लिए अनेक क्रांतिकारी चरणों से क्यों न गुजरे?”
कोई भी व्यवस्था अंततः समाज में रहने वालों के लिए और उन मनुष्यों के अनुरूप होती है. कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर सोवियत संघ में जो व्यवस्था लागू की गई उसने ‘नए मनुष्य’ के निर्माण का काम अपने हाथ में नहीं लिया. नतीजतन, व्यक्ति और व्यवस्था में दूरी बनती-बढ़ती रही. इस दूरी का अंदाज हम सोवियत संघ के ढहने के चंद दिनों के भीतर चर्चों की बेतहाशा वृद्धि में देखते हैं. नए युवा जोड़ों ने अपनी सगाई की अंगूठियां तक इन चर्चों के निर्माण के लिए दान कर दीं. व्यक्तिगत संपत्ति के निषेध की संकल्पना के साथ अस्तित्व में आयी व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं, प्रशासकों और कर्मचारियों को अनैतिक, भ्रष्ट और बेतरह संपन्न होते देखती रही. बिडम्बना के दूसरे छोर पर निपट गरीबी में छटपटाते लोगों की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती संख्या दिखी. आंबेडकर को इस स्थिति का पूर्वाभास भले न रहा हो मगर वे इस बात पर आग्रह करते नज़र आते हैं कि कम्युनिस्ट समाज को बनाए रखने में बुद्ध धम्म सहायक हो सकता है. उन्होंने कहा- “बल प्रयोग हटाने पर साम्यवादी व्यवस्था का संरक्षण सिर्फ धर्म ही कर सकता है.” अब सवाल है कि यह काम कौन-सा धर्म करेगा? लेकिन, उससे पहले यह कि क्या कम्युनिस्ट धर्म वाले विकल्प को स्वीकार भी करेंगे? ईसाइयत को कम्युनिस्ट स्वीकार नहीं कर पाते. ईसाई धर्म ने ‘गरीबी का उदात्तीकरण किया और गरीबों को स्वर्ग की सुखद कल्पना में भटका दिया.’ लेकिन बुद्ध का धम्म ऐसा नहीं. वह साम्यवाद के लिए उपयोगी हो सकता है. डॉ.आंबेडकर के शब्द हैं- “रूसी लोग बल-प्रयोग समाप्त करने के बाद साम्यवाद को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए एक पुख्ता सहायक की दृष्टि से बौद्धधम्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं.” सोवियत संघ की स्थापना के साढ़े तीन दशक बाद आया यह सुझाव किस चिंता से प्रेरित है, इसे अलग से स्पष्ट करने की जरूरत नहीं. आंबेडकर की इस पीड़ा का मूल्य साम्यवादी व्यवस्था के समर्थकों की समझ में क्यों नहीं आया यह किसी भी नए अध्येता के लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है. रावसाहेब कसबे ने लिखा- “आंबेडकर ने बौद्धधम्म को साम्यवाद का अंतिम सहायक माना, इस बात को बौद्ध जगत भी स्वीकार करेगा कहा नहीं जा सकता. साथ ही मूलतः कम्युनिस्ट-विरोधी और स्वयं को आंबेडकरवादी कहने वाले तक आंबेडकर द्वारा दी गई इस प्रस्थापना को पचा पाएंगे, यह कहना मुश्किल है. बाबासाहेब द्वारा बौद्धधम्म को प्रदान किए गए इस श्रेष्ठतम स्थान को समझने में कम्युनिस्टों की तरह वे भी ‘कोरे’ हैं. कम्युनिस्ट और बौद्ध दोनों ही परस्पर एक-दूसरे की परिभाषाओं को नहीं समझना चाहते और दोनों ही अब विनाश के कगार पर खड़े हैं.” (वही, पृ.48)
साम्यवाद पर सबसे ज्यादा हमला ‘सर्वहारा के अधिनायकत्व’ को लेकर होता है. आलोचक इसे ‘कम्युनिस्ट तानाशाही’ कहते हैं. आंबेडकर ने इस तानाशाही पर विचार किया. उन्होंने ‘दीर्घकालीन तानाशाही’ से असहमति जताई परंतु साथ ही यह भी स्वीकारा कि ‘सोवियत संघ में कम्युनिस्ट तानाशाही ने आश्चर्यजनक प्रगति की है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता.’ इससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने सुझाव दिया कि “सोवियत तानाशाही अन्य पिछड़े देशों के लिए भी उपयुक्त हो सकती है.” बेहद अंतर्दृष्टिपूर्ण ढंग से उन्होंने कहा कि मनुष्य को भौतिक विकास के साथ आत्मिक विकास भी करना होता है. “दीर्घकालीन तानाशाही ने मनुष्य के आत्मिक मूल्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया.”समानता पर्याप्त नहीं है. वह स्वतंत्रता और बंधुत्व के साथ मिलकर ही पूर्णतर होती है. साम्यवाद समानता पर एकाग्र होकर रह जाता है. ‘बुद्ध के बताए रास्ते का अनुसरण करने पर ही ये तीनों चीजें एक साथ मिल सकती हैं.’
आंबेडकर का धम्म परंपरागत बौद्ध मत नहीं है. वह हीनयान और महायान से भिन्न नवयान है. यह संघबद्ध या संस्थागत धर्म न होकर मुक्ति का वैयक्तिक मार्ग है. बिचौलियों से रहित. इसमें संघम् शरणम् गच्छामि की जगह ‘अत्त दीप भव’ (‘अप्प दीपो भव’- स्वयं अपना दीपक बनो) पर ज़ोर है. मार्क्स ने जिस ‘समग्र मानव’ का सपना देखा था उसका गहरा संबंध इस नवयान की अवधारणा में स्थित मनुष्य से है. वैयक्तिकता की चिंता आंबेडकर के यहाँ मिलती है तो मार्क्स भी इस चिंता में साझीदार नज़र आते हैं. पूंजीवादी हड़पू व्यक्तिवाद भी वैयक्तिकता की बहुत परवाह करता प्रतीत होता है. इनमें अंतर व्यक्तिगत संपत्ति के मुद्दे पर है. आंबेडकर और मार्क्स दोनों ही निजी संपत्ति की अवधारणा को ख़ारिज करते हैं.आंबेडकर यों तो हिंसा के प्रयोग को प्रायः किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं देते लेकिन निजी संपत्ति में निहित हिंसाचार को पहचानने के कारण वे कहते हैं-“अतः जिसकी निजी संपत्ति अन्य लोगों के दुःख का कारण बनती है, ऐसे अर्थ-पिशाच को क्यों न मारा जाए? कोई निजी संपत्ति को इतना पवित्र क्यों माने?” आंबेडकर इस आरोप पर कि सिर्फ कम्युनिस्ट राज्यों में हिंसा होती है निराकरण करते हुए कहते हैं-“ग़ैर कम्युनिस्ट देश एक-दूसरे से युद्ध करते हैं, उन युद्धों में लाखों लोग मारे जाते हैं, क्या यह हिंसा नहीं है?” हिंसा के प्रश्न पर बुद्ध और मार्क्स की तुलना करते हुए उन्होंने लिखा-“बुद्ध और मार्क्स के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं, पहले उन्हें दूर करना जरूरी है. सबसे पहले हम हिंसा पर विचार करते हैं. कुछ लोग हिंसा के बारे में सोचते ही थर-थर कांपने लगते हैं. यह सिर्फ एक भावना हैं. मानव-जाति कभी भी हिंसा से दूर नहीं रह पाई है… बुद्ध भी हिंसा का विरोधी था, परंतु वह न्याय के पक्ष में था. जहां न्याय की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग की अनिवार्यता हो, वहां इसका प्रयोग करने की वह अनुमति देता था.”(पृ.45-46)
सिद्धांत और व्यवहार में एकरूपता पर बल मार्क्स और आंबेडकर दोनों के यहाँ समान रूप से है. किसी भी कार्य के पीछे चिंतन का होना जरूरी है और बगैर क्रियाशीलता के कोई चिंतन बेमतलब का है. मार्क्स का क्रांतिकारी कथन है- “बिना कर्म का कोई दर्शन या तो हवा में उड़ जाने वाला होता है या फिर श्रद्धा को धंधा बनाने वालों की रूढ़ियों में जड़ हो जाता है. बिना दर्शन के कोई क्रिया निकट-दृष्टिदोष बन जाती है या फिर औपचारिक और नीरस कर्मकांड बन जाती है.” मार्क्स से पहले का भौतिकवाद मनुष्य को परिस्थितियों के अधीन मानता था. मार्क्स ने ‘थीसिस आन फायरबाख’ में लिखा कि ‘मनुष्य स्वयं भी परिस्थितियों को बदलता है.’ पुराने यांत्रिक भौतिकवाद से मार्क्स के क्रांतिकारी भौतिकवाद का यह फर्क है. रावसाहेब कसबे बताते हैं कि “बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक में बाबासाहेब ने कार्ल मार्क्स का व्यावहारिक दर्शन (प्रैक्सिस) उनकी भाषा में ही प्रस्तुत किया है.” (पृ.82) अपनी इस बात के समर्थन में उन्होंने पुस्तक से दो उदाहरण दिए है. पहला उदाहरण उस समय का है जब ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध के मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा था कि उपदेश दिया जाए अथवा नहीं. आंबेडकर ने लिखा- ‘भगवान बुद्ध को अहसास हुआ कि इस दुनिया को बदल कर बेहतर बनाना जरूरी है.’ मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है- “अनेक दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की सिर्फ व्याख्या की है, परंतु असली सवाल है उसे बदलना.”बुद्ध और उनका धम्म में आंबेडकर पारम्परिक धर्म से अपने धम्म का अंतर बताते हुए कहते हैं- “ ‘धर्म’ का उद्देश्य इस दुनिया की उत्पत्ति को समझाना है, परंतु ‘धम्म’का उद्देश्य इस दुनिया की पुनर्रचना करना है.” (पृ.82) रावसाहेब की टिप्पणी है कि बुद्ध और उनका धम्म में अपने नव बौद्ध धम्म की प्रस्थापना करते हुए आंबेडकर कार्ल मार्क्स के नजदीक पहुंचते हैं और “उनकी प्रस्थापना मार्क्सवाद का विकल्प देने के स्थान पर मार्क्सवाद के पूरक (अल्टीमेट ऐड) के रूप में दिखाई देती है.” (पृ.81)
मार्क्स दुनिया के इतिहास को वर्गीय इतिहास के रूप में देखते थे. आंबेडकर भी इससे असहमत नहीं- “वर्गीय समाज का अस्तित्व एक वैश्विक तथ्य है इसलिए आरंभिक हिंदू समाज भी इसका अपवाद नहीं है.” अब सवाल था कि इस वर्ग से जाति कैसे बनी? आंबेडकर ने लिखा-“भारत में वर्ग गोलबंद हो गए, परंतु अन्य देशों में ऐसा नहीं हुआ. जाति और वर्ग एक दूसरे के पड़ोसी हैं और जाति ही गोलबंद वर्ग है.” (पृ.92) मनुस्मृति में जाति प्रथा का समर्थन है परंतु मनु इस प्रथा का जनक नहीं. उसने जाति-संस्था को सैद्धांतिक रूप देने में अपनी भूमिका निभाई. अगर धर्मग्रन्थ जाति के निर्माण और निरंतरता के जिम्मेदार नहीं तो उनकी आलोचना तक सीमित रहकर इस प्रथा का उन्मूलन भी नहीं किया जा सकता. आंबेडकर के शब्द हैं- “जाति-संस्था का निर्माण उपदेश मात्र से नहीं हुआ है और न ही उसे केवल उपदेशों से समाप्त किया जा सकता है.” जब तक आर्थिक संबंध नहीं बदलते, उत्पादन के साधनों पर पारंपरिक स्वामित्व का अंत नहीं होता तब तक जाति संरचना में आधारभूत परिवर्तन संभव नहीं लगता. जो विचारक मात्र धर्मग्रंथो की निंदा को जाति-उन्मूलन का हेतु मानकर संतुष्ट हो जाते हैं और आंदोलन का ध्यान वास्तविक भौतिक स्थितियों की ओर जाने में रुचि नहीं लेते उसके नतीज़ों पर रावसाहेब कसबे लिखते हैं-“आजकल दलित सांस्कृतिक आंदोलन में जो उग्रता दिखाई देती है, उसके मूल में संस्कृति के उद्भव के प्रति अज्ञान है.सांस्कृतिक संघर्ष महज देवी-देवता, धर्म-ग्रंथ और दर्शन का विरोध करके सफल नहीं होता बल्कि यह संस्कृति जिस भौतिक आधार पर खड़ी है उसे बदलना अनिवार्य है.बाबासाहेब के संस्कृति संबंधी इन विचारों को यदि स्वीकार कर लिया जाए, तो सांस्कृतिक आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में लड़ने वालों को हवा में तलवार भांजने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी.”(पृ.97)
 |
| डा आम्बेडकर के बाद के भारत में दलित आन्दोलन के प्रमुख हस्ताक्षर नामदेव ढसाल |
अपने वक्त की राजनीतिक शक्तियों के वर्गीय स्वरूप की पहचान आंबेडकर को थी. 1937 में मैसूर में दलित-वर्ग की जिला परिषद आयोजित की गई थी. इसके अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने गांधीजी और कांग्रेस के वर्ग-चरित्र पर टिप्पणी करते हुए कहा-“मुझे पूरी आशंका है कि गांधीजी कभी भी मजदूरों और दलितों का पक्ष नहीं लेंगे…साधारण मनुष्य को अपना विकास करने की स्वतंत्रता और अवसर मिले, इस सामाजिक-आर्थिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य को घोषित करने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं है. जब तक उत्पादन के साधनों पर अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कुछ लोगों का ही अधिकार होगा, तब तक साधारण मनुष्य के विकास की आशा नहीं की जा सकती.”(पृ.128) आंबेडकर की ऐसी स्पष्ट समझ परवर्ती दलित आन्दोलन में विस्मृत होती गई लेकिन साथ ही उनके समर्थकों की संख्या और समाज में उनकी दृश्य-स्वीकृति का दायरा बढ़ता गया. 1938 में आंबेडकर ने कहा कि “कांग्रेस यदि सचमुच ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष छेड़ती तो मैं इसमें शामिल हो जाता. परंतु वस्तुस्थिति विपरीत है. कांग्रेस द्वारा प्राप्त राजनीतिक शक्ति का उपयोग स्वार्थी लोगों के हितों के पोषण के लिए किया जा रहा है और वह किसान-मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रही है.” (पृ.129)आंबेडकर की छवि को धूमिल करने के तमाम प्रयास हुए. उनकी राष्ट्रनिष्ठा पर शक किया गया. उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया. इन कुचेष्टाओं के बावजूद उनकी छवि चोटिल होने की बजाए निखरती गई. असल में उनका राष्ट्रवाद राजाओं, नवाबों, जमींदारों, महंथों की चिंता से परिभाषित न होकर मजदूरों-दलितों-किसानों-स्त्रियों के सरोकारों से निर्मित था. वे इनके लिए स्वराज चाहते थे.
आज अगर आंबेडकर होते तो उनकी क्या भूमिका होती? वे निश्चित तौर पर नवसाम्राज्यवादी हमलों के विरुद्ध मोर्चा खोलते, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते जाल को छिन्न-भिन्न करने में संलग्न होते, राष्ट्रीय संपत्तियों (जल-जंगल-जमीन) को निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ़ लोगों को लामबंद करते. दलितों पर बढ़ रही हिंसा का पुरजोर प्रतिरोध तैयार करते… जो उनकी विरासत से अपने को जोड़ते हैं आज उनका यही कार्यभार होना चाहिए. साथ ही, मार्क्सवादी धारा से जुड़े दलों, संगठनों और व्यक्तियों को भी नए सिरे से सक्रिय होने की जरूरत है. दोनों विचारधाराओं में सच्चा सहयोग भाव अगर आज नहीं बना तो फिर कब बनेगा! रावसाहेब कसबे की चेतावनीभरी सलाह समय रहते सुन-समझ लेनी होगी. अभी पूना के भारत भूषण तिवारी (विचारक-अनुवादक) से मिली सूचना थोड़ी आश्वस्ति पैदा करने वाली है. नई सरकार ने आते ही सबसे पहले रेलवे के विनिवेशीकरण का द्वार खोलने की घोषणा की. भारतीय रेलवे सबसे अधिक नौकरियाँ प्रदान करने के लिए जाना जाता है. उसमें दलित समुदाय के कर्मचारियों की भी अच्छी संख्या है. उसके विनिवेशीकरण का नतीजा बहुत स्पष्ट है. शायद इस खतरे को भांपने का परिणाम है कि पहली बार ‘द सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (ई.सी.सी. सोसाइटी)के पंचवर्षीय चुनाव (गुप्त मतदान) में सीटू (CITU) से जुड़े नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (NRMU) का आल इंडिया शिड्यूल कास्ट एंड शिड्यूल ट्राइब रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन से गठबंधन हुआ है. दूसरी ओर कांग्रेस/इंटक से जुड़े सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का अपेक्षाकृत नए संगठन रेल कामगार सेना (भारत भूषण का अनुमान है कि यह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शाखा होगी) से अलायंस हुआ है. एक शताब्दी पुरानी ई.सी.सी.सोसाइटी में घटने वाली यह चुनावी परिघटना दूरगामी आशय समेटे हुए है. आखिरकार, हम सबको अपना-अपना पक्ष चुनना ही होगा.
वरिष्ठ आंबेडकरवादी आलोचक और ‘अपेक्षा’ पत्रिका के संपादक डॉ. तेज सिंह का पंद्रह जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से अकस्मात निधन हो गया. एक दर्ज़न से अधिक किताबों के लेखक-संपादक डॉ.तेज सिंह दलित लेखक संघ के पहले अध्यक्ष थे. वे इससे पहले जनवादी लेखक संघ के सक्रिय सदस्य थे. उनकी हमेशा यह कोशिश रही कि दोनों विचारधाराओं में सार्थक संवाद और नीतिगत मुद्दों पर एका हो. उनके परिनिर्वाण से समूचे परिवर्तनकामी और प्रगतिशील आंदोलन को धक्का लगा है. यह लेख उन्हीं की स्मृति को समर्पित है.
( कथादेश से साभार )