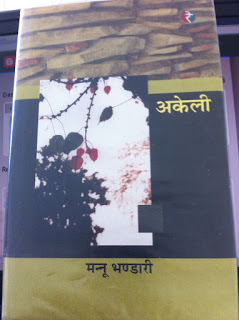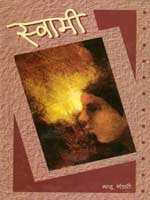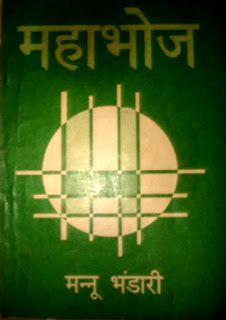वरिष्ठ लेखिका मन्नू भंडारी के जन्मदिन पर विशेष
अलग -अलग समय की स्त्री रचनाकारों ने हमेशा मुझे यह देखने और समझने के लिए उकसाया कि किस तरह वे स्त्री की तयशुदा सामाजिक भूमिकाओं से अलग उसके अपने स्वत्व और उसकी अपनी सामाजिकता के सवाल उठा रही थी. पितृसत्ता द्वारा की जा रही स्त्री के सामाजीकरण की प्रक्रिया को पहचानना एक मुश्किल और उतना ही बारीक समझ का काम है. इसे मन्नू भंडारी की ‘अकेली’ कहानी में उसकी पेंचदगियों और उससे बननेवाली टकराहटों के साथ अभिव्यक्त किया गया है. स्त्री के उपर थोपे गए समाज और सहज मानवीय जरूरतों से बनने वाले समाज के अंतर को यह कहानी बखूबी दिखा देती है, साथ ही यह भी दिखाने से नहीं चूकती कि स्त्री इस थोपे गए समाज के बरक्स अपना समाज रचने को लगातार उससे जूझती, टकराती और इस क्रम में अपनी दिमागी कंडिशनिंग को कुछ ढीला करती, व्यवस्था और उसकी नियमावली को प्रश्नांकित भी करती चलती है. सामाजीकरण की इस पूरी प्रक्रिया में की गई स्त्री की दिमागी कंडिशनिंग उसे इस बात के लिए तैयार करती है कि वह स्वयं ही यह मान ले कि उसके जीवन की सार्थकता मातृत्व में है और मातृत्व की महती उॅचाई प्राप्त कर लेने के बाद स्त्री का जीवन संपूर्ण और लक्ष्य समाप्त हो जाता है. इसे खो देने पर जीवन निरर्थक और समाज के लिए भविष्योन्मुखी न होने के कारण व्यर्थ हो जाता है. समाज ऐसे स्त्री जीवन को पग पग पर खारिज करता चलता है. यहाॅ यह ध्यान देना जरूरी है कि मातृत्व की पूरी अवधारणा मात्र पुत्र के संदर्भ में है, कन्या के जन्म को इसमें गिना नहीं गया है. इसलिए मातृत्व की यह अवधारणा अजीब तरह से पुंसोमुखी हो कर मनुष्यविरोधी बन जाती है.
यह अवधारणा स्त्री के समूचे अस्तित्व को ढक कर उसे सीमित और दयनीय बना देती है. जबकि देखने की बात यह है कि भारतीय संस्कृति में इस मातृत्व का इतना गुणगान किया गया है और इसी मातृ पद के कारण उसे समाज में अत्यंत गौरवमय और काव्य में अत्यंत करूणामय, साथ ही महिमामय स्थान दे डाला गया है, परंतु व्यवहारिकता इसके उलट है. जिस मातृत्व को इतना विशिष्ट स्थान दे कर पितृसत्ता ने उसे अपने माथे पर मुकुट की धारण किया हुआ दिखाया, उसी माँ को उसके ही बच्चों के सामने पिता किसी तरह का आदर न देकर लगातार अपमानित, लक्षित करता रहता है. ऐसे उदाहरण आप आए दिन अपने घरों में या आस पास देख सकते हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में यह दृश्य इतना आम हो चुका है कि किसी का ध्यान भी नहीं जाता कि यही वह महिमामय पद है, जिसके बिना स्त्री जीवन ही निरर्थक बना दिया जाता है, फिर इसकी ऐसी बे-कदरी ! यह इतना बड़ा झूठ उसके सिर पर थोप दिया गया और जब उसने इसे समझना शुरू किया तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं ! यहां मेरे कहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि माएं अपने पुत्रों को प्यार न करें या देखभाल न करें, बच्चे को प्रेम करना एक सहज स्थिति है और उसे सहज ही बने रहना चाहिए। अब दूसरी स्थिति देखिए, जहां इसी हमारे पौराणिक इतिहास की तमाम कहानियां यह बताती हैं कि यदि स्त्री ने पितृसत्ता की नियमावली का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया तो मातृत्व के गौरव से युक्त स्त्री को उसी की संतान के हाथों दंडित करवाया जायेगा. इस तरह संतान का पद पाने वाले पुत्र को माता को सजा देने की क्रूरता के लिए भी मानसिक रूप से तैयार कर देने की स्थितियाॅ पहले ही बता दी जाती हैं।
यह नृशंसता का भयानक उदाहरण है कि पिता के आदेश पर पुत्र माता का वध करे, पिता के आदेश पर पुत्र माता की जिह्वा काट ले आदि. शायद यह पुरूष के भीतर, मां के लिए गहरे बैठी संरक्षकत्व की भावना को जड़ से उखाड़ फेंकने और स्वयं को मां से अधिक वर्चस्वशाली की स्थिति में मान लेने का भाव पैदा करने के लिए भी रचा गया होगा और पुत्र के भीतर की कोमल भावनाओं को सुखा कर, तोड़ कर, उसे स्त्री के प्रति क्रूर, एक निर्मित समाज का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया जाना भी होगा. इस तरह दिया गया मातृत्व का पद भी एक टिकाउ और विश्वसनीय पद नहीं बना रह जाता. चूॅकि पुत्री को दूसरे घर कन्यादान में दिया जाना है, इसलिए बचपन से ही उसे तरह तरह से अनुकूलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है. स्त्री स्वत्व को कुचल देने की यह प्रक्रिया इतनी बारीक रही है और इतनी महिमा मंडित की जाती रही है कि बहुत छोटी लड़कियां भी बिना बताए अपने जीवन को व्यवस्था के अनुरूप ढालने का श्रम शुरू कर देती हैं. उन्हें अपने जीवन का आदर्श स्वतः ही पूर्व पीढ़ियों से हस्तांतरित होता हुआ मिलता रहता है. यातना का आदर्श स्त्री के लिए जिस तरह से रचा गया है, मानसिक अनुकूलन से थोड़ा सा निकल कर देखने पर ही वह हैरान कर देने वाली अमानवीयता से भरा दिखाई पड़ेगा. ऐसे में स्त्री का अपना कोई समाज नहीं रह जाता. वह एक दिए हुए समाज में, उसी के अनुसार आचार व्यवहार करने के लिए तैयार की जाती है, ऐसा न करने पर विवश बनाई जाती है या बहिष्कृत की जाती है. ऐसी निर्मित स्त्री से उसका मनोवांछित समाज रच ले जाने की अपेक्षा करना थोड़ा ज्यादा लग सकता है. परंतु यह निर्मित स्त्री भी अपने प्रयत्नों में सहज सामाजिक संबंधों के निर्माण और निर्वाह की तरफ जाना चाहती है. जैसा कि हम उपर्युक्त कहानी की प्रमुख पात्र सोमा बुआ में देख सकते हैं.
दरअसल यह अनुकूलन प्रायः ही स्त्री को सुख और संतुष्टि की तरफ नहीं ले पाता. उसे तयशुदा जीवन के अगल बगल कुछ और चाहिए, जो उसकी आकांक्षा से जुड़ता हो, जो उसके मन के निकट हो, जिसमें उसके स्वत्व की भागीदारी हो, जिसमें मानवीय जीवन की बुनियादी गरिमा शामिल हो, उसकी बुद्धि और समझदारी की भी एक जगह बनती हो, इसी दुनिया के भीतर उसकी अपनी तरह की नितांत निजी और नितांत सामाजिक दुनिया भी हो. यह छटपटाहट तब और भी मुखर हो उठती है जब मातृत्व का पद उसके हाथ से जा चुका होता है और अब वह इस समाज के भीतर निरे खाली हाथ, समाज के गणित में शून्य साबित की गई की तरह खड़ी हो. तब नए सिरे से स्त्री अपने जीने की जद्दोजहद में राह बनाती सामाजिक संबंधों के निर्माण और निर्वाह की तरफ जाना चाहती है. वह समाज से अपने इस अतिरिक्त श्रम के एवज में अपनी पहचान और अपनी जगह की मांग करती है. यह समझते हुए भी कि यह समाज उसका बनाया नहीं है, वह इसी में अपनी जगह तलाशती, संबंधों को नए रूप में सिरजती, जीवन को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है. यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में सोमा बुआ को रख कर देखेंगे तो वे एक भौतिक प्राणी की प्रतिकूल बना दी गई परिस्थितियों के बीच की जा रही बेहद मानवीय कोशिशों की तरह पढ़ी जायेंगी.
मन्नू भंडारी की उपर्युक्त कहानी उनके दूसरे कहानी संग्रह ‘तीन निगाहों की एक तस्वीर’ में संकलित है. यह संग्रह सन् 1958 में प्रकाशित हुआ था. तात्पर्य यह है कि कहानी में वर्णित परिस्थितियाॅ साठवें दशक के उत्तरार्ध की अथवा उससे पहले की हैं किंतु स्त्री के लिए यह स्थिति कमोबेश आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है. सहज भाषा में रची गई यह कहानी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के भीतर अकेली बना दी गई स्त्री के साथ साथ समाज संरचना की बारीक पड़ताल भी एकदम चुपचाप तरीके से करती चलती है. उपर्युक्त कहानी की प्रारम्भिक तीन पंक्तियाॅ स्त्री जीवन का पूरा समाजशास्त्र अपने में समेटे हुए हैं –
‘‘सोमा बुआ बुढिया हैं/ सोमा बुआ परित्यक्ता हैं/सोमा बुआ अकेली हैं.’’ स्त्री को अकेला बना देने के दो सबसे बड़े कारण यहाॅ दिए हुए हैं- ‘बुढ़िया और परित्यक्ता’. यदि दोनों एक साथ हैं तो यह अकेलापन कई गुना भारी है. तो क्या इन दोनों कारणों के नहीं होने पर स्त्री अकेली नहीं है? कुछ देर को यह भ्रम हो सकता है कि भरे पूरे परिवार के बीच स्त्री किसी भी प्रकार के अकेलेपन से दूर हो जायेगी, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि पूरी संरचना स्त्री के विरूद्ध कुछ इस तरह से है कि वह कभी भी अकेली बना दी जा सकती है अथवा प्रायः ही अकेली है, असंगठित है, घर के भीतर भी और घर के बाहर भी. असंगठित होने के कारण अशक्त भी है और बेचारी भी. इसलिए यहाॅ उपर्युक्त दोनों शब्द स्त्री जीवन की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने के लिए अपनेआप में प्र्याप्त हो जाते हैं.
पहला कारण है सोमा बुआ का बुढ़िया होना. ‘बुढ़िया’ हो जाने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से अशक्त हो जाना भर नहीं है, क्योंकि हम पाते हैं कि सोमा बुआ लगातार सक्रिय हैं. बुढ़ापे के बावजूद वे लोगों के घरों में होने वाले बड़े बड़े आयोजनों में घरेलू कामों में उनकी मदद करने पूरे मन से पॅहुच जाती हैं. लोगों को उनकी मदद लेने में कोई गुरेज भी नहीं है, पर उनकी इस पूरे मन से की गई मदद अर्थात श्रमशीलता का कोई सम्मान नहीं दिखता. न ही स्त्री द्वारा इस किए गए अतिरिक्त श्रम से, स्त्री की कोई जगह समाज निर्धारित करता है. दरअसल ‘बुढ़ापा’ स्त्री जीवन को एक भिन्न अर्थ में भी अकेला करता है. वह स्त्री जीवन की अर्थवत्ता के लिए तय किए गए सौंदर्य के मानदंडों को ‘बुढ़ापा’ आते ही खो देती है, साथ ही संतानोतपत्ति की उपयोगिता भी. परिणामतः वह पुंसवादी समाज के लिए व्यर्थ मान ली जाती है. और उसका श्रम एक मजदूर अथवा दास के श्रम से अधिक नहीं गिना जा सकता है. इस तरह उसके श्रम का सदा ही अवमूल्यन किया गया. इसलिए अपनी तय सामाजिक भूमिका के नकार को मिटाने के लिए, वह जो अपने श्रम द्वारा संबंधों के निर्माण की तरफ जाना चाहती है, समाज उसे उचित सम्मान नहीं दे पाता. यद्धपि समाज उसके श्रम का उपयोग अपने लाभ के लिए कर लेता है परंतु मूल्यांकन करते समय उसे उसका उचित स्थान नहीं देना चाहता बल्कि श्रम की मानवीय गरिमा भी नहीं प्रदान करना चाहता है.
सन् 1934 में ही महादेवी वर्मा ने अपने निबंध ‘हिंदू स्त्री का पत्नीत्व’ में बहुत साफ शब्दों में भारतीय स्त्री की सामाजिक स्थिति की बात कह दी थी- ‘‘ भारतीय स्त्री की सामाजिक स्थिति का इतिहास भी उसके विकृत से विकृततर होने की कहानी मात्र है. बीती हुई शताब्दियां उसके सामाजिक प्रासाद के लिए नींव के पत्थर नहीं बनीं, वरन् उसे ढहाने के लिए वज्रपात बनती रही हैं. फलतः उसकी स्थिति उत्तरोत्तर दृढ़ तथा सुंदर होने के बदले दुर्बल और कुत्सित होती गई.’’2. स्त्री श्रम, आज के आधुनिक समाज में भी एक जटिल स्थिति है. उसके श्रम का दोहन भी होता है और समाज उसे श्रमिक के रूप में मान्यता भी नहीं देता. यहां तक कि उसके श्रम को अतयंत नगण्य की श्रेणी में डाल दिया जाता है. जबकि उसके हिस्से श्रम का अधिकतम भाग है. सीमान द बोउवा ने समाज के भीतर स्त्री श्रम की इस जटिलता पर गहराई से विचार किया और कामकाजी स्त्रियों की स्थिति को अधिक जटिल पाया. वे लिखली हैं कि ‘‘ फैक्ट्री में काम करने के कारण जो आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें मिली है, उससे इनकी घरेलू जिंदगी का बोझ कम नहीं हो जाता. उन्हें न समाज और न अपने पति से वह सहारा मिल पाता है, जिससे वे यथार्थ जीवन में पुरूष के बराबर हो सकें.’’3.
इसतरह समाज वृद्ध स्त्री के श्रम का दोहन करने के बावजूद उसे स्वीकरता नहीं है. लगातार उसका अवमूल्यन करता और उसके अपने सामाजिक संबंध निर्माण की प्रक्रिया को बाधित तथा खारिज करता चलता है. तथापि स्त्री की जीजिविषा और सामाजिक प्राणी होने का उसका प्रकृत्ति प्रदत्त दावा उसे इस विरूपता से टकराने के लिए उत्प्रेरित करता ही है. वृद्ध होने से उसका मनुष्य होना झूठा नहीं पड़ सकता. अतः बार बार लहूलुहान होकर भी वह मानवीय आकांक्षाओं से उतनी ही युक्त बनी रहती है और अपने परिश्रम से अपना समाज बनाना चाहती, जितना कोई भी सामाजिक प्राणी कहा जाने वाला मनुष्य चाहेगा. दूसरी स्थिति ‘परित्यक्ता’ की है. यह स्थिति पहली से भी भयावह है. ‘परित्यक्ता’ की स्थिति हीनतर स्थिति है. समाज द्वारा तय की गई सुरक्षा की गारंटी ऐसी स्त्री के हाथ से छिन चुकी है. वह निरूपाय और बेबस मान ली गई है, जबकि बेबस है नहीं. वह सोमा बुआ की तरह श्रमशील हो सकती है या आज की स्त्री की भाॅति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर. यद्धपि आर्थिक आत्मनिर्भरता ने स्त्री को पहले से कुछ मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है और परित्यक्ता जैसी स्थिति में वह अपने जीवन को ठीक ढंग से जी सकने में सक्षम हुई है तथापि समाज में आज भी परित्यक्ता के लिए नकारात्मक सोच बनी हुई है.
सोमा बुआ का समय तो साठ के दशक का पूर्वार्द्ध या उससे कुछ पहले का है जब स्त्री के लिए शिक्षा के द्वार तो खुल गए थे परंतु आजीविका के विविध साधनों में उनका प्रवेश नगण्य था। इसलिए अतिरिक्त श्रम के बावजूद सोमा बुआ की आजीविका का कोई बेहतर और नियमित प्रबंध एक समस्या ही है और सोमा बुआ की स्थिति प्रछन्न परित्यक्ता की है भी नहीं. वे अपनी आजीविका का इंतजाम जैसे तैसे करने में लगी रहती हैं परंतु उनके इस संघर्ष में एक और दुखद यर्थाथ जुड़ा है- पुत्र शोक का. उनके पति ने पुत्र के देहांत के बाद सन्यासी का जीवन अपना लिया था.हर साल एक महीने के लिए उनके पति, उनके पास आकर रहते थे. लेकिन पति के रहने पर उनका अकेलापन दूर होने की बजाय और बढ़ जाता था. कारण कि ‘‘ पति के स्नेह हीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता. उस समय उनका घूमना, फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि दो मीठे बोल बोल कर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दें, जिसका आसरा ले कर वह उनके वियोग के ग्यारह महीने काट दें.’’ 4.पति के साथ दुख बाॅटना भारतीय समाज में प्रायः एक कल्पित स्थिति है. यद्धपि आज कहीं कहीं बहुत नगण्य
ही पर स्थिति कुछ बेहतर की तरफ बढ़ी है परंतु अब भी मित्रता की सुखद स्थिति में नहीं पॅहुच पाई है.
दूसरे बुआ के सन्यासी पति की उपस्थिति में उनकी जीवन गति का निषेध हो जाता है. उनका घूमना, फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता है अर्थात जिंदगी ठहर कर सन्यासी जी के इर्द गिर्द केन्द्रित हो जाती है. सामाजिकता से कट जाना और पति का संग साथ भी न मिल पाना दुखी और अकेली सोमा बुआ के लिए कितना बोझिल बन जाता है, इससे सन्यासी जी को कोई सरोकार नहीं है. बल्कि किसी न किसी बात पर ताने मार कर वे, उन्हें नियन्त्रित करने का प्रयत्न भी वे करते ही रहते हैं। पति के जाते ही सोमा बुआ की दिनचर्या का यह रूका बाॅध टूट जाता है और आस पड़ोस के सुख दुख में शामिल हो कर अपना जीवन काटने की कोशिश करने लगती हैं. पति के संग का यह दुखद यर्थाथ भारतीय दाम्पत्य के खोखले आदर्श के रेशे उधेड़ देता है। इस दुःसह पति संग और पुत्र वियोग दोनों को भुलाने का उपाय भी बुआ के पास अपने श्रम के बल पर समाज में शामिल होने के प्रयत्न में छिपा है. इसके लिए वे किसी पास पड़ोस के बुलावे का इंतजार नहीं करतीं. अपने घर के न रहने पर पूरा मोहल्ला उनका घर है. बिन बुलावे के उनकी यह उपस्थिति बड़ी मर्मभेदक है.
यह स्त्री की, समाज के भीतर जीने की बेहद मानवीय इच्छा है. इसलिए बुलावा न भेजने पर वे पड़ोस को माफ करती रहती हैं और उपाय भी क्या है? यह माफ कर देना एक तरह से स्वयं को दिलासा देना है कि सामाजिक उपेक्षा दरअसल जानबूझ कर नहीं की गई है. इस दिलासा में वे अपना होना भी खोजती चलती हैं – ‘‘ बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती ?….. मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ ….. आज हरखू नहीं है इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हॅू.’’ 5. और बुआ राधा भाभी के आगे फूट फूट कर रो पड़ती हैं. यह रो पड़ना बुआ के भीतर गहरे धंसे सामाजिकता के खोखले सत्य को खोल देता है. अर्थात बुआ के आगे उपेक्षा का यह यर्थाथ भ्रमात्मक नहीं है. लाख उपेक्षा के बावजूद यह पास पड़ोस ही है, जो बुआ के जीने का सहारा है न कि पति का संग साथ. पति की दुनिया एक समानान्तर संसार है, जिसमें पत्नी की जगह नहीं है. परंतु गृहिणी धर्म में उनकी जरा भी लावरवाही सन्यासी जी को बर्दाश्त नहीं है.
भारतीय दर्शन में वैराग्य एक ऐसा यूटोपिया है, जो सबसे पहले पुरूष के निकट स्त्री सत्य को वज्रय बनाता है।.इसतरह एक बड़े सामाजिक यर्थाथ के बीच बनने वाले उत्तरदायित्व से पुरूष को मुक्त कर देता है. इसी के साथ पितृसत्ता का वह आत्मविश्वास भी उन्हें प्राप्त है जो समाज के बीच बुआ के प्रयत्नों को उपहास्यास्पद और अंततः व्यर्थ मान कर चलता है. वे वैरागी जरूर हैं पर खासे दुनियादार भी हैं. समाज को अच्छी तरह समझते तो हैं पर मनुष्य के सुख दुख में शामिल नहीं होना चाहते. बल्कि संयास ले कर पुत्र शोक से उत्पन्न यथार्थ की समस्याओं से भी भागते हैं. अपने दुख को वे संयास की महिमा से मंडित कर के जी रहे हैं और सोमा बुआ का दुख ? इसके लिए उनके पास सांत्वना का कोई शब्द नहीं है. इस तरह घर और समाज दोनों तरफ से बुआ के हिस्से में अकेलापन ही आता है. इस अकेलेपन से जूझती बुआ क्या समाज के बीच अपनी पूर्णता को खोजना चाहती हैं ? या कि समाज द्वारा प्रदत्त मातृत्व पद में स्त्री की अंतिम परिणति को खो देने के कारण अपनी अपूर्णता को ढकने की कोशिश में लगी हुई हैं ? समाज का व्यावहारिक गणित ऐसी स्त्री में कोई भविष्य नहीं देखता, जो परित्यक्त है और जिसका पुत्र नहीं रहा. क्या सोमा बुआ ऐसी ही प्रदत्त सामाजिकता की शिकार नहीं हैं ? फिर सोमा बुआ की इन कोशिशों के परिणाम क्या निकल सकेंगे ?
मुझे बार बार ऐसा लगता है कि सोमा बुआ अपनी इन कोशिशों से लगातार एक निहायत मानवीय और अपना मनचीता समाज, जिसमें स्त्री सहज, स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्तित्व के साथ शामिल हो सके, रच डालने की जिद में लगी हैं. यह जिद उन्हें कई बार बेचारा बना डालती है पर हर बार व्यवस्था के विरूद्ध, स्त्री के लिए तय कर दी गई सामाजिकता के विरूद्ध और उसके जीवन की निर्मित की गई सामाजीकरण की प्रक्रिया के विरूद्ध भी उन्हें खड़ा कर देती है. उनकी इन कोशिशों में लगातार हार है, परंतु यह हार उन्हें फिर भी समाप्त कर डालने तक नहीं पहचानती बुआ, जो अपना बेटा खो चुकी हैं, अपने पति द्वारा त्याज्य जैसी स्थिति में हैं, समाज उन्हें बार बार तिरस्कृत करता है, फिर भी क्या है, जो उन्हें हर बार पिछले को भूल कर नई कोशिशों के लिए तैयार कर देता है ! वे दुख की नदी में अपने को डूब मरने के लिए नहीं छोड़तीं. लगातार अपने को सामुदायिक हलचलों से जोड़े रखती हैं. यहां वे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समाज के भीतर किए गए महत कर्म को बड़ा तप मानने जैसे तर्क के साथ बड़ा तप करती दिखती हैं. ‘‘एकांत का तप बड़ा तप नहीं है. समाज में जाओ.’’ आचार्य जी की यह बात बुआ पर खरी उतरती है. इसीलिए तो एक धक्के केे कोई सप्ताह भर बाद ही वे जीवन से फिर जुड़ जाती हैं और प्रसन्न मन से संयासी जी से कहती हैं -‘‘ सुनते हो, देवर जी के ससुरालवालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहां हुआ है. वे सब लोग यहीं आ कर ब्याह कर रहे हैं. देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी हैं तो समधी ही. वे तो तुमको भी बुलाये बिना नहीं मानेंगे. समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं?’’ और बुआ पुलकित हो कर हंस पड़ीं.’’6.
यह है बुआ के भीतर गहरे पड़े दुख में भी सांस लेने की इच्छा. जीवन का उत्साह, उमंग, इच्छाएं, हरा भरा सब दबा पड़ा है उनमें. वे कुछ देर को अपना दुख भूल कर, दूसरों के सुख में प्रसन्न हो जाने की सामर्थ्य रखती हैं पर संयासी जी नहीं. इन्हीं छोटे छोटे क्षणों में उनके भीतर का दबा कुचला जीवन अपनी झलक दिखला जाता है. शादी में जाने की तैयारी का हुलास बुआ में भी कम नहीं है- ‘‘ गली में बुआ ने चूड़ीवाले की आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी चूड़ियों पर जा कर टिक गई. कल समधियों के यहां जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम काॅच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले. पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया, कोई देख लेगा तो. लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी पीछे के दरवाजे पर पॅहुच गईं और एक रूपया कलदार खर्च कर के लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए. पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके-ढुके फिरीं.’’ 7. स्त्रीत्व, मातृत्व और पत्नीत्व से अलग है. बुआ का लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन कर शादी में जाने की तैयारी के लिए मन ही मन उत्साहित होना, साड़ी पीले रंग में रंगना और राधा भाभी से पूछना कि -‘‘ क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं ?’’ 8. शादी में दिए जाने वाले सामान की तैयारी करना आदि उनके भीतर की स्त्री से परिचित कराता है, जो सारे दुखों, उपेक्षाओं, तिरस्कार के बावजूद स्त्री है और विवाह में शामिल होने की अपनी बेहद सामान्य सी हुलस को ; जो कि सोमा बुआ जैसी स्त्रियों के लिए स्वीकृत नहीं है द्ध रोक नहीं पाती हैं.
यहां लेखिका ने कहानी को स्त्री के व्यक्तिगत दुख की परिधि से निकाल कर सत्रीत्व की व्यापक परिधि में खड़ा कर दिया है. किंतु यथार्थ यह है कि परित्यक्त और पुत्र शोक से ग्रस्त स्त्री के लिए जीवन की यह हरियाली समाज में छिपाने की बात है. बुआ इस छिपाने में भी कैशोर्य लज्जा का भान करा जाती हैं. बुआ को अपना मन उस समाज से छिपाना है, जिसमें शामिल होने की इच्छा के आगे समर्पित हो कर उन्होंने अपने पुत्र की एकमात्र निशानी सोने की अंगूठी को बेच दिया है. चूॅकि यह अंगूठी पुत्र की निशानी के साथ साथ उनका एकमात्र धन भी है, इसलिए समधी को रस्म के तौर पर कुछ देने का यह प्रयास, समधी को देने से ज्यादा अपने लिए कुछ पा लेना है या अपने एकांत को कुछ भर लेना अधिक है. नहीं तो राधा भाभी का सुझाया विकल्प तो था ही -‘‘ तो जाओ ही मत. चलो, छुट्टी हुई. इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं.’’ 9. पर यह विकल्प बुआ को स्वीकार्य नहीं है. फिर इस विकल्प से तो पही होना है जो स्त्री के लिए तय किया गया है. इसतरह स्त्री छूटती चली जाएगी और अपने प्राणघातक एकांत में कैद होकर रह जाएगी। बुआ को इससे इंकार है.
आखिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो स्त्री भी सामाजिक प्राणी है. परंतु पितृसत्तात्मक संरचना के भीतर उसे उनकी शर्तों पर शामिल होना है न कि मनुष्य होने के कारण. परिणामतः कदम कदम पर उसे निषेधों से जूझना है. और चूॅकि वह मनुष्य है इसलिए एक अदद अपने समाज की उसकी इच्छा अंततः नहीं मरती. सोमा बुआ की भी यह इच्छा अंततः बची रह जाती है, जो उन्हें बार बार की निराशा में भी उठा कर खड़ा कर देती है. हांलाकि इस बार हरखू की एकमात्र निशानी को नातेदारी में होने वाली शादी के उपहार पर न्यौछावर कर देने के बाद बुलावे के इंतजार में छत पर खड़ी बुआ, जो समधियों के यहां बिना बुलावे के नहीं जा सकती थीं, जिस तरह संयत बने रहने की कोशिश करती हैं और अपने निकट पसरे यथार्थ को स्वीकार कर अपनी दिनचर्या में लौटती हैं, वह विचलित करने वाला है और कोई भी सहृदय पाठक यहां पहुंच कर बुआ से फिर उठ खड़े होने की अपील करने से अपने को शायद ही रोक पाए
संदर्भ
1. मन्नू भंडारी की चुनी हुई कहानियाॅ, अकेली, साहित्य भंडार, इलाहाबाद, पृ. 29
2. श्रृंखला की कड़ियाॅ, महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 76
3. स्त्री: उपेक्षिता, सीमोन द बोउवा, अनुवाद – प्रभा खेतान, पृ. 318
4. मन्नू भंडारी की चुनी हुई कहानियाॅ, अकेली, साहित्य भंडार, इलाहाबाद, पृ. 29
5. वही, पृ. 31
6. वही, पृ. 31
7. वही, पृ. 33
8. वही, पृ. 34
9. वही, पृ. 33