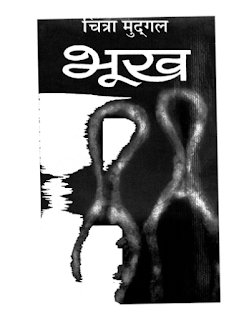हिन्दी विश्वविद्यालय में स्त्री अध्ययन विभाग में प्रोफ़ेसर. सम्पर्क : ई मेल- shambhugupt@gmail.com, मोबाइल: 8600552663
हिन्दी विश्वविद्यालय में स्त्री अध्ययन विभाग में प्रोफ़ेसर. सम्पर्क : ई मेल- shambhugupt@gmail.com, मोबाइल: 8600552663
वरिष्ठ कथालेखिका चित्रा मुद्गल की कहानियाँ एक बार फिर चर्चा में हैं. ख़ास तौर से ‘मामला आगे बढ़ेगा अभी’, ‘भूख’, ‘जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं’, ‘प्रेतयोनि’ आदि. आज से दस साल पहले भी इन कहानियों की लगभग यही स्थिति थी. लेकिन आज जब फिर से इन पर चर्चा ज़ोरों पर है तो इस बहाने मेरे जैसे पाठक को यह मौक़ा मिलता है कि इन्हें कथित चर्चेबाज़ी, चर्चेबाज़ी की राजनीति से अलग समय के असल आईने में देखा जाए, इन कहानियों को पढ़ने के बाद एक सामान्य पाठक के बतौर मैं किस तरह, क्या सोचता हूँ, इसे बेखटके सबके सामने लाऊँ; क्योंकि हिन्दी में चर्चेबाज़ी का एक धड़ा ऐसा भी है, जो प्रश्न भी ख़ुद तैयार करता है और बहुत ही सूफ़ियाना तरीक़े से उनके उत्तर भी ख़ुद डिक्टेट करता है. हिन्दी में हिन्दी की अन्तरात्मा को ठेस पहुँचाती ‘पीआरशिप’ की यह प्रवृत्ति पिछले दिनों ख़ूब पनपी है और इसने लगभग एक परम्परा का स्वरूप अख़्तियार कर लिया है. आम पाठक के पास इस इन्द्रजाल को पहचानने/काटने का कोई ज़रिया नहीं, सिवा इसके कि वह ख़ुद मोर्चा सम्भाले और आलोचकों के तिलिस्म को तार-तार करे!
कोई आलोचक किस कृति के बारे में कैसे, क्या सोचता है, यह उसका अपना मामला है क्योंकि आलोचक भी इसी लागलपेट भरी दुनिया का हिस्सा है और यह क़तई नहीं माना जा सकता कि इस पीआरशिप की चपेट में वह बिल्कुल न आया हुआ होगा! सब धान बाईस पँसेरी हमारा मन्तव्य नहीं है. बहुत विनम्रतापूर्वक सिर्फ़ इतना कहना है कि आलोचकों को भी कभी-कभी आईने में अपना चेहरा देख लेना चाहिए. आलोचना की पहली और आख़िरी कसौटी ख़ुद रचना होती है, होनी चाहिए; न कि यह कि लेखक या लेखिका की हैसियत और पहुँच क्या और कहाँ तक है, वह कितने बड़े, फ़ायदा पहुँचा सकने वाले आहदे पर है या कहें कि किसी का कुछ बना या बिगाड़ सकने की कितनी सामथ्र्य उसमें है! अरसे से हिन्दी आलोचना के बहुत सारे ‘प्रतिमान’ इसी ‘उर्वरा’ भूमि से निकलकर आ रहे हैं, पाठक को ऐसा दरकिनार किया गया कि लगभग उसे ‘हाँका’ गया! होना तो दरअसल यह चाहिए था कि जैसा कि एक जनतान्त्रिक व्यवस्था में होता है कि देश के हर नागरिक की उसमें प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी/भूमिका होती है; लेखक की रचना-प्रक्रिया में पाठक की भी लगभग यही हैसियत होती है, होनी चाहिए. हुआ यह है कि जैसे राजनीति आम आदमी को किनारे कर के चलती है और उसी के कन्धों पर सवार होकर उसी को चकमा देती रहती है, ठीक वैसे ही साहित्य में भी आम आदमी, शोषित -उत्पीड़ित वर्गों, निम्नवर्गीय जीवन इत्यादि का इस्तेमाल ही किया गया. यह ठीक है कि साहित्य क्रान्ति नहीं करता पर उसकी भूमिका और मानसिकता तो बनाता है. लेकिन यदि वह यह भी न कर पाए तो आप क्या कहेंगे?
कोई रचनाकार जब आम आदमी,शोषित-उत्पीड़ित वर्गों, निम्नवर्गीय जीवन इत्यादि को अपना विषय बनाता है तो तय है कि वह इस तथ्य से तो सुपरिचित होगा ही कि ऐसा किए जाने के लिए तत्वतः और स्पष्टत: उसे डिक्लास/डिकास्ट होने की प्रक्रिया से गुज़रना ज़रूरी है. वह भी पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ. राजनेताओं की तरह साहित्यकार भी यदि ऐसा करने लगेंगे कि पहले वे समस्या गढ़ेंगे और फिर उसका समाधान भी और इस चक्कर में सारा ज़मीन-आसमान एक कर देंगे तो यह तो वही बात हो जाएगी न कि यह मेरी खेती! इसे जैसे मैं बोऊँ-काटूँ! हालाँकि अपने कहानी-संग्रहों की भूमिकाओं में चित्राजी बाक़ायदा इस ‘उपभोक्तावाद’ का विरोध करती हैं और इसकी लम्बी ख़बर लेती हैं. जैसे कि ‘लपटें’ की भूमिका ‘द्वन्द्व’ में एक जगह उन्होंने लिखा है-‘‘आज लेखक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वह अपने समय-समाज के सच से मुठभेड़ करने का ख़तरा उठा रहा है? उन छिपे ख़तरों के भयावह और लगभग तबाह कर देनेवाले दूरगामी परिणामों को टोहने-सूँघने का उपक्रम कर रहा है? गगग वे उन्हें नहीं पहचान रहे तो क्यों? या पहचान कर भी उन्हें देखा-अनदेखा कर वादों और खेमों की छतरियों के नीचे सुरक्षित-सीमित उखाड़ पछाड़ तथा श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, प्रतिबद्ध-अप्रतिबद्ध की क्षुद्र राजनीति में उलझे हुए वर्चस्ववाद के पैंतरे भाँजते एक-दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी समूची सर्जनात्मक ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं? उनकी चिन्ता में आम आदमी कितना और कहाँ तक रह गया है, सोचते ही बेचैनियाँ आँखों में उँगलियाँ डालने लगती हैं कि हमने उनके लिए कुछ किया है तो मात्र इतना कि उन्हें वैचारिक उल्टियों, चश्मे से बँधी-रची कृतियों, पोस्टरों, नुक्कड़ नाटकों, चौंधियाहट लदे-फँदे नारों में क़ैद कर उन्हें उनकी ज़मीन से ख़ुद बेदख़ल कर इस्तेमाल की छद्म हित-चिन्तक राजनीति का मोहरा बना डाला! कलम के इस उपभोक्तावाद को हम किस खाँचे में डालेंगे? क्या नाम देंगे इसे?’’ (लपटें, भारतीय ज्ञानपीठ, पाँचवाँ संस्करण 2004, पृष्ठ छह). आगे इस क्रम में इसे वे ‘अभिव्यक्ति में ख़ालिस व्यक्तिवादी रवैये’ का ‘अनुगामी’ कहते हुए इससे ‘सामाजिक सरोकारों के प्रति शब्दशक्ति’ के प्रज्ज्वलन की असम्भवता का प्रतिपादन करते हुए आह्वान करती हैं कि लेखक लोग अपनी ‘कलम की दराँती को छद्म के पाश से मुक्त’ करें, ताकि ‘‘मारक दबावों की चौतरफ़ा मार से त्रस्त-ध्वस्त लगभग जड़ावस्था में पहुँच रहे जनमानस की ग़ुलामी की हदें छूती सहिष्णुता को अभिव्यक्ति की तीव्रता दरका सके, उन्हें उनका सही पाठ सौंप सके, उनमें अपेक्षित आँच-ताप जगा सके कि ऐसा होना उनकी नियति नहीं है, न निरपेक्षता उसका समाधान!’’ (वही).
इस लम्बे उद्धरण की प्रासंगिकता इसमें निहित वह अन्तर्विरोध है, जो न केवल चित्रा मुद्गल के वक्तव्यों, उनके पीछे सक्रिय विचारों, उनमें निहित उनकी कथित ’अवधारणाओं’ बल्कि आगे चलकर उनकी रचनाओं की अन्तर्वस्तु को अंतर्दृष्टिपरक संभ्रम वैचारिकता के संकट से संग्रस्त कर देता है. इस उद्धरण में एक तरफ़ वे वादों-खेमों, प्रतिबद्धता-अप्रतिबद्धता जैसे अवधारणात्मक शब्दों की एक तरह से खिल्ली उड़ाती हैं तो दूसरी तरफ़ अन्त तक पहुँचते-पहुँचते ‘निरपेक्षता ’ का भी निषेध करती चलती हैं. दो नावों पर एक साथ सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेकिन चित्रा मुद्गल वक्तव्यों में भी और रचना में भी जब-तब इसकी चपेट में आ ही जाती हैं. उनके साथ दरअसल दिक़्क़त यह है कि यथार्थ की अन्दरूनी सतह तक पहुँचने से काफ़ी पहले ही उनकी विचारचिन्तना और सृजनात्मकता ज़बाव देने लगती है और इस स्थिति में वे अगल-बगल और आगे-पीछे और ऊपर-नीचे के घटना, पात्रों, स्थितियों के लम्बे-लम्बे ब्यौरों और भाषायी खेल का सहारा लेते हुए कहानी को एक अंज़ाम तक पहुँचाती हैं. मसलन उनकी ‘जिनावर’ कहानी को देखा जाए. विशेषतः इसके अन्तिम हिस्से को, जहाँ घोड़ी सरवरी की मौत और उसके हर्ज़ाने के बाद असलम के ठीक से सो न पाने और उसके किसी गहरे अपराध-बोध और क्षोभ की गिरफ़्त में आ फँसने की मनःस्थिति का कथांकन है. यहाँ दो दृश्य हैं. पहला यह कि उसे सोते में सरवरी का रुन-झुन हिनहिनाहट का प्रखर स्वर बार-बार बेताबी के साथ सुनाई देता है और उसकी नींद उचट जाती है. वह हड़बड़ाकर कोठरी के बाहर आता है पर वहाँ उसे बिना सरवरी के अकेले उदास खड़े ताँगे के अलावा कुछ नहीं नज़र आता. ठीक इसी क्षण उसे यह अपराध-बोध सालना शुरू होता है-‘‘सरवरी यहां हो भी कैसे सकती है? उसे तो वह वहीं सड़क पर मुर्दा छोड़ आया था-नगरपालिका की बेजान लावारिस पशुओं की लाशें ढोने वाली गाड़ी के भरोसे. कितनी तेजी से वह तांगा लेकर भागा था घटनास्थल से.’’ (आदि-अनादि -3, चित्रा मुद्गल की सम्पूर्ण कहानियां; सामयिक प्रकाशन 2009; पृ. 52). दूसरा दृश्य वह है, जिसमें वह हर्ज़ाने में मिले नोटों को लानत भेजता हुआ अपनी हरामज़दगी/बेमुरौव्वती का बखान/ऐलान करता हुआ बेतरह ख़ुद को कोसता चला जाता है-‘‘नहीं, वह जुदा नहीं हुई, उसके जुदा होने से पहले ही मैंने उसे मार दिया, मैंने उसकी मौत से सौदा कर लिया, बीबी! जान-बूझकर उसे गाड़ी से भेड़ दिया! यही सोचकर कि अपनी मौत तो वह मरेगी ही, आगे-पीछे किसी गाड़ी से भेड़ दूंगा तो वह मरते-मरते अपनी कीमत अदा कर जाएगी…ये नोट, नोट नहीं, मेरी सरवरी की बोटियां हैं…बोटियां, बीबी…’’ (वही).
इन दोनों दृश्यों का समेकन और समाकलन करने पर जो चीज हाथ लगती है, वह क्या है, पता नहीं! चित्राजी के बारे में कहा जाता है कि वे समाज के निम्नवर्गीय तबक़े की विशेषज्ञ हैं, उनके बीच वे एक सहानुभूतिशील कार्यकर्ता की तरह सक्रिय रही हैं, इस तबक़े के यथार्थ-चित्रण में वे सिद्धहस्त हैं, आदि-आदि. हमें इस कथन से कोई गुरेज़ नहीं है, बशर्ते यह कहीं एक ‘किंवदन्ती’ न बन जाए! जो हो. तो, किस तरह का निम्नवर्गीय यथार्थ यह कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करती है? क्या लेखिका निम्नवर्गीय मानसिकता के किसी काइयांपन, टुच्चेपन, बेहयाई-बेमुरौव्वती इत्यादि का खुलासा करने के मक़सद से इस कहानी को लिखती प्रतीत होती है? क्या सचमुच इस कहानी में निहित वर्ग-दृष्टि इतनी प्रकृष्ट है कि इससे हमारी आँखें खुल जाती हैं! पता नहीं, सच क्या है! एक पाठक के रूप में मैं भारी सम्भ्रम/दिग्भ्रम की स्थिति में हूँ! क्योंकि अब तक निम्नवर्गीय मानसिकता के किसी काइयांपन, टुच्चेपन, बेहयाई-बेमुरौव्वती इत्यादि का खुलासा जिस तरह कहानियों में होते देखा है, उसमें लेखक का रुख़ और रवैया कहानी के एकदम प्रारम्भ से क्रिटिकल या तुर्श देखा गया है. अपने पात्र/चरित्र पर वह बराबर तीखी पैनी खरादभरी निगाह रखता चलता था; कुछ इस तरह कि देखें बच्चू, बचकर कहाँ जाता है! ठीक वैसे जैसे इस कहानी में लेखिका का असलम की बीबी जुबैदा के प्रति लगातार तीखा रवैया है. पाठक के मन में उसके प्रति अन्त तक एक तरह की वितृष्णा और अनमनापन-सा बना रहा आता है तो दरअसल इसलिए कि वह हमारे अज़ीज़ बेचारे कथानायक असलम को लगातार कोसती, परेशान करती रहती है! असलम के प्रति एक पाठक के बतौर सहानुभूति का ग्राफ़ हमारे मन में लगातार ऊपर चढ़ता चलता है. अतः जब हम उसे ऐसा काइयांपन और टुच्चापन करते देखते हैं तो यक़ायक़ यक़ीन नहीं हो पाता कि यह वही हमारा नायक है, जो एक तरफ़ ग़रीबी तो दूसरी तरफ़ बीबी के दबावों से परेशान है! जब हम उसे अपने दिलोजान से प्यारी सरवरी के साथ ऐसी ग़द्दारी करते देखते हैं तो हमारा सारा तिलिस्म तार-तार हो जाता है और कहानी नितान्त अविश्वसनीय हो उठती है कि आख़िर लेखिका हमारी पाठकीय अस्मिता के साथ यह कैसा खिलवाड़ अब तक करती रही! एक पाठक के बतौर हम तय नहीं कर पाते कि लेखिका पहले वाले असलम के साथ है या इस दूसरे वाले ग़द्दार असलम की खोचड़ी वह करना चाह रही है? इस स्पष्ट पक्ष -ग्रहण या स्टैंड के अभाव में कहानी गुड्डे-गुड़ियों का खेल बनकर रह जाती है. भाववादी या मनभावन तरीक़े से कहानी कैसे लिखी जाती है, यह कहानी उसका उल्लेखनीय उदाहरण है.
इसी तरह उनकी एक और कथित रूप से अतिचर्चित कहानी ‘प्रेतयोनि’ को लिया जाए. इस कहानी पर कानपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित दो उदग्र श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का जो हवाला चित्राजी ने अपनी ‘चर्चित कहानियाँ’ (सामयिक 2006) की भूमिका ‘पाठकों की सत्ता’ में दिया है, उसमें यह चीज समझ से परे है कि डा. सुरेश अवस्थी और डा. प्रेमा रश्मि में से डा. प्रेमा रश्मि की ही प्रतिक्रिया लेखिका को क्यों पसन्द आई? क्या इसलिए कि वह लेखिका के अभिप्रायानुकूल है? फिर यह पाठक की सत्ता कहाँ हुई; यह तो अन्ततः लेखक की ही सत्ता स्थापित हुई न! हमें लेखक की सत्ता से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वह पाठक के जनतान्त्रिक अधिकारों के आड़े न आने लगे. डा. सुरेश अवस्थी का अभिमत, हो सकता है, थोड़ा पूर्वाग्रही हो, जिसमें उन्होंने कहा कि ‘‘कहानी को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने के लालच में लेखिका ने मां के भीतर अविश्वास आरोपित किया है. यथार्थ में कोई मां अपनी बेटी के प्रति इस कदर अमानवीय नहीं हो सकती.’’ (चर्चित कहानियाँ, सामयिक प्रकाशन 2006, पृ. 07). लेकिन डा. प्रेमा रश्मि का यह अभिमत और ख़ुद लेखिका द्वारा उसे उद्धृत किया जाना तो और भी ज़्यादा गड़बड़ है कि जिसमें उन्होंने कहा कि ‘‘कहानी में वर्णित सत्य में रत्ती भर भी अतिशयोक्ति नहीं. वास्तविकता यही है कि जिस समाज में बेटे के सात खून माफ कर देने की परंपरा हो उसी समाज में निर्दोश बेटी के साथ लोकापवाद की आड़ में किस सीमा तक अमानवीय हुआ जा सकता है, इसका अनुमान मां के आंचल में विशेश दर्जा पाने वाले पुत्रों को होना असंभव है…’’ (वही).
यानी कि डा. सुरेश अवस्थी के अभिमत को आप इसलिए नकार देंगी कि वह एक बेटे (पुरुष ) के मुँह से निकला है! हम, निश्चय ही, जैसा कि हमने कहा, यह आवश्यक नहीं कि डा. सुरेश अवस्थी के मत से इत्तिफ़ाक़ रखा ही जाए; लेकिन यह तो और भी अनावश्यक होगा कि आप उसे इसलिए नकारें कि वह एक पुरुष का अभिमत है! निश्चय ही हम यह मानते हैं कि हर व्यक्ति की अभिव्यक्तियों/प्रतिक्रियाओं की संरचना में उसके जेण्डर का कहीं न कहीं कुछ न कुछ हस्तक्शेप अवश्य होता है, लेकिन डिक्लास और डिकास्ट होने की तरह डिजेण्डर या कि जेण्डर न्यूट्रल होने की भी एक प्रक्रिया होती है जो डिक्लास और डिकास्ट होने की ही तरह बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही असुविधाकारी और दुरूह होती है. असम्भव होती है, ऐसा नहीं; यह बिल्कुल सम्भवनीय है, बशर्ते कि आपका मष्तिष्क अनुनादी और सूक्ष्मरन्ध्र उभयलिंगी मस्तिष्क जैसी पूर्ण विकासावस्था को प्राप्त हो चुका हो. ऐसा पूर्ण विकसित उभयलिंगी मस्तिष्क ही सृजनात्मक होता है. (वर्जीनिया वुल्फ). एकलिंगी मस्तिष्क; चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का; लैंगिक विभाजन के आग्रहों से मुक्त नहीं हो सकता. अतः उक्त दोनों प्रतिक्रियाओं को हमें इसी उभयलिंगी मस्तिष्क के स्वभावानुसार ग्रहण करना होगा. खेद है कि चित्राजी ऐसा नहीं कर पातीं! ऐसा नहीं है कि वे ऐसा कर नहीं सकती थीं. बाक़ायदा वे ऐसा कर सकती थीं. अपनी कई कहानियों में उन्होंने अपने उभयलिंगी सृजनात्मक मस्तिष्क का उल्लेखनीय परिचय दिया है, जैसे कि ‘त्रिशंकु’, ‘पाली का आदमी’, ‘अपनी वापसी’ आदि; हालाँकि इन कहानियों में भी कुछ गहरी और ध्यानाकार्षी गड़बड़ियाँ हो गई हैं, जिन पर विचार आगे. ‘प्रेतयोनि’ पर डा. रश्मि के उक्त अभिमत के सामने वे विवश हैं क्योंकि दरअसल यह गड़बड़ कहानी में ख़ुद उनकी की हुई है.
पाठक विचार करें कि लोकापवाद क्या इस कहानी की अन्तर्वस्तु का अपना स्वाभाविक हिस्सा है? मेरी बात कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है, पर कहानी की वस्तु को ज़रा ग़ौर से देखिए तो पता चलेगा कि लेखिका ने जानबूझकर कहानी में ट्विस्ट पैदा किया है. कहानी साफ़ दो विपरीत दिशाओं में एक साथ चलती दिखाई दे रही है. यह ज़रा तसल्ली से सोचने की बात है कि कुमारी अनिता गुप्ता की बहादुरी, संघर्शशीलता और संघर्शक्शमता, प्रत्युत्पन्नमति, आत्मविश्वास, आत्मबल, धैर्य, प्रतिरोध इत्यादि का मूलाधार, मूलस्रोत और उत्प्रेरणा क्या और कहाँ अवस्थित रही हैं? उसमें झाँसी की रानी और दुर्गा जैसी सक्शमताएँ कहाँ से आईं? कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. ख़ुद कहानी बाक़ायदा इसका स्पश्ट ज़वाब देती दिख जाएगी. दरअसल यह उसका अपना परिवार ही था; विशेशतः उसके अम्मा-बाबूजी; सबसे ज़्यादा बाबूजी; जहाँ से यह ऊर्जा उसे मिली थी, मिलती थी. कहानी में एक नहीं अनेक जगह साफ़ इसके हवाले आए हैं. जैसे यह कि ‘‘कहां से संचित किया था आत्मबल अपने रोम-रोम में? बाबूजी से ही पाया था न?’’ (आदि-अनादि -3, पृ. 97). कहानी में इन बाबूजी के विशय में और जो कुछ कहा गया है, वह निहायत ही एक जेण्डर न्यूट्रल उभयलिंगी विकसित सृजनात्मक मस्तिष्क की उपस्थिति की सूचना देने वाला है कि बाबूजी स्त्री सम्बन्धी परम्परागत पितृसत्तावादी सोच से एकदम मुक्त हैं कि ‘‘बाबूजी ही कहते थे न-बेटियां ही मेरे बुढ़ापे की लकुटिया बनेंगी. यही व्यक्ति है, जो अम्मा से हमेशा इस बात के लिए लड़ता-भिड़ता रहा कि मैं अपनी लड़कियों को कुछ दहेज में दूंगा तो सिर्फ शिक्षा. शिक्षा ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी. अपनी ऊंच-नीच स्वयं निबटेंगी.’’ (वही, पृ. 96-97). शायद इसी मस्तिष्क से उपजा यह वाक्य भी था, जो अपनी बेटी के लौटने के समय उनके मुँह से फूटा था कि ‘‘भूल जा बेटी, जो कुछ तुझ पर बीती, सोच ले, दुःस्वप्न था. हमारे लिए यही बहुत है कि तू जीवित है…हमारी आंखों के सामने है. तू एक नहीं, दो-दो यमराजों को पछाड़कर आ रही है.’’ (वही, पृ. 99).
यह कहानी की एक दिशा थी.
कहानी की दूसरी दिशा वहाँ से शुरू होती है, जहाँ अख़बार में एक दिन पहले उसके साथ घटे वाक़ये की ख़बर ‘एक बहादुर लड़की की शौर्यगाथा’ बाॅक्स आइटम के रूप में उनके दृष्टि पथ से गुज़रती है और लेखिका के सहयोग से एकदम बेतरह पलटी खाते हुए वे खाप पंचायतों के प्रवक्ताओं-प्रतिनिधियों के निम्नतम ग़लीज़ स्तर पर उतर आते हैं. इस ख़बर के बाद पूरे परिवार का जो पितृसत्तात्मक ध्रुवीकरण क़दम-दर-क़दम उभरकर सामने आता है, वह हैरतअंगेज़ है. इस ध्रुवीकरण को अपरिक्राम्य और सहज-स्वाभाविक बनाने के लिए कुछ मिर्च-मसाले भी डाले गए हैं, जैसे यह कि ‘‘नाड़ा?’’ ‘‘टूट गया? कैसे?’’ नाड़ा गठियाया हुआ नहीं था, फिर भी टूट गया; इसका मतलब? यानी कि कहीं कुछ ‘गड़बड़’/‘ग़लत’ ज़रूर हुआ! लड़की के कहने से क्या होता है कि ‘‘भागते-भागते…’’ ‘‘टूट गया’’ (वही, पृ. 102). और यह कि ‘‘हाथ आई को मर्द छोड़ता है कहीं?’’ (वही, पृ. 108). और यह भी कि ‘‘महीने को कितने दिन शेष हैं?’’ (वही, पृ. 102). कोई लाख चाहे यह कहता रहे कि ‘‘हाथ आती तब न! तुमसे झूठ बोला है कभी?’’ (वही). और कहानी भी चाहे पाठकों को बराबर यह बताती रहे कि ‘‘अपने आत्मसंघर्ष के बूते पर पाई मुक्ति’’ (वही, पृ. 93), ‘‘साहसी अनिता ने बड़ी बहादुरी से वहशी टैक्सी-चालक का सामना किया और किसी प्रकार उस दरिंदे के चंगुल से निकल भागने में सफल हुई.’’ (वही, पृ. 95), ‘अम्मा, तुम जिस आशंका से पीड़ित होकर यह प्रश्न पूछ रही हो, वैसा कुछ उस कामुक राक्षस की पूरी कोशिश के बावजूद संभव नहीं हो पाया! मैं प्राणपण से लड़ी हूं…’ (वही, पृ. 102-03); आदि-आदि; पर लेखिका ने जो तय किया हुआ है, उसे उससे राई-रत्ती टस से मस नहीं होना है! आख़िर क्या तय किया हुआ है, लेखिका ने?
दरअसल यही कि उसे एक ऐसी कहानी लिख मारनी है जो लोकापवाद का सांघातिक यथार्थ उजागर कर सके. इस विनिश्चय में कोई बुराई नहीं थी. लोकापवाद एक भारी भावुकतावादी समस्या है. लेकिन इस कहानी में तो वह भी नहीं है. यहाँ दरअसल लोकापवाद नहीं, उसका ‘प्रेत’ है. यानी कि लोकापवाद नहीं, मात्र उसका आभास! आभासी लोकापवाद! सारी कहानी की ऊर्जा का कचूमर इस एक जानबूझकर लाए गए ‘लेखकीय’ वाक्य ने निकाल कर रख दिया; जो कि ख़ुद लेखिका भी जानती थी कि यह निर्मूल है-‘‘भोपाल से आ रही अनिता गुप्ता मथुरा के निकट शहर से दूर एक निर्जन स्थान पर कामुक टैक्सी-चालक की हवस का शिकार हुई.’’ (वही, पृ. 94). इसके अगले ही वाक्य में हालाँकि इसका स्पष्टीकरण है कि यह एक अर्धसत्य ही है. ‘हवस का शिकार हुई’ का वह अर्थ नहीं है, जो लिया जाता है. बलात्कार दरअसल हुआ ही नहीं. लेखिका बार-बार हमें याद दिलाती चलती है कि ध्यान रहे, बलात्कार हुआ नहीं! जब बलात्कार हुआ ही नहीं तो चिन्ता की बात क्या? इस कहानी की ‘तारीफ़’ यह है कि बलात्कार से ज़्यादा भयावह स्थितियाँ इसने पैदा कर दीं! क्यों आख़िर लेखिका को बार-बार यह साफ़ करना पड़ रहा कि बलात्कार नहीं हुआ? यदि हो जाता तो कहानी की संरचना में क्या फ़र्क पड़ जाता?
लेखिका का पहला दुराग्रह यह है कि बलात्कार नहीं हुआ और दूसरा दुराग्रह यह कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, घर वाले तो मान रहे हैं कि हुआ! पाठक देखें कि माँ आख़िर उसे कौन-सा काढ़ा पिलाने पर आमादा है! ये सन्दर्भ ऊपर आ चुके हैं. माँ को लग गया है कि बेटी की माहवारी में शायद देरी हो गई है और यह भी कि क्यों? वह यह पक्के तौर पर मान कर चल रही है कि अब कुछ बचा नहीं है! इसीलिए वह कहती है-‘‘काढ़ा पी लेने से महीना किसी हालत में नहीं रुकेगा…’’ (वही, पृ. 108). यानी कि आभासी यथार्थ का ऐसा घटाटोप कि कथानायिका के साथ पाठक भी पनाह माँगने लगे! कहानी ख़ुद यहाँ अपने केन्द्रीय चरित्र के ख़िलाफ़ चली जाती है. डा. सुरेश अवस्थी ने शायद इसीलिए इस अविश्वास के मार्फ़त लेखिका के कहानी को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने के लालच वाली बात उठाई थी. लेकिन डा. अवस्थाी शायद एक बात भूल गए. उन्हें दरअसल कहना चाहिए था कि कहानी को नहीं, कहानी में सायास आरोपित एक आभासी यथार्थ को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने का लालच वस्तुतः लेखिका के मन में था!
एक तरह से कहा जाए तो दरअसल आभासी यथार्थ का चरमोत्कर्ष ही चित्रा मुद्गल की कहानी-कला का नाभि-केन्द्र है. उनकी कोई भी कहानी उठाकर देखी जाए; आभासी यथार्थ उसके केन्द्र में मिलेगा. आभासी यथार्थ अर्थात् यथार्थ का सम्भ्रम अर्थात् एक प्रकार का अयथार्थ यथार्थ अर्थात् भाववाद या भावुकतावाद; और थोड़ा आगे चलें तो, एक प्रकार का गढ़ा हुआ यथार्थ. यह गढ़ा हुआ यथार्थ उनकी अधिकांश कहानियों में अधिकांशतः देखा जा सकता है. चाहे वह उनकी प्रारम्भिक कहानी हो या परवर्ती. जिन्हें वे अपनी ‘बहुचर्चित’ कहानियाँ मानती हैं, वे दरअसल इसी गढ़े हुए यथार्थ से आक्रान्त कहानियाँ हैं. चाहे वह ‘अपनी वापसी’ हो या ‘भूख’ हो या ‘लकड़बग्घा’ हो या ‘मामला आगे बढ़ेगा अभी’ हो. ये सब की सब कहानियाँ अन्दर ही अन्दर कुछ ऐसी दरारों से भरी पड़ी हैं कि मन यक़ायक़ झुँझला उठता है कि आख़िर इतनी-सी बात लेखिका के दिमाग़ में आने से कैसे रह गई! जैसे कि ‘भूख’ कहानी को ही लिया जाए तो कहानी ख़त्म करने के बाद सबसे पहली बात दिमाग़ में यही आती है कि क्या कहानी इसी तरह गढ़ी जाती है! भूख में निहित ‘यातना, अमानवीयकरण, शोषणजन्य हत्या’ इत्यादि (चर्चित कहानियाँ, पृ. 07) से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है. हम तो सिर्फ़ यह जानना चाहते थे कि इस कहानी की लक्ष्मा आख़िर कैसी माँ रही कि शाम से सुबह तक छोटू उसके पास होता था फिर भी वह उसकी यह असलियत नहीं समझ पाई कि दिन भर खाने को उसे कुछ नहीं मिला है, वह निपट भूखा है! क्या यह माना जा सकता है कि छोटू जितने छोटे बच्चे की भूख का पता ही न चले? यह अज़ीब है कि कांबले तायी को तो यह पता है कि भीख माँगने के लिए इस तरह किराए पर लिए बच्चों की क्या नियति होती है कि-‘‘वो छिनाल बच्चे का पेट भरती तो बच्चा आराम से गोदी में सोता, पिच्छू उसको भीक कौन देता? अरे वो बच्चे को फकत भुक्काच नईं रक्खते, रोता नईं तो चिकोटी काट-काट के रुलाते कि लोगों का दिल पिघलना…’’ (वही, पृ. 48-49) पर लक्ष्मा लगातार इसी मुग़लते में है कि ‘‘वो तो बोलती होती कि वो उसको दूध देती…बिस्किट खिलाती…’’ (वही, पृ. 48). लक्ष्मा का यह ‘भोलापन’ कितना विश्वसनीय है, पाठक ख़ुद इस पर विचार करें. हम तो सिर्फ़ इतना कहना चाहते हैं कि इतने छोटे बच्चे में रात भर में भूख का कोई लक्षण न दिखे, यह क़तई एक अनहोनी और मनगढ़न्त बात है. क्या यक़ायक़ ऐसा हो सकता है कि रातों-रात किसी बच्चे की आँतें सूखकर चिपक जाएँ! बड़े से बड़ा रोग भी सांघातिक होने के पहले अपने कुछ लक्षण दिखाता है. जो हो.
यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि लक्ष्मा को अपने छोटे-से बच्चे की इस स्थिति की क़तई भनक तक नहीं लगी! कहानी में सिर्फ़ इतना उल्लेख है कि ‘‘इधर छोटू बोत चीं-चीं करने लगा है.’’ (वही, पृ. 46). लेकिन लक्ष्मा इसे उसकी नखरेबाज़ी से अधिक कुछ नहीं समझती-‘‘उसे लगता है कि दिनभर जग्गूबाई की गोदी चढ़े रहने और घर से बाहर रहने के कारण छोटू को घुमक्कड़ी की बुरी लत हो गई. यही वजह है कि घर में घुसते ही वह लगातार मिमियाता रहता है और चाहता है कि कोइ-न-कोई उसे गोदी में उठाए ही रहे.’’ (वही). इसीलिए जब यह सुनकर कि बच्चा भूख से मर गया, उसकी आँतें सूखकर चिपक गईं; उसके गले से ‘आरी-सी काटती एक करुण चीख फूट पड़ी’ (वही, पृ. 48) तो एकाएक विश्वास नहीं हो पाता कि यह सचमुच एक माँ की चीख है! पता नहीं, कृष्णदत पालीवाल सचमुच में ही इससे भीतर तक हिल गए थे (द्रष्टव्य वही, पृ. 07) या शायद उन्हें भी लगा कि नहीं हिलेंगे तो उन्हें सहृदय पाठक कौन मानेगा! निश्चय ही भीतर तक तो मैं भी हिला, लेकिन इसलिए नहीं कि लक्ष्मा के दुःख, उसके तड़पते ममत्व से मुझे कोई सहानुभूति थी. दरअसल कहानी की अन्तर्वस्तु ममत्व है ही नहीं. भूख भी एक सीमा तक ही कहानी की वस्तु बनी रहती है. उससे आगे वह भी चुक जाती है. तो फिर इस कहानी की असल अन्तर्वस्तु क्या है?
मेरी दृष्टि में इस कहानी की अन्तर्वस्तु दरअसल निम्न/सर्वहारा वर्ग का वह शर्मनाक यथार्थ है, जिसमें एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए अपने दुधमुँहे बच्चे को भिखमंगी औरतों को किराए पर उठाने को विवश है. लेकिन यथार्थ का यह सिर्फ़ एक व पूर्ववर्ती पहलू है. इस यथार्थ का दूसरा व उत्तरवर्ती पहलू यह है कि यह यथार्थ नहीं यथार्थवाद है और हर्गिज़ इसके चंगुल में फँसने की ज़रूरत नहीं है! यथार्थ वास्तविकता तो यह है कि भिखारिनों को भीख माँगने के लिए अपने दुधमुँहे बच्चे को किराए पर दे देना लोगों के लिए अब एक धन्धा बन चुका है. यहाँ भावुकता, रिश्तों की संवेदना इत्यादि का कोई स्थान नहीं, यह शुद्ध एक ‘धन्धा’ है. देशभर में बाक़ायदा इसका पूरा जाल बिछा है. कहानी में भी एक जगह इसे धन्धा ही कहा गया है.लक्ष्मा के मँझले बेटे किस्तू से एक जगह कहलवाया गया है,-‘‘छोटू धन्धे पर से नहीं आया? आएगा तो पिच्छू भाकरी देगी?’’ (वही, पृ. 46). गड़बड़ दरअसल यह हुई है कि लेखिका ने अपना सारा ध्यान इस यथार्थ के पहले पक्ष पर केन्द्रित कर दिया जो कि इस यथार्थ का सिर्फ़ एक भाववादी पहलू है. एक माँ की पीड़ा को नज़रन्दाज़ करना हमारा मक़सद नहीं है. ऐसी हिमाक़त कोई भला कर भी कैसे सकता है! लेकिन कोई भला क्या इस जघन्य वास्तविकता से भी आँख चुरा सकने की हिमाक़त कर सकता है कि अपने दुधमुँहे बच्चों को भिखमंगी औरतों को किराए पर दे देने का चलन अब एक व्यवस्थित व्यवसाय बन गया है? मेरा विनम्र ख्याल है कि चित्राजी यदि इस बिन्दु की संकेन्द्रीयता से इस कहानी को उठातीं तो कहानी कहीं ज़्यादा मौज़ूँ और ठोस यथार्थपरक हो आती. इस वस्तु को इस कोण से यदि विकसित और निरूपित किया जाता, समझा जाता तो शायद और ज़्यादा गहरी कारुणिक आरी-सी काटती चीख ख़ुद पाठक को अपने अन्दर से फूट पड़ती सुनाई पड़ती जो उसके कलेजे को चीर कर रख देती. फ़िलहाल तो यह कहानी कथित ममत्व के इकतरफ़ा भाववाद में सिमटकर रह गई है.
इसी तरह का एक इकतरफ़ापन उनकी ‘मामला आगे बढ़ेगा अभी’ कहानी में भी दिखाई देता है बल्कि कुछ डिग्री ज़्यादा ही जहाँ, एक सर्वहारा किशोर अपनी मालकिन के आभासी मातृत्व के फेर में लगभग पागलपन की स्थिति में पहुँच रहा है. इस कहानी के बारे में कहा जा सकता है कि यह एक ‘पीड़ित ममत्व’ की कहानी है. पीड़ित ममत्व किसका? तय है कि मोट्या का! आख़िर क्यों? यह मेम साहब की तरफ़ से क्यों नहीं? मोट्या की तरफ़ से ही क्यों? मोट्या की तरफ़ से इसलिए कि वह बेचारा मातृत्व-विहीन अभागा अनाथ ‘बच्चा’ है और अपनी ज़िन्दगी में पहली बार जो वह एक अधेड़ औरत के सम्पर्क में आया तो फिर जैसे न केवल उसकी नौकरी बल्कि उसकी अब तक की कमी माँ की ज़रूरत भी उससे पूरी होती दिखी. लिहाज़ा वह अपनी मेमसा’ब माँ को साधिकार अपना दिल दे बैठा. उसका दिमाग़ ठनका तब जब बीमारी के कारण ड्यूटी में हुए नागा के चलते उसकी पगार में कटौती कर ली गई, ‘खाड़ा’ काटा गया और मेमसा’ब ने उसे कटने दिया. न केवल इतना बल्कि यह भी कि सा’ब ने खाड़ा के वास्ते झगड़ने पर मोट्या को ‘‘झापड़ चढ़ा के दफा हो जाने को बोला’’ (वही, पृ. 123) और इसके साथ ‘‘धक्का मारके घर से बाहर कर दिया…’’ (वही). मोट्या को दरअसल यह पीड़ा नहीं है कि सा’ब ने उसके साथ ऐसी क्रूरता बरती, बल्कि उसकी असल पीड़ा इस पूरे मामले में मेमसा’ब की लगातार चुप्पी को लेकर है. मेमसा’ब के इस अप्रत्याशित/संदिग्ध व्यवहार से उसे असल चोट पहुँची है. वह न केवल तावड़े के सामने यह सब साफ़-साफ़ बयान कर देता है (द्रश्टव्य, वही) बल्कि ख़ुद मेमसा’ब के सामने तक यह उलाहना देने से नहीं चूकता कि ‘‘तुमने खाड़ा कटवा दिया न मेमसा’ब…अपने सामने चांटा मारने कू दिया न!…मैं…मैं…’’ (वही, पृ. 125). सा’ब ने क्रूरता बरती और मेमसा’ब का उसे मूक समर्थन मिला; लिहाज़ा अब मोट्या के पास इसके अलावा और क्या रास्ता है कि वह इस ‘अपनी’ पर उतर आए और उन सबको बता दे कि वह क्या चीज है!
इस पूरे वाक़ये को पढ़-सुनकर क्या किसी को कहीं लग सकता है कि यह वर्गचेतना से जुड़ा मामला है? मोट्या के निम्न और सक्सेना सा’ब-मेमसा’ब के उच्च वर्ग से जुड़े होने मात्र से तो यह कहानी वर्गचेतना का प्रतिपादन करने वाली कहानी हो नहीं जाएगी. वर्गदृष्टि का प्रतिनिधित्व तो यहाँ चौकीदार तावड़े कर रहा है जो बार-बार मोट्या को अपने भले-बुरे का ज्ञान कराता रहता है.
बात दरअसल अपने भले-बुरे के ज्ञान की यहाँ नहीं है. बात यह है कि मोट्या का मामला आगे कहाँ तक बढ़ेगा और कुछ बढ़ेगा भी या नहीं? लेकिन इससे पहले तो यही तय करना पड़ेगा कि मोट्या का मामला आख़िर है क्या? ऊपर हमने अपनी समझ से इस कहानी के बारे में जो कयास लगाया है, उसके हिसाब से तो मोट्या का मामला विशुद्ध रूप से एक भावनात्मक विक्षोभ का मामला है. हिन्दी की मसाला फ़िल्मों में ऐसे भावनात्मक दृश्य आए दिन आपको देखने को मिल जाएँगे जहाँ अमीर माँ अपने नौकर को अपने बेटे जैसा समझती देखी जाती है या इसके उलट भी कि किसी ग़रीब माँ के चरणों में किसी अमीरज़ादे होनहार को ज़न्नत के दर्शन होते दिखाई देने लगते हैं. क्या सचमुच इस भावुकतावाद का कोई भविष्य होता है? क्या चित्राजी मोट्या के आक्रोश को वर्गीय आक्रोश के बतौर पेश करना चाह रही थीं? यदि ऐसा है तो हिन्दी फ़िल्मों में अमिताभ बच्चन की सारी एंग्री-यंगमैन की भूमिकाएँ तथा और भी बहुत सारे टपोरी टाइप कैरेक्टर सर्वहारा के वर्गीय आक्रोश की प्रतिमूर्ति हो उठेंगे. फिर भला क्रान्ति आने और सक्सेना सा’ब जैसे जनविरोधी लोगों और मेमसा’ब जैसी गद्दारों की अक़्ल ठिकाने आने में क्या देर लगनी! हम मानते हैं कि मोट्या के दिल को गहरी ठेस लगी है और वह चुप बैठने वाला नहीं है. चाहे इकतरफ़ा ही सही, भावुकता का कुछ न कुछ असर तो आदमी पर पड़ता ही है. तो आगे क्या करेगा मोट्या? उसका आक्रोश किस रूप में विस्फोट करेगा आगे? जो हो, जैसा भी हो, मेरा यह दृढ़ मत है कि वह नितान्त वैयक्तिक और निजी, कुछ हद तक शायद षड्यन्त्रमूलक भी; होगा. इसके अलावा कुछ नहीं. कम से कम उसका कोई वर्गीय-जैसा चरित्र तो नहीं ही होगा. पता नहीं, मोट्या में कौन-सी वर्गीय सम्भावना लोगों को दिखाई देती है?
मेरा मानना है कि जैसा कि ऊपर उनके एक संग्रह की भूमिका के एक अंश के मार्फ़त मैंने संकेत किया; चित्राजी बहुत सारी चीजों को एक साथ समेटकर चलने की कोशिश करती हैं. इन बहुत सारी चीजों में कुछ एक-दूसरे की धुर विरोधी और कुचालक भी होती हैं. दुर्भाग्यवश वे इनकी छँटनी करना भूल जाती हैं या कई बार ऐसा भी होता है कि जानते-बूझते उन्हें वे अपने साथ लगाए-लगाए फिरती हैं कि शायद इनके बिना वे सत्ता-विहीन हो जाएँगी! सत्ता और विमर्श के बीच के अन्तर्सम्बन्धों की रवायत को ध्यान में रखते हुए आज चित्रा मुद्गल ही नहीं, और भी कई रचनाकारों की रचनाओं का पुनराकलन करने का वक़्त आ गया है.
दलित स्त्रीवाद , मेरा कमरा, जाति के प्रश्न पर कबीर
अमेजन पर ऑनलाइन महिषासुर,बहुजन साहित्य,पेरियार के प्रतिनिधि विचार और चिंतन के जनसरोकार सहित अन्य सभी किताबें उपलब्ध हैं.
फ्लिपकार्ट पर भी सारी किताबें उपलब्ध हैं.
दलित स्त्रीवाद किताब ‘द मार्जिनलाइज्ड’ से खरीदने पर विद्यार्थियों के लिए 200 रूपये में उपलब्ध कराई जायेगी.विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थान के आईकार्ड की कॉपी आर्डर के साथ उपलब्ध करानी होगी. अन्य किताबें भी ‘द मार्जिनलाइज्ड’ से संपर्क कर खरीदी जा सकती हैं.
संपर्क: राजीव सुमन: 9650164016,themarginalisedpublication@gmail.com