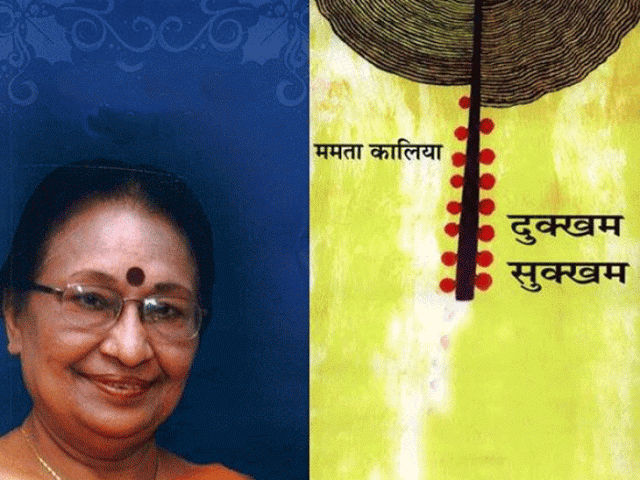ममता कालिया साठोत्तर कथा परिदृश्य की सशक्त रचनाकार हैं। ममता कालिया का लेखन-काल स्त्री चेतना का काल है, जब स्त्री -प्रश्न सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में था-विवाह, परिवार, स्त्री -पुरुष, स्त्री की यौनता और उस पर नियंत्रण के मुद्दों का केंद्रीय विमर्श बन जाना महिला आंदोलन और स्त्री की अपनी अभिव्यक्ति का प्रतिफल था। दहेज, सती, बलात्कार, यौन-उत्पीड़न, परिवार में असमानता के सवाल पर स्त्रियां सड़कों पर थीं और अनेक मुद्दों पर बेबाक राय दे रही थीं, हस्तक्षेप कर रही थीं। हिंदी का महिला कथा लेखन एक रूमानियत के दौर से निकल कर इन मूलभूत प्रश्नों के साथ दो-चार हो रहा था। ठीक उसी समय दलित आंदोलन भी अपने तेवर में था। साहित्य और इन सामाजिक आंदोलनों के अंतर्संबंध अथवा संवाद की समीक्षा होनी चाहिए, साहित्य के सामाजिक सरोकारों का एक परिदृश्य स्पष्ट होगा और साथ ही किसी रचनाकार के सरोकारों का भी। तीन दशकों के अंतराल के बाद यद्यपि प्रश्न बहुत बदले नहीं हैं परंतु राजनीतिक-आर्थिक- सांस्कृतिक, सामाजिक बदलावों के साथ कुछ नए प्रश्न उपस्थित हुए हैं। इन्हीं संदर्भों में जय कौशल ने ममता कालिया से संवाद बनाया। यहसंवाद अस्मिताबोधी सरोकारों का आपसी संवाद है, जो वर्गीय और वर्णगत विरोधाभासों को भी स्पष्ट करता है। निर्भीक प्रश्नों के घेरे में ममता कालिया मानवीय संवेदनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और लेखकीय सरोकारों के साथ, निर्मितिगत सीमाओं के बीच।
संपादक
ममता जी, विवाह संस्था के विषय में आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या सोचती हैं?
आज विवाह संस्था पुनर्परिभाषित होने के कगार पर है, विवाह से संबंधित सारी प्रचलित परंपराएं, रीतिरिवाज आदि अनिवार्यताओं को अगर हमने फिर से परिभाषित नहीं किया तो यह संस्था दिन पर दिन चोट खाती जाएगी। नई पीढ़ी के सामने अब विवाह जिस रूप में आ रहा है, उसमें घर का कोई तसव्वुर नहीं है। मेरा बेटा और पुत्रवधू सुबह आठ बजे मुंबई में काम पर निकलते हैं, रात में मेरा बेटा तो नौ बजे तक लौट आता है लेकिन पुत्रवधू रात को ग्यारह बजे तक आ पाती है। जब तक वे एक-दूसरे को समझ रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तब तक तो उनका परिवार चलेगा, लेकिन जिस दिन बेटे ने इसे समझना बंद कर झल्लाना शुरू कर दिया, उस दिन अंत हा जाएगा क्योंकि लड़की भी (पुत्रवधू) अपने कैरियर के उस ग्रॉफ पर है कि नौकरी नहीं छोड़ेगी। पति, परिवार और बच्चा छोड़ देगी लेकिन नौकरी नहीं और मैं इस मामले में बेटों का नहीं, बहू का साथ दूंगी। कुल मिलाकर अब परिवार का पूरा का पूरा तसव्वुर ही बदल गया है। हम खुद दम्पत्ति के रूप में नौकरीपेशा रहे हैं। यहां तक कि हमारा एक वक्त का खाना नौकरों के हाथ में ही रहा, लेकिन रवीन्द्र ने घर संभालने, बच्चों को पालने में पूरा सहयोग दिया। ऐसा नहीं है कि रवि पारंपरिक परिवार से नहीं आए थे परंतु शादी के बाद उन्होंने काफी छूट दी कि मैं अपना काम कर सकूं। मैं अपना काम छोड़कर नहीं आ सकती थी, परंतु मेरी कोशिश यही रही कि वे अप्रसन्न भी न रहें।
सातवें-आठवें दशक में विवाह के स्वरूप और आज उसके स्वरूप में क्या बदलाव आया है?
तब विवाह के स्वरूप में संक्रमण के बिंदु थोड़े कम थे। पहले लड़कियां मुख्यतः शिक्षण के क्षेत्र में जाती थीं। तब व्यापार प्रबंधन में उनकी संख्या बहुत कम थी, एम.बी.ए. जैसी जादुई चीज भी तब कहां थी? व्यापार प्रबंधन में लड़के भागते थे, एम-कॉम किया और मैनेजर बन गए, थोड़ी बहुत अतिरिक्त डिग्रियां, तो मैनेजिंग डायरेक्टर आदि बन ही जाते थे। लड़कियों के आगे नौकरी के क्षेत्र कम थे। कुछ के क्षेत्र तब भी थे, ऐसे क्षेत्रों में जहां लड़कियों की नाइट ड्यूटी होती थी, जैसे डॉक्टर, नर्स आदि। पहले समग्रतः लड़कियां शिक्षण के क्षेत्र में ही जाती थीं, अब नौकरियों के द्वारा अनेक हैं, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अवसर दे रही हैं। लड़कियों में भी रोजगार की चेतना प्रबल हुई। अगर हमें कहीं दूर आकर्षक वेतन भत्तों पर भेजा जाता तो हम शायद न जा पाते, हममें इस प्रकार की आकांक्षा सुनामी लहरों की भांति नहीं थी, जबकि आज की लड़कियों में नौकरी को लेकर यह आकांक्षा खूब है-वे इतिहास, भूगोल की कोई सीमा अब स्वीकार नहीं करती हैं। ये बात मुझे अच्छी लगती है कि उनमें यह जुझारूपन इक्कीसवीं शताब्दी की शुरुआत में ही आया है कि अब वे पुरुषों के साथ वाकई स्पर्धा में आ गई हैं। हम खाली कंधे से कंधा मिलाना चाहते थे। ये अपना कंधा आगे रखना चाहती हैं।
मतलब रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) का लेबल बढ़ा है, तो तलाक के मामले भी बढ़े हैं?
मेरे ख्याल से।
सत्तर-अस्सी में जब आप कहानियां लिख रही थीं तब वहां रेजिस्टेंस तो दिखता है, लेकिन तुरंत समझौते भी दिख जाते हैं, कोई सॉल्युशन जैसा नहीं दिख रहा है। क्या इसके पीछे विकल्पहीनता की स्थिति थी-खासकर आपकी कहानियों में?
एक लेखक और एक व्यक्ति दोनों स्तरों पर मुझे यह लगा कि अगर विवाह के बाहर आप जाते हैं, तो यह भी एक किस्म की पराजय है, मैं इसको एक प्रतियोगिता की तरह लेती हूं कि आप इसमें फेल न कर जाएं। सवाल इसका नहीं कि विकल्प है कि नहीं। मैं जानना चाहूंगी कि उनके सामने भी क्या विकल्प है? जो शादी की हद से कूदकर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोग खूब हाथ-पैर मारते हों, परंतु स्थायित्व तो चाहते ही होंगे। चाहे वह नौकरी में हों, चाहे रोजगार में हों, चाहे डिप्रेशन में हो या सुसाइड में हो या लिव-इन-रिलेशनशिप में हों-ये सारे विकल्प लचर हैं, उस स्त्री के आगे, जो अपनी रणनीति के साथ थोड़ी देर के लिए युद्ध-शांति घोषित कर लेती है। मुझे लगता है कि यह भी एक रणनीति का हिस्सा है कि आप किस समय अपनी लड़ाई में थोड़ी देर के लिए संधि कर लें। हारना भी एक नीति का अंग है। आप जिस विकल्पहीनता की बात कर रहे हैं, जो लोग इस फ्रेम से बाहर निकलते हैं, उनके सामने जो विकल्प हैं, उसमें कहीं न कहीं दुःख भी शामिल है। मैं यह मानती हूं कि छोटी-छोटी लड़ाइयां, जैसी मेरी कहानियों में आती हैं, उनमें संधि पत्र दे देना ज्यादा अच्छा है। बहुत बड़ी कोई बात है जो स्त्री के अस्तित्व पर आघात करती है, जैसे दीपक शर्मा की कहानियों में, जहां या तो वह रहेगी या नहीं रहेगी, वहां उसे लांघ लेना बेहतर है।
लेकिन सत्तर के दशक में जब आप लिख रही हैं, वहीं आपके लेखन में मध्यवर्गीय विमर्श जैसा दिखता है। जबकि उसी समय एक तीव्र महिला आंदोलन भी खड़ा होता है, जो सभी सवालों से जूझता दिखता है।
एक मिनट, आप जिस सत्तर के दशक के महिला आंदोलन की बात कर रहे हैं, वह पश्चिम से आया हुआ आंदोलन था। इसे ध्यान में रखिए। पश्चिम से जो नारीवाद आया, नारी स्वातंत्रय की चेतना आई, वह सैद्धांतिक रूप में हमने भले ही ग्रहण की हो, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष हमारे नजदीक बिल्कुल नहीं था।
उस समय कई धाराएं थीं, पश्चिम की धारा तो थी ही, लेकिन तब हम प्रेरणा ले रहे थे सावित्रीबाई फुले की धारा से खासकर महाराष्ट्र में। तब का महिला आंदोलन परिवार की बेसिक आलोचना कर रहा था, वह महिला श्रम, स्त्री-पुरुष के बीच समान श्रम अधिकार की बात कर रहा था, जबकि आप लोगों की कहानियों में मनोवैज्ञानिक गुत्थियां ज्यादा दिखाई पड़ती हैं।
सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे आदि ने 19वीं शताब्दी के अंत में आंदोलन को जहां तक ला दिया था, उसमें कोई प्रगति आधुनिक महिला आंदोलन में नहीं दिखती, क्योंकि जो मूलभूत प्रश्न जैसे समान अवसर की बात हो, जेंडर वर्गीकरण और श्रम की बात-ये सब बातें दीगर रह गईं और हम लोग पश्चिम वाली नारी स्वातंत्रय की धारा में बह गए। हम मनोवैज्ञानिक दाव पेचों में ज्यादा लग गए। मेरे से ज्यादा अन्य लेखिकाएं इस पर लिख रही थीं। मुझमें कन्फ्यूजन शायद कम है, औरों में ज्यादा। वह इसलिए कि सावित्रबाई फूले का आंदोलन बाद में प्रगति नहीं कर पाया, बल्कि उसमें एक गतिरोध भी आ गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने इतने प्रखर सुधारवादी आंदालनों को लगभग भुला दिया। वह शायद इसलिए कि भातर पर पाश्चात्य विचारधाराओं, सभ्यताओं और वहां के सोचने के नजरिए का बहुत घातक प्रभाव पड़ा है। हमने अपना बहुत समय नष्ट किया-कहीं अस्तित्ववाद बीच में आ रहा है, जिसके साथ आत्मघाती प्रवृत्तियां आ रही हैं, कहीं हमारे ऊपर एब्सर्ड थिएटर आ रहा है, कहीं निहलिज्म आ रहा है, इन सबके साहित्य पर घातक असर पड़ेगा, जिसके कारण बहुत व्यक्तिवादी किस्म के आंदोलन तब की कहानियों में दिखते हैं।
लेकिन आज जहां से कथ्य ले रही हैं, जिस समाज की कथा लिख रही थीं, उसी समाज में इक्वल ऑपरचुनिटी का मामला, घरेलू श्रम के वेजेज का मामला, जो सत्तर में उठाए जा रहे थे, आप लोगों की रचनाओं में नहीं दिखते-हालांकि ये सारे प्रश्न पश्चिम के महिला आंदोलन से प्रेरित होकर भी आए थे, जिसे मार्क्सवादी नारीवादियों ने उठाया था। आप लोगों के यहां इगो, मेल-शॉबिनज्म से टकराव, मनोवैज्ञानिक मुद्दे ज्यादा उठते हैं।
इस बात में आंशिक सत्य है, अगर आपने मेरा उपन्यास ‘नरक दर नरक’ पढ़ा हो, उसमें आप देखेंगे कि ऊषा की लड़ाई केवल स्त्री -पुरुष की लड़ाई नहीं है, वह लड़ाई एक ऐसे युवा दंपति की है, जो संघर्ष करके समाज में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहा है। असल में लेखक भी पाठक के साथ धीरे-धीरे बड़ा होता है। मैं मानती हूं कि मंजुल भगत, चित्रा मुद्गल और मेरी कहानियां हमारे समय को ज्यादा अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित करती हैं, वहीं मृदुला शिल्पवादी लेखिका हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं, कुछ ऐसी कहानियों को आधार बनाकर कह रहे हैं, जो शुरुआती दौर की हैं और जिनसे मैं खुद पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं।
आपने मृदुला गर्ग की बात की है, तो याद आया कि अभी उन्होंने हंस के एक सेमिनार में कहा था कि स्त्री के दलित होने का मैं सख्त विरोध करती हूं।
मैंने 1978 में ही एक सेमिनार में यह बात उठाई थी कि स्त्री को दलितों से न जोड़ा जाए।
परंतु सवर्ण और दलित स्त्रियों की समस्याएं एवं प्रतिरोध का स्तर तो अलग है, ऐसा आप मानती ही होंगी।
देखिए, किसी चीज के लिए कोई सामान्यीकरण तो किया नहीं जा सकता, लेकिन दलित स्त्री की समस्याएं कहीं अधिक हैं, उसकी पहली समस्या तो अस्तित्व से ही जुड़ी हैं। उसे जीवित रहने दिया जाए, यही एक अहम मुद्दा बन जाता है। जबकि संबंधों के मामले में दलित स्त्रियां ज्यादा उन्मुक्त होती हैं, बजाए सवर्ण स्त्रियों के। वह संबंधों के घेरे से बाहर आकर नए संबंध बना लेती हैं, जबकि सवर्ण स्त्री अपनी भीरूताओं और समाज की रूढ़ियों से इतनी घिरी रही है कि उसके लिए घेरा तोड़ना एक दुस्साहसिक कदम है। वह जल्दी अपनी चौखटे से बाहर नहीं आ पाती। बल्कि चौखटा लगातार उसका पीछा करता है, अगर वह एक से बाहर आ भी जाती है तो एक नया चौखटा उसका इंतजार करता रहता है।
सिर्फ आप ही नहीं, देखा जाए तो आपके समय का पूरा महिला लेखन सवर्ण महिलाओं के मध्यमवर्गीय तबके का विमर्श ज्यादा दिखाई देता है-वहां देह टैबू के रूप में आती है। कुछ लेखिकाओं ने रेडिकल होकर देह को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, मृदुला गर्ग को इसमें शामिल किया जा सकता है। आपके समय के महिला लेखन में दलित प्रश्न या श्रमिक प्रश्न तो गायब ही हैं।
लेकिन नब्बे के दशक में आकर सारा परिदृश्य बदल जाता है, बीच के तीन दशकों का जो समय है, उसमें आपकी बात ठीक हो सकती है, मुझे लगता है कि साहस धीरे-धीरे विकसित होता है। हम लोगों ने साहस यह दिखाया था कि उस जमाने में हम बाहर निकलकर नौकरी कर सकें और हमने कहानी को वहां से निकाला, जहां कहानी शिवानी, दीप्ति खंडेलवाल और चंद्रकिरण सोनरक्सा में फंस गई थी, जहां पर केवल एक चरित्र को फ्रीज फ्रेम में प्रस्तुत किया जाता था। उन्होंने कहानी को जहां पहुंचाया, वहां एक सुंदर किस्म की झीनी-झीनी सी कहानी का ही संदर्भ बनता दिखता है। हमने पहली बार उसमें व्यक्तित्व के प्रश्न उठाए। प्रति चेतना लगातार उसमें दिखइार् पड़ती है, बाहर आने की बेचैनी मिलती है। आप मेरी ‘दर्पण’ कहानी पढ़िए, ‘राजू’, ‘अलमारी’, ‘अट्ठावनवां साल’, ‘उसका यौवन’ आदि कहानियों में बदलते समाज की चेतना मिलेगी।
कहा जा रहा है कि स्त्री सबलीकरण हुआ है परंतु साथ ही अत्याचारों के मामले भी बढ़ते गए हैं। अकेले दिल्ली इस गवाह है।
ज्यों-ज्यों स्त्री चैतन्य होगी, शिक्षित होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, उसके खतरे बढ़ेंगे। समाज उसे आगे कहां स्वीकार कर पाता है। समाज में स्त्री की प्रक्षेपित छवि ही उसकी वास्तविक इयत्ता को चुनौती दे रही है। स्त्री की छवि को केवल मनोरंजन के आब्जेक्ट के रूप में दिखाया जा रहा है, फैशन चैनल, एम.टी.वी. देखिए तो ऐसा कतई नहीं लगेगा कि उनमें काम करने वाली लड़कियां किसी जबरदस्ती का शिकार हैं। कहीं न कहीं वे पैसे या ग्लैमर के लिए स्वेच्छा से काम कर रही हैं। मुझे लगता है स्त्री के जो सपने हैं, जो उसके काम करने के जोखिम भरे इलाके हैं, वे भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। अब सामान्य सी लगने वाली कोई लड़की शाम 7 बजे स्कूल से घर जा रही है, उसका भी बलात्कार हो जाता है। वह लड़की न तो देह प्रदर्शन कर रही होती है या न ही किसी प्रकार के आक्रमण को बढ़ावा देर ही होती है, लेकिन शिकार बन रही है क्योंकि नगरीय परिदृश्य पर जो माहौल बना है वह लड़कियों के लिए काफी चुनौती भरा है। आज नारी स्वातंत्रय का मतलब ही यह समझा जा रहा है कि स्त्री खतरों से कितना खेल सकती है। स्त्रियों को अपने संकट को पहचानना चाहिए।
आज कम पहनने को आजादी का खुलेपन का प्रतीक माना जा रहा है।
पिछले चालीस सालों से हम अपनी लड़ाई वैचारिक खुलेपन के लिए लड़ रहे हैं, उसका इतना सरलीकरण उचित नहीं है। मुझे लगता है कि हम आदिम संस्कृति की ओर लौट रहे हैं और इससे उसकी बर्बरता भी आ रही है। लड़की लाख पढ़-लिख जाए,उसे देखा सेक्स आब्जेक्ट ही जाता है। मैं इसे खुलेपन का हास्यास्पद विस्तार मानती हूं, हमें अपने वैचारिकी की बात करनी चाहिए। परंतु मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कहते हुए मैं किसी प्रकार की ड्रेस कोडिंग में विश्वास नहीं रखती हूं। खैर, प्रचलित खुलेपन के पीछे बाजार, मीडिया जैसे माध्यम जिम्मेवार हैं जो खुलेपन का छद्म बनाते हैं।
हम भी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं। नारीवादी आंदोलन जैसे अकादमिक भर रह गया हो। खैर, मैं पुनः परिवार, विवाह और कैरियर के सवाल की ओर लौटता हूं। आज की तारीख में क्या अतिरिक्त केरियरिज्म का दबाव परिवार और खुद स्त्री के जीवन पर नहीं बन रहा है।
हां, आज हमारे सामने जो लड़की आ रही है, उसके जीवन की प्राथमिकताएं एकदम बदल चुकी हैं। मैं सचमुच जानना चाहूंगी कि ऐसी लड़की के जीवन में प्रेम का पायदान क्या है? प्रेम कहीं न कहीं आपका मूलाधार है। मैं अपने मामले में हमेशा ये मानती रही कि नौकरी तो शायद फिर मिल जाएगी, लेकिन एक दोस्त नहीं मिलेगा। इसलिए रवि के कहीं जाने से पहले मैं उसके साथ चल देती हूं परंतु यह बात तो है कि अब हमें प्रेम को आज के नए रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। उन्नीसवीं सदी में प्रेम जिस रूप में बंगाली उपन्यासों में हमारे सामने आता है, बाद में हिंदी उपन्यासों में आता है, उसे अब बदलना होगा। पुरुषों को भी अपने मेंटल फ्रेम को ठीक करना होगा। आज भले ही प्रेम की तीव्रता और तन्मयता थोड़ी कम हुई हो लेकिन उसकी वास्तविकता व्यवहारिकता बढ़ी है। कैरियर की इस उठा पटक में प्रेम और परिवार का स्वरूप बदल गया है।
एंगेल्स ने अपनी पुस्तक ‘परिवार, संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति’ में कहा था कि परिवार में पुरुष सामंत होता है और स्त्री सर्वहारा। इस कथन को भारतीय परिवार के संदर्भ में आज की तारीख में कैसे देखा जाएगा?
नब्बे प्रतिशत परिवारों के लिए आज भी यह एक सच्चाई है, जहां पुरुष अकेला कमाता है, कमाई पर उनका पूरा अधिकार है, वहां स्त्री को चीजें कृपापूर्वक ही दी जाती हैं। मुझे स्त्री का शायद 10 प्रतिशत वर्ग ही उच्च शिक्षित हुआ लगता है। औसत परिवारों में आज भी सामंती व्यवस्था कायम है, बल्कि पढ़े-लिखे परिवारों में भी स्थितियां कुछ भिन्न नहीं हैं। मेरी ‘दर्पण’ में औरत को उसका पति ड्रेसिंग टेबल तब लाकर देता है, जब अपने को देखने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता। जहां पुरुष स्त्री के साथ सामंती मालिक की भूमिका में आता है या इसी ढर्रे पर सोचता है, वहां-वहां संघर्ष के मुद्दे पैदा होते हैं। रचनाकार की दृष्टि वहीं होनी चाहिए। कोई मुझे यह कहता है कि मैं पुराने प्रश्नों पर कहानियां लिखती हूं, तो मैं मानती हूं कि समाज इतनी जल्दी नया नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने अपने घर पर कारपेट बदल दिया और सब की सब चीजें नई हो गईं।
एक क्लेम यह है कि मार्क्सवादी समाज में जेंडर आधारित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अभी तक तो स्त्री को इकाई, एक व्यक्ति या मनुष्य माने जाने की प्रवृत्ति ही विकसित नहीं हो पाई। माना कि मार्क्सवादी समाज नहीं बना, लेकिन मार्क्सवादी प्रैक्टिस तो हुई है परंतु इस प्रैक्टिस में शामिल महिलाओं ने जेंडर आधारित विभेद ज्यों का त्यों पाया।
मुझे लगता है कि स्त्री विमर्श का सारा प्रश्न कहीं न कहीं एक व्यापक मानवीय विमर्श की मांग करता है। अगर परस्पर संबंध मनुष्य के बीच विकसित हो तो ज्यादा संतुलन आएगा। विचारणीय यह भी है स्त्री तब तक प्रोडक्टिव लेयर में शामिल नहीं होगी, तब तक उसे इकाई नहीं माना जाएगा। अगर वह घर-गृहस्थी में ही काम करती रहेगी तो उसे कभी प्रोडक्टिव इकाई में शामिल नहीं किया जाएगा, यह बड़ विसंगति है कि जो समाज की संरचना करता है उसे ही नॉन प्रोडक्टिव माना जा रहा है।
फिर सवाल साहित्य से, जहां दलित महिला और दलित पुरुष अपनी अलग-अलग आवाजें उठा रहे हैं। साहित्य में इस अभिव्यक्ति को आप कहां देखती हैं?
दलित महिला चेतना के स्तर पर जो आवाज उठा रही हैं, वह बहुत थोड़ी है, इनमें निर्मला पुतुल की कविताएं, उर्मिला पवार की आत्मकथा या कौशल्या बैसंत्री की रचनाएं देखिए तो फिर भी हम देखते हैं कि लक्ष्य अभी बहुत दूर है। सवाल यह भी है कि जिए समाज को आप जानते भी नहीं, उसके विषय में लिखने का आपको अधिकार भी नहीं। दलित लेखकों में ऐसे कितने लेखक हैं, जो मुंह पर रूमाल रखे बिना अमृतलाल नागर की तरह दलित बस्ती में घुसे और ‘नाच्यो बहुत गोपाल’ जैसा उपन्यास लिखे।
लेकिन कहा तो यह जाता है कि जिसने भोगा, वही प्रामाणिक लिख भी सकता है। अपनी पीढ़ी की प्रामाणिक अभिव्यक्ति एक दलित ही कर सकता है। इसीलिए कुछ आलोचकों ने ‘नाच्यो बहुत गोपाल’ को झूठा उपन्यास माना है।
चूंकि यह गैर दलित द्वारा लिखा उपन्यास है इसीलिए दलितों में लोकप्रिय होने के लिए इसे झूठा कहा जा रहा होगा। मुझे उपन्यास पढ़ते हुए कहीं नहीं लगा कि उसमें दलित पीड़ा की अभिव्यक्ति कमतर दर्ज हुई हो या कहीं से नागर जी ने उसे रोमांटीसाइज किया हो। घोड़े पर लिखने के लिए क्या घोड़ा होना पड़ेगा? वेश्या पर कहानी लिखने के लिए क्या मंटो वेश्या बन गए। हां, ऐसा माना जा सकता है कि दलितों को स्वयं लिखने से बहुत-सी प्रामाणिक चीजें पता चलती हैं, दया पवार, मोहनदास नैमिशराय, ओमप्रकाश वाल्मीकि आदि अच्छे लेखक हैं, लेकिन संवेदना और सहानुभूति को इस तरह खानों में न बांटिए।
लेकिन महिलाओं और दलितों के लिए बेसिक समया तो ये लोग खुद ही लेकर आए, बहस के केंद्र में या चिंताओं की गंभीरता में इनके मुद्दे इनके द्वारा ही लाए गए।
असल में दलित और स्त्री विमर्श अचानक इतने प्रबल हुए परंतु मुझे लगता है कि यह आवेग ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, क्योंकि साहित्य केवल हाय-हाय करते हुए फटी कमीज दिखाने भर से साहित्य नहीं होता। ‘फूलो का कुर्ता’ पढ़िए, तो फूलो नामक एक लड़की आपके सामने साक्षात् खड़ी हो जाती है, जो अपने पति को देखकर अपनी फ्रॉक अपने मुंह पर डाल लेती है। कहानी में दलित लड़की की पीड़ा, उसका भोलापन, लेखक ने मार्मिक ढंग से रखा है। किसी दलित लेखक की ऐसी कहानी बताइए, जिसमें ऐसी पीड़ा दर्ज हुई हो। हां, दलितवादी और नारीवादी हाय-हाय करना अलग है। इसीलिए मैं मानती हूं कि केवल स्त्री और दलित लेखन अपने आप में अधूरी लड़ाई है।
परंतु मैं फिर कहूंगा कि पीड़ा के उस गहरे स्तर तक सिर्फ और सिर्फ दलित या स्त्री ही जा सकते हैं।
यह ठीक है, लेकिन क्या आप उसे व्यक्त करने का शउर है, एक साहित्यिक तैयारी होती है, अभिव्यक्ति के लिए। हमेशा चित्कार और उच्छवास ही लेखन नहीं है, ऐसा होगा तो लेखन आंचल में दूध और आंखों में पानी वाला रह जाएगा।लेखकों को दलित और सवर्ण खेमें में बांटना एक राजनीति है। इसे वोट बैंक के लिए ही रहने दिया जाए। लेखन में उत्कृष्टता देखी जाती है, देखा यह जाता है कि रचना कितने साल तक जीवित रहेगी। कुछ कहानियां बड़ी भीषण और लाउड होती हैं, मल-मूत्र मार्ग की कहानियां, ऐसी रचनाएं आपने पढ़ी और पखाने में सिर से पैर तक नहा गए। लेकिन साहित्यिक मानदंडों पर ऐसी रचनाएं क्या आपको संतुष्ट करती हैं? आप उसे कृति कहेंगे या विकृति कहेंगे।
मगर ये मानदंड बनाए किसने? मानदंडों में हस्तक्षेप की जरूरत है, जैसे स्त्रियों ने हस्तक्षेप किया है या फिर दलितों या ब्लैक का भी हस्तक्षेप हुआ है। जैसे सौंदर्यबोध का मसला।
देखिए, लिखने के बाद समग्र साहित्य की धारा के बीच मूल्यांकित होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप महिला लेखन के अंतर्गत दस सतही लेखिकाओं को शामिल करें, सिर्फ वे इसलिए कि स्त्रियां हैं। मेरी कहानियों को ज्ञानरंजन, काशीनाथ सिंह, रवीन्द्र कालिया की टक्कर में देखा जाए न कि मुझे महिला होने की रियायत दी जाए।
महिलाओं की लिखी रचनाओं को कोई खारिज करे या रियायत की दृष्टि से देखे यह अलग बात है लेकिन महिला लेखन की विशेषताओं का जो मामला है, उस लिहाज से तो महिला लेखन के लिए अलग मानदंड तो बनाने होंगे।
जाहिर है कि स्त्री संसार में मुझे जहां तक पासपोर्ट मिला है, आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं जो लिखूंगी वह अंतःप्रदेश की रचनाएं होंगी, लेकिन लिखने के बाद रचना साहित्यिक सामाजिक वस्तु हो जाती है। अब उसका मूल्यांकन समाज की मुख्यधारा में होगा। मेरी पीढ़ी से लेकर उदय प्रकाश, धीरेन्द्र अस्थाना, मनोज रूपड़ा की नवीनतम पीढ़ी तक, वहां कोई आरक्षण की बात नहीं।
थोड़ा हटकर एक सवाल, युवा लेखिकाओं में संभावना के स्तर पर आप किन्हें शामिल करना चाहेंगी?
संभावना तो बहुत है युवा लेखन में। ये लोग नए प्रयोग खूब कर रही हैं। नई लेखिकाओं में मधु कांकरिया, महुआ मांझी, अल्पना मिश्र, कविता, पंखुरी सिन्हा, अर्चना पेन्युली आदि लेखिकाएं मुझे संभावनाओं से भरी दिखती हैं।
 |
| जय कौशल |
मुद्दों के स्तर पर इनमें और अपनी पीढ़ी में क्या भिन्नताएं हैं?
बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। कविता की कहानियां पढ़ते हुए कई बार मुझे लगा कि ये मेरी ही कहानियां हैं क्योंकि उनमें वही पुरुष, अपने साथी को समझाने की आतुरता और चुहल नजर आती है। मधु कांकरिया समाज में असमानता, विसंगतियों की पड़ताल कर रही हैं। वह सोनागाछी तक में जाकर घूमती है। यह हम लोगों में साहस नहीं था, आज की लेखिकाएं काफी फील्ड वर्क कर रही हैं। साहित्य इनमें ऐसी अपेक्षाएं रखता है। मधु कांकरिया का बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पर लिखा गया उपन्यास ‘पत्ताखोर’ मुझे बहुत आकर्षित करता है, जो बाकायदा सुधार गृहों में जाकर लिखा गया है।
अश्लीलता का ठप्पा लगता है। जवाब में इनका कहना है कि हमने जैसा झेला वही लिखेंगे।
लेकिन उसमें भी फर्क होता है। एक तरफ मंटों की कहानी ‘खोल दो’ है, सामान्यतः यह कहानी अश्लील लगेगी। ‘तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूं’ तथाकथित अश्लील है। ‘झूठा-सच’ में कई प्रसंग बड़े नग्न किस्म के हैं, जबकि यशपाल ने जो हमें चेतावनी दी थी वह जेलों में ए.बी.सी. क्लास की तरह झेला जा रहा है, सवाल यह है कि लेखक के सामने असली मुद्दा क्या है? बलात्कृत स्त्री अपने बारे में लिख रही हो तो उसमें बलात्कार ही नहीं होगा, उसकी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, प्रतिशोध भी तो होंगे, जो आने चाहिए रचनाओं में। चित्रा मुद्गल की कहानी ‘प्रेमयोनि’ पढ़िए। ‘आवां’ स्त्री लेखन की एक सशक्त रचना मानी जानी चाहिए, उसमें भी अश्लील कहे जाने वाले प्रसंग हैं परंतु वे ही उपन्यास के मूल कथ्य नहीं हैं। मूल तो है संघर्ष धर्मिता।
जयकौशल त्रिपुरा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं. संपर्क: kaushal@gmail.com
आपका आर्थिक सहयोग स्त्रीकाल (प्रिंट, ऑनलाइन और यू ट्यूब) के सुचारू रूप से संचालन में मददगार होगा.