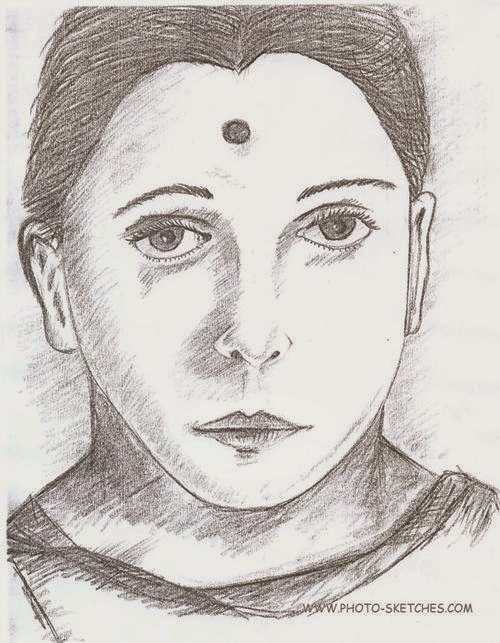अर्चना वर्मा प्रसिद्ध कथाकार और स्त्रीवादी विचारक हैं. संपर्क : जे-901, हाई-बर्ड, निहो स्कॉटिश गार्डेन, अहिंसा खण्ड-2, इन्दिरापुरम, ग़ाज़ियाबाद – 201014, इनसे इनके ई मेल आइ डी mamushu46@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है.
( ‘अन्या से अनन्या’ (प्रभा खेतान) ‘एक कहानी यह भी’ (मन्नू भण्डारी)
‘लगता नहीं है दिल मेरा’ (कृष्णा अग्नहोत्री) ‘जो कहा नहीं गया’ (कुसुम
अंसल)’हादसे’ (रमणिका गुप्ता) ‘कस्तूरी कुण्डल बसै’ (मैत्रेयी पुष्पा), तथा
अनुवादों में आँधेरे आलो (बेबी हालदार -बंगाली), ‘रसीदी टिकट’ (अमृता
प्रीतम-पंजाबी), ‘नंगे पाँवों का सफ़र’ (दिलीपकौर टिवाणा-पंजाबी),
‘खानाबदोश’ (अजीत कौर- पंजाबी), ‘कहती हूँ सुनो’ (हंसा वाडकर-मराठी)
‘स्मृतिचित्र’ (लक्ष्मी -मराठी) ‘नटी विनोदिनी’ (विनोदिनी–बंगाली), ‘आमार
जीबोन’ (राशुन्दरी देवी-बंगाली) आदि स्त्री – आत्मकथाओं के आलोक में
अर्चना वर्मा का यह आलेख महान पुरुषों’ की महानता ग्रंथि और उसके लिए
उन्हें प्राप्त सामाजिक -सांस्कृतिक सुविधा और समर्थन तथा स्त्री -आत्मकथाओ
के लिए सामाजिक -सांस्कृतिक अवरोध की व्याख्या करता है . दो किश्तों में प्रकाश्य आलेख की अंतिम किश्त . पहली किश्त पर क्लिक करें )
विचार के विकास के इतिहास में उत्तर
आधुनिक मोड़ पर आत्म और अस्मिता के विषय मेँ मान्यता है कि अस्मिता जन्मजात
नहीं, रचित होती है लेकिन जीवनकथा कोटि के साहित्य के विद्वानों ने उसके
सैद्धान्तीकरण में अस्मिता की भौतिक वास्तविकता पर बल दिया है – विशेषतः
नस्ल, सांस्कृतिक प्रजाति, वर्ग, लिंग और लैंगिकता के भौतिक नतीजों पर।
आत्मकथात्मक वृत्तान्त अपनी संस्कृति में उपलब्ध अस्मिता-कोटियों और
परम्परा-प्रसूत सांस्कृतिक वृत्तान्तों से प्रभावित होते हैँ। निजी प्रज्ञा
और व्यक्तिगत प्रयास/प्रतिरोध/आग्रह/संघर्ष/संकल्प से इस भौतिकता का
उल्लंघन, वैकल्पिक अस्मिता की रचना संभव होती है लेकिन नस्ल, सांस्कृतिक
प्रजाति, वर्ग, लिंग और लैंगिकता जैसी कोटियों से इतना तो तय हो ही जाता है
कि किस प्रकार के नियामक या दमनशील विमर्शों के विरुद्ध यह
प्रयास/प्रतिरोध/आग्रह/संघर्ष/संकल्प सक्रिय होगा और न केवल यह कि वह कैसा
रूप ग्रहण करेगा बल्कि शायद यह भी कि उससे जन्म लेने वाली वैकल्पिक अस्मिता
का रूप क्या होगा।
इन भौतिक वास्तविकताओं पर नज़र रखते हुए
आत्मकथाओं में व्यक्त स्त्री-आत्म तथा पुरुष-आत्म के अन्तर को देखा गया है।
पितृसत्ता में पुरुषों को सीमाओं के भीतर अपनी अस्मिता की उपलब्धि के लिये
संघर्ष की इजाज़त है, जबकि स्त्रियों पर उनकी अस्मिता लाद दी गयी है। पुरुष
के पास अवसर है कि जो उसको बनना है, बने जबकि स्त्री को बता दिया गया है
कि वह क्या है। जिन रिश्तोंी के ताने बाने मेँ वह जीवित हैं, उसके
विन्यासों के भीतर ही उसे अपनी निजता ओर वैयक्तिकता को उपलब्ध और अभिव्यक्त
करना है। ऐसा कोई नियम तो नहीं लेकिन अधिकांशतः एक
निश्शंक/निर्द्वन्द्व/आत्मकेन्द्रित/समंजित/समन्वित/एकीकृत अस्मिता की
अभिव्यक्ति पुरुष की आत्मकथा का लक्षण है और सम्बन्धों के ताने-बाने में
बँटे हुए आत्म का निरूपण स्त्री की आत्मकथा का। सम्बन्धजाल के भीतर
आत्म-निरुपण स्त्री की आत्मकथा की शैली का लक्षण है। न केवल सर्जनात्मक चयन
बल्कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरत के द्वारा भी स्त्री अपनी जीवनकथाओं को
आत्म की रचना या तलाश के वृत्तान्त की तरह नहीं देखतीं, ‘ऐसा हुआ’ के
वृत्तान्त की तरह दर्ज करके रह जाती है।
अपने ‘आत्म’ की अनुभूति स्त्री को
आबद्ध-स्वयं या सम्बद्ध-स्वयं की तरह उपलब्ध होती है। आबद्ध-स्वयं अपनी
विवशताओं का बन्दी है। सम्बद्ध-स्वयं में सम्बन्धों का दबाव तो है किन्तु
स्वेच्छा और परस्परता की भावना के साथ।विच्छिन्न/ अलगावपूर्ण/
स्वयंपर्याप्त/ अहम्-केन्द्रित आत्म इसका विलोम है।
आत्मानुभूति/आत्मज्ञान/आत्मोपलब्धि की ये दो शैलियाँ हैं। पुनः, ऐसा कोई
नियम नहीं कि ज्ञान के ये दो प्रकार अनिवार्यतः दोनो प्रकारों की लैंगिक
अस्मिताओं अलग अलग जुड़े हुए हों लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि
विच्छिन्न/ अलगावपूर्ण/ आत्मकेन्द्रित/एकोन्मुख/अहंप्रधान ज्ञान की
सार्वजनिक भाषा पुरुष के आत्मवृत्तान्त में अधिक पाई जाती है। वह श्रोता को
संगी की अपेक्षा शत्रु के रूप में कल्पित करती है और चुनौती की आवाज़ में
बोलती है। जैसे रूसो के ‘कन्फ़ेशन्स’ में – “एकत्र हों मेरे चारो ओर मेरे
अनगिनत साथी और सुनें मेरी आत्मस्वीकृति – मेरी अयोग्यताओं पर सिर धुनें और
मेरी अपूर्णताओं पर शरमाएँ।और फिर उनमें से हर एक स्पष्टता के साथ,
सिंहासन के चरणों में अपने हृदय के रहस्य का उद्घाटन करे और यदि साहस हो तो
कहे कि मैँ इस आदमी से अच्छा हूँ।”
स्त्री के आत्मवृत्तान्त की भाषा इससे अलग
सार्वजनिक भाषा के औपचारिक विन्यास और व्यक्तिगत भाषा के बीच एक निरन्तरता
बनाए रखने वाली अनुरोध की भाषा है।स्त्री के ‘आत्मज्ञान’ का विकास जिन
विभिन्न सरणियों से होकर गुजरता है उनमें पहली भाषापूर्व मौन अबोधता की है
जहाँ से शुरू करके वह समाज के नियामक विमर्शों और संस्कारों द्वारा प्रदत्त
ज्ञान तक, प्रदत्त ज्ञान से अनुभव द्वारा संचित और ग्रहीत ज्ञान तक, दोनो
के सामंजस्य/असमंजसता/समन्विति/टकराहट से रचित आत्मज्ञान तक, आत्मज्ञान से
उन रीतियों और प्रथाओं के ज्ञान तक पहुँचती है जिनसे सामाजिक स्वीकृति
मिलेगी। यह अन्तिम परिणति अनेक आवाज़ों का समुच्चय कही जा सकती है जो अन्ततः
समन्वित होकर उसकी अपनी ज्ञान-गढ़न्त बनती है।उसकी अपनी ज्ञान-गढ़न्त का
अर्थ प्रदत्त-ग्रहीत-अनुभूत ज्ञान की ऐसी निष्पत्ति जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय
सम्बद्ध हो जाते हैँ। यह निष्पत्ति केवल कोई घरेलू आवाज़ मात्र नहीं,
सार्वजनिक विमर्श का विषय है लेकिन उसमें भी वह परिस्थितिजन्य हितों और
व्यक्तियों के–तथाकथित व्यक्तिगत मामलों के–सन्दर्भों को ध्यान में रखते
हुए ही संप्रेषण पर बल देती है। व्यक्तिगत और राजनीतिक का समन्वय(‘पर्सनल
इज़ पोलिटिकल’) या ‘भिन्नताओं का समारोह’ (सेलीब्रेशन ऑफ़ डाइवर्सिटीज़) जैसी
निष्पत्तियाँ इसी स्वभाव का नतीजा हैं। ‘सम्बद्ध’ आत्म की इस ज्ञानगढन्त
में परस्परता की आकांक्षा मौजूद होती है। वह अमूर्त/ सैद्धान्तिक/ तटस्थ/
सार्वभौम चौखटा-स्वरूप निष्पत्ति नहीं है। इसीलिये उनकी आत्मकथाओं के
विन्यास गैरपरम्परागत और विविध हुआ करते हैं और विधागत कानूनों या आधिकारिक
अहम् के मर्दाने प्रत्ययों में आसानी से दाखिल नहीं होते।
लैंगिकताद्वय द्वन्द्वात्मक विभक्ति की अन्तिम
ओर स्थायी कोटि नहीं है, अन्य अनेक वैकल्पिक लैंगिकताएँ संभव हैँ, यह
मानते हुए भी देखा जा सकता है आत्म व अहम् की एक स्त्री-कोटि है जिसमें
प्रवृत्ति/रुचि/रुख/रुझान के अनुसार पुरुष भी शामिल हो सकते हैं और दूसरी
पुरुषकोटि है जिसमेँ ठीक उन्हीं कारणों से स्त्रियाँ भी शामिल हो सकती हैं।
पुरुषकोटि की आत्मकथाओं में अपनी स्वयंता की एकान्विति और समन्वय को बढ़ावा
और उसकी दिशा मेँ विकास का उद्यम होता है जबकि स्त्री की आत्मकथाओं का
सामान्य निष्कर्ष स्वयं को पाने की तलाश का नतीजा स्वयं को खो देना यानी कि
अपने आपे के बाहर कहीं पाना है। स्त्री के लिये इससे अलग और अलावा अपने
आपे की तलाश में निकलना वस्तुतः असंभव की तलाश में निकलना है। अपने आबद्ध
या सम्बद्ध-स्वयं के सहज भाव-क्षेत्र में रहते हुए एकान्वित अहं की तलाश का
अर्थ शब्दशः पागलपन की तरफ़ जाने वाली आत्मकथा हो सकता है। हिन्दी की अबतक
उपलब्ध आत्मकथाओं मेँ चाहे नहीं, लेकिन दुनिया की बहुत सी भाषाओं में
स्त्री की आत्मकथा का अधिकांश पागलपन तक जाने की कहानी भी है लेकिन बहुत
बार इस पागलपन का कारण एकान्वित अहं की तलाश नहीं बल्कि उत्पीड़न की हदों के
बर्दाश्ते-बाहर हो जाने का नतीजा है।
स्त्री की आत्मकथा वस्तुतः
कथाबहुल, अस्मिताबहुल संभावनाओं के लपेटे में रचित ऐसा आत्मबिम्ब है जिसमें
प्रत्येक कथा, या कथा का प्रत्येक खण्ड उसके ‘स्वयं’ को ही प्रतिबिम्बित
करता है लेकिन ये सब की सब कहानियाँ आंशिक और अस्थायी हैं। स्वयं के किसी
एक श्रेणी – पत्नी, माँ, बहन, बेटी, दासी आदि– तक सीमित रह जाने से इंकार
करने वाली ये भूमिकाबहुल कहानियाँ विखण्डन और अनिश्च्य से शुरू और उसी मेँ
ख़त्म होती हैँ। प्रायः एकरैखिक, कालानुक्रमिक, वैयक्तिक, विगत के अनुभवों
के संचित पुंज और पहले से मौजूद किसी ऐसे एकान्वित स्वयं की उपलब्धि तक
नहीं जातीं जिसे उद्घाटित भर करना है और जो प्रायः आत्मकथा लेखन का
परम्परागत अनुकरणीय आदर्श है।
‘अन्या से अनन्या’ (प्रभा खेतान), ‘एक कहानी यह भी (मन्नू
भण्डारी) की ‘तद्भव’ मेँ प्रकाशित अपनी समीक्षा में अभय कुमार दूबे ने
दर्ज किया था कि वास्तव में ये स्त्री के आत्म-सशक्तीकरण
(self-empowerment) की कहानियाँ हैँ लेकिन इनकी लेखिकाओं में स्वयं इस बात
की पहचान नहीं है। यह टिप्पणी वास्तव में स्त्री के सम्बद्ध-स्वयं की
संरचना से पुरुष-आत्म के अपरिचय का नतीजा है। इन कहानियों मेँ अंकित मुक्ति
वस्तुतः उत्पीड़न और यंत्रणा के तात्कालिक संदर्भ से मुक्ति तथा विखण्डित
आत्म के साथ सामंजस्य और समायोजन की, संघात से उबरने की कहानियाँ हैं, उनके
साथ संबद्धता से मुक्ति की नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता, आत्म-निर्भरता,
आत्म-निर्णय की क्षमता इत्यादि स्त्री के आत्म-सशक्तीकरण के महज़ आंशिक
उपकरण हैं, उसके ‘स्वयं’ की सम्पूर्णता का पर्याय नहीं।
आत्मकथा का औचित्य क्या है? किसी की निजी
ज़िन्दग़ी के स्याह-सफ़ेद मेँ ताकाझाँकी के पाठकीय कौतूहल और दिलचस्पी को
तृप्त करने के मनोरंजन-मसाले के अलावा भी आत्मकथा कुछ सामाजिक, नैतिक,
राजनैतिक, उपचारगत कार्य संपन्न करती है।अस्मिता और अनुभव की गढ़न्त सामाजिक
तौर पर होती है और ऐतिहासिक सांस्कृतिक सन्दर्भों के भीतर दैनिक जीवन तथा
वैयक्तिक अस्मिता में ढल जाती है। आत्मकथा का औचित्य उसके
लेखक-प्रवक्ता-चरित्र के आत्मचिन्तन/अन्तर्दर्शन/आत्मान्वेषण/अन्तरीक्षण की
अभिव्यक्ति में है।आत्मकथा का लेखक सदैव खुद को एक नैतिक औचित्य की सीमाओं
में रखता है और प्रवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्त करता है, चरित्र ने भले
ही उन सीमाओं का उल्लंघन करते हुए ही अपनी जीवनकथा को गढ़ा हो। चूँकि
लेखक-प्रवक्ता-चरित्र तीनो एक ही हैं, लेकिन रचना की प्रक्रिया के स्तर पर
अभिन्न नहीं हैं अतः प्रवक्ताप्रवक्ता ‘चरित्र के आचरण का ‘साक्षी’ है और
लेखक उसका ‘निर्णायक’ और न्यायाधीश। लेकिन यह निर्णय और न्याय चरित्र के
विपक्ष में नहीं, उसके आचरण के नैतिक औचित्य का उद्घा टन करने के लिये है।
अपने किये-धरे लेखा-जोखा, सामाजिक अनौचित्य का हिसाब और पाठक के समक्ष अपने
कर्मों की सफ़ाई आत्मकथा को उसका कारण देती है।
लिंग/लैंगिकता/कामभावना के सिलसिले में समाज
के नैतिक पाखण्डों का पूरा बोझा स्त्री की कमज़ोर पीठ पर है।समाज के नियामक
विमर्शों की जकड़ का दमघोट दबाव उसके अस्तित्व की नाप से कहीं अधिक छोटा है
और उसे साँस लेने भर की जगह भी नहीं देता।उसकी
भूमिकाओं/दायित्त्वों/कर्त्तव्यों/कसौटियों का फैलाव उसकी सकत और सामर्थ्य
से बहुत अधिक बड़ा है। वह सामाजिक नैतिकता का पर्याय बन चुका है। उसका
दारोमदार सदियों से स्त्री की चुप्पी और स्वीकार पर टिका रहता आया है।
स्त्री-विमर्श के दायरे में प्रतिरोध के हथियार की तरह स्त्री की आत्मकथा
इस चुप्पी को तोड़ने और इस दोमुँहे नैतिक पाखण्ड को पलीता लगाने का काम करती
है। अन्याय और उत्पीड़न की तथाकथित नैतिक कसौटियों पर अनैतिक साबित होना
प्रतिरोध की राजनीति मेँ कहीं अधिक नैतिक हो सकता है। नैतिक प्रतिरोध की
तरह अनैतिक का चुनाव, और चुनाव से भी बढ़कर उसका बयान सामाजिक असहिष्णुता,
तिरस्कार से लेकर सार्वजनिक चीरहरण, दाग, दाह, संगसार, फाँसी जैसे
विधिसम्मत दण्ड का भागी होता है लेकिन तथाकथित समाजसम्मत सही रास्ते पर लगे
रहने की असफलता, अपने अनुभव के प्रकाश में नियामक विमर्शों की कसौटियों का
मूल्यांकन और विचलन का औचित्य इस ध्वंस को एक पवित्रता दे देता है।
सम्वेद से साभार