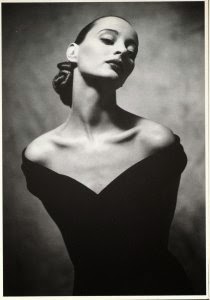हाल के दिनों में प्रकाशित ‘ दलाल की बीबी’ उपन्यास के रचनाकार रवि बुले पेशे से पत्रकार हैं. संपर्क : 09594972277
हाल के दिनों में प्रकाशित ‘ दलाल की बीबी’ उपन्यास के रचनाकार रवि बुले पेशे से पत्रकार हैं. संपर्क : 09594972277
( प्रज्ञा पांडे के अतिथि सम्पादन में हिन्दी की पत्रिका ‘ निकट ‘ ने स्त्री -शुचितावाद और विवाह की व्यवस्था पर एक परिचर्चा आयोजित की है . निकट से साभार हम उस परिचर्चा को क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं , आज साहित्यकार एवं मीडियाकर्मी रवि बुले के जवाब इस परिचर्चा के अन्य विचार पढ़ने के लिए क्लिक करें : )
जो वैध व कानूनी है वह पुरुष का है : अरविंद जैन
वह हमेशा रहस्यमयी आख्यायित की गयी : प्रज्ञा पांडे
अमानवीय और क्रूर प्रथायें स्त्री को अशक्त और गुलाम बनाने की कवायद हैं : सुधा अरोडा
अपराधबोध और हीनभावना से रहित होना ही मेरी समझ में स्त्री की शुचिता है : राजेन्द्र राव
बकौल सिमोन द बोउआर स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। आपकी दृष्टि में स्त्राी का आदिम स्वरूप क्या है?
मनुष्यता के जैविक-ऐतिहासिक कालक्रम में पुरुष और स्त्राी दोनों ने विकास किया है। परंतु माना यही जाता है कि चूँकि स्त्री के पास प्रजनन की प्राकृतिक और समूह/समाज द्वारा दी गई पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थीं, इसलिए वह पुरुषों के मुकाबले भौतिक विकास की दौड़ में पिछड़ गई। उसका विकास पुरुष के मुकाबले कम हुआ/आँका गया। हम परिवारों के विकास पर अमूमन चर्चा नहीं करते। परिवारों के बनने और उनके बहाने सामाजिक/राष्ट्रीय विकास में स्त्री की भूमिका पर बात नहीं होती। विकास की अवधरणा चूँकि सामाजिकता, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता से जुड़ी है अतः यह सहज पुरुषों के विकास के जोड़ दी गई
स्त्री घर में थी, अतः उस पर ध्यान नहीं गया। बाहर पुरुष का आधिपत्य था, तो मान लिया गया कि घर और स्त्री पर भी उसका ही अधिकार है। स्त्री का सब कुछ पुरुष का है, स्त्री पुरुष की है। इस तरह स्त्री के उस चरित्र की नींव रख दी गई, जिसकी पुरुष और उसके बाहुबल से चलने वाला समाज अपेक्षा करता है। ऐसे में सिमोन का यह कथन सही साबित हुआ कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। बाहर ही नहीं, घर के लिए बने नियम कायदे उसके आचार-विचार को तराशते रहे हैं। प्राकृतिक रूप से स्त्री शारीरिक रूप से पुरुष से थोड़ी भिन्न है। मगर यह भिन्नता इतनी बड़ी बना दी गई कि कालक्रम में शरीर ही स्त्री की मुख्य पहचान बन गया। यह आज भी है। अतः पुरुष से इतर स्त्री केंद्रित हर किस्म के बाजार विकसित हुए। जिसने स्त्री को स्त्री बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। अब भी यह जारी है।
क्या दैहिक शुचिता की अवधरणा स्त्री के खिलापफ कोई साजिश है?
यह समाज के विकासक्रम में स्त्री -पुरुषों, वर्ण-धर्मों और जाति-वर्गों के लिए तय की गई तमाम अवधरणाओं में से एक है। मनुष्य समाज ने ऐसी कई साजिशें आपस में एक-दूसरे के लिए रची हैं। स्त्री की दैहिक शुचिता का संबंध् यौन प्रकरणों से है। प्रकृति का सारा कारोबार ही इसी यौनिकता से चल रहा है। पेड़-पौधे से लेकर पशु-पक्षी तक अपनी संतति के लिए निरंतर गतिवान हैं। इसमें एक साथी के साथ संबंधें की मजबूरी या बाध्यता कहीं नहीं है। मानव समाज ने देश-काल के अनुसार इस बारे में नियम बनाए, जो बदलते भी रहे। चूंकि स्त्री को पुरुष के मुकाबले कमजोर माना गया, ऐसे में पुरुष की इच्छा और बल को ही प्राथमिकता मिलती रही। दैहिक/यौनिक शुचिता स्त्री को घर में कैद रखने का एक खास बहाना रही, जिसने सदियों तक उसके विकास में सबसे बड़ी बाध का काम किया। स्त्री अपने पिता, भाई और पति की संपत्ति बनी रही। उसकी दैहिक शुचिता परिवार के पुरुष के मान-सम्मान का प्रतीक रही। विवाह में सदियों तक यह शुचिता सबसे ऊपर रही। हालांकि यह अब भी सबसे ऊपर मानी जाती है, परंतु आंशिक ही सही यह मान्यता नई पीढ़ी में खंडित हो रही है। इसी बीच सदियों तक स्वयं स्त्री को अपनी पवित्राता के प्रति सजग और जिम्मेदार बनाया जाता रहा है। माहवारी के दिनों में उसे घर की स्त्री ही एहसास दिलाती रही हैं कि वह अपवित्र है। ऐसा धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। हालाँकि अब ऐसी देह-शुचिता के मसले पर समाज में धीरे -धीरे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।
समाज के संदर्भ में शुचितावाद और वर्जनाओं को किस तरह परिभाषित किया जाए ?
शुचितावाद और वर्जनाएँ स्त्री के प्रति परिवार और समाज के व्यवहार को तय करती हैं। इसमें स्त्री के प्रति स्त्री का और स्त्री के प्रति पुरुष का व्यवहार शामिल है। वक्त के साथ इनमें सेंध् लग चुकी है। खास तौर पर टेलीविजन के विस्तार ने इसमें परिवर्तन लाना शुरू किया है। उसने लोगों को जागरूक बनाया है। अब गाँवों में भी यह संदेश पहुँचने लगा है कि बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। ऐसे में शुचिता की अवधरणाएँ और वर्जनाओं में ढील आने लगी है। हालाँकि इनसे पूरी तरह मुक्त होने में वक्त लग सकता है।
यदि स्वयं के लिए वर्जनाओं का निर्धरण स्वयं स्त्री करे तो क्या हो ?
स्त्री क्यों अपने लिए वर्जनाएँ स्वीकार करे और किसके लिए करे? इन वर्जनाओं की शुरुआत संभवतः इस बात को लेकर है कि उसके पास प्रजनन की जिम्मेदारी है। यह प्राकृतिक तथ्य है कि नर अपनी संतति को आगे बढ़ाता रहना चाहता है। इसके लिए वह ज्यादा से ज्यादा मौके और गर्भ तलाशता है। सदियों तक स्त्री के गर्भ पर भी पुरुष का अधिकार रहा है। लेकिन अब आधी सदी से ज्यादा हो चुका है जब गर्भनिरोधकों के आविष्कार के साथ स्त्री अनिच्छा से गर्भाधरण की लड़ाई जीत चुकी है। वैसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि तमाम सर्वे बताते हैं, अधिकांश पुरुष अपने इस्तेमाल के लिए बने गर्भनिरोधक (कंडोम ) का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। अतः आज भी गर्भनिरोधक के प्रयोग कि जिम्मेदारी ज्यादातर स्त्री को ही उठानी पड़ती है। वैसे विज्ञान की तरक्की के नजरिये से देखें तो आने वाले कुछ दशकों में स्त्री अपने गर्भ से भी आजाद हो सकती है। फिलहाल इतना तो हो ही चुका है कि वैज्ञानिक एक तय समय सीमा तक गर्भ के अंडाणुओं को फ्रीज करके रख लें, जिन्हें पुनः स्त्री के गर्भ में स्थापित किया जा सकता है। आज यह खास तौर पर बेहद प्रतिभाशाली और बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदों पर काम करने वाली स्त्री के लिए बेहद मुफीद है। वे किसी भी उम्र में अपने बच्चे की माँ बन सकती हैं। सरोगेट मदर एक और राह है। हालाँकि ये नई बहसों के मुद्दे हैं कि इनसे स्त्री का जीवन कितना आसान होगा और कितना जटिल। वैसे विज्ञान इस बात की भी संभावना टटोलने में लगा है कि भविष्य में प्रजनन के लिए स्त्री को पुरुष की आवश्यकता ही न रहे। आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले कुछ दशकों में सचमुच यह हुआ। इसके बाद का समाज फिलहाल सिर्फ कल्पनाओं में हो सकता है।
विवाह की व्यवस्था में स्त्री की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ कितनी स्त्री के पक्ष में है ?
इस वक्त यह व्यवस्था बहुत ज्यादा स्त्री के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि जहाँ-जहाँ स्त्री अपने लिए निर्णायक संघर्ष करती है, वहाँ अधिकतर मामलों में विवाह टूट जाते हैं। इस वक्त समाज में कम से कम यह तो हुआ है कि विवाह टूटना अजूबा नहीं माना जाता और इसमें सिर्फ स्त्री को कठघरे में नहीं खड़ा किया जाता। मनोवैज्ञानिक रूप से परिवार की जिम्मेदारियाँ आज भी पूरी तरह से स्त्री पर हैं। टीवी पर आने वाले विज्ञापन में हम देखते हैं कि दफ्तर में जो स्त्री पति की बाॅस है वही घर में आकर खाना पकाती है। किचन परिवार के केंद्र में है और यह स्त्री की ही चिंता है। मनोवैज्ञानिक-सामाजिक रूप से भी विवाह स्त्री के लिए संसार में उसका अपना ‘घर’ होने की विधि है । करिअर में सफल होने के बाद भी उसकी अंतिम परिणती अपना परिवार, अपना घर, अपने बच्चे ही है। आर्थिक मोर्चे पर स्त्री जरूर पहले के मुकाबले कुछ राहत की स्थिति में है। परंतु जहाँ परिवार की जिम्मेदारी कमोबेश उसके कंधें पर है, वहाँ आर्थिक राहत ही उसके लिए बोझ बन जाती है। आर्थित जरूरतों को पूरी करने का ध्न के अलावा और कोई विकल्प किसी के पास नहीं है।
मातृसत्तात्मक व्यवस्था में विवाह संस्था क्या अधिक सुदृढ़ और समर्थ होती। तब समाज भ्रूण हत्या, दहेज, हत्या एवं बलात्कार जैसे अपराधें से कितना मुक्त होता?
पारंपरिक अवधरणा के रूप में विवाह की संस्था आज भी सुदृढ़ और समर्थ है। परिवार टूटे, यह न स्त्री चाहती है और न पुरुष। बात सिर्फ इस संस्था में स्त्री के साथ समानधर्म व्यवहार की है। समय के साथ हो रहे सामाजिक बदलावों को स्वीकारने और उन्हें अनुकूल ढंग से जीवन में स्थान देने की है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था में निःसंदेह अपराध आज के मुकाबले काफी कम होते।
सह जीवन की अवधरणा क्या स्त्री के पक्ष में दिखाई देती है?
दिखती तो है, मगर सह-जीवन अगर वैवाहिक जीवन के जैसा है तो स्त्री पुरुष के लिए वह विशिष्ट कैसे हो सकता है। वही उम्मीदें, वही अपेक्षाएँ, वही चक्र। सिर्फ एक सुविधा कि जिस पल किसी को और साथी पसंद आ जाएगा या आगे साथ जीवनयापन की इच्छा नहीं होगी तो सह-जीवन से जाने की स्वतंत्राता है! फिर सवाल कि यह स्वतंत्रता रास न आई तब? मनुष्य सिर्फ समाज में ही जीवन नहीं जीता, वह अपने मन-मस्तिष्क में भी जीता है।
साथ होकर भी पुरुष एवं स्त्री की स्वतंत्रापरिधि है?
साथ होकर दोनों ही स्वतंत्र नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि एक-दूसरे को अधिक समझें। एक-दूसरे के पूरक बनें।