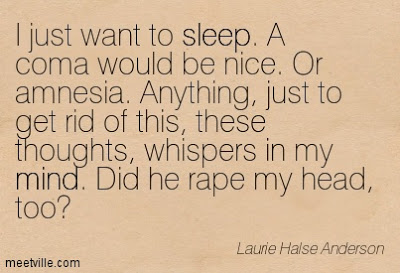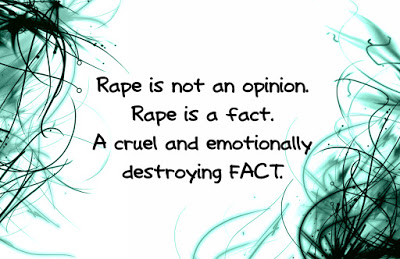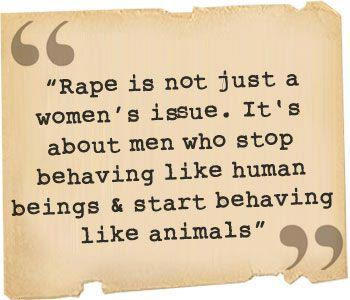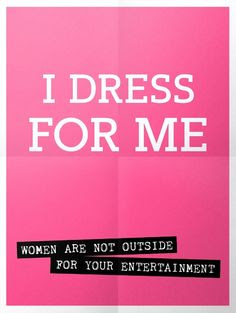रोहिणी अग्रवाल स्त्रीवादी आलोचक हैं , महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं . ई मेल- rohini1959@gmail.com
रोहिणी अग्रवाल स्त्रीवादी आलोचक हैं , महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं . ई मेल- rohini1959@gmail.com
देह के द्वार पर अनादृत स्त्रियां और हिंदी कथा साहित्य: दूसरी क़िस्त
( रोहिणी अग्रवाल का शोध -आलेख . हिन्दी साहित्य में ‘ बलात्कृत स्त्री की पीड़ा ‘ की अभिव्यक्ति का उन्होंने ‘ स्त्रीवादी’ पाठ किया है . )
पहली क़िस्त के लिए क्लिक करें : देह के द्वार पर अनादृत स्त्रियां और हिंदी कथा साहित्य: पहली क़िस्त
बलात्कार सम्बन्धी स्त्री लेखन को विश्लेषित करते हुए दो अवस्थायें लक्षित की जा सकती हैं। पहली अवस्था में पीड़िता के मानसिक आघातजन्य अनुभवों को केन्द्र में रख कर परिवार तथा समाज के साथ उत्तरोत्तर असामान्य होते चलते सम्बन्धों का आकलन करते हुए स्थिति के उस विद्रूप को विशेष रूप से उभारा गया है, जहाँ निरपराध पीड़िता मानसिक-भावनात्मक सम्बल पाने की बजाय कलंकिनी एवं अपराधिनी के रूप में सामाजिक दंड विधान की क्रूरता झेलने को बाध्य होती है। यह स्थिति अपनी सूक्ष्म व्यंजना में शब्दों से परे अहसास के स्तर पर एक सवाल भी उठाती है कि असल बलात्कारी कौन है – पुरुष विशेष या उसे अभयदान देता समाज? उल्लेखनीय है कि पहली अवस्था की इन रचनाओं में बलात्कारी जितना अमूर्त और अशरीरी है, दूसरी अवस्था की रचनाओं में विकृति का पुंजीभूत रूप बन कर वह उतना ही तिरस्कृत और विश्लेषित हुआ है। विशेष रूप से दसवें दशक में पनपी दूसरी अवस्था का लेखन आंसू और हाहाकार से भरसक पल्ला छुड़ाते हुए समस्या के सामाजिक-सांस्कृतिक-मनोवैज्ञानिक-राजनीतिक कारणों के तटस्थ विश्लेषण में अधिक रमा है। जाहिर है जाने-अनजाने उस पर ब्राउन और जोन्स की उन पूर्वोक्त मांगों का प्रभाव पड़ा है जो किसी भी मानवीय समस्या को अद्भुत युद्ध-कौशल के साथ निपटाने और अपनी परिधि का विस्तार करने की ललक को अपने होने की पहली शर्त मानती हैं। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि उपन्यास की अपेक्षा कहानी के संक्षिप्त कलेवर में लेखिकाओं ने अपनी-अपनी तरह से समस्या का सांगोपांग चित्रण करते हुए इसकी विभीषिका को पैने ढंग से उजागर करने का प्रयास किया है, हालांकि यह तथ्य भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बलात्कार को पहली बार ‘सूरजमुखी अंधेरे के’ उपन्यास में एक सम्पूर्ण समस्या (घटना/स्थिति नहीं) का दर्जा देकर विस्तृत फलक पर विश्लेषित किया गया था।
गौरतलब है कि जिस ठंडे सुलझे ढंग से रत्ती की मनोग्रंथियों को खोलते हुए उसकी पीड़ा भरी चीत्कारों के आवेग को कृष्णा सोबती ने गहन-गझिन जिजीविषा के बिंदु पर बांध लिया है, वह परवर्ती स्त्री लेखन में प्रायः आंसुओं की उफनती नदी में घिर कर आक्रोश और आत्मदया में घिर गया है। बेशक इस तथ्य को रेखांकित करना भी उतना ही जरूरी है कि आक्रोश और आत्मदया ने उन्हें व्यवस्था से लड़ने और आत्मबल संचित करने में भरपूर ताकत भी दी है। ‘कठगुलाब’ की स्मिता, ‘इदन्नमम’ की मंदा और ‘छिन्नमस्ता’ की प्रिया को एक कोष्ठक में रखते हुए भी उन भिन्नताओं की ओर संकेत करना अनुचित न होगा जो बड़े भाई के यौन अतिचार की शिकार प्रिया (छिन्नमस्ता) के बचपन को रौंद कर उसे असुरक्षा एवं अकेलेपन से धीरज और सामर्थ्य जुटाने की प्रेरणा देती हैं, जीजा के पाशविक बलात्कार से अनेक मनोग्रंथियों की शिकार स्मिता (कठगुलाब) को पलायन और हताशा की निरर्थकता से गुजार कर जीवन से सीधे जुड़ने का बल देती हैं तो परित्यक्ता कुसुमा भाभी की परिपक्व सोच सही एवं सामयिक नसीहत के माध्यम से बिरगवां गांव के कैलाश मास्टर के बलात्कार से क्षत-विक्षत बालिका मंदा (इदन्नमम) को दूरगामी मानसिक-सामाजिक परिणामों के बारे मेें सोचने का अवकाश ही नहीं देती – ”इतनी बड़ी ज़िंदगी में अच्छा-बुरा घट जाता है बिटिया, उसके कारन मन में गांठ लगाने से क्या फायदा। जो तुमने किया ही नहीं, उसके लिए अपने को दोसी क्यों मानना? . . .अरे, उसकी जात हुई मैली जो हम पर धोखे से करती है हमला। . . .अपनी जिंदगानी के सही-गलत का निरनय तो हमें ही लेना हे बिन्नू। काट फेंको जीवन से इस कुघड़ी को। तुम अच्छत हो मंदा।”(इदन्नमम,पृ0 94-95) शायद यही वजह है कि अवचेतन में पड़ी खरोंच और ग्रंथि में उलझने की बजाय मंदा एक नई ताज़गी-स्फूर्ति-मिशन के साथ ज़िंदगी को चुनौती के रूप में लेती है, जिसके बारे में आन गांव में प्रसिद्ध है कि ”किसी भी लरका-बिटिया के संग जोर-जुलम नहीं होने देगी मंदा।” (वही, पृ0 333)
बलात्कार के साथ जुड़ा सामाजिक कलंक का भाव सीधे-सीधे यौन शुचिता की उस परंपरापोषित मान्यता का परिणाम है जो पुरुष/कबीले/समाज/धर्म/जाति को अचल जमीन और पशु संपदा की तरह स्त्री को हस्तगत करने का अलिखित अधिकार देेता है। इसलिए शत्रु को नीचा दिखाने के लिए उसकी चल-अचल सम्पत्ति छीनने की तरह उस समुदाय की स्त्री पर बलात्कार को महज एक रणनीति की तरह देखने का चलन रहा है। अपने अधिकारों के लिए सिर उठाते दलितों को मज़ा चखाने के लिए सवर्णों द्वारा दलित स्त्रियों से बलात्कार की वारदात हो या पाकिस्तान में ‘ऑनर किलिंग’ की बढ़ती संख्या, देह की कीमत पर स्त्री को पुरुष/जाति/धर्म की आपसी रंजिशों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ‘नष्ट लड़की नष्ट गद्य’ में ‘फायर गर्ल’ तसलीमा नसरीन का वक्तव्य कि ”चरित्र की कालिमा पुरुष तो चार इंच के कपड़े से ही पोंछ सकता है . . . और स्त्रियों के चरित्र की कालिमा बारह हाथ के कपड़े से ढंक कर भी नहीं छिपाई जा सकती”(पृ0 127) स्थिति के विद्रूप को नहीं उभारता, बल्कि समाज की जड़ सोच पर कुठाराघात करता है। ”लड़की की इज्ज्त तो कांच होती है . . . बाल बराबर तरेड़ पड़ी कि . . .” – सच घिनौना नहीं होता, सच को किसी एक खास दिशा में सर्जित और मजबूत करने वाली परिस्थितियां घिनौनी होती हैं जिनमें जरा सी खरोंच लगते ही हाहाकार करते आम आदमी की पुरजोर सहमति और सक्रियता ज्यादा मुखर होती है। व्यवहार और सिद्धांत – निरंतर दो स्तरों पर जीता है व्यक्ति, अपने आप से अपने को ‘डस’ सकने वाले सच से छिपाते हुए। इसी दुराव-छिपाव के बीच वर्जना बन कर आतंक पैदा करने की ताकत पाती हैं कमजोरियां और खोखली होती चलती हैं मूल्यधर्मी अंदरूनी ताकतें। कांच के साथ लड़की की इज्जत के मिथक को केन्द्र में रख कर लवलीन ‘सुरंग पार की रोशनी’ कहानी में आसन्न बलात्कार के भय से खौफजदा स्त्री की मनोव्यथा प्रस्तुत नहीं करतीं, बल्कि उन कड़वी प्रतीतियों को ठोस रूप में उभारती हैं, जहाँ स्वतंत्र व्यक्तित्व सम्पन्न बुद्धिजीवी-समाजसेवी निर्भीक स्त्री स्वयं को ‘मादा’ समझने के अपमानजनक अनुभव से गुज़रने को बाध्य होती है। ”यही मेरी सार्वजनिक पहचान थी। मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा से अलग महज एक शरीर – शरीर भी नहीं, महज एक सूराख।” स्थिति तब और भयावह होती है जब बुद्धि, चेतना और संगठन के बल पर स्वयं को ‘विशिष्ट’ समझने का दंभ पालने वाली यह स्त्री एक ओर अपने को भंवरीबाई की तरह ‘तख्ती और नारे में बदलते हुए देख रही थी’ तो दूसरी ओर ‘मूढ़’ स्त्रियों के प्रति किए गए विश्लेषण को अपने पर राई-रत्ती लागू होते देख शर्मसार – ”उन्हें अपनी अस्मिता (अस्मत नही) के लिए अड़ना और लड़ना नहीं आता क्योंकि समाज की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं है। स्त्री अपने आप में अपूर्ण घटक है, कमजोर निर्बल फिनामिना है। स्त्री समाज के दबाव और शोषण के विरुद्ध प्रतिकार और विरोध भी दर्ज नहीं करा पाती।” (वही, पृ0 75) जब अस्मिता की लड़ाई से कहीं बड़ी हो जाती है अस्मत को बचाने की हड़बड़ी और लुटी अस्मत को सौ-सौ तालों में छुपाने की चौकसी, तब शेष रहती है एक ही नसीहत – ”जहर का घूंट पी ले बेटी, तभी सबको जीवन दान मिलेगा” या मर्मांतक कटूक्तियां -”तू न मरी उन डेढ़ सौ सवारियों के साथ कुलच्छन।” बेशक इस पलायनवादी पारंपरिक दृष्टिकोण को धता बता कर नई पीढ़ी की नवयुवती अदालत का द्वार खटखटाने लगी है, लेकिन सुपरिचित आत्मीय सम्बन्धों में सेंध लगा कर घुस आती अपरिचित अनात्मीयता से मुक्ति नहीं पा सकी है। चित्रा मुद्गल ने ‘प्रेतयोनि’ तथा उर्मिला शिरीष ने ‘चीख’ कहानी में जिस मुखर भाव से पारिवारिक सदस्यों – मां, पिता, भाई, बहन – की अपने-अपने तईं अतिरिक्त चिंता, असहज सांत्वना, और सामाजिक कलंक की आशंका से अपने ही खोल में दुबक जाने की निर्मम सजगता को बलात्कृता किशोरी के इर्द-गिर्द बुना है, वे उसकी पीड़ा को ग्लानि, ग्लानि को अपराध बोध तथा अपराध बोध को जीवन के प्रति वितृष्णा तक ले जाने वाले क्रमिक मानसिक व्यूहों की रचना करते हैं।
बलात्कार केवल पुरुष का स्वछंद यौनाचार या प्रतिशोधपरक वासना का विकृत रूप नहीं, वरन् स्त्री और उसके पूरे परिवार को धुरीविहीन कर डालने वाला जलजला है जिसकी भयावह धमक सब कुछ शेष हो जाने के बाद भी सभी दिशाओं में देर तक प्रतिगुंजित रहती है। ”बस, इतना ही है स्त्री का चरम गोपन रहस्य – छलात्कार या बलात्कार’ – अर्चना वर्मा की ‘जोकर’ कहानी में अनायास एक ही छत के नीचे जुट आई तीन स्त्रियां हंस-हंस कर तीन निर्द्वंद्व-स्वछंद ज़िंदगियां जीती दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वे बेहतर जानती हैं कि ” यह हंसी रोने की बजाय हंस पड़ने के फैसले से निकली हुई हंसी है। इसलिए कमबख्त हर समय आती रहती है।”(हंस, अगस्त 1995, पृ0 44) कुशल फाइनेंस कंट्रोलर के रूप में प्राइवेट कम्पनी में कार्यरत चपला सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र में बलात्कार की शिकार होकर पुरुष मात्र से इस कदर भयभीत है कि साल छः महीने में एकाध बार घृणा, अपमान और आत्मधिक्कार के मर्मांतक दौर से गुजरने को बाध्य हो जाती है। पांच वर्ष की अवस्था में अपने ही चाचा की नियमित कामवासना का सुलभ पात्र बन जाने की मजबूरी ने विज्ञापन दुनिया की साम्राज्ञी सुपर मॉडल सुगंधा को ब्लैकमेलिंग के साथ-साथ देह को हथियार बना कर पुरुषों को नचाने की कला में माहिर अवश्य कर दिया है, लेकिन असल में ‘मातृका’ जैसी समाजसेवी संस्था से जुड़ कर प्रताड़ित स्त्रियों के जख्मों पर फाहा रखने के प्रयास में वह अपने भीतर की अंधेरी अरक्षित दुनिया के बीहड़ों को कम कर लेना चाहती है। और कथावाचिका मिसेज प्रतिभाकांत? भले ही ‘मातृका’ के संस्थापक और उत्साही समाजसेवी पति के सान्निध्य में पकी परिपक्व सोच के कारण सूनी दोपहरी की निर्जनता का लाभ उठा कर बलात्कार के असफल प्रयास में अपने पर ही लज्जित हो उठने वाले ”अधगंजे, अधबूढे . . ज़िंदगी से बेजार, कंकाला बीवी या दुष्टा बहू के सताए हुए से दीखते आदमी”(वही, पृ0 50) की किसी अनाम कुंठा पर ठठा कर हंस पड़ती है (और बाद में बलात्कार नहीं, ग्लानिजन्य हिंसा का शिकार बनती है), लेकिन यह घटना शशिकांत के भीतर छिपे ‘निखालिस’ पति को आहत करने को पर्याप्त है। पति – जिसके पास है अकूत वर्चस्व, वैधानिक स्वामित्व, क्षमा-संरक्षण का पुख्ता अधिकार। लेकिन इन सबसे बेखबर पत्नी इन्हें ले ही न, तो? बलात्कारी के कुंठित प्रयास पर हंस दे और ‘यूं ही आए गए’ भाव से घटना का बयान कर रोजमर्रा के जीवन में जुट जाए, तो? सच कहा है ‘स्त्रिश्चरित्रम् पुरुषस्य भाग्यम् देवो न जानाति कुतो मनुष्याः’। संदेह और वितृष्णा, हिंसा और आतंक – इन हथियारों से ही तो साधना पड़ेगा न उसे पत्नी को। ”उनके यूं टूट पड़ने, नोचने-खसोटने, पटकने से मुझे फिर उसी फोटोग्राफर की शक्ल दिखाई दी। मानो उनके लिए यही असली तृप्ति थी, यही हिंसा। इसके पहले जो हम नितांत निजी एकांत में देह और मन का एकाग्र संगीत रचा करते थे, वह दरअसल किसी असली चीज़ की फीकी, बेरंग धूमिल सी अनुकृति भर थी। . . . फिर मेरे लिए उसमें न कुछ निजी रहता, न एकांत। तब जो नहीं हुई थी अपनी देह से, वह घिन अब होने लगी। लाख नहाने पर भी न छूटती। फिर वही घिन शशिकांत से भी होने लगी। उनका देहांत मेरे लिए छुटकारे की सांस थी। उनके लिए भी। मतलब सांस नहीं, छुटकारा।” (वही, पृ0 51)
यहीं वह नरक है जो सम्बन्धों में छिपी सड़ांध को झेलने और जिलाए रखने को बाध्य करता है, भले ही बलात्कारी खुद पिता ही क्यों न हो और उस नर-पिशाच की दैहिक-भौतिक भूख की तृप्ति हेतु उसे वेश्यावृत्ति क्यों न करनी पड़े। समाजशास्त्रीय आंकड़े इस तथ्य की गहरी पुष्टि करते हैं कि बलात्कार की शिकार स्त्रियां वेश्यावृत्ति के लिए प्रवृत्त कर दी जाती हैं या आरोपी सम्बन्धी और परिवार की स्त्रियों की जुबान सी कर रखने की नसीहत तले एक बड़ा झूठ सलीब की तरह ढोने के लिए विवश कर दी जाती हैं। यहाँ दूर्वा सहाय की कहानी ‘जिरह’ विशेष रूप से उल्लेखनीय है जहाँ बलात्कार के आरोपी प्रभात की मां की मनोवेदना और मंथन को केन्द्र में रख कर लेखिका उसके अतीत को बलात्कृत बारह वर्षीया लड़की के वर्तमान के साथ जोड़ कर एक अनाम से सखीभाव का अंकुरण करती है। बलात्कारी बेटे की मां के रूप में उसकी पीड़ा को जिस प्रकार बलात्कार/यौन छेड़छाड़ से भरपूर बचपन की कंटीली स्मृतियां तार-तार कर फरियादी के निकट ला खड़ा करती हैं, वह सामाजिक न्याय के लिए गुहार लगाती स्त्री की अंतश्चेतना की पहली स्प्ष्ट एवं निर्भीक अभिव्यक्ति है। एक ऐसी मानवीय स्थिति जहाँ सम्बन्धों के दबाव और ‘इज्जत’ के छल तिरोहित होकर स्त्री की रौंदी गई मानवीय गरिमा को न्याय दिला सके।
स्त्री देह के साथ जुड़ी पुरुष जाति की ‘इज्जत’ ने अपना पता बदला हो या न हो, स्त्रियां अब इन छद्म आवरणों को उतार फेंकने को व्यग्र हैं। बेशक ”काश् ऐसा होता कि मस्तिष्क की कोई नस काट कर फेंक दी जाती ताकि हम बेजान हो जाते . . . क्यों नहीं मेरी स्मृतियों पर विक्षिप्तता छा जाती? मैं मर जाती” – उस चोट की मर्मांतक प्रतिध्वनियां हैं जिसके चिन्ह आत्मा की गहराइयों तक खुद गए हैं, लेकिन एक वक्त का हाहाकार पूरे जीवन का सत्य नहीं बन सकता। मनुष्य के मानस की जटिल संरचना में महीन तंतु की तरह लिपटी जिजीविषा ऐसी संजीवनी बूटी है जो सिर्फ रोग का उपचार नहीं करती, रोग के उन्मूलन में जुट जाती है। इसलिए अपने चारों ओर बुने जा रहे डर से उबर कर यह स्त्री पहले अपने आप से ही पूछ लेना चाहती है कि उसे ”देह को लेकर तड़पते रहना है या आत्मा की आवाज पर चलना है।”(वही, पृ0 143) यकीनन आत्मा की आवाज़ पर क्योंकि जिजीविषा और अंतरात्मा में जैसा सघन-आत्मीय संवाद होता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। ”उस भेड़िए को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, चाहे मेरी अपनी ज़िंदगी गर्क हो जाए।” परिवार की जानलेवा नफरत और बलात्कारी नरेश के प्रतिष्ठित-सम्पन्न माता-पिता की ओर से विवाह प्रस्ताव (मामले को रफा-दफा करने का प्रलोभन मात्र) – दोनों को समान निर्लिप्त संकल्पबद्धता से ठुकरा कर लम्बी अपमानित कर देने वाली अदालती कार्यवाही से गुज़र कर अपराधी को आठ साल का दंड दिला देने के बाद ही सहज हो पाती है कथावाचिका की फरियादी बहन। बेशक ‘इज्जत’ तो उसने खो दी है। खबर फैलते ही मंगनी टूटना, खामोश भाव से अपनी चरित्रहीनता की कल्पित कहानियां सुनना और पिता द्वारा सपरिवार ‘इज्जत’ बचाने के प्रयास में जमी जमाई घर-गृहस्थी-व्यापार उखाड़ कर दूसरे शहर में स्थानांतरित हो जाना – इज्जत के नाम पर पीड़िता का मनोबल तोड़ने के प्रयास तो हैं ही, साथ ही निर्दोष होते हुए भी अपराधी की नाईं ज़िंदगी गुजारने की घुट्टी भी। लेकिन कोई भी नई परिभाषा गढ़ने के लिए पुरानी कसौटियों और लकीरों को त्यागना तो होता है न! ”यहाँ जैसे चींटे हैं, मच्छर हैं, खटमल हैं, वैसे ही मर्द भी हैं। क्या जरूरी है कि शेर, भेड़िया, भालू ही कहो? उपमान ही तो हैं, बदल दो।” कसक से संकल्प में पर्यवसित होता स्त्री लेखन ‘बीइंग’ से ‘बिकमिंग’ तक की प्रत्यक्ष ऊर्ध्व यात्रा ही तो है, साथ ही समाज से अपनी मानवीय गरिमा छीन लेने की प्रत्यक्ष घोषणा भी।
‘विवाह का अर्थ है बलात्कार महोत्सव’
स्त्रीवाद के उग्रतर होते चलने के साथ ही विवाह संस्था को वेश्यावृत्ति तथा बलात्कार के साथ जोड़ने का चलन अकारण या जबरन नहीं है, रति सम्बन्धों में स्त्री को निष्क्रिय (पैसिव) पार्टनर मान उसकी योनिकता पर पुरुष अंकुश के सामंती दंभ का विरोध है। ”औरत की देह औरत का देश है” कह कर रघुवीर सहाय जैसे उदारवादी लेखक-विचारक स्त्री की मानवीय अस्मिता के संरक्षण को उसका मौलिक अधिकार मानते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कानून के मर्दवादी दृष्टिकोण के चलते क्या ऐसे ‘मौलिक अधिकार’ का ग्रासरूट तक संक्रमण संभव है? अरविंद जैन ‘औरत होने की सजा’ में पेच-दर-पेच जटिलताओं का पिरामिड खड़ा करते कानून की आंतरिक संरचना के अंतर्विरोधों और दुर्बलताओं (लूपहोल्स) को खोलते हुए बताते हैं कि जहाँ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 (6) के अनुसार किसी भी पुरुष द्वारा सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री की सहमति/असहमति से उसके साथ संभोग करना बलात्कार है, वहीं ”अपनी ही पत्नी जिसकी उम्र पंद्रह साल से कम न हो, के साथ सहवास करना बलात्कार नहीं है।” (वही, पृ0 55) विचित्र विडम्बना है कि यह वही कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को ‘बालविवाह’ का नाम देकर गैरकानूनी मानता है। दूसरे, ‘मनुष्य’ होने की तमाम संवेदनाओं से परे सहवास हेतु पत्नी की सहमति/असहमति जैसे सवाल पर विचार करने की जरूरत नहीं समझता। हालांकि हिंदी कथा लेखन में वैवाहिक बलात्कार की यंत्रणा झेलती स्त्री की मानसिक व्यथा का उद्घाटन अपेक्षाकृत कम हुआ है, किंतु मृदुला गर्ग ‘चितकोबरा’ उपन्यास तथा ‘तुक’ कहानी में स्त्री के अंतरंग को दो भिन्न दृष्टियों से प्रस्तुत करती हैं। व्यंग्य की नुकीली धार के साथ कथानायिका मीरा (तुक) के वक्तव्य के जरिए पहले वे ‘व्यवसाय’ के रूप में स्त्री का दैहिक-मानसिक, बौद्धिक-भावनात्मक शोषण करने वाली विवाह संस्था के बर्बर रूप को उद्घाटित करती हैं , फिर वेश्यावृत्ति और बलात्कार में अंतर्लीन होते इसके डगमगाते असंतुलित स्वरूप को। पति को लौकिक आकर्षणों (क्लब और ब्रिज के खेल) से दूर कर समग्रतः पाने के प्रयास में वह अनायास अपने को ‘वेश्या’ रूप में पाती है तो उसके मूड के अनुरूप (ब्रिज में हार और जीत) सहवास के नाम पर उग्रता और अनुकंपा को बलात्कार के रूप में। ”अपनी हार का मुआवजा वह मेरे बदन के सिवा वसूल करता भी कहाँ से? तभी मेरी समझ में आ गया कि उसके लिए ताश का खेल भी बैंक में नौकरी की तरह एक व्यवसाय है और मैं वह फुटकर कैश जिसका प्रयोग वह व्यवसाय में हुए नुकसान को भरने के लिए या लाभ पर खुशी मनाने के लिए करता है।” (तुक, पृ0 116) हालांकि पति के प्यार में डूबी स्त्री छवि के मिथक में बांध कर निरंतर अपराध बोध से अपने आपको निहारने वाली इस कथानायिका की नियति की ओर लेखिका ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं किया है, किंतु इस कहानी के पूरक पाठ के रूप में ‘वितृष्णा’ कहानी उन त्रासद परिणतियों की ओर अवश्य संकेत करती है जहाँ बलात्कार और वेश्यावृत्ति के बीच अपनी मानवीय इयत्ता खो डालने की संवेदनशून्यता से उपजी यांत्रिकता सम्बन्धों की रागात्मकता को लील चुकने के बाद सामाजिक संस्थाओं की उपयोगिता पर बड़ा सा सवाल खड़ा करती है।
दूसरी दृष्टि ‘चितकोबरा’ उपन्यास में स्त्री के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को देह और दिमाग दो खंडों में विखंडित कर देने के उद्योग में जुटी विवाह संस्था की चूलों पर कुठाराघात करती है जहाँ बार-बार किए जाने वाला बलात्कार आदत में शुमार होकर मनोभूमि को बेहद बंजर बना देता है। ”आज रात महेश मुझे प्यार करेगा” – चेतना के द्वार पर पत्नी-कर्त्तव्य की दस्तक और मनु का ‘आपरेशन से पहले मरीज की सफाई करती नर्स की तरह’ पूरी तरह शरीर में तब्दील हो जाना – न, ‘बलात्कार’ की कानूनी परिभाषा के मुताबिक असहमति या वितृष्णा का एक भी बिंदु नहीं यहाँ। लेकिन रतिक्रिया के दौरान शरीर पर खेले जा रहे एक-एक दांव-पेंच से वाकिफ उनकी क्रमिक प्रतीक्षा में ‘एक लम्बी सीत्कार के साथ जड़’ हो जाने तक के यवनिका पात का दृश्य देह और मन के एकाग्र संगीत की उस अनिवार्य स्थिति का विलोम है जिसकी अनुपस्थिति में स्त्री के लिए पति ठीक उसी तर्क और अनुपात में बलात्कारी हो जाता है जिस तर्क और अनुपात में पुरुष के लिए अंधेरे की चादर में दुबकी हर बिल्ली काली और हर स्त्री काली बिल्ली।
विवाह संस्था के स्वरूप की गहरी पड़ताल करते हुए मृदुला गर्ग हिंसा के पाशविक प्रदर्शन से अछूती उस स्थिति में भी बलात्कार की क्रूरता को देख पाती हैं, जहाँ अतिरिक्त दुलार-पुचकार को हथियार बना पति अपनी पत्नी का मानसिक-भावनात्मक शोषण कर उसकी स्वतंत्रता और इयत्ता को चकनाचूर कर देता है। अंततः बलात्कार अति गूढ़ व्यंजना में स्त्री की पुष्ट अस्मिता को छिन्न-भिन्न करने का पौरुषयुक्त षड्यंत्र ही तो है। ”हम अपना बच्चा बनाएंगे, फ्लैश ऑव अवर फ्लैश” – मातृत्व पाने के लिए तड़पती मारियान को बहका-फुसला कर उसके मानस उपन्यास ‘वुमैन ऑव द अर्थ’ को हड़प कर अपने नाम से प्रकाशित करवा डालना एक ओर जेल्डा फिटजेराल्ड की त्रासदी का विस्तार है ै, तो दूसरी ओर वैवाहिक बलात्कार के इस शातिर-सूक्ष्म स्वरूप को चीन्हने की जरूरत का आह्नान भी। सवाल उठता है कि बलात्कार की परिभाषा और कोटि का निर्धारण पुराने वक्तों की (अधिकांश कानून मूलतः 1860 के हैं जिनमें समय-समय पर पैबंद लगाने और रफू-मुरम्मत करने के अंदाज में छोटे-मोटे संशोधन-परिवर्धन हुए है।) पुरुष दृष्टि से ही क्यों? घूंट-घूंट वेदना पीती स्त्री दृष्टि और न्याय से क्यों नहीं?